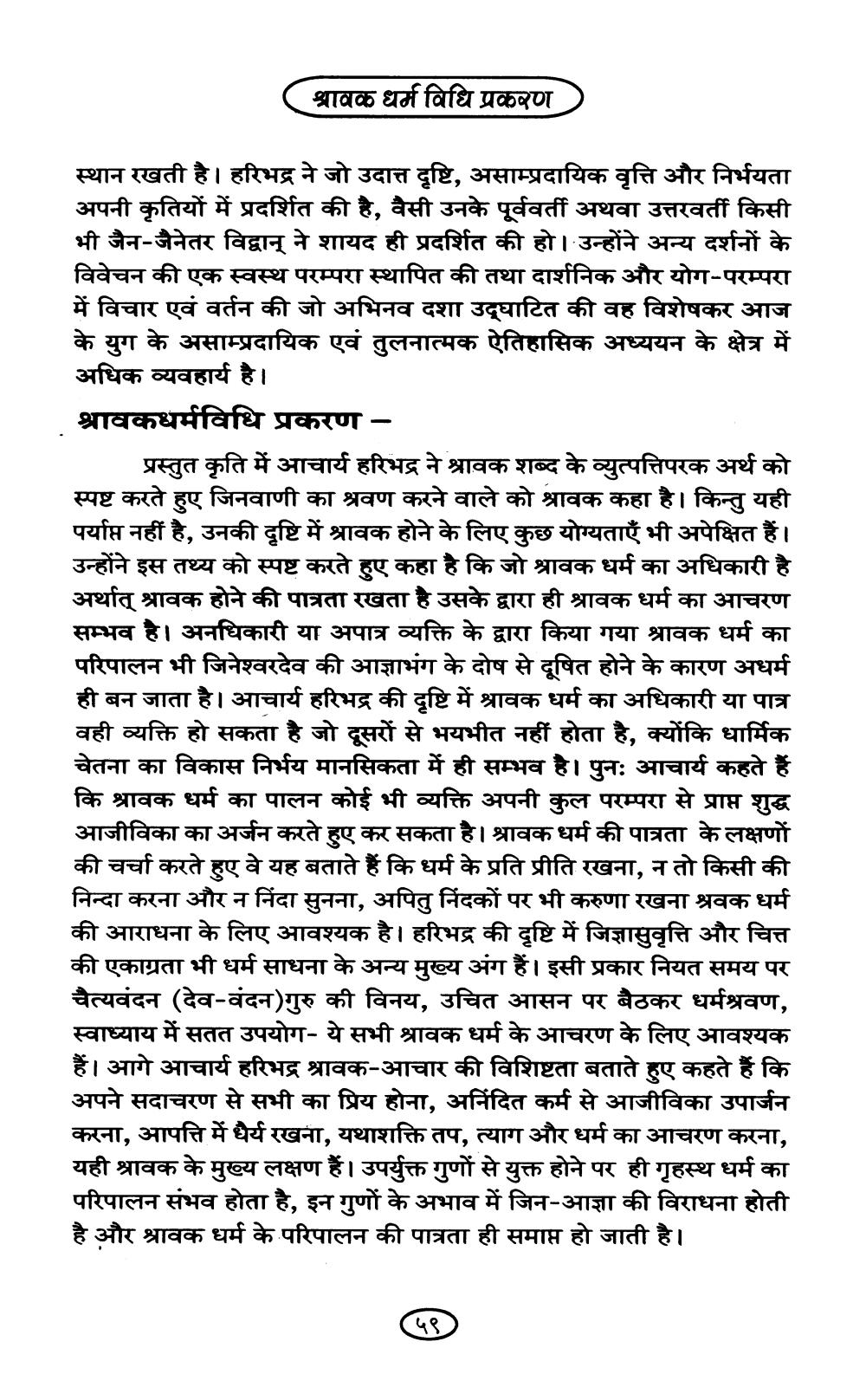________________
(श्रावक धर्म विधि प्रकरण )
स्थान रखती है। हरिभद्र ने जो उदात्त दृष्टि, असाम्प्रदायिक वृत्ति और निर्भयता अपनी कृतियों में प्रदर्शित की है, वैसी उनके पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती किसी भी जैन-जैनेतर विद्वान् ने शायद ही प्रदर्शित की हो। उन्होंने अन्य दर्शनों के विवेचन की एक स्वस्थ परम्परा स्थापित की तथा दार्शनिक और योग-परम्परा में विचार एवं वर्तन की जो अभिनव दशा उद्घाटित की वह विशेषकर आज के युग के असाम्प्रदायिक एवं तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में अधिक व्यवहार्य है। श्रावकधर्मविधि प्रकरण -
प्रस्तुत कृति में आचार्य हरिभद्र ने श्रावक शब्द के व्युत्पत्तिपरक अर्थ को स्पष्ट करते हुए जिनवाणी का श्रवण करने वाले को श्रावक कहा है। किन्तु यही पर्याप्त नहीं है, उनकी दृष्टि में श्रावक होने के लिए कुछ योग्यताएँ भी अपेक्षित हैं। उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो श्रावक धर्म का अधिकारी है अर्थात् श्रावक होने की पात्रता रखता है उसके द्वारा ही श्रावक धर्म का आचरण सम्भव है। अनधिकारी या अपात्र व्यक्ति के द्वारा किया गया श्रावक धर्म का परिपालन भी जिनेश्वरदेव की आज्ञाभंग के दोष से दूषित होने के कारण अधर्म ही बन जाता है। आचार्य हरिभद्र की दृष्टि में श्रावक धर्म का अधिकारी या पात्र वही व्यक्ति हो सकता है जो दूसरों से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक चेतना का विकास निर्भय मानसिकता में ही सम्भव है। पुन: आचार्य कहते हैं कि श्रावक धर्म का पालन कोई भी व्यक्ति अपनी कुल परम्परा से प्राप्त शुद्ध आजीविका का अर्जन करते हुए कर सकता है। श्रावक धर्म की पात्रता के लक्षणों की चर्चा करते हुए वे यह बताते हैं कि धर्म के प्रति प्रीति रखना, न तो किसी की निन्दा करना और न निंदा सुनना, अपितु निंदकों पर भी करुणा रखना श्रवक धर्म की आराधना के लिए आवश्यक है। हरिभद्र की दृष्टि में जिज्ञासुवृत्ति और चित्त की एकाग्रता भी धर्म साधना के अन्य मुख्य अंग हैं। इसी प्रकार नियत समय पर चैत्यवंदन (देव-वंदन)गुरु की विनय, उचित आसन पर बैठकर धर्मश्रवण, स्वाध्याय में सतत उपयोग- ये सभी श्रावक धर्म के आचरण के लिए आवश्यक हैं। आगे आचार्य हरिभद्र श्रावक-आचार की विशिष्टता बताते हुए कहते हैं कि अपने सदाचरण से सभी का प्रिय होना, अनिंदित कर्म से आजीविका उपार्जन करना, आपत्ति में धैर्य रखना, यथाशक्ति तप, त्याग और धर्म का आचरण करना, यही श्रावक के मुख्य लक्षण हैं। उपर्युक्त गुणों से युक्त होने पर ही गृहस्थ धर्म का परिपालन संभव होता है, इन गुणों के अभाव में जिन-आज्ञा की विराधना होती है और श्रावक धर्म के परिपालन की पात्रता ही समाप्त हो जाती है।
(५९