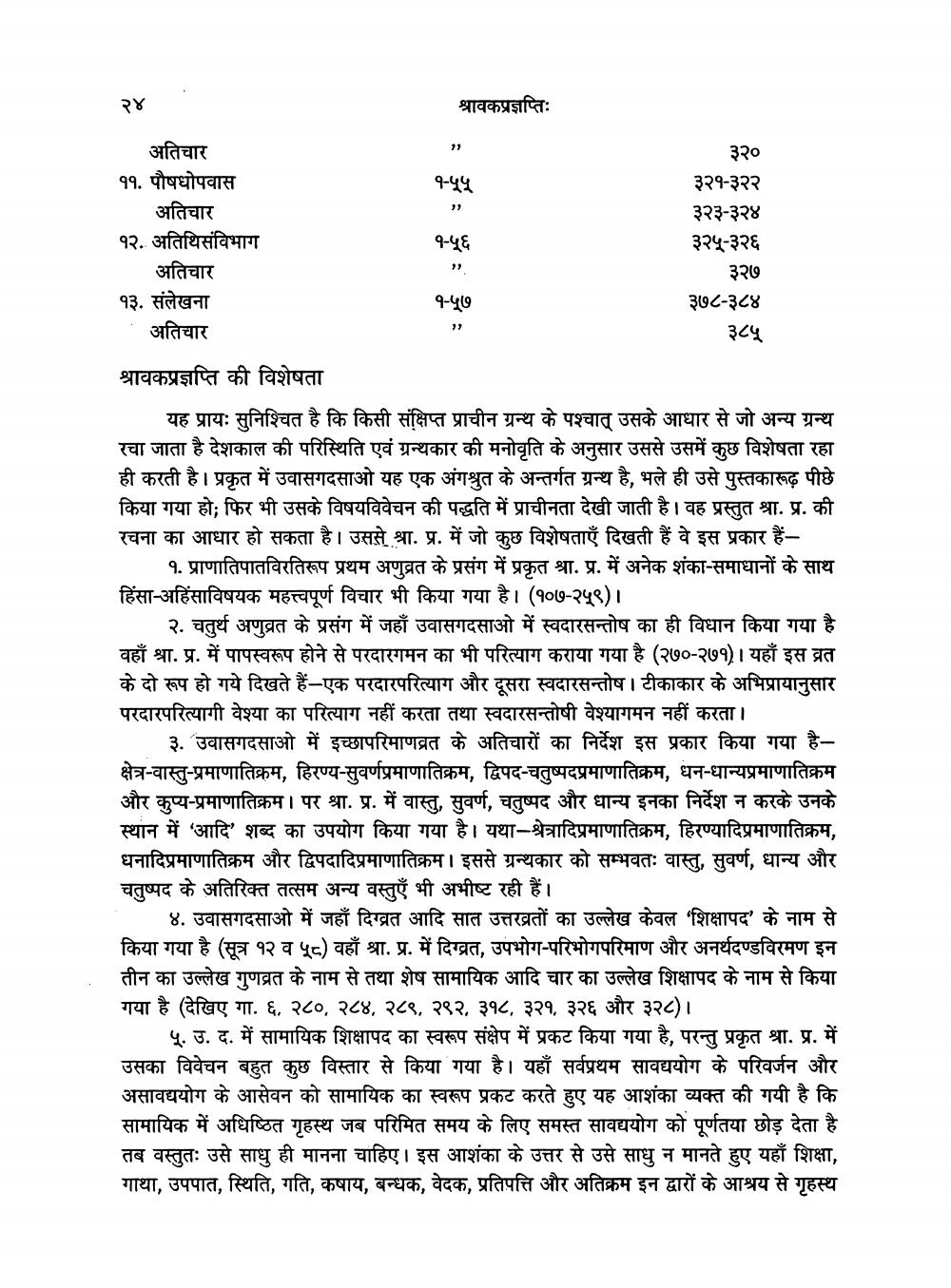________________
२४
श्रावकप्रज्ञप्तिः
१-५५
अतिचार ११. पौषधोपवास
अतिचार १२. अतिथिसंविभाग
अतिचार १३. संलेखना
अतिचार
१-५६
३२० ३२१-३२२ ३२३-३२४ ३२५-३२६
३२७ ३७८-३८४
३८५
श्रावकप्रज्ञप्ति की विशेषता
यह प्रायः सुनिश्चित है कि किसी संक्षिप्त प्राचीन ग्रन्थ के पश्चात् उसके आधार से जो अन्य ग्रन्थ रचा जाता है देशकाल की परिस्थिति एवं ग्रन्थकार की मनोवृति के अनुसार उससे उसमें कुछ विशेषता रहा ही करती है। प्रकृत में उवासगदसाओ यह एक अंगश्रुत के अन्तर्गत ग्रन्थ है, भले ही उसे पुस्तकारूढ़ पीछे किया गया हो; फिर भी उसके विषयविवेचन की पद्धति में प्राचीनता देखी जाती है। वह प्रस्तुत श्रा. प्र. की रचना का आधार हो सकता है। उससे श्रा. प्र. में जो कुछ विशेषताएँ दिखती हैं वे इस प्रकार हैं
१. प्राणातिपातविरतिरूप प्रथम अणुव्रत के प्रसंग में प्रकृत श्रा. प्र. में अनेक शंका-समाधानों के साथ हिंसा-अहिंसाविषयक महत्त्वपूर्ण विचार भी किया गया है। (१०७-२५९)।
२. चतुर्थ अणुव्रत के प्रसंग में जहाँ उवासगदसाओ में स्वदारसन्तोष का ही विधान किया गया है वहाँ श्रा. प्र. में पापस्वरूप होने से परदारगमन का भी परित्याग कराया गया है (२७०-२७१)। यहाँ इस व्रत के दो रूप हो गये दिखते हैं-एक परदारपरित्याग और दूसरा स्वदारसन्तोष। टीकाकार के अभिप्रायानुसार परदारपरित्यागी वेश्या का परित्याग नहीं करता तथा स्वदारसन्तोषी वेश्यागमन नहीं करता।
३. उवासगदसाओ में इच्छापरिमाणव्रत के अतिचारों का निर्देश इस प्रकार किया गया हैक्षेत्र-वास्तु-प्रमाणातिक्रम, हिरण्य-सुवर्णप्रमाणातिक्रम, द्विपद-चतुष्पदप्रमाणातिक्रम, धन-धान्यप्रमाणातिक्रम
और कुप्य-प्रमाणातिक्रम। पर श्रा. प्र. में वास्तु, सुवर्ण, चतुष्पद और धान्य इनका निर्देश न करके उनके स्थान में 'आदि' शब्द का उपयोग किया गया है। यथा-श्रेत्रादिप्रमाणातिक्रम, हिरण्यादिप्रमाणातिक्रम, धनादिप्रमाणातिक्रम और द्विपदादिप्रमाणातिक्रम। इससे ग्रन्थकार को सम्भवतः वास्तु, सुवर्ण, धान्य और चतुष्पद के अतिरिक्त तत्सम अन्य वस्तुएँ भी अभीष्ट रही हैं।
४. उवासगदसाओ में जहाँ दिग्वत आदि सात उत्तखतों का उल्लेख केवल 'शिक्षापद' के नाम से किया गया है (सूत्र १२ व ५८) वहाँ श्रा. प्र. में दिग्वत, उपभोग-परिभोगपरिमाण और अनर्थदण्डविरमण इन तीन का उल्लेख गुणव्रत के नाम से तथा शेष सामायिक आदि चार का उल्लेख शिक्षापद के नाम से किया गया है (देखिए गा. ६, २८०, २८४, २८९, २९२, ३१८, ३२१, ३२६ और ३२८)।
५. उ. द. में सामायिक शिक्षापद का स्वरूप संक्षेप में प्रकट किया गया है, परन्तु प्रकृत श्रा. प्र. में उसका विवेचन बहुत कुछ विस्तार से किया गया है। यहाँ सर्वप्रथम सावद्ययोग के परिवर्जन और असावद्ययोग के आसेवन को सामायिक का स्वरूप प्रकट करते हुए यह आशंका व्यक्त की गयी है कि सामायिक में अधिष्ठित गृहस्थ जब परिमित समय के लिए समस्त सावधयोग को पूर्णतया छोड़ देता है तब वस्तुतः उसे साधु ही मानना चाहिए। इस आशंका के उत्तर से उसे साधु न मानते हुए यहाँ शिक्षा, गाथा, उपपात, स्थिति, गति, कषाय, बन्धक, वेदक, प्रतिपत्ति और अतिक्रम इन द्वारों के आश्रय से गृहस्थ