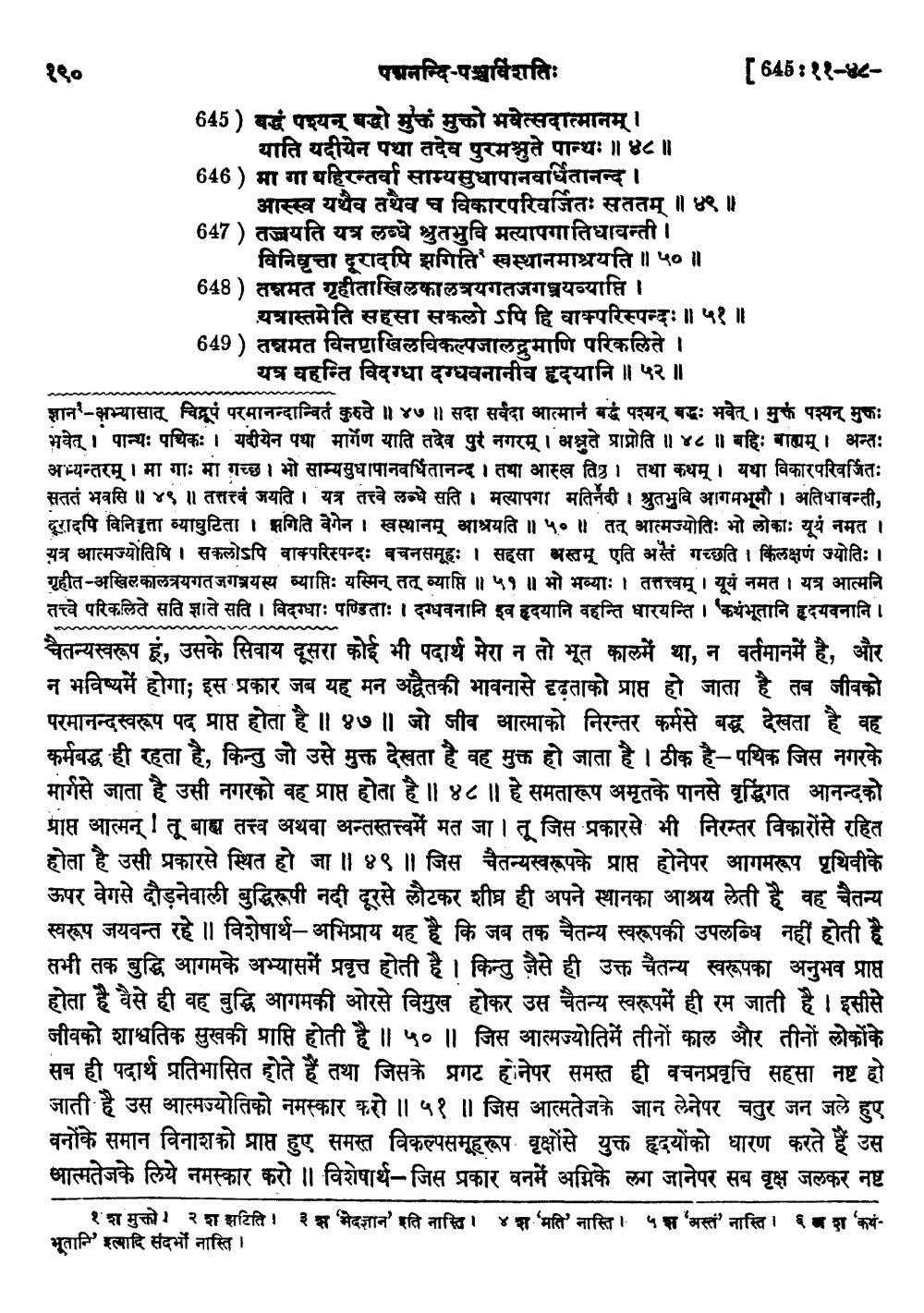________________
१९०
पचनन्दि-पश्चविंशतिः
[645:११-४८645 ) बद्धं पश्यन् बद्धो मुक्तं मुक्तो भवेत्सदात्मानम् ।
__ याति यदीयेन पथा तदेव पुरमश्नुते पान्थः ॥४८॥ 646) मा गा पहिरन्तर्वा साम्यसुधापानवर्धितानन्द ।
आस्स्व यथैव तथैव च विकारपरिवर्जितः सततम् ॥४९॥ 647 ) तज्जयति यत्र लब्धे श्रुतभुवि मत्यापगातिधावन्ती ।
विनिवृत्ता दूरादपि झगिति' स्वस्थानमाश्रयति ॥५०॥ 648 ) तन्नमत गृहीताखिलकालत्रयगतजगन्नयव्याप्ति ।
यत्रास्तमेति सहसा सकलो ऽपि हि वाक्परिस्पन्दः॥५१॥ 649 ) तन्नमत विनष्टाखिलविकल्पजालमाणि परिकलिते ।
यत्र वहन्ति विदग्धा दग्धवनानीव हृदयानि ॥ ५२ ॥ ज्ञान-अभ्यासात् चिद्रूपं परमानन्दान्वितं कुरुते ॥४७॥ सदा सर्वदा आत्मानं बद्ध पश्यन् बदः भवेत् । मुक्तं पश्यन् मुकः भवेत् । पान्यः पथिकः । यदीयेन पथा मार्गेण याति तदेव पुरै नगरम् । अश्नुते प्राप्नोति ॥४८॥ बहिः बाह्यम् । अन्तः अभ्यन्तरम् । मा गाः मा गच्छ । भो साम्यसुधापानवधितानन्द । तथा आस्व तिष्ठ। तथा कथम् । यथा विकारपरिवर्जितः सततं भवसि ॥ ४९ ॥ तत्तत्त्वं जयति । यत्र तत्त्वे लन्धे सति । मत्यापगा मति दी। श्रुतभुवि आगमभूमौ । अतिधावन्ती, दूरादपि विनिवृत्ता व्याधुटिता । गिति वेगेन । खस्थानम् आश्रयति ॥५०॥ तत् आत्मज्योतिः भो लोकाः यूयं नमत । यत्र आत्मज्योतिषि । सकलोऽपि वाक्परिस्पन्दः वचनसमूहः । सहसा अस्तम एति अस्तं गच्छति । किंलक्षणं ज्योतिः। गृहीत-अखिलकालत्रयगतजगत्रयस्य व्याप्तिः यस्मिन् तत् व्याप्ति ॥५१॥ भो भव्याः। तत्तत्त्वम् । यूयं नमत । यत्र आत्मनि तत्त्वे परिकलिते सति ज्ञाते सति । विदग्धाः पण्डिताः । दग्धवनानि इव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति । कथंभूतानि हृदयवनानि । चैतन्यस्वरूप हूं, उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा न तो भूत कालमें था, न वर्तमानमें है, और न भविष्यमें होगा। इस प्रकार जब यह मन अद्वैतकी भावनासे दृढ़ताको प्राप्त हो जाता है तब जीवको परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ जो जीव आत्माको निरन्तर कर्मसे बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है, किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है । ठीक है-पथिक जिस नगरके मार्गसे जाता है उसी नगरको वह प्राप्त होता है ॥ ४८॥ हे समतारूप अमृतके पानसे वृद्धिंगत आनन्दको प्राप्त आत्मन् ! तू बाह्य तत्त्व अथवा अन्तस्तत्त्वमें मत जा । तू जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोंसे रहित होता है उसी प्रकारसे स्थित हो जा ॥ ४९ ॥ जिस चैतन्यस्वरूपके प्राप्त होनेपर आगमरूप पृथिवीके ऊपर वेगसे दौड़नेवाली बुद्धिरूपी नदी दूरसे लौटकर शीघ्र ही अपने स्थानका आश्रय लेती है वह चैतन्य स्वरूप जयवन्त रहे ॥ विशेषार्थ- अभिप्राय यह है कि जब तक चैतन्य स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती है सभी तक बुद्धि आगमके अभ्यासमें प्रवृत्त होती है। किन्तु जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूपका अनुभव प्राप्त होता है वैसे ही वह बुद्धि आगमकी ओरसे विमुख होकर उस चैतन्य स्वरूपमें ही रम जाती है । इसीसे जीवको शाश्वतिक सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ जिस आत्मज्योतिमें तीनों काल और तीनों लोकोंके सब ही पदार्थ प्रतिभासित होते हैं तथा जिसके प्रगट होनेपर समस्त ही वचनप्रवृत्ति सहसा नष्ट हो जाती है उस आत्मज्योतिको नमस्कार करो ।। ५१ ॥ जिस आत्मतेजके जान लेनेपर चतुर जन जले हुए वनोंके समान विनाशको प्राप्त हुए समस्त विकल्पसमूहरूप वृक्षोंसे युक्त हृदयोंको धारण करते हैं उस आत्मतेजके लिये नमस्कार करो ॥ विशेषार्थ-जिस प्रकार वनमें अग्निके लग जानेपर सब वृक्ष जलकर नष्ट
१श मुक्तो। २ श झटिति । ३श 'मेदज्ञान' इति नास्ति। ४ शमति' नास्ति। ५ 'अस्तं' नास्ति । ६. श कथंभूतानि इत्यादि संदर्भो नास्ति ।