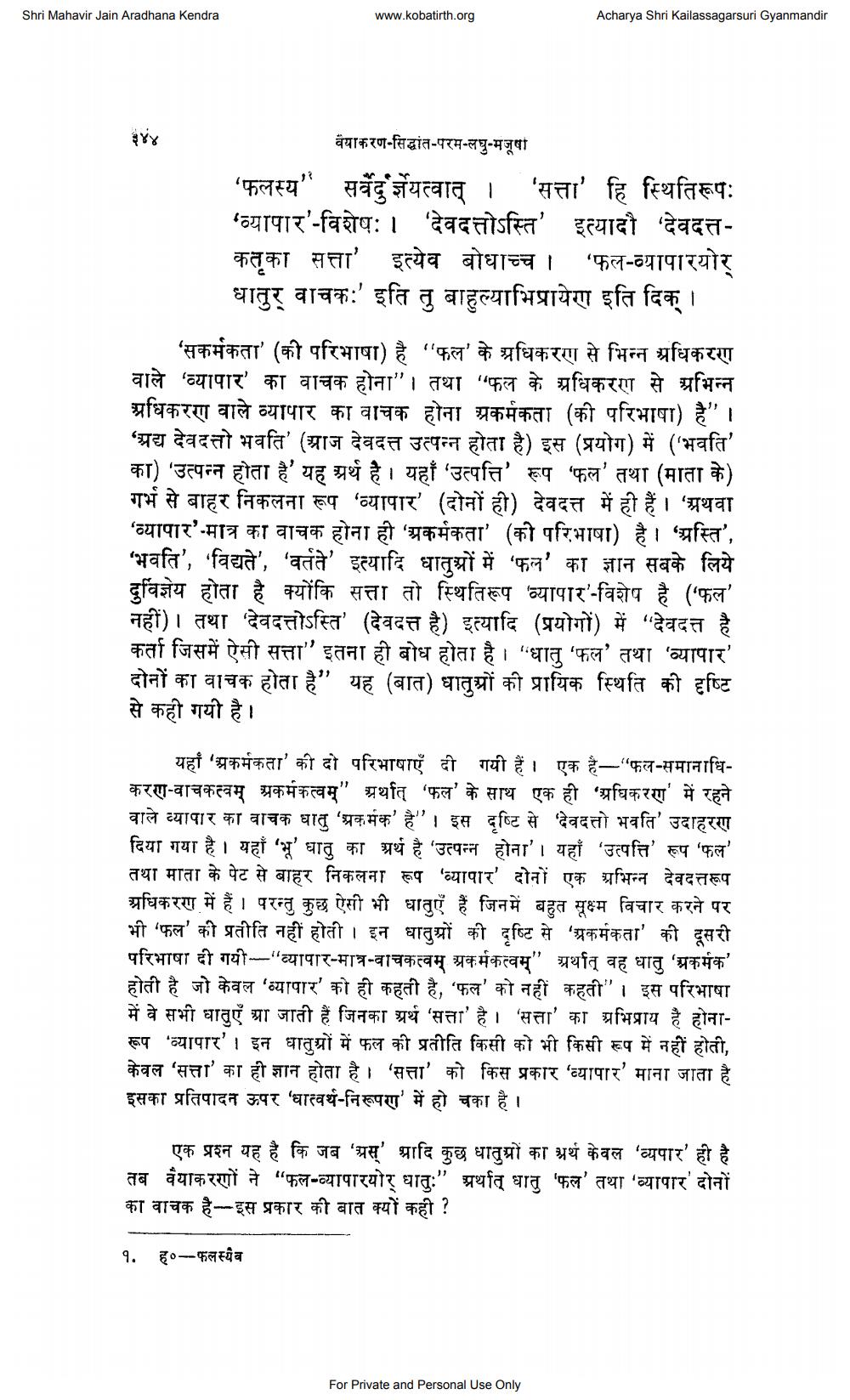________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
वैयाकरण-सिद्धांत-परम-लघु-मजूषा 'फलस्य" सर्वैर्दुज्ञेयत्वात् । 'सत्ता' हि स्थितिरूपः 'व्यापार'-विशेषः । 'देवदत्तोऽस्ति' इत्यादौ 'देवदत्तकतृका सत्ता' इत्येव बोधाच्च । 'फल-व्यापारयोर्
धातुर् वाचकः' इति तु बाहुल्याभिप्रायेण इति दिक् । 'सकर्मकता' (की परिभाषा) है “फल' के अधिकरण से भिन्न अधिकरण वाले 'व्यापार' का वाचक होना"। तथा “फल के अधिकरण से अभिन्न अधिकरण वाले व्यापार का वाचक होना अकर्मकता (की परिभाषा) है"। 'अद्य देवदत्तो भवति' (अाज देवदत्त उत्पन्न होता है) इस (प्रयोग) में ('भवति' का) 'उत्पन्न होता है' यह अर्थ है। यहाँ 'उत्पत्ति' रूप 'फल' तथा (माता के) गर्भ से बाहर निकलना रूप 'व्यापार' (दोनों ही) देवदत्त में ही हैं। 'अथवा 'व्यापार'-मात्र का वाचक होना ही 'अकर्मकता' (की परिभाषा) है। 'अस्ति', 'भवति', 'विद्यते', 'वर्तते' इत्यादि धातुओं में 'फल' का ज्ञान सबके लिये दुर्विज्ञेय होता है क्योंकि सत्ता तो स्थितिरूप 'व्यापार'-विशेष है ('फल' नहीं)। तथा 'देवदत्तोऽस्ति' (देवदत्त है) इत्यादि (प्रयोगों) में “देवदत्त है कर्ता जिसमें ऐसी सत्ता" इतना ही बोध होता है। “धातु 'फल' तथा 'व्यापार' दोनों का वाचक होता है" यह (बात) धातुओं की प्रायिक स्थिति की दृष्टि से कही गयी है।
यहाँ 'अकर्मकता' की दो परिभाषाएँ दी गयी हैं। एक है-“फल-समानाधिकरण-वाचकत्वम् अकर्मकत्वम्" अर्थात् 'फल' के साथ एक ही 'अधिकरण' में रहने वाले व्यापार का वाचक धातु 'अकर्मक' है। इस दृष्टि से 'देवदत्तो भवति' उदाहरण दिया गया है। यहाँ 'भू' धातु का अर्थ है 'उत्पन्न होना'। यहाँ 'उत्पत्ति' रूप 'फल' तथा माता के पेट से बाहर निकलना रूप 'व्यापार' दोनों एक अभिन्न देवदत्तरूप अधिकरण में हैं । परन्तु कुछ ऐसी भी धातुएँ हैं जिनमें बहुत सूक्ष्म विचार करने पर भी 'फल' की प्रतीति नहीं होती। इन धातुओं की दृष्टि से 'अकर्मकता' की दूसरी परिभाषा दी गयी-"व्यापार-मात्र-वाचकत्वम् अकर्मकत्वम्' अर्थात् वह धातु 'अकर्मक' होती है जो केवल 'व्यापार' को ही कहती है, 'फल' को नहीं कहती'। इस परिभाषा में वे सभी धातुएँ आ जाती हैं जिनका अर्थ 'सत्ता' है। 'सत्ता' का अभिप्राय है होनारूप 'व्यापार'। इन धातुओं में फल की प्रतीति किसी को भी किसी रूप में नहीं होती, केवल 'सत्ता' का ही ज्ञान होता है। 'सत्ता' को किस प्रकार 'व्यापार' माना जाता है इसका प्रतिपादन ऊपर 'धात्वर्थ-निरूपण' में हो चका है।
एक प्रश्न यह है कि जब 'अस्' प्रादि कुछ धातुओं का अर्थ केवल 'व्यपार' ही है तब वैयाकरणों ने “फल-व्यापारयोर् धातुः" अर्थात् धातु 'फल' तथा 'व्यापार' दोनों का वाचक है-इस प्रकार की बात क्यों कही?
१. ह०-फलस्यैव
For Private and Personal Use Only