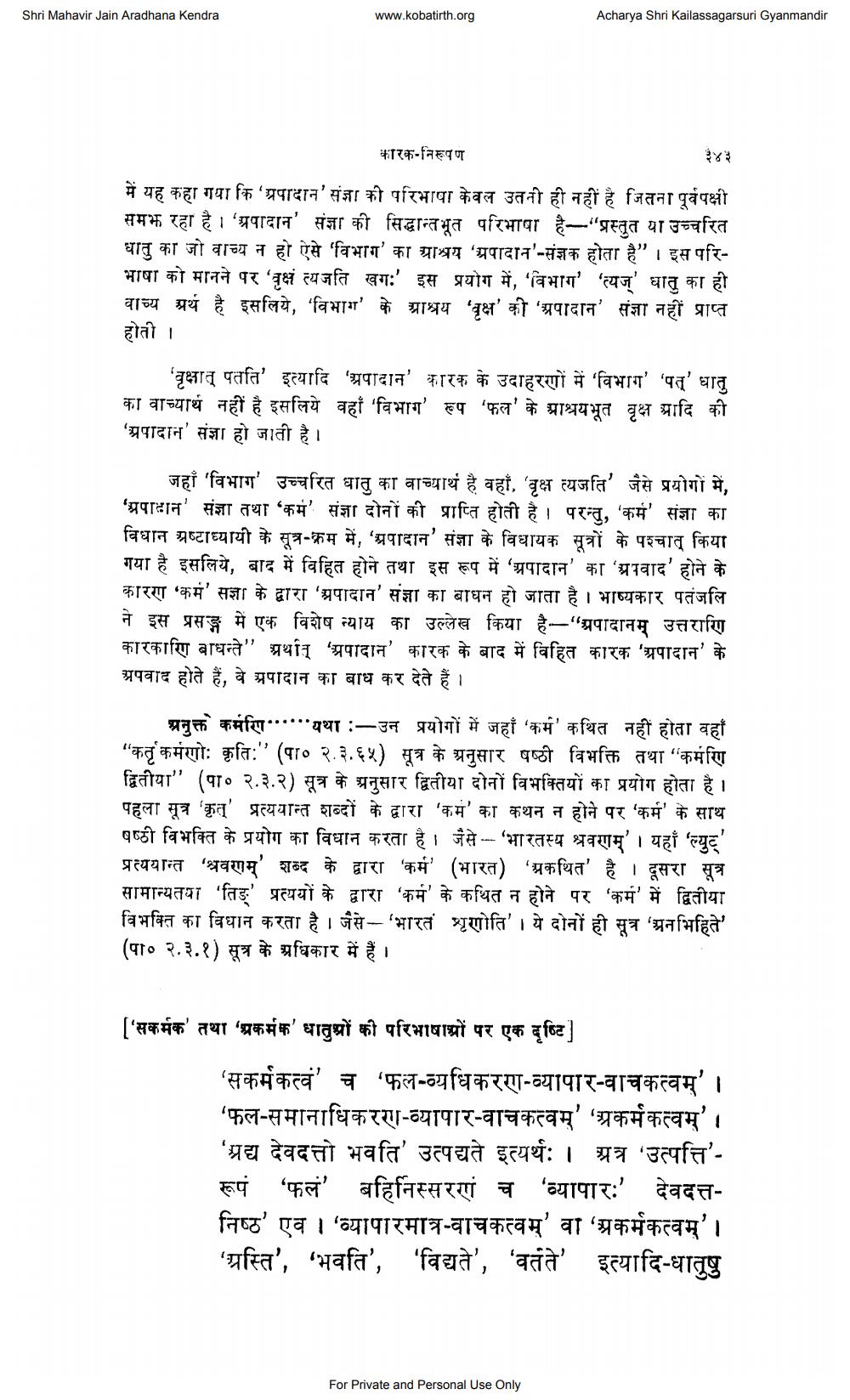________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
३४३
कारक - निरूपण
1
में यह कहा गया कि 'पादान' संज्ञा की परिभाषा केवल उतनी ही नहीं है जितना पूर्वपक्षी समझ रहा है । 'अपादान' संज्ञा की सिद्धान्तभूत परिभाषा है - "प्रस्तुत या उच्चरित धातु का जो वाच्य न हो ऐसे 'विभाग' का ग्राश्रय 'अपादान' - संज्ञक होता है"। इस परिभाषा को मानने पर 'वृक्षं त्यजति खगः ' इस प्रयोग में, 'विभाग' 'त्यज्' धातु का ही वाच्य अर्थ है इसलिये, 'विभाग' के श्राश्रय 'वृक्ष' की 'अपादान' संज्ञा नहीं प्राप्त होती ।
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
'वृक्षात् पतति' इत्यादि 'अपादान' कारक के उदाहरणों 'विभाग' 'पत्' धातु का वाच्यार्थ नहीं है इसलिये वहाँ 'विभाग' रूप 'फल' के प्राश्रयभूत वृक्ष प्रादि की 'अपादान' संज्ञा हो जाती है ।
जहाँ 'विभाग' उच्चरित धातु का वाच्यार्थ है वहाँ 'वृक्ष त्यजति' जैसे प्रयोगों में, 'अपादान' संज्ञा तथा 'कर्म' संज्ञा दोनों की प्राप्ति होती है । परन्तु, 'कर्म' संज्ञा का विधान अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम में, 'अपादान' संज्ञा के विधायक सूत्रों के पश्चात् किया गया है इसलिये, बाद में विहित होने तथा इस रूप में 'अपादान' का 'अपवाद' होने के कारण 'कर्म' सज्ञा के द्वारा 'अपादान' संज्ञा का बाधन हो जाता है । भाष्यकार पतंजलि ने इस प्रसङ्ग में एक विशेष न्याय का उल्लेख किया है - " अपादानम् उत्तराणि कारकारिण बाधन्ते " अर्थात् 'अपादान' कारक के बाद में विहित कारक 'अपादान' के अपवाद होते हैं, वे अपादान का बाध कर देते हैं ।
मुक्त कर्मणि यथा :- उन प्रयोगों में जहाँ 'कर्म' कथित नहीं होता वहाँ "कर्तृकर्मणोः कृति:" ( पा० २.३.६५ ) सूत्र के अनुसार षष्ठी विभक्ति तथा "कर्मणि द्वितीया" ( पा० २.३.२ ) सूत्र के अनुसार द्वितीया दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है । पहला सूत्र 'कृत्' प्रत्ययान्त शब्दों के द्वारा 'कर्म' का कथन न होने पर 'कर्म' के साथ षष्ठी विभक्ति के प्रयोग का विधान करता है। जैसे- 'भारतस्य श्रवणम्' । यहाँ 'ल्युट् ' प्रत्ययान्त 'श्रवणम्' शब्द के द्वारा 'कर्म' (भारत) 'प्रकथित' है । दूसरा सूत्र सामान्यतया 'तिङ्' प्रत्ययों के द्वारा 'कर्म' के कथित न होने पर 'कर्म' में द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। जैसे- 'भारतं शृणोति' । ये दोनों ही सूत्र 'अनभिहिते ' ( पा० २.३.१ ) सूत्र के अधिकार में हैं ।
[' सकर्मक' तथा 'कर्मक' धातुओंों की परिभाषाओं पर एक दृष्टि ]
' सकर्मकत्वं' च 'फल- व्यधिकरण - व्यापार-वाचकत्वम्' । 'फल-समानाधिकरण - व्यापार - वाचकत्वम्' 'कर्मकत्वम्' । 'प्रद्य देवदत्तो भवति' उत्पद्यते इत्यर्थः । अत्र 'उत्पत्ति'रूपं 'फलं' बहिनिस्सरणं च 'व्यापारः' देवदत्तनिष्ठ' एव । 'व्यापारमात्र वाचकत्वम्' वा 'अकर्मकत्वम्' । 'ग्रस्ति', 'भवति', 'विद्यते', 'वर्तते' इत्यादि धातुषु
For Private and Personal Use Only
-