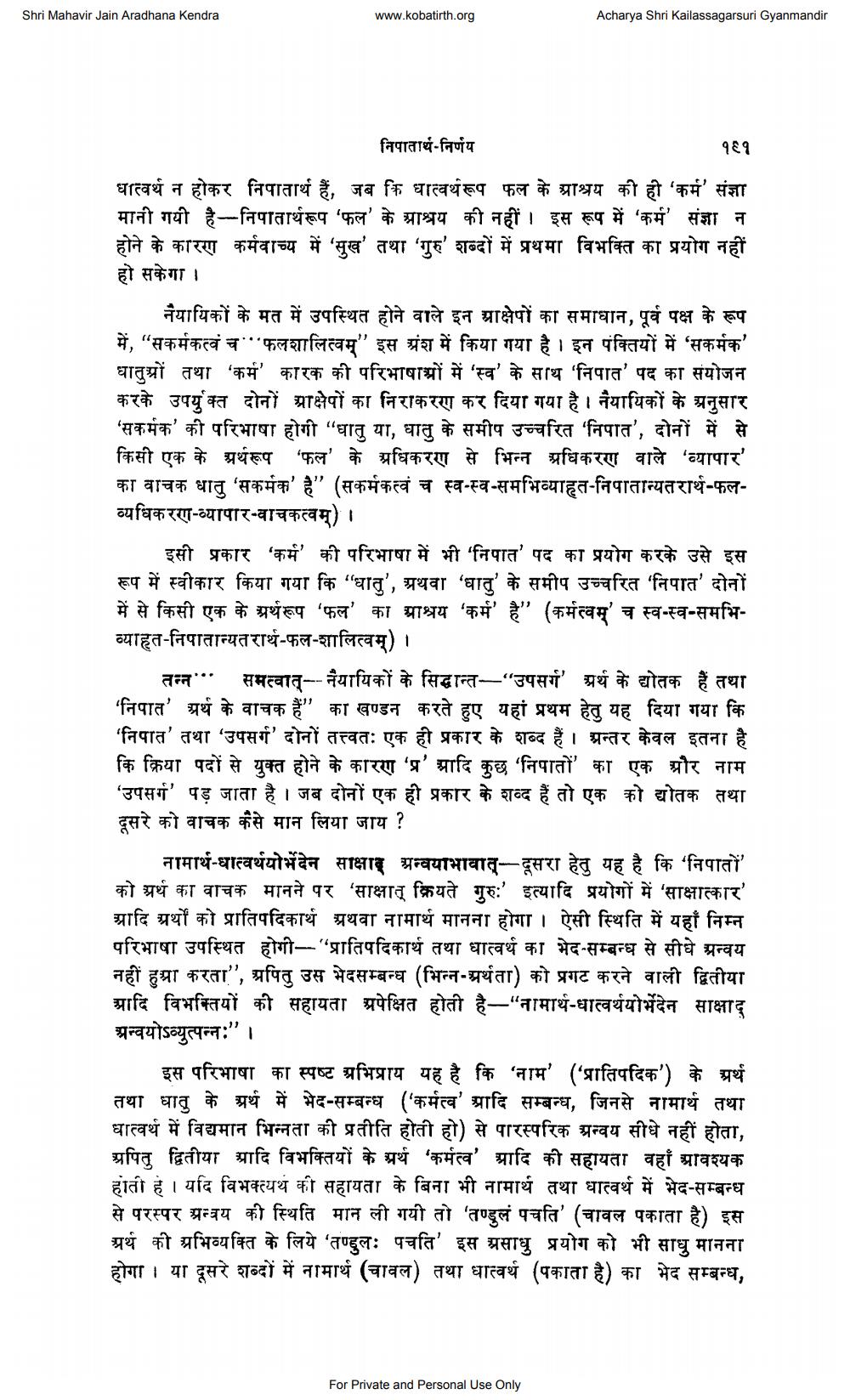________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
निपातार्थ-निर्णय
१९१
धात्वर्थ न होकर निपातार्थ हैं, जब कि धात्वर्थरूप फल के आश्रय की ही 'कर्म' संज्ञा मानी गयी है-निपातार्थरूप 'फल' के आश्रय की नहीं। इस रूप में 'कर्म' संज्ञा न होने के कारण कर्मवाच्य में 'सुख' तथा 'गुरु' शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकेगा।
नैयायिकों के मत में उपस्थित होने वाले इन आक्षेपों का समाधान, पूर्व पक्ष के रूप में, “सकर्मकत्वं च फलशालित्वम्" इस अंश में किया गया है। इन पंक्तियों में 'सकर्मक' धातुओं तथा 'कर्म' कारक की परिभाषाओं में 'स्व' के साथ निपात' पद का संयोजन करके उपर्युक्त दोनों प्राक्षेपों का निराकरण कर दिया गया है। नैयायिकों के अनुसार 'सकर्मक' की परिभाषा होगी "धातु या, धातु के समीप उच्चरित 'निपात', दोनों में से किसी एक के अर्थरूप 'फल' के अधिकरण से भिन्न अधिकरण वाले 'व्यापार' का वाचक धातु 'सकर्मक' है" (सकर्मकत्वं च स्व-स्व-समभिव्याहृत-निपातान्यतरार्थ-फलव्यधिकरण-व्यापार-वाचकत्वम्) ।
इसी प्रकार 'कर्म' की परिभाषा में भी 'निपात' पद का प्रयोग करके उसे इस रूप में स्वीकार किया गया कि "धातु', अथवा 'धातु' के समीप उच्चरित 'निपात' दोनों में से किसी एक के अर्थरूप 'फल' का प्राश्रय 'कर्म' है" (कर्मत्वम्' च स्व-स्व-समभिव्याहृत-निपातान्यतरार्थ-फल-शालित्वम्)।
तन्न... समत्वात्-- नैयायिकों के सिद्धान्त-“उपसर्ग' अर्थ के द्योतक हैं तथा 'निपात' अर्थ के वाचक हैं' का खण्डन करते हुए यहां प्रथम हेतु यह दिया गया कि 'निपात' तथा 'उपसर्ग' दोनों तत्त्वतः एक ही प्रकार के शब्द हैं । अन्तर केवल इतना है कि क्रिया पदों से युक्त होने के कारण 'प्र' आदि कुछ 'निपातों' का एक और नाम 'उपसर्ग' पड़ जाता है । जब दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं तो एक को द्योतक तथा दूसरे को वाचक कैसे मान लिया जाय ?
नामार्थ-धात्वर्थयो)देन साक्षात् अन्वयाभावात्-दूसरा हेतु यह है कि 'निपातों' को अर्थ का वाचक मानने पर 'साक्षात् क्रियते गुरुः' इत्यादि प्रयोगों में 'साक्षात्कार' आदि अर्थों को प्रातिपदिकार्थ अथवा नामार्थ मानना होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ निम्न परिभाषा उपस्थित होगी- "प्रातिपदिकार्थ तथा धात्वर्थ का भेद-सम्बन्ध से सीधे अन्वय नहीं हुआ करता", अपितु उस भेदसम्बन्ध (भिन्न-अर्थता) को प्रगट करने वाली द्वितीया आदि विभक्तियों की सहायता अपेक्षित होती है-"नामार्थ-धात्वर्थयोर्भेदेन साक्षाद् अन्वयोऽव्युत्पन्नः"।
इस परिभाषा का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि 'नाम' ('प्रातिपदिक') के अर्थ तथा धातु के अर्थ में भेद-सम्बन्ध ('कर्मत्व' आदि सम्बन्ध, जिनसे नामार्थ तथा धात्वर्थ में विद्यमान भिन्नता की प्रतीति होती हो) से पारस्परिक अन्वय सीधे नहीं होता, अपितु द्वितीया आदि विभक्तियों के अर्थ 'कर्मत्व' आदि की सहायता वहाँ आवश्यक होती है । यदि विभक्त्यथ की सहायता के बिना भी नामार्थ तथा धात्वर्थ में भेद-सम्बन्ध से परस्पर अन्वय की स्थिति मान ली गयी तो 'तण्डुलं पचति' (चावल पकाता है) इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये 'तण्डुलः पचति' इस असाधु प्रयोग को भी साधु मानना होगा। या दूसरे शब्दों में नामार्थ (चावल) तथा धात्वर्थ (पकाता है) का भेद सम्बन्ध,
For Private and Personal Use Only