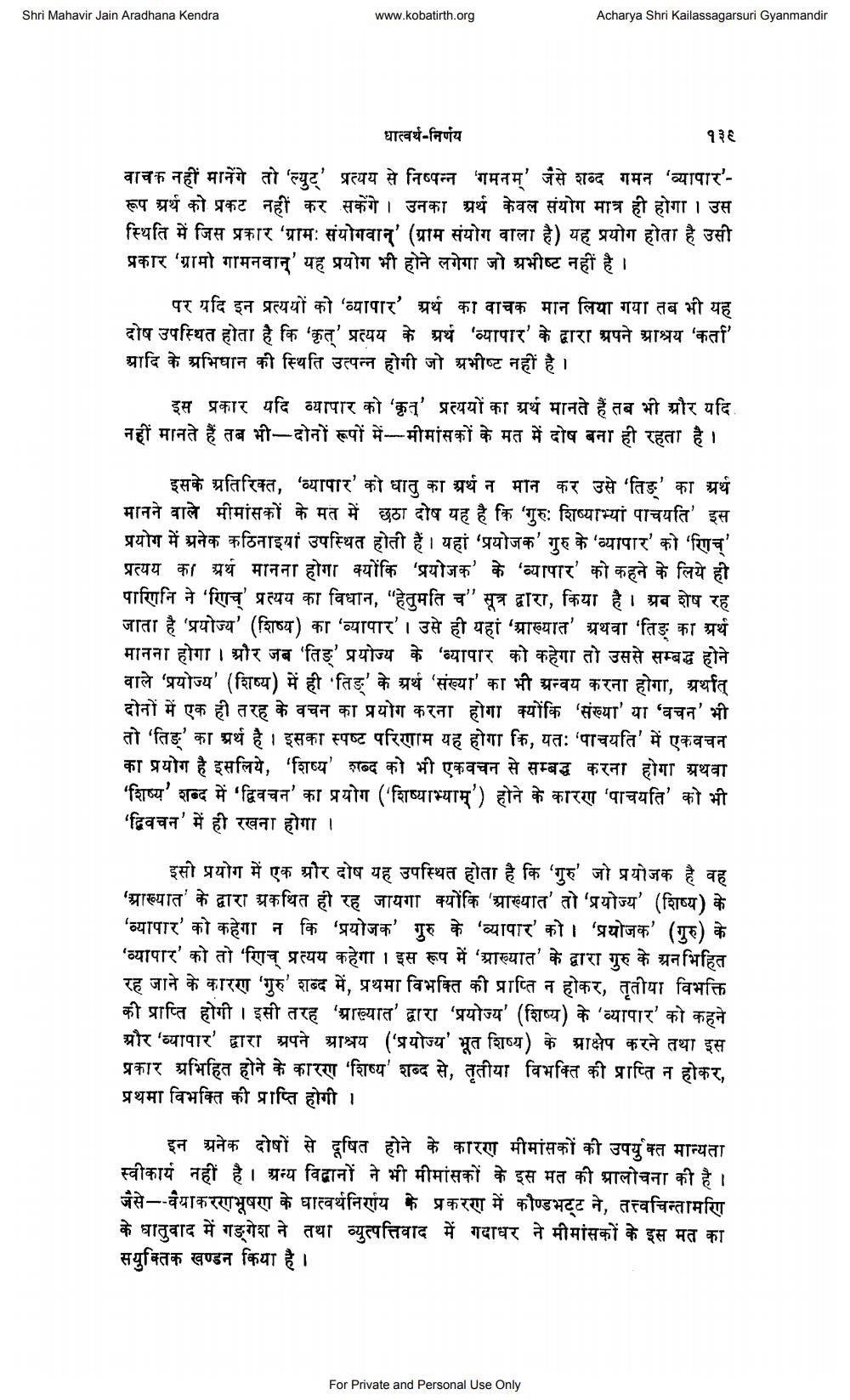________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
धात्वर्थ-निर्णय
१३६
वाचक नहीं मानेंगे तो 'ल्युट' प्रत्यय से निष्पन्न गमनम्' जैसे शब्द गमन 'व्यापार'रूप अर्थ को प्रकट नहीं कर सकेंगे। उनका अर्थ केवल संयोग मात्र ही होगा । उस स्थिति में जिस प्रकार 'ग्रामः संयोगवान्' (ग्राम संयोग वाला है) यह प्रयोग होता है उसी प्रकार 'ग्रामो गामनवान्' यह प्रयोग भी होने लगेगा जो अभीष्ट नहीं है ।
पर यदि इन प्रत्ययों को 'व्यापार' अर्थ का वाचक मान लिया गया तब भी यह दोष उपस्थित होता है कि 'कृत्' प्रत्यय के अर्थ 'व्यापार' के द्वारा अपने आश्रय 'कर्ता' आदि के अभिधान की स्थिति उत्पन्न होगी जो अभीष्ट नहीं है।
इस प्रकार यदि व्यापार को 'कृत' प्रत्ययों का अर्थ मानते हैं तब भी और यदि नहीं मानते हैं तब भी दोनों रूपों में-मीमांसकों के मत में दोष बना ही रहता है।
___ इसके अतिरिक्त, 'व्यापार' को धातु का अर्थ न मान कर उसे 'तिङ' का अर्थ मानने वाले मीमांसकों के मत में छठा दोष यह है कि 'गुरुः शिष्याभ्यां पाचयति' इस प्रयोग में अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। यहां 'प्रयोजक' गुरु के 'व्यापार' को 'णिच्' प्रत्यय का अर्थ मानना होगा क्योंकि 'प्रयोजक' के 'व्यापार' को कहने के लिये ही पाणिनि ने 'रिणच्' प्रत्यय का विधान, "हेतुमति च" सूत्र द्वारा, किया है। अब शेष रह जाता है 'प्रयोज्य' (शिष्य) का 'व्यापार'। उसे ही यहां 'पाख्यात' अथवा 'तिङ् का अर्थ मानना होगा। और जब 'तिङ्' प्रयोज्य के 'व्यापार को कहेगा तो उससे सम्बद्ध होने वाले 'प्रयोज्य' (शिष्य) में ही 'तिङ्' के अर्थ 'संख्या' का भी अन्वय करना होगा, अर्थात् दोनों में एक ही तरह के वचन का प्रयोग करना होगा क्योंकि 'संख्या' या 'वचन' भी तो 'तिङ् का अर्थ है। इसका स्पष्ट परिणाम यह होगा कि, यतः 'पाचयति' में एकवचन का प्रयोग है इसलिये, 'शिष्य' काब्द को भी एकवचन से सम्बद्ध करना होगा अथवा 'शिष्य' शब्द में "द्विवचन' का प्रयोग ('शिष्याभ्याम्') होने के कारण 'पाचयति' को भी 'द्विवचन' में ही रखना होगा ।
इसी प्रयोग में एक और दोष यह उपस्थित होता है कि 'गुरु' जो प्रयोजक है वह 'पाख्यात' के द्वारा अकथित ही रह जायगा क्योंकि 'पाख्यात' तो 'प्रयोज्य' (शिष्य) के 'व्यापार' को कहेगा न कि 'प्रयोजक' गुरु के 'व्यापार' को। 'प्रयोजक' (गुरु) के 'व्यापार' को तो 'णिच् प्रत्यय कहेगा । इस रूप में 'पाख्यात' के द्वारा गुरु के अनभिहित रह जाने के कारण 'गुरु' शब्द में, प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति न होकर, तृतीया विभक्ति की प्राप्ति होगी। इसी तरह 'पाख्यात' द्वारा 'प्रयोज्य' (शिष्य) के 'व्यापार' को कहने और 'व्यापार' द्वारा अपने आश्रय ('प्रयोज्य' भूत शिष्य) के आक्षेप करने तथा इस प्रकार अभिहित होने के कारण 'शिष्य' शब्द से, तृतीया विभक्ति की प्राप्ति न होकर, प्रथमा विभक्ति की प्राप्ति होगी।
इन अनेक दोषों से दूषित होने के कारण मीमांसकों की उपर्युक्त मान्यता स्वीकार्य नहीं है। अन्य विद्वानों ने भी मीमांसकों के इस मत की आलोचना की है। जैसे-वैयाकरणभूषण के धात्वर्थनिर्णय के प्रकरण में कौण्डभट्ट ने, तत्त्वचिन्तामणि के धातुवाद में गङ्गेश ने तथा व्युत्पत्तिवाद में गदाधर ने मीमांसकों के इस मत का सयुक्तिक खण्डन किया है।
For Private and Personal Use Only