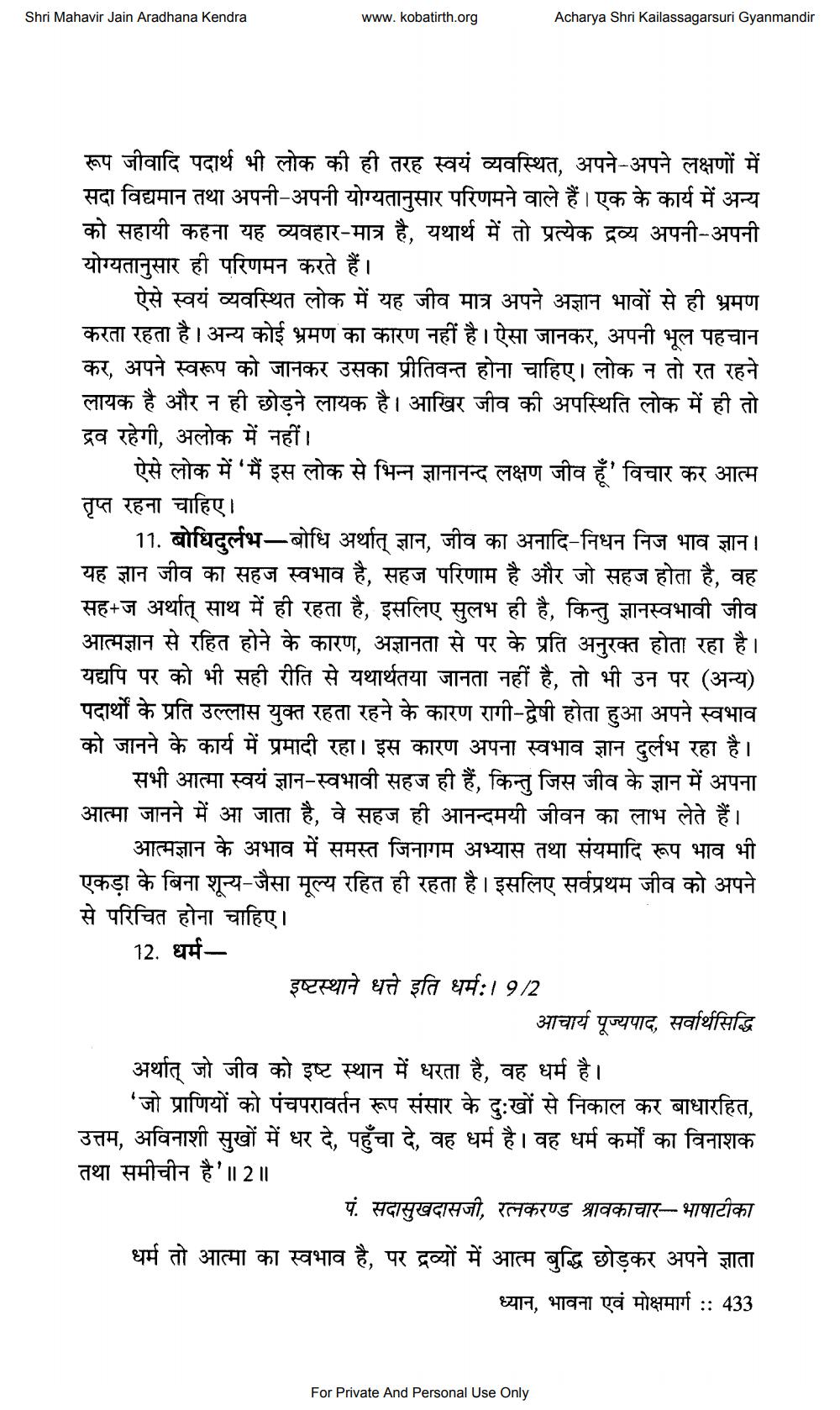________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www. kobatirth.org
रूप जीवादि पदार्थ भी लोक की ही तरह स्वयं व्यवस्थित, अपने-अपने लक्षणों में सदा विद्यमान तथा अपनी-अपनी योग्यतानुसार परिणमने वाले हैं। एक के कार्य में अन्य को सहाय कहना यह व्यवहार - मात्र है, यथार्थ में तो प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी योग्यतानुसार ही परिणमन करते हैं।
ऐसे स्वयं व्यवस्थित लोक में यह जीव मात्र अपने अज्ञान भावों से ही भ्रमण करता रहता है । अन्य कोई भ्रमण का कारण नहीं है। ऐसा जानकर, अपनी भूल पहचान कर, अपने स्वरूप को जानकर उसका प्रीतिवन्त होना चाहिए। लोक न तो रत रहने लायक है और न ही छोड़ने लायक है। आखिर जीव की अपस्थिति लोक में ही तो द्रव रहेगी, अलोक में नहीं ।
ऐसे लोक में 'मैं इस लोक से भिन्न ज्ञानानन्द लक्षण जीव हूँ' विचार कर आत्म तृप्त रहना चाहिए।
11. बोधिदुर्लभ—बोधि अर्थात् ज्ञान, जीव का अनादि-निधन निज भाव ज्ञान। यह ज्ञान जीव का सहज स्वभाव है, सहज परिणाम है और जो सहज होता है, वह सह+ज अर्थात् साथ में ही रहता है, इसलिए सुलभ ही है, किन्तु ज्ञानस्वभावी जीव आत्मज्ञान से रहित होने के कारण, अज्ञानता से पर के प्रति अनुरक्त होता रहा है । यद्यपि पर को भी सही रीति से यथार्थतया जानता नहीं है, तो भी उन पर (अन्य) पदार्थों के प्रति उल्लास युक्त रहता रहने के कारण रागी -द्वेषी होता हुआ अपने स्वभाव को जानने के कार्य में प्रमादी रहा। इस कारण अपना स्वभाव ज्ञान दुर्लभ रहा है ।
सभी आत्मा स्वयं ज्ञान - स्वभावी सहज ही हैं, किन्तु जिस जीव के ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आ जाता है, वे सहज ही आनन्दमयी जीवन का लाभ लेते हैं । आत्मज्ञान के अभाव में समस्त जिनागम अभ्यास तथा संयमादि रूप भाव भी एकड़ा के बिना शून्य-जैसा मूल्य रहित ही रहता है। इसलिए सर्वप्रथम जीव को अपने से परिचित होना चाहिए । 12. धर्म
इष्टस्थाने धत्ते इति धर्मः। 9/2
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि
अर्थात् जो जीव को इष्ट स्थान में धरता है, वह धर्म है।
'जो प्राणियों को पंचपरावर्तन रूप संसार के दुःखों से निकाल कर बाधारहित, उत्तम, अविनाशी सुखों में धर दे, पहुँचा दे, वह धर्म है । वह धर्म कर्मों का विनाशक तथा समीचीन है ' ॥ 2 ॥
For Private And Personal Use Only
पं. सदासुखदासजी, रत्नकरण्ड श्रावकाचार - भाषाटीका
धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता
ध्यान, भावना एवं मोक्षमार्ग :: 433