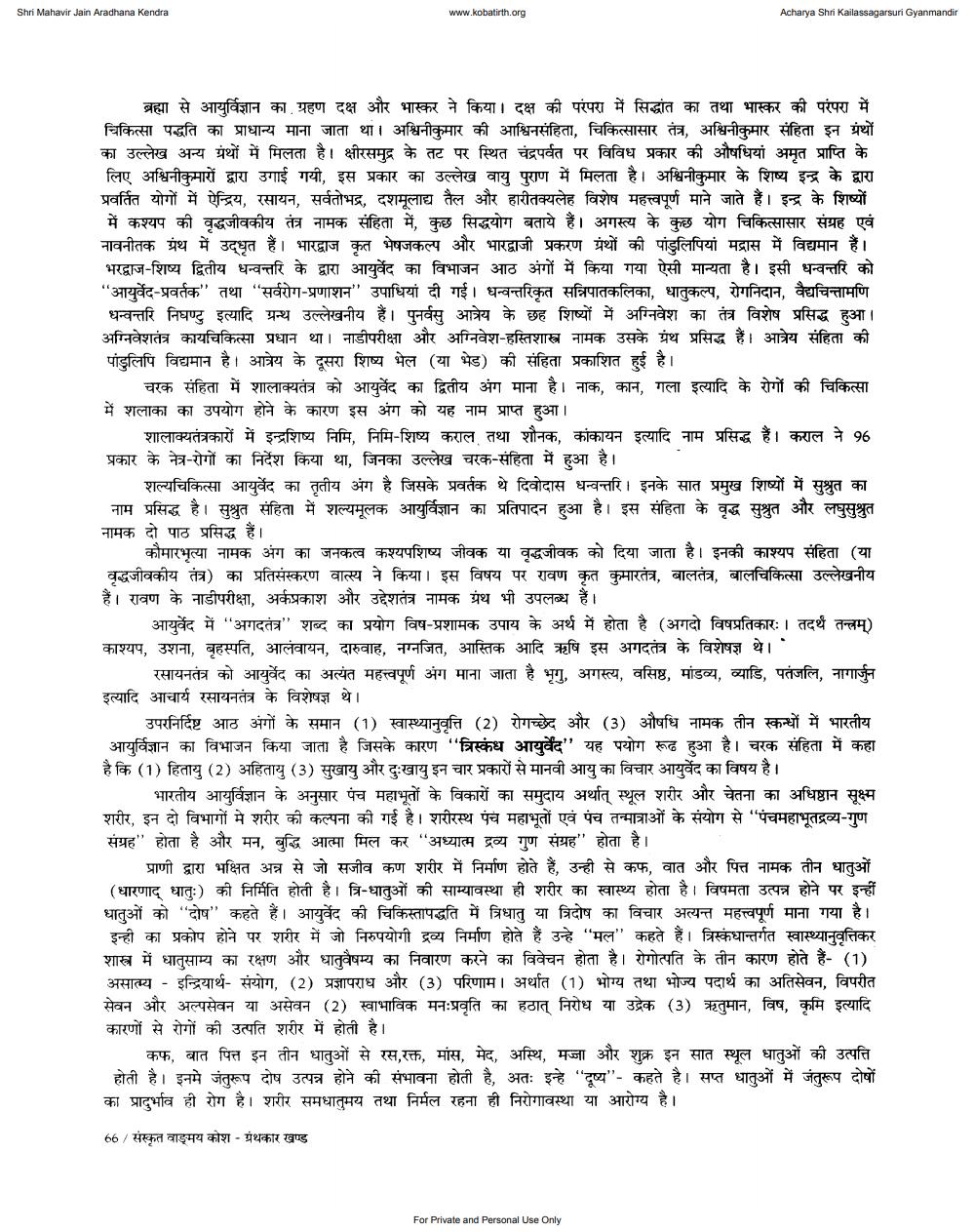________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
ब्रह्मा से आयुर्विज्ञान का ग्रहण दक्ष और भास्कर ने किया। दक्ष की परंपरा में सिद्धांत का तथा भास्कर की परंपरा में चिकित्सा पद्धति का प्राधान्य माना जाता था। अश्विनीकुमार की आश्विनसंहिता, चिकित्सासार तंत्र, अश्विनीकुमार संहिता इन ग्रंथों का उल्लेख अन्य ग्रंथों में मिलता है। क्षीरसमुद्र के तट पर स्थित चंद्रपर्वत पर विविध प्रकार की औषधियां अमृत प्राप्ति के लिए अश्विनीकुमारों द्वारा उगाई गयी, इस प्रकार का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। अश्विनीकुमार के शिष्य इन्द्र के द्वारा प्रवर्तित योगों में ऐन्द्रिय, रसायन, सर्वतोभद्र, दशमूलाद्य तैल और हारीतक्यलेह विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्द्र के शिष्यों में कश्यप की वृद्धजीवकीय तंत्र नामक संहिता में, कुछ सिद्धयोग बताये हैं। अगस्त्य के कुछ योग चिकित्सासार संग्रह एवं नावनीतक ग्रंथ में उद्धृत हैं। भारद्वाज कृत भेषजकल्प और भारद्वाजी प्रकरण ग्रंथों की पांडुलिपियां मद्रास में विद्यमान हैं। भरद्वाज-शिष्य द्वितीय धन्वन्तरि के द्वारा आयुर्वेद का विभाजन आठ अंगों में किया गया ऐसी मान्यता है। इसी धन्वन्तरि को "आयर्वेद-प्रवर्तक" तथा "सर्वरोग-प्रणाशन" उपाधियां दी गई। धन्वन्तरिकृत सन्निपातकलिका, धातुकल्प, रोगनिदान, वैद्यचिन्तामणि धन्वन्तरि निघण्टु इत्यादि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। पुनर्वसु आत्रेय के छह शिष्यों में अग्निवेश का तंत्र विशेष प्रसिद्ध हुआ। अग्निवेशतंत्र कायचिकित्सा प्रधान था। नाडीपरीक्षा और अग्निवेश-हस्तिशास्त्र नामक उसके ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। आत्रेय संहिता की पांडुलिपि विद्यमान है। आत्रेय के दूसरा शिष्य भेल (या भेड) की संहिता प्रकाशित हुई है।
चरक संहिता में शालाक्यतंत्र को आयुर्वेद का द्वितीय अंग माना है। नाक, कान, गला इत्यादि के रोगों की चिकित्सा में शलाका का उपयोग होने के कारण इस अंग को यह नाम प्राप्त हुआ।
शालाक्यतंत्रकारों में इन्द्रशिष्य निमि, निमि-शिष्य कराल तथा शौनक, कांकायन इत्यादि नाम प्रसिद्ध हैं। कराल ने 96 प्रकार के नेत्र-रोगों का निर्देश किया था, जिनका उल्लेख चरक-संहिता में हुआ है।
शल्यचिकित्सा आयुर्वेद का तृतीय अंग है जिसके प्रवर्तक थे दिवोदास धन्वन्तरि। इनके सात प्रमुख शिष्यों में सुश्रुत का नाम प्रसिद्ध है। सुश्रुत संहिता में शल्यमूलक आयुर्विज्ञान का प्रतिपादन हुआ है। इस संहिता के वृद्ध सुश्रुत और लघुसुश्रुत नामक दो पाठ प्रसिद्ध हैं।
कौमारभृत्या नामक अंग का जनकत्व कश्यपशिष्य जीवक या वृद्धजीवक को दिया जाता है। इनकी काश्यप संहिता (या वृद्धजीवकीय तंत्र) का प्रतिसंस्करण वात्स्य ने किया। इस विषय पर रावण कृत कुमारतंत्र, बालतंत्र, बालचिकित्सा उल्लेखनीय हैं। रावण के नाडीपरीक्षा, अर्कप्रकाश और उद्देशतंत्र नामक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं।
आयुर्वेद में "अगदतंत्र" शब्द का प्रयोग विष-प्रशामक उपाय के अर्थ में होता है (अगदो विषप्रतिकारः। तदर्थं तन्त्रम्) काश्यप, उशना, बृहस्पति, आलंवायन, दारुवाह, नग्नजित, आस्तिक आदि ऋषि इस अगदतंत्र के विशेषज्ञ थे।
रसायनतंत्र को आयुर्वेद का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है भृगु, अगस्त्य, वसिष्ठ, मांडव्य, व्याडि, पतंजलि, नागार्जुन इत्यादि आचार्य रसायनतंत्र के विशेषज्ञ थे।
उपरनिर्दिष्ट आठ अंगों के समान (1) स्वास्थ्यानुवृत्ति (2) रोगच्छेद और (3) औषधि नामक तीन स्कन्धों में भारतीय आयुर्विज्ञान का विभाजन किया जाता है जिसके कारण "त्रिस्कंध आयुर्वेद" यह पयोग रूढ हुआ है। चरक संहिता में कहा है कि (1) हितायु (2) अहितायु (3) सुखायु और दुःखायु इन चार प्रकारों से मानवी आयु का विचार आयुर्वेद का विषय है।
भारतीय आयुर्विज्ञान के अनुसार पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय अर्थात् स्थूल शरीर और चेतना का अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर, इन दो विभागों में शरीर की कल्पना की गई है। शरीरस्थ पंच महाभूतों एवं पंच तन्मात्राओं के संयोग से “पंचमहाभूतद्रव्य-गुण संग्रह" होता है और मन, बुद्धि आत्मा मिल कर “अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह" होता है।
___ प्राणी द्वारा भक्षित अन्न से जो सजीव कण शरीर में निर्माण होते हैं, उन्ही से कफ, वात और पित्त नामक तीन धातुओं (धारणाद् धातः) की निर्मिति होती है। त्रि-धातुओं की साम्यावस्था ही शरीर का स्वास्थ्य होता है। विषमता उत्पन्न होने पर इन्हीं धातुओं को "दोष' कहते हैं। आयुर्वेद की चिकिस्तापद्धति में त्रिधातु या त्रिदोष का विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है। इन्ही का प्रकोप होने पर शरीर में जो निरुपयोगी द्रव्य निर्माण होते हैं उन्हे “मल" कहते हैं। विस्कंधान्तर्गत स्वास्थ्यानुवृत्तिकर शास्त्र में धातुसाम्य का रक्षण और धातुवैषम्य का निवारण करने का विवेचन होता है। रोगोत्पति के तीन कारण होते हैं- (1) असात्म्य - इन्द्रियार्थ- संयोग, (2) प्रज्ञापराध और (3) परिणाम। अर्थात (1) भोग्य तथा भोज्य पदार्थ का अतिसेवन, विपरीत सेवन और अल्पसेवन या असेवन (2) स्वाभाविक मनःप्रवृति का हठात् निरोध या उद्रेक (3) ऋतुमान, विष, कृमि इत्यादि कारणों से रोगों की उत्पति शरीर में होती है।
कफ, बात पित्त इन तीन धातुओं से रस,रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन सात स्थूल धातुओं की उत्पत्ति होती है। इनमे जंतुरूप दोष उत्पन्न होने की संभावना होती है, अतः इन्हे “दूष्य"- कहते है। सप्त धातुओं में जंतुरूप दोषों का प्रादुर्भाव ही रोग है। शरीर समधातुमय तथा निर्मल रहना ही निरोगावस्था या आरोग्य है।
66 / संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only