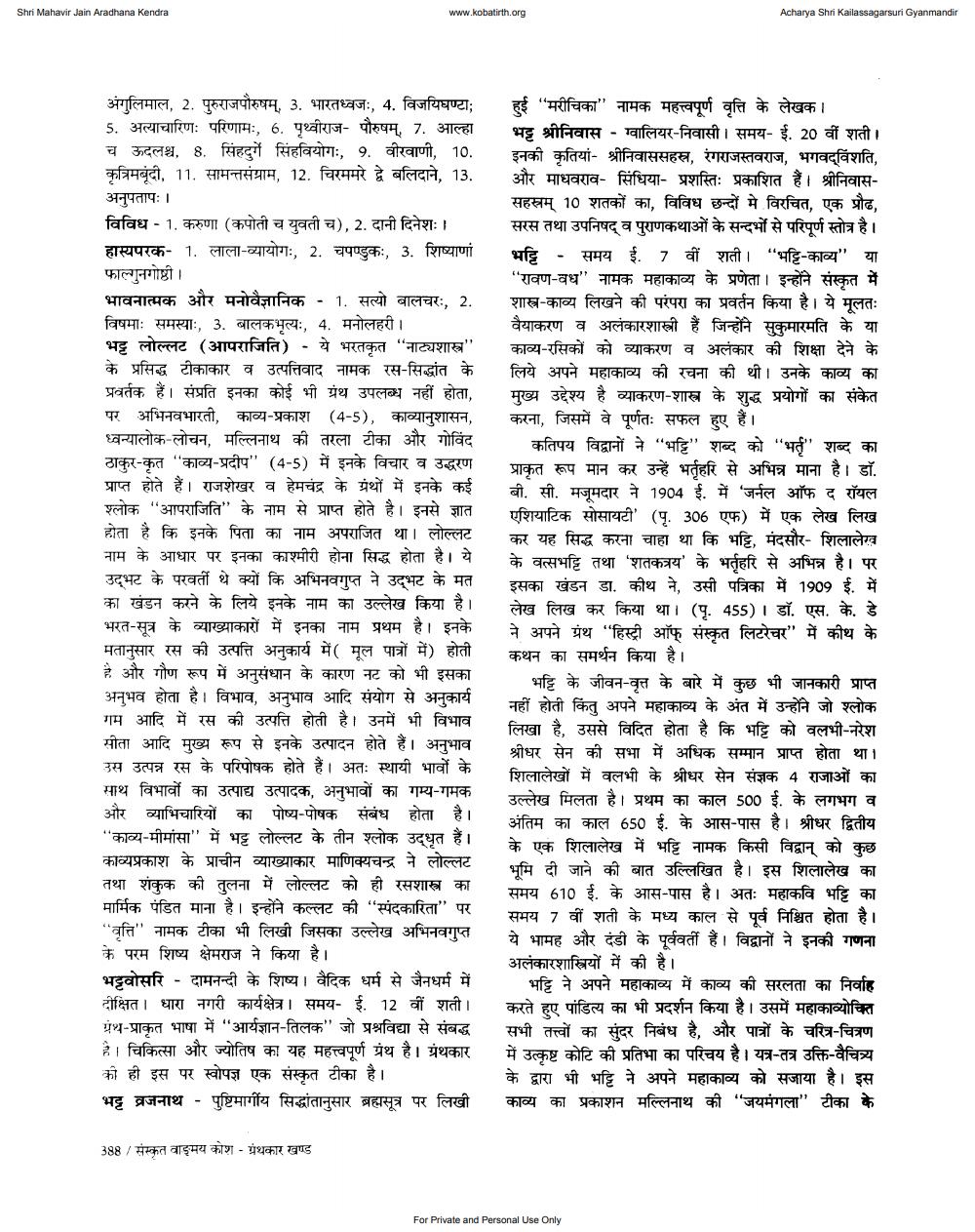________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
अंगुलिमाल, 2. पुरुराजपौरुषम्, 3. भारतध्वजः, 4. विजयिघण्टा; 5. अत्याचारिणः परिणामः, 6. पृथ्वीराज- पौरुषम्, 7. आल्हा च ऊदलच, 8, सिंहदुर्गे सिंहवियोगः, 9. वीरवाणी, 10. कृत्रिमबूंदी, 11. सामन्तसंग्राम, 12. चिरममरे द्वे बलिदाने, 13. अनुपतापः। विविध - 1. करुणा (कपोती च युवती च), 2. दानी दिनेशः। हास्यपरक- 1. लाला-व्यायोगः, 2. चपण्डुकः, 3. शिष्याणां फाल्गुनगोष्ठी। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक - 1. सत्यो बालचरः, 2. विषमाः समस्याः, 3. बालकभृत्यः, 4. मनोलहरी। भट्ट लोल्लट (आपराजिति) - ये भरतकृत "नाट्यशास्त्र" के प्रसिद्ध टीकाकार व उत्पत्तिवाद नामक रस-सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। संप्रति इनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, पर अभिनवभारती, काव्य-प्रकाश (4-5), काव्यानुशासन, ध्वन्यालोक-लोचन, मल्लिनाथ की तरला टीका और गोविंद ठाकुर-कृत "काव्य-प्रदीप" (4-5) में इनके विचार व उद्धरण प्राप्त होते हैं। राजशेखर व हेमचंद्र के ग्रंथों में इनके कई श्लोक "आपराजिति" के नाम से प्राप्त होते है। इनसे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम अपराजित था। लोल्लट नाम के आधार पर इनका काश्मीरी होना सिद्ध होता है। ये उद्भट के परवर्ती थे क्यों कि अभिनवगुप्त ने उद्भट के मत का खंडन करने के लिये इनके नाम का उल्लेख किया है। भरत-सूत्र के व्याख्याकारों में इनका नाम प्रथम है। इनके मतानुसार रस की उत्पत्ति अनुकार्य में( मूल पात्रों में) होती है, और गौण रूप में अनुसंधान के कारण नट को भी इसका अनुभव होता है। विभाव, अनुभाव आदि संयोग से अनुकार्य गम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। उनमें भी विभाव सीता आदि मुख्य रूप से इनके उत्पादन होते हैं। अनुभाव उस उत्पन्न रस के परिपोषक होते हैं। अतः स्थायी भावों के साथ विभावों का उत्पाद्य उत्पादक, अनुभावों का गम्य-गमक
और व्याभिचारियों का पोष्य-पोषक संबंध होता है। "काव्य-मीमांसा' में भट्ट लोल्लट के तीन श्लोक उद्धृत हैं। काव्यप्रकाश के प्राचीन व्याख्याकार माणिक्यचन्द्र ने लोल्लट तथा शंकुक की तुलना में लोल्लट को ही रसशास्त्र का मार्मिक पंडित माना है। इन्होंने कल्लट की "स्पंदकारिता" पर "वृत्ति' नामक टीका भी लिखी जिसका उल्लेख अभिनवगुप्त के परम शिष्य क्षेमराज ने किया है। भट्टवोसरि - दामनन्दी के शिष्य। वैदिक धर्म से जैनधर्म में दीक्षित। धारा नगरी कार्यक्षेत्र। समय- ई. 12 वीं शती। ग्रंथ-प्राकृत भाषा में "आर्यज्ञान-तिलक" जो प्रश्नविद्या से संबद्ध है। चिकित्सा और ज्योतिष का यह महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथकार को ही इस पर स्वोपज्ञ एक संस्कृत टीका है। भट्ट व्रजनाथ - पुष्टिमार्गीय सिद्धांतानुसार ब्रह्मसूत्र पर लिखी
हुई "मरीचिका" नामक महत्त्वपूर्ण वृत्ति के लेखक। भट्ट श्रीनिवास - ग्वालियर-निवासी। समय- ई. 20 वीं शती। इनकी कृतियां- श्रीनिवाससहस्र, रंगराजस्तवराज, भगवविंशति,
और माधवराव- सिंधिया- प्रशस्तिः प्रकाशित हैं। श्रीनिवाससहस्रम् 10 शतकों का, विविध छन्दों मे विरचित, एक प्रौढ, सरस तथा उपनिषद् व पुराणकथाओं के सन्दर्भो से परिपूर्ण स्तोत्र है। भट्टि • समय ई. 7 वीं शती। “भट्टि-काव्य" या "रावण-वध" नामक महाकाव्य के प्रणेता। इन्होंने संस्कृत में शास्त्र-काव्य लिखने की परंपरा का प्रवर्तन किया है। ये मूलतः वैयाकरण व अलंकारशास्त्री हैं जिन्होंने सुकुमारमति के या काव्य-रसिकों को व्याकरण व अलंकार की शिक्षा देने के लिये अपने महाकाव्य की रचना की थी। उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण-शास्त्र के शुद्ध प्रयोगों का संकेत करना, जिसमें वे पूर्णतः सफल हुए हैं।
कतिपय विद्वानों ने “भट्टि" शब्द को "भर्तृ" शब्द का प्राकृत रूप मान कर उन्हें भर्तृहरि से अभिन्न माना है। डॉ. बी. सी. मजूमदार ने 1904 ई. में 'जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी' (पृ. 306 एफ) में एक लेख लिख कर यह सिद्ध करना चाहा था कि भट्टि, मंदसौर- शिलालेख के वत्सभट्टि तथा 'शतकत्रय' के भर्तृहरि से अभिन्न है। पर इसका खंडन डा. कीथ ने, उसी पत्रिका में 1909 ई. में लेख लिख कर किया था। (पृ. 455)। डॉ. एस. के. डे ने अपने ग्रंथ "हिस्ट्री ऑफ् संस्कृत लिटरेचर" में कीथ के कथन का समर्थन किया है। ___ भट्टि के जीवन-वृत्त के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती किंतु अपने महाकाव्य के अंत में उन्होंने जो श्लोक लिखा है, उससे विदित होता है कि भट्टि को वलभी-नरेश श्रीधर सेन की सभा में अधिक सम्मान प्राप्त होता था। शिलालेखों में वलभी के श्रीधर सेन संज्ञक 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम का काल 500 ई. के लगभग व अंतिम का काल 650 ई. के आस-पास है। श्रीधर द्वितीय के एक शिलालेख में भट्टि नामक किसी विद्वान् को कुछ भूमि दी जाने की बात उल्लिखित है। इस शिलालेख का समय 610 ई. के आस-पास है। अतः महाकवि भट्टि का समय 7 वीं शती के मध्य काल से पूर्व निश्चित होता है। ये भामह और दंडी के पूर्ववर्ती हैं। विद्वानों ने इनकी गणना अलंकारशास्त्रियों में की है।
भट्टि ने अपने महाकाव्य में काव्य की सरलता का निर्वाह करते हए पांडित्य का भी प्रदर्शन किया है। उसमें महाकाव्योचित सभी तत्त्वों का सुंदर निबंध है, और पात्रों के चरित्र-चित्रण में उत्कष्ट कोटि की प्रतिभा का परिचय है। यत्र-तत्र उक्ति-वैचित्र्य के द्वारा भी भट्टि ने अपने महाकाव्य को सजाया है। इस काव्य का प्रकाशन मल्लिनाथ की "जयमंगला" टीका के
388 / संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only