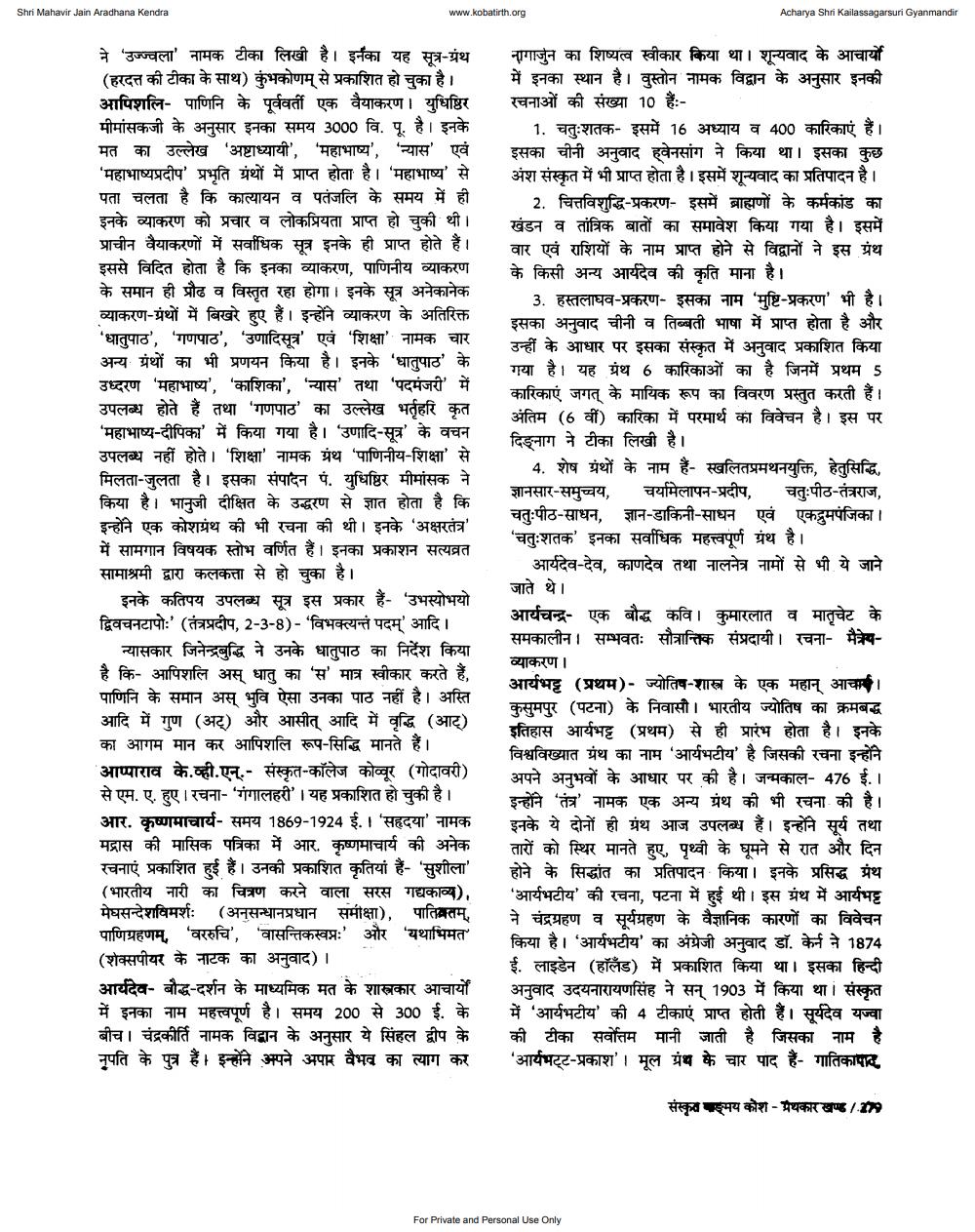________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
ने 'उज्ज्वला' नामक टीका लिखी है। इनका यह सूत्र-ग्रंथ (हरदत्त की टीका के साथ) कुंभकोणम् से प्रकाशित हो चुका है। आपिशलि- पाणिनि के पूर्ववर्ती एक वैयाकरण। युधिष्ठिर मीमांसकजी के अनुसार इनका समय 3000 वि. पू. है। इनके मत का उल्लेख 'अष्टाध्यायी', 'महाभाष्य', 'न्यास' एवं 'महाभाष्यप्रदीप' प्रभृति ग्रंथों में प्राप्त होता है। 'महाभाष्य' से पता चलता है कि कात्यायन व पतंजलि के समय में ही इनके व्याकरण को प्रचार व लोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी। प्राचीन वैयाकरणों में सर्वाधिक सूत्र इनके ही प्राप्त होते हैं। इससे विदित होता है कि इनका व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण के समान ही प्रौढ व विस्तृत रहा होगा। इनके सूत्र अनेकानेक व्याकरण-ग्रंथों में बिखरे हुए हैं। इन्होंने व्याकरण के अतिरिक्त 'धातुपाठ', 'गणपाठ', 'उणादिसूत्र' एवं 'शिक्षा' नामक चार
अन्य ग्रंथों का भी प्रणयन किया है। इनके 'धातुपाठ' के उध्दरण 'महाभाष्य', 'काशिका', 'न्यास' तथा 'पदमंजरी' में उपलब्ध होते हैं तथा 'गणपाठ' का उल्लेख भर्तृहरि कृत 'महाभाष्य-दीपिका' में किया गया है। 'उणादि-सूत्र' के वचन उपलब्ध नहीं होते। 'शिक्षा' नामक ग्रंथ 'पाणिनीय-शिक्षा' से मिलता-जुलता है। इसका संपादन पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने किया है। भानुजी दीक्षित के उद्धरण से ज्ञात होता है कि इन्होंने एक कोशग्रंथ की भी रचना की थी। इनके 'अक्षरतंत्र' में सामगान विषयक स्तोभ वर्णित हैं। इनका प्रकाशन सत्यव्रत सामाश्रमी द्वारा कलकत्ता से हो चुका है।
इनके कतिपय उपलब्ध सूत्र इस प्रकार हैं- 'उभस्योभयो द्विवचनटापोः' (तंत्रप्रदीप, 2-3-8)- 'विभक्त्यन्तं पदम्' आदि।
न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि ने उनके धातुपाठ का निर्देश किया है कि- आपिशलि अस् धातु का 'स' मात्र स्वीकार करते हैं, पाणिनि के समान अस् भुवि ऐसा उनका पाठ नहीं है। अस्ति आदि में गुण (अट्) और आसीत् आदि में वृद्धि (आट्) का आगम मान कर आपिशलि रूप-सिद्धि मानते हैं। आप्पाराव के.व्ही.एन.- संस्कृत-कॉलेज कोवूर (गोदावरी) से एम. ए. हुए । रचना- 'गंगालहरी' । यह प्रकाशित हो चुकी है। आर. कृष्णमाचार्य- समय 1869-1924 ई. । 'सहृदया' नामक मद्रास की मासिक पत्रिका में आर. कृष्णमाचार्य की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं- 'सुशीला' (भारतीय नारी का चित्रण करने वाला सरस गद्यकाव्य), मेघसन्देशविमर्शः (अनुसन्धानप्रधान समीक्षा), पातिव्रतम्, पाणिग्रहणम्, 'वररुचि', 'वासन्तिकस्वप्नः' और 'यथाभिमत' (शेक्सपीयर के नाटक का अनुवाद)। आर्यदेव- बौद्ध-दर्शन के माध्यमिक मत के शास्त्रकार आचार्यों में इनका नाम महत्त्वपूर्ण है। समय 200 से 300 ई. के बीच। चंद्रकीर्ति नामक विद्वान के अनुसार ये सिंहल द्वीप के नृपति के पुत्र हैं। इन्होंने अपने अपार वैभव का त्याग कर
नागार्जुन का शिष्यत्व स्वीकार किया था। शून्यवाद के आचार्यो में इनका स्थान है। वुस्तोन नामक विद्वान के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 10 हैं:
1. चतुःशतक- इसमें 16 अध्याय व 400 कारिकाएं हैं। इसका चीनी अनुवाद ह्वेनसांग ने किया था। इसका कुछ अंश संस्कृत में भी प्राप्त होता है। इसमें शून्यवाद का प्रतिपादन है।
2. चित्तविशुद्धि-प्रकरण- इसमें ब्राह्मणों के कर्मकांड का खंडन व तांत्रिक बातों का समावेश किया गया है। इसमें वार एवं राशियों के नाम प्राप्त होने से विद्वानों ने इस ग्रंथ के किसी अन्य आर्यदेव की कृति माना है। ___3. हस्तलाघव-प्रकरण- इसका नाम 'मुष्टि-प्रकरण' भी है। इसका अनुवाद चीनी व तिब्बती भाषा में प्राप्त होता है और उन्हीं के आधार पर इसका संस्कृत में अनुवाद प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ 6 कारिकाओं का है जिनमें प्रथम 5 कारिकाएं जगत् के मायिक रूप का विवरण प्रस्तुत करती हैं। अंतिम (6 वीं) कारिका में परमार्थ का विवेचन है। इस पर दिङ्नाग ने टीका लिखी है।
4. शेष ग्रंथों के नाम हैं- स्खलितप्रमथनयुक्ति, हेतुसिद्धि, ज्ञानसार-समुच्चय, चर्यामेलापन-प्रदीप, चतुःपीठ-तंत्रराज, चतुःपीठ-साधन, ज्ञान-डाकिनी-साधन एवं एकद्रुमपंजिका। 'चतुःशतक' इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। ___ आर्यदेव-देव, काणदेव तथा नालनेत्र नामों से भी ये जाने जाते थे। आर्यचन्द्र- एक बौद्ध कवि। कुमारलात व मातृचेट के समकालीन। सम्भवतः सौत्रान्तिक संप्रदायी। रचना- मैत्रेयव्याकरण। आर्यभट्ट (प्रथम)- ज्योतिष शास्त्र के एक महान् आचार्य। कुसुमपुर (पटना) के निवासी। भारतीय ज्योतिष का क्रमबद्ध इतिहास आर्यभट्ट (प्रथम) से ही प्रारंभ होता है। इनके विश्वविख्यात ग्रंथ का नाम 'आर्यभटीय' है जिसकी रचना इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर की है। जन्मकाल- 476 ई. । इन्होंने "तंत्र' नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। इनके ये दोनों ही ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। इन्होंने सूर्य तथा तारों को स्थिर मानते हुए, पृथ्वी के घूमने से रात और दिन होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'आर्यभटीय' की रचना, पटना में हुई थी। इस ग्रंथ में आर्यभट्ट ने चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहण के वैज्ञानिक कारणों का विवेचन किया है। 'आर्यभटीय' का अंग्रेजी अनुवाद डॉ. केर्न ने 1874 ई. लाइडेन (हॉलैंड) में प्रकाशित किया था। इसका हिन्दी अनुवाद उदयनारायणसिंह ने सन् 1903 में किया था। संस्कृत में 'आर्यभटीय' की 4 टीकाएं प्राप्त होती है। सूर्यदेव यज्वा की टीका सर्वोत्तम मानी जाती है जिसका नाम है 'आर्यभट्ट-प्रकाश'। मूल ग्रंथ के चार पाद हैं- गातिकापाद
संस्कृत वाङ्मय कोश-पथकारखण्ड/m
For Private and Personal Use Only