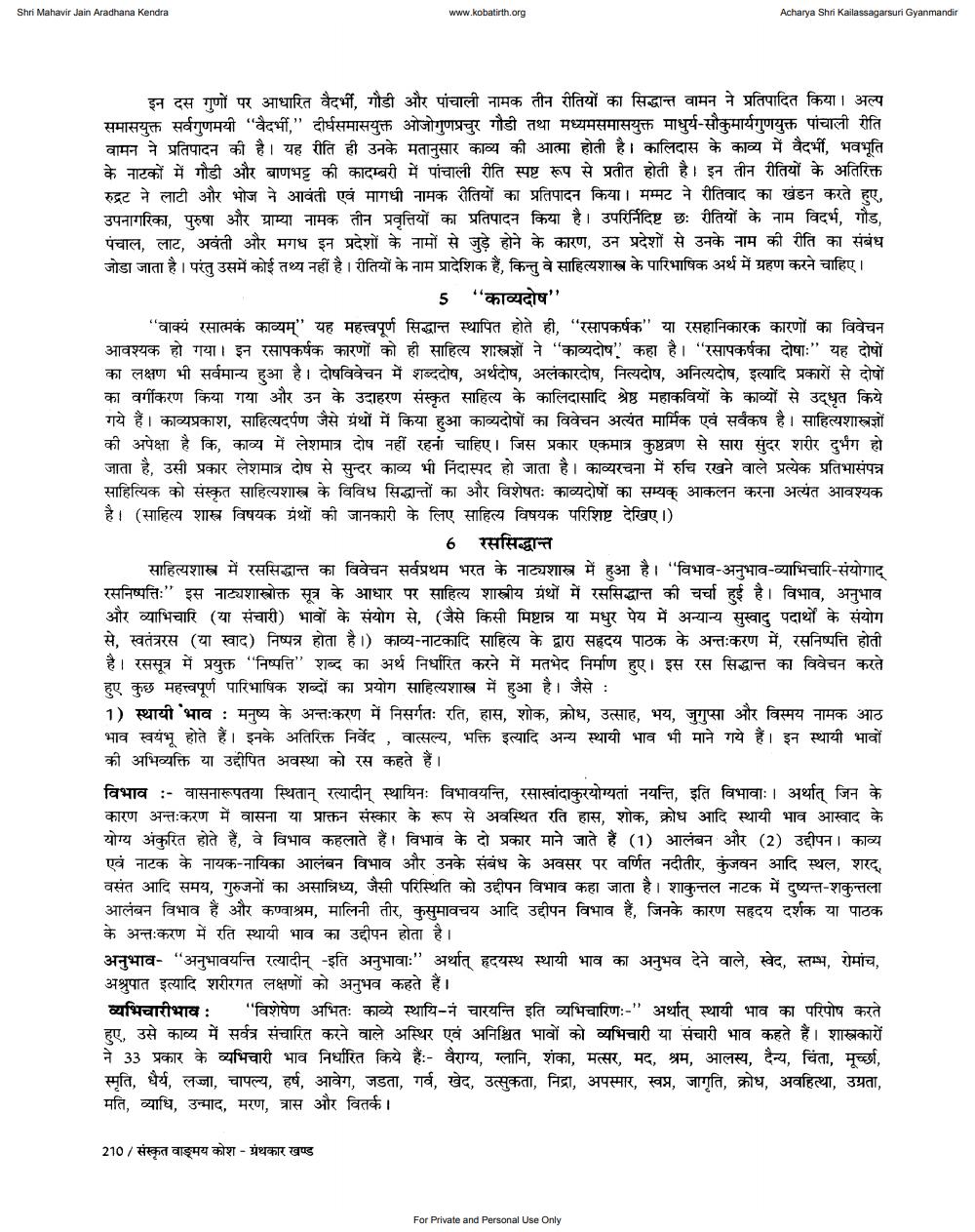________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
इन दस गुणों पर आधारित वैदर्भी, गौडी और पांचाली नामक तीन रीतियों का सिद्धान्त वामन ने प्रतिपादित किया। अल्प समासयुक्त सर्वगुणमयी “वैदर्भी," दीर्घसमासयुक्त ओजोगुणप्रचुर गौडी तथा मध्यमसमासयुक्त माधुर्य-सौकुमार्यगुणयुक्त पांचाली रीति वामन ने प्रतिपादन की है। यह रीति ही उनके मतानुसार काव्य की आत्मा होती है। कालिदास के काव्य में वैदर्भी, भवभूति के नाटकों में गौडी और बाणभट्ट की कादम्बरी में पांचाली रीति स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। इन तीन रीतियों के अतिरिक्त रुद्रट ने लाटी और भोज ने आवंती एवं मागधी नामक रीतियों का प्रतिपादन किया। मम्मट ने रीतिवाद का खंडन करते हुए, उपनागरिका, पुरुषा और ग्राम्या नामक तीन प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया है। उपरिनिदिष्ट छ: रीतियों के नाम विदर्भ, गौड, पंचाल, लाट, अवंती और मगध इन प्रदेशों के नामों से जुड़े होने के कारण, उन प्रदेशों से उनके नाम की रीति का संबंध जोडा जाता है। परंतु उसमें कोई तथ्य नहीं है। रीतियों के नाम प्रादेशिक हैं, किन्तु वे साहित्यशास्त्र के पारिभाषिक अर्थ में ग्रहण करने चाहिए।
5 "काव्यदोष" "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्" यह महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित होते ही, "रसापकर्षक" या रसहानिकारक कारणों का विवेचन आवश्यक हो गया। इन रसापकर्षक कारणों को ही साहित्य शास्त्रज्ञों ने “काव्यदोष' कहा है। "रसापकर्षका दोषाः" यह दोषों का लक्षण भी सर्वमान्य हुआ है। दोषविवेचन में शब्ददोष, अर्थदोष, अलंकारदोष, नित्यदोष, अनित्यदोष, इत्यादि प्रकारों से दोषों का वर्गीकरण किया गया और उन के उदाहरण संस्कृत साहित्य के कालिदासादि श्रेष्ठ महाकवियों के काव्यों से उद्धृत किये गये हैं। काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण जैसे ग्रंथों में किया हुआ काव्यदोषों का विवेचन अत्यंत मार्मिक एवं सर्वंकष है। साहित्यशास्त्रज्ञों की अपेक्षा है कि, काव्य में लेशमात्र दोष नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार एकमात्र कुष्ठव्रण से सारा सुंदर शरीर दुभंग हो जाता है, उसी प्रकार लेशमात्र दोष से सुन्दर काव्य भी निंदास्पद हो जाता है। काव्यरचना में रुचि रखने वाले प्रत्येक प्रतिभासंपन्न साहित्यिक को संस्कृत साहित्यशास्त्र के विविध सिद्धान्तों का और विशेषतः काव्यदोषों का सम्यक् आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। (साहित्य शास्त्र विषयक ग्रंथों की जानकारी के लिए साहित्य विषयक परिशिष्ट देखिए।)
6 रससिद्धान्त साहित्यशास्त्र में रससिद्धान्त का विवेचन सर्वप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र में हुआ है। "विभाव-अनुभाव-व्याभिचारि-संयोगाद् रसनिष्पत्तिः” इस नाट्यशास्त्रोक्त सूत्र के आधार पर साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में रससिद्धान्त की चर्चा हुई है। विभाव, अनुभाव
और व्याभिचारि (या संचारी) भावों के संयोग से, (जैसे किसी मिष्टान्न या मधुर पेय में अन्यान्य सुस्वादु पदार्थों के संयोग से, स्वतंत्ररस (या स्वाद) निष्पन्न होता है।) काव्य-नाटकादि साहित्य के द्वारा सहृदय पाठक के अन्तःकरण में, रसनिष्पत्ति होती है। रससूत्र में प्रयुक्त “निष्पत्ति" शब्द का अर्थ निर्धारित करने में मतभेद निर्माण हुए। इस रस सिद्धान्त का विवेचन करते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग साहित्यशास्त्र में हुआ है। जैसे : 1) स्थायी भाव : मनुष्य के अन्तःकरण में निसर्गतः रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय नामक आठ भाव स्वयंभू होते हैं। इनके अतिरिक्त निर्वेद , वात्सल्य, भक्ति इत्यादि अन्य स्थायी भाव भी माने गये हैं। इन स्थायी भावों की अभिव्यक्ति या उद्दीपित अवस्था को रस कहते हैं। विभाव :- वासनारूपतया स्थितान् रत्यादीन् स्थायिनः विभावयन्ति, रसास्वादाकुरयोग्यतां नयन्ति, इति विभावाः। अर्थात् जिन के कारण अन्तःकरण में वासना या प्राक्तन संस्कार के रूप से अवस्थित रति हास, शोक, क्रोध आदि स्थायी भाव आस्वाद के योग्य अंकुरित होते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो प्रकार माने जाते हैं (1) आलंबन और (2) उद्दीपन। काव्य एवं नाटक के नायक-नायिका आलंबन विभाव और उनके संबंध के अवसर पर वर्णित नदीतीर, कुंजवन आदि स्थल, शरद्, वसंत आदि समय, गुरुजनों का असान्निध्य, जैसी परिस्थिति को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। शाकुन्तल नाटक में दुष्यन्त-शकुन्तला आलंबन विभाव हैं और कण्वाश्रम, मालिनी तीर, कुसुमावचय आदि उद्दीपन विभाव हैं, जिनके कारण सहृदय दर्शक या पाठक के अन्तःकरण में रति स्थायी भाव का उद्दीपन होता है। अनुभाव- "अनुभावयन्ति रत्यादीन् -इति अनुभावाः" अर्थात् हृदयस्थ स्थायी भाव का अनुभव देने वाले, स्वेद, स्तम्भ, रोमांच, अश्रुपात इत्यादि शरीरगत लक्षणों को अनुभव कहते हैं। व्यभिचारीभाव : "विशेषेण अभितः काव्ये स्थायि-नं चारयन्ति इति व्यभिचारिणः-" अर्थात् स्थायी भाव का परिपोष करते हुए, उसे काव्य में सर्वत्र संचारित करने वाले अस्थिर एवं अनिश्चित भावों को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। शास्त्रकारों ने 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव निर्धारित किये हैं:- वैराग्य, ग्लानि, शंका, मत्सर, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मूर्छा, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, खेद, उत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, जागृति, क्रोध, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क।
स भाव कहते हैं। शास्र
शका, मत्सर, मद,
गर्व, खेद, उ
210/ संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only