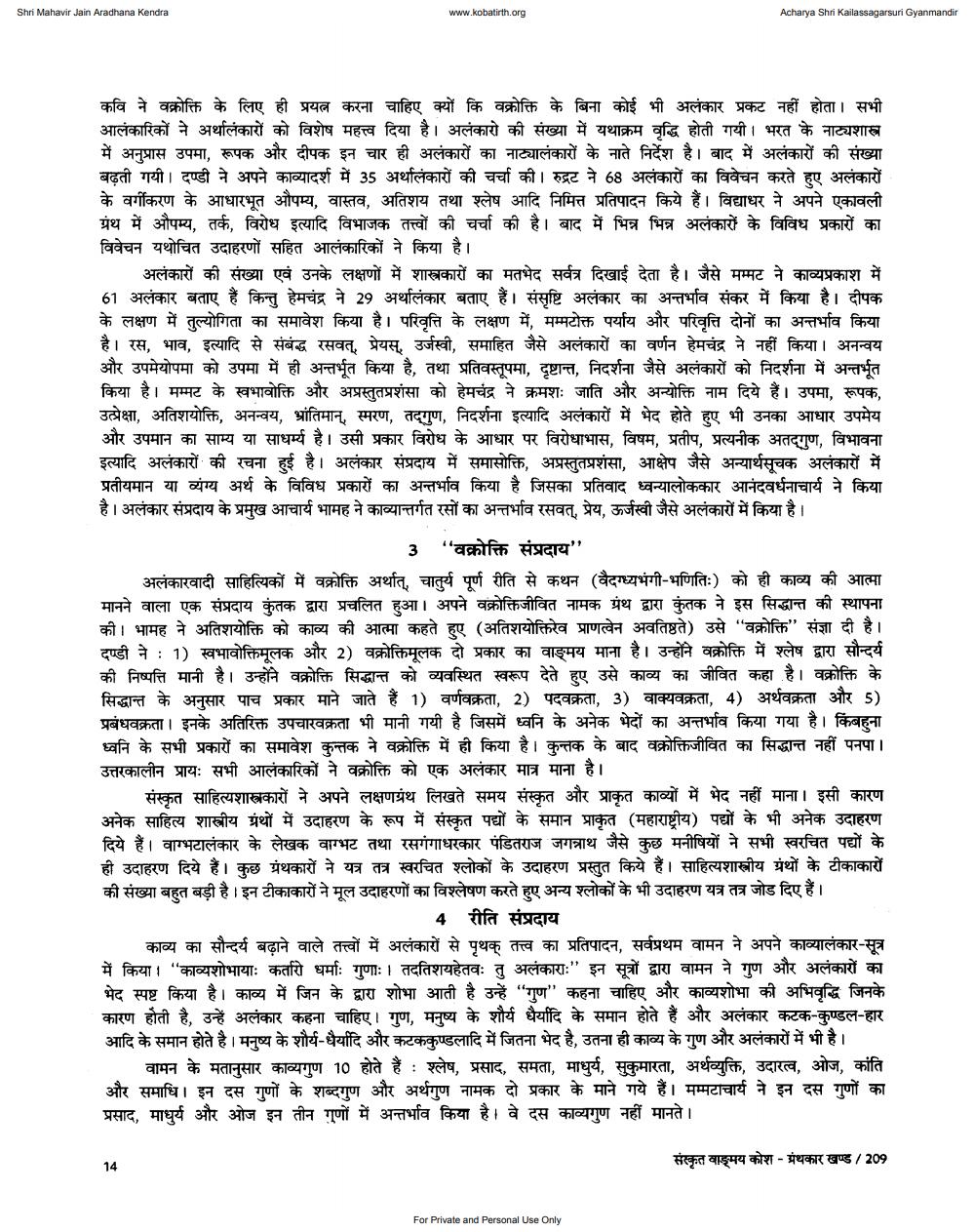________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
कवि ने वक्रोक्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए क्यों कि वक्रोक्ति के बिना कोई भी अलंकार प्रकट नहीं होता। सभी आलंकारिकों ने अर्थालंकारों को विशेष महत्त्व दिया है। अलंकारो की संख्या में यथाक्रम वृद्धि होती गयी। भरत के नाट्यशास्त्र में अनुप्रास उपमा, रूपक और दीपक इन चार ही अलंकारों का नाट्यालंकारों के नाते निर्देश है। बाद में अलंकारों की संख्या बढ़ती गयी। दण्डी ने अपने काव्यादर्श में 35 अर्थालंकारों की चर्चा की। रुद्रट ने 68 अलंकारों का विवेचन करते हुए अलंकारों के वर्गीकरण के आधारभूत औपम्य, वास्तव, अतिशय तथा श्लेष आदि निमित्त प्रतिपादन किये हैं। विद्याधर ने अपने एकावली ग्रंथ में औपम्य, तर्क, विरोध इत्यादि विभाजक तत्त्वों की चर्चा की है। बाद में भिन्न भिन्न अलंकारों के विविध प्रकारों का विवेचन यथोचित उदाहरणों सहित आलंकारिकों ने किया है।
अलंकारों की संख्या एवं उनके लक्षणों में शास्त्रकारों का मतभेद सर्वत्र दिखाई देता है। जैसे मम्मट ने काव्यप्रकाश में 61 अलंकार बताए हैं किन्तु हेमचंद्र ने 29 अर्थालंकार बताए हैं। संसृष्टि अलंकार का अन्तर्भाव संकर में किया है। दीपक के लक्षण में तुल्योगिता का समावेश किया है। परिवृत्ति के लक्षण में, मम्मटोक्त पर्याय और परिवृत्ति दोनों का अन्तर्भाव किया है। रस, भाव, इत्यादि से संबंद्ध रसवत्, प्रेयस्, उर्जस्वी, समाहित जैसे अलंकारों का वर्णन हेमचंद्र ने नहीं किया। अनन्वय
और उपमेयोपमा को उपमा में ही अन्तर्भूत किया है, तथा प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना जैसे अलंकारों को निदर्शना में अन्तर्भूत किया है। मम्मट के स्वभावोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंसा को हेमचंद्र ने क्रमशः जाति और अन्योक्ति नाम दिये हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनन्वय, भ्रांतिमान्, स्मरण, तद्गुण, निदर्शना इत्यादि अलंकारों में भेद होते हुए भी उनका आधार उपमेय
और उपमान का साम्य या साधर्म्य है। उसी प्रकार विरोध के आधार पर विरोधाभास, विषम, प्रतीप, प्रत्यनीक अतद्गुण, विभावना इत्यादि अलंकारों की रचना हुई है। अलंकार संप्रदाय में समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, आक्षेप जैसे अन्यार्थसूचक अलंकारों में प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थ के विविध प्रकारों का अन्तर्भाव किया है जिसका प्रतिवाद ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य ने किया है। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भामह ने काव्यान्तर्गत रसों का अन्तर्भाव रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वी जैसे अलंकारों में किया है।
3 "वक्रोक्ति संप्रदाय" अलंकारवादी साहित्यिकों में वक्रोक्ति अर्थात्, चातुर्य पूर्ण रीति से कथन (वैदग्ध्यभंगी-भणितिः) को ही काव्य की आत्मा मानने वाला एक संप्रदाय कुंतक द्वारा प्रचलित हुआ। अपने वक्रोक्तिजीवित नामक ग्रंथ द्वारा कुंतक ने इस सिद्धान्त की स्थापना की। भामह ने अतिशयोक्ति को काव्य की आत्मा कहते हुए (अतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेन अवतिष्ठते) उसे “वक्रोक्ति" संज्ञा दी है। दण्डी ने : 1) स्वभावोक्तिमूलक और 2) वक्रोक्तिमूलक दो प्रकार का वाङ्मय माना है। उन्होंने वक्रोक्ति में श्लेष द्वारा सौन्दर्य की निष्पत्ति मानी है। उन्होंने वक्रोक्ति सिद्धान्त को व्यवस्थित स्वरूप देते हुए उसे काव्य का जीवित कहा है। वक्रोक्ति के सिद्धान्त के अनुसार पाच प्रकार माने जाते हैं 1) वर्णवक्रता, 2) पदवक्रता, 3) वाक्यवक्रता, 4) अर्थवक्रता और 5) प्रबंधवक्रता। इनके अतिरिक्त उपचारवक्रता भी मानी गयी है जिसमें ध्वनि के अनेक भेदों का अन्तर्भाव किया गया है। किंबहुना ध्वनि के सभी प्रकारों का समावेश कुन्तक ने वक्रोक्ति में ही किया है। कुन्तक के बाद वक्रोक्तिजीवित का सिद्धान्त नहीं पनपा। उत्तरकालीन प्रायः सभी आलंकारिकों ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मात्र माना है।
संस्कृत साहित्यशास्त्रकारों ने अपने लक्षणग्रंथ लिखते समय संस्कृत और प्राकृत काव्यों में भेद नहीं माना। इसी कारण अनेक साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में उदाहरण के रूप में संस्कृत पद्यों के समान प्राकृत (महाराष्ट्रीय) पद्यों के भी अनेक उदाहरण दिये हैं। वाग्भटालंकार के लेखक वाग्भट तथा रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ जैसे कुछ मनीषियों ने सभी स्वरचित पद्यों के ही उदाहरण दिये हैं। कुछ ग्रंथकारों ने यत्र तत्र स्वरचित श्लोकों के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। साहित्यशास्त्रीय ग्रंथों के टीकाकारों की संख्या बहुत बड़ी है। इन टीकाकारों ने मूल उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए अन्य श्लोकों के भी उदाहरण यत्र तत्र जोड दिए हैं।
4 रीति संप्रदाय काव्य का सौन्दर्य बढ़ाने वाले तत्त्वों में अलंकारों से पृथक् तत्त्व का प्रतिपादन, सर्वप्रथम वामन ने अपने काव्यालंकार-सूत्र में किया। "काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। तदतिशयहेतवः तु अलंकाराः" इन सूत्रों द्वारा वामन ने गुण और अलंकारों का भेद स्पष्ट किया है। काव्य में जिन के द्वारा शोभा आती है उन्हें "गुण" कहना चाहिए और काव्यशोभा की अभिवृद्धि जिनके कारण होती है, उन्हें अलंकार कहना चाहिए। गुण, मनुष्य के शौर्य धैर्यादि के समान होते हैं और अलंकार कटक-कुण्डल-हार आदि के समान होते है। मनुष्य के शौर्य-धैर्यादि और कटककुण्डलादि में जितना भेद है, उतना ही काव्य के गुण और अलंकारों में भी है।
वामन के मतानुसार काव्यगुण 10 होते हैं : श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्युक्ति, उदारत्व, ओज, कांति और समाधि। इन दस गुणों के शब्दगुण और अर्थगुण नामक दो प्रकार के माने गये हैं। मम्मटाचार्य ने इन दस गुणों का प्रसाद, माधुर्य और ओज इन तीन गुणों में अन्तर्भाव किया है। वे दस काव्यगुण नहीं मानते।
14
संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड / 209
For Private and Personal Use Only