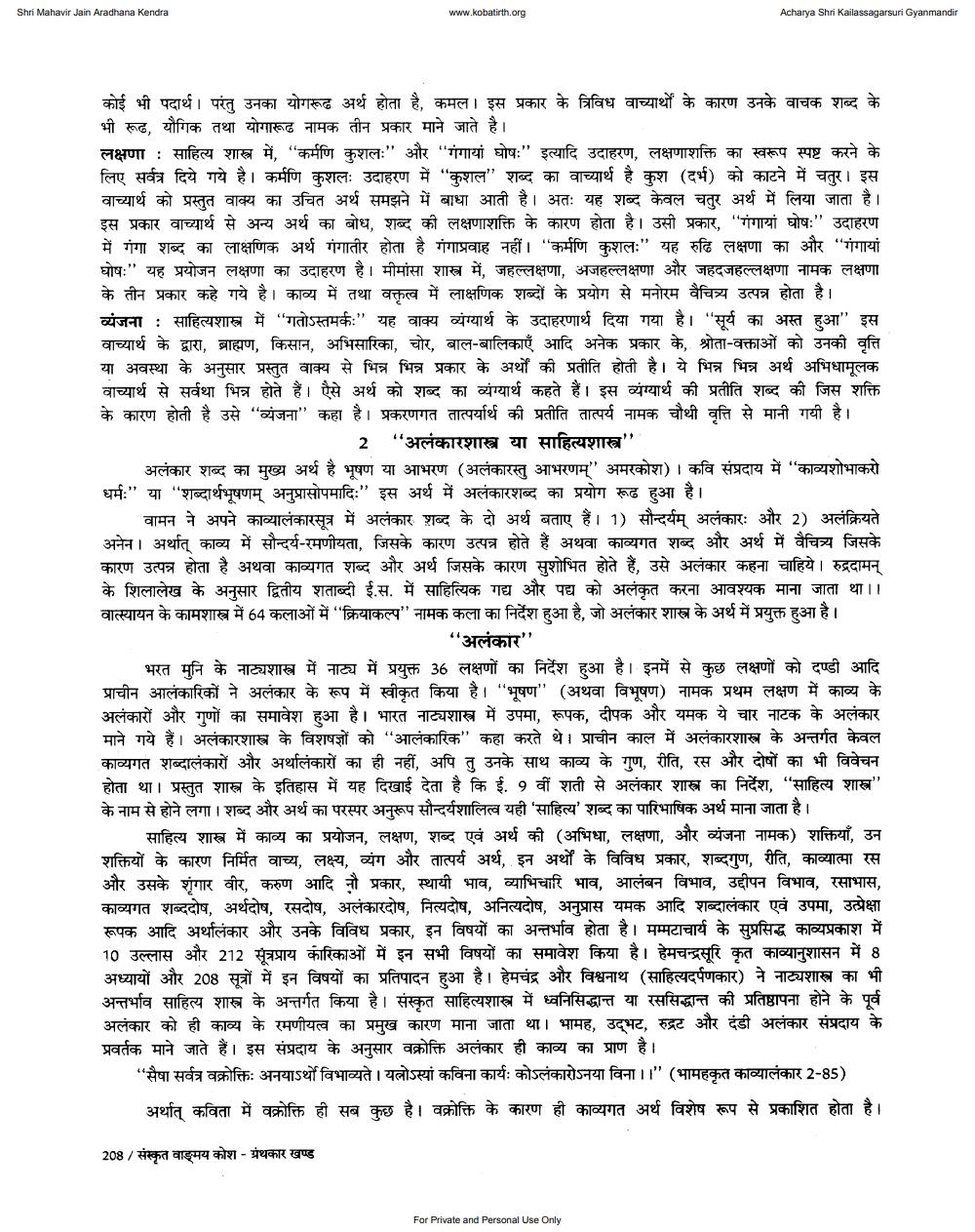________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
कोई भी पदार्थ। परंतु उनका योगरूढ अर्थ होता है, कमल। इस प्रकार के त्रिविध वाच्यार्थों के कारण उनके वाचक शब्द के भी रूढ, यौगिक तथा योगारूढ नामक तीन प्रकार माने जाते है। लक्षणा : साहित्य शास्त्र में, “कर्मणि कुशलः" और "गंगायां घोषः" इत्यादि उदाहरण, लक्षणाशक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए सर्वत्र दिये गये है। कर्मणि कुशलः उदाहरण में "कुशल" शब्द का वाच्यार्थ है कुश (दर्भ) को काटने में चतुर। इस वाच्यार्थ को प्रस्तुत वाक्य का उचित अर्थ समझने में बाधा आती है। अतः यह शब्द केवल चतुर अर्थ में लिया जाता है। इस प्रकार वाच्यार्थ से अन्य अर्थ का बोध, शब्द की लक्षणाशक्ति के कारण होता है। उसी प्रकार, "गंगायां घोषः" उदाहरण में गंगा शब्द का लाक्षणिक अर्थ गंगातीर होता है गंगाप्रवाह नहीं। "कर्मणि कुशलः" यह रुढि लक्षणा का और "गंगायां घोषः" यह प्रयोजन लक्षणा का उदाहरण है। मीमांसा शास्त्र में, जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा और जहदजहल्लक्षणा नामक लक्षणा के तीन प्रकार कहे गये है। काव्य में तथा वक्तृत्व में लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से मनोरम वैचित्र्य उत्पन्न होता है। व्यंजना : साहित्यशास्त्र में “गतोऽस्तमर्कः" यह वाक्य व्यंग्यार्थ के उदाहरणार्थ दिया गया है। "सूर्य का अस्त हुआ" इस वाच्यार्थ के द्वारा, ब्राह्मण, किसान, अभिसारिका, चोर, बाल-बालिकाएँ आदि अनेक प्रकार के, श्रोता-वक्ताओं को उनकी वृत्ति या अवस्था के अनुसार प्रस्तुत वाक्य से भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों की प्रतीति होती है। ये भिन्न भिन्न अर्थ अभिधामूलक वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे अर्थ को शब्द का व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस व्यंग्यार्थ की प्रतीति शब्द की जिस शक्ति के कारण होती है उसे "व्यंजना" कहा है। प्रकरणगत तात्पर्यार्थ की प्रतीति तात्पर्य नामक चौथी वृत्ति से मानी गयी है।
2 "अलंकारशास्त्र या साहित्यशास्त्र" ___ अलंकार शब्द का मुख्य अर्थ है भूषण या आभरण (अलंकारस्तु आभरणम्" अमरकोश)। कवि संप्रदाय में “काव्यशोभाकरो धर्मः" या "शब्दार्थभूषणम् अनुप्रासोपमादिः” इस अर्थ में अलंकारशब्द का प्रयोग रूढ हुआ है।
__ वामन ने अपने काव्यालंकारसूत्र में अलंकार शब्द के दो अर्थ बताए हैं। 1) सौन्दर्यम् अलंकारः और 2) अलंक्रियते अनेन। अर्थात् काव्य में सौन्दर्य-रमणीयता, जिसके कारण उत्पन्न होते हैं अथवा काव्यगत शब्द और अर्थ में वैचित्र्य जिसके कारण उत्पन्न होता है अथवा काव्यगत शब्द और अर्थ जिसके कारण सुशोभित होते हैं, उसे अलंकार कहना चाहिये। रुद्रदामन् के शिलालेख के अनुसार द्वितीय शताब्दी ई.स. में साहित्यिक गद्य और पद्य को अलंकृत करना आवश्यक माना जाता था।। वात्स्यायन के कामशास्त्र में 64 कलाओं में "क्रियाकल्प" नामक कला का निर्देश हुआ है, जो अलंकार शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
"अलंकार" भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाट्य में प्रयुक्त 36 लक्षणों का निर्देश हुआ है। इनमें से कुछ लक्षणों को दण्डी आदि प्राचीन आलंकारिकों ने अलंकार के रूप में स्वीकृत किया है। "भूषण" (अथवा विभूषण) नामक प्रथम लक्षण में काव्य के अलंकारों और गुणों का समावेश हुआ है। भारत नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और यमक ये चार नाटक के अलंकार माने गये हैं। अलंकारशास्त्र के विशषज्ञों को “आलंकारिक" कहा करते थे। प्राचीन काल में अलंकारशास्त्र के अन्तर्गत केवल काव्यगत शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का ही नहीं, अपि तु उनके साथ काव्य के गुण, रीति, रस और दोषों का भी विवेचन होता था। प्रस्तुत शास्त्र के इतिहास में यह दिखाई देता है कि ई. 9 वीं शती से अलंकार शास्त्र का निर्देश, “साहित्य शास्त्र" के नाम से होने लगा। शब्द और अर्थ का परस्पर अनुरूप सौन्दर्यशालित्व यही 'साहित्य' शब्द का पारिभाषिक अर्थ माना जाता है।
साहित्य शास्त्र में काव्य का प्रयोजन, लक्षण, शब्द एवं अर्थ की (अभिधा, लक्षणा, और व्यंजना नामक) शक्तियाँ, उन शक्तियों के कारण निर्मित वाच्य, लक्ष्य, व्यंग और तात्पर्य अर्थ, इन अर्थों के विविध प्रकार, शब्दगुण, रीति, काव्यात्मा रस और उसके शृंगार वीर, करुण आदि नौ प्रकार, स्थायी भाव, व्याभिचारि भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, रसाभास, काव्यगत शब्ददोष, अर्थदोष, रसदोष, अलंकारदोष, नित्यदोष, अनित्यदोष, अनुप्रास यमक आदि शब्दालंकार एवं उपमा, उत्प्रेक्षा रूपक आदि अर्थालंकार और उनके विविध प्रकार, इन विषयों का अन्तर्भाव होता है। मम्मटाचार्य के सुप्रसिद्ध काव्यप्रकाश में 10 उल्लास और 212 सूत्रप्राय कारिकाओं में इन सभी विषयों का समावेश किया है। हेमचन्द्रसूरि कृत काव्यानुशासन में 8 अध्यायों और 208 सूत्रों में इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है। हेमचंद्र और विश्वनाथ (साहित्यदर्पणकार) ने नाट्यशास्त्र का भी अन्तर्भाव साहित्य शास्त्र के अन्तर्गत किया है। संस्कृत साहित्यशास्त्र में ध्वनिसिद्धान्त या रससिद्धान्त की प्रतिष्ठापना होने के पूर्व अलंकार को ही काव्य के रमणीयत्व का प्रमुख कारण माना जाता था। भामह, उद्भट, रुद्रट और दंडी अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय के अनुसार वक्रोक्ति अलंकार ही काव्य का प्राण है।
"सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः अनयाऽर्थो विभाव्यते । यत्रोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।।" (भामहकृत काव्यालंकार 2-85) अर्थात् कविता में वक्रोक्ति ही सब कुछ है। वक्रोक्ति के कारण ही काव्यगत अर्थ विशेष रूप से प्रकाशित होता है।
208 / संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only