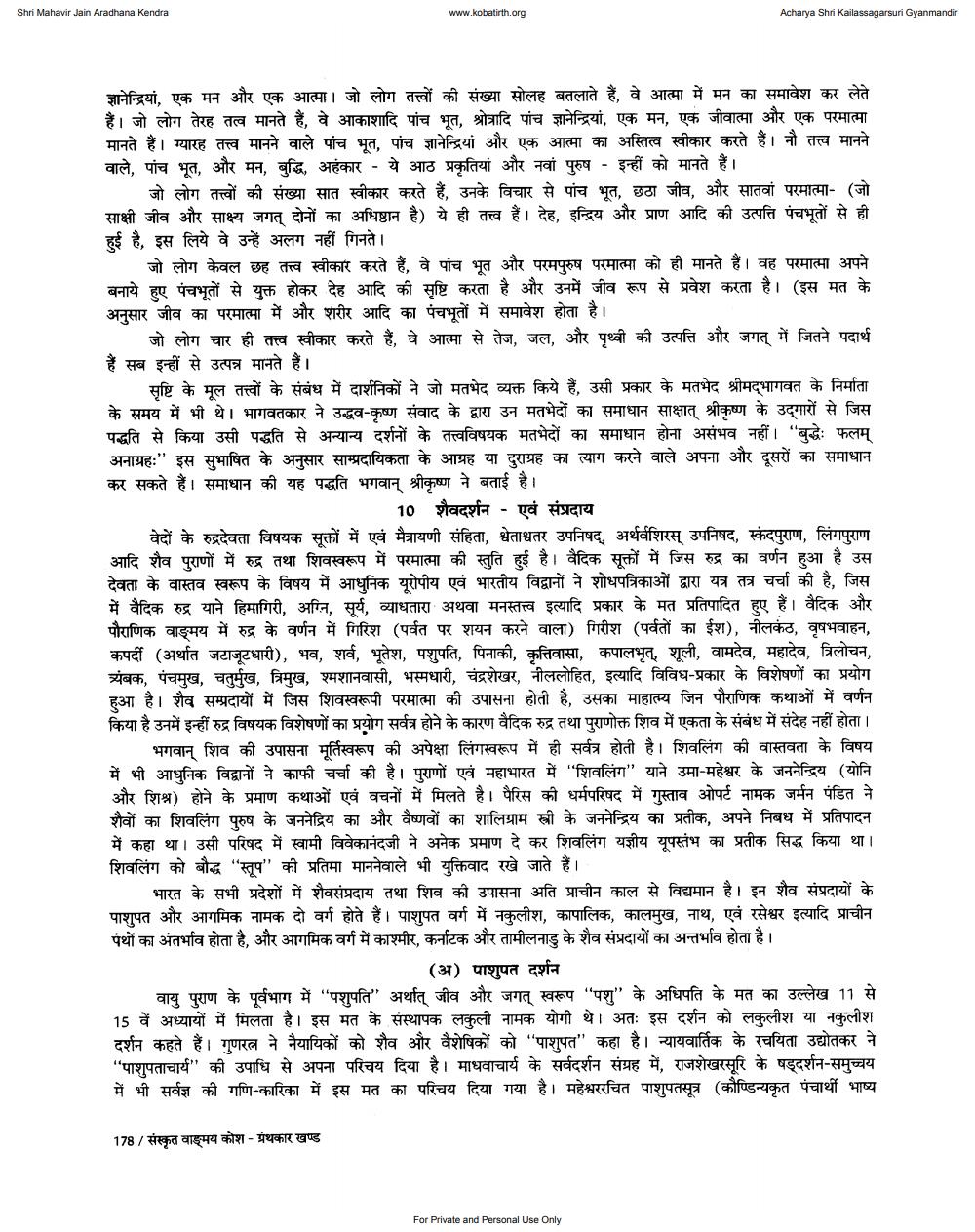________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
ज्ञानेन्द्रियां, एक मन और एक आत्मा। जो लोग तत्त्वों की संख्या सोलह बतलाते हैं, वे आत्मा में मन का समावेश कर लेते हैं। जो लोग तेरह तत्व मानते हैं, वे आकाशादि पांच भूत, श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियां, एक मन, एक जीवात्मा और एक परमात्मा मानते हैं। ग्यारह तत्त्व मानने वाले पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। नौ तत्त्व मानने वाले, पांच भूत, और मन, बुद्धि, अहंकार - ये आठ प्रकृतियां और नवां पुरुष - इन्हीं को मानते हैं।
जो लोग तत्त्वों की संख्या सात स्वीकार करते हैं, उनके विचार से पांच भूत, छठा जीव, और सातवां परमात्मा- (जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत् दोनों का अधिष्ठान है) ये ही तत्त्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति पंचभूतों से ही हुई है, इस लिये वे उन्हें अलग नहीं गिनते।
जो लोग केवल छह तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे पांच भूत और परमपुरुष परमात्मा को ही मानते हैं। वह परमात्मा अपने बनाये हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। (इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश होता है।
जो लोग चार ही तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे आत्मा से तेज, जल, और पृथ्वी की उत्पत्ति और जगत् में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न मानते हैं।
सृष्टि के मूल तत्त्वों के संबंध में दार्शनिकों ने जो मतभेद व्यक्त किये हैं, उसी प्रकार के मतभेद श्रीमद्भागवत के निर्माता के समय में भी थे। भागवतकार ने उद्धव-कृष्ण संवाद के द्वारा उन मतभेदों का समाधान साक्षात् श्रीकृष्ण के उद्गारों से जिस पद्धति से किया उसी पद्धति से अन्यान्य दर्शनों के तत्त्वविषयक मतभेदों का समाधान होना असंभव नहीं। "बुद्धेः फलम् अनाग्रहः” इस सुभाषित के अनुसार साम्प्रदायिकता के आग्रह या दुराग्रह का त्याग करने वाले अपना और दूसरों का समाधान कर सकते हैं। समाधान की यह पद्धति भगवान् श्रीकृष्ण ने बताई है।
10 शैवदर्शन - एवं संप्रदाय वेदों के रुद्रदेवता विषयक सूक्तों में एवं मैत्रायणी संहिता, श्वेताश्वतर उपनिषद्, अर्थर्वशिरस् उपनिषद, स्कंदपुराण, लिंगपुराण आदि शैव पुराणों में रुद्र तथा शिवस्वरूप में परमात्मा की स्तुति हुई है। वैदिक सूक्तों में जिस रुद्र का वर्णन हुआ है उस देवता के वास्तव स्वरूप के विषय में आधुनिक यूरोपीय एवं भारतीय विद्वानों ने शोधपत्रिकाओं द्वारा यत्र तत्र चर्चा की है, जिस में वैदिक रुद्र याने हिमागिरी, अग्नि, सूर्य, व्याधतारा अथवा मनस्तत्त्व इत्यादि प्रकार के मत प्रतिपादित हुए हैं। वैदिक और पौराणिक वाङ्मय में रुद्र के वर्णन में गिरिश (पर्वत पर शयन करने वाला) गिरीश (पर्वतों का ईश), नीलकंठ, वृषभवाहन, कपर्दी (अर्थात जटाजूटधारी), भव, शर्व, भूतेश, पशुपति, पिनाकी, कृत्तिवासा, कपालभृत्, शूली, वामदेव, महादेव, त्रिलोचन, त्र्यंबक, पंचमुख, चतुर्मुख, त्रिमुख, श्मशानवासी, भस्मधारी, चंद्रशेखर, नीललोहित, इत्यादि विविध-प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है। शैव सम्प्रदायों में जिस शिवस्वरूपी परमात्मा की उपासना होती है, उसका माहात्म्य जिन पौराणिक कथाओं में वर्णन किया है उनमें इन्हीं रुद्र विषयक विशेषणों का प्रयोग सर्वत्र होने के कारण वैदिक रुद्र तथा पुराणोक्त शिव में एकता के संबंध में संदेह नहीं होता।
भगवान् शिव की उपासना मूर्तिस्वरूप की अपेक्षा लिंगस्वरूप में ही सर्वत्र होती है। शिवलिंग की वास्तवता के विषय में भी आधुनिक विद्वानों ने काफी चर्चा की है। पुराणों एवं महाभारत में "शिवलिंग" याने उमा-महेश्वर के जननेन्द्रिय (योनि
और शिश्न) होने के प्रमाण कथाओं एवं वचनों में मिलते है। पैरिस की धर्मपरिषद में गुस्ताव ओपर्ट नामक जर्मन पंडित ने शैवों का शिवलिंग पुरुष के जननेद्रिय का और वैष्णवों का शालिग्राम स्त्री के जननेन्द्रिय का प्रतीक, अपने निबध में प्रतिपादन में कहा था। उसी परिषद में स्वामी विवेकानंदजी ने अनेक प्रमाण दे कर शिवलिंग यज्ञीय यूपस्तंभ का प्रतीक सिद्ध किया था। शिवलिंग को बौद्ध "स्तूप" की प्रतिमा माननेवाले भी युक्तिवाद रखे जाते हैं।
___भारत के सभी प्रदेशों में शैवसंप्रदाय तथा शिव की उपासना अति प्राचीन काल से विद्यमान है। इन शैव संप्रदायों के पाशुपत और आगमिक नामक दो वर्ग होते हैं। पाशुपत वर्ग में नकुलीश, कापालिक, कालमुख, नाथ, एवं रसेश्वर इत्यादि प्राचीन पंथों का अंतर्भाव होता है, और आगमिक वर्ग में काश्मीर, कर्नाटक और तामीलनाडु के शैव संप्रदायों का अन्तर्भाव होता है।
(अ) पाशुपत दर्शन। वायु पुराण के पूर्वभाग में "पशुपति" अर्थात् जीव और जगत् स्वरूप “पशु" के अधिपति के मत का उल्लेख 11 से 15 वें अध्यायों में मिलता है। इस मत के संस्थापक लकुली नामक योगी थे। अतः इस दर्शन को लकुलीश या नकुलीश दर्शन कहते हैं। गुणरत्न ने नैयायिकों को शैव और वैशेषिकों को "पाशुपत" कहा है। न्यायवार्तिक के रचयिता उद्योतकर ने "पाशुपताचार्य" की उपाधि से अपना परिचय दिया है। माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह में, राजशेखरसूरि के षड्दर्शन-समुच्चय में भी सर्वज्ञ की गणि-कारिका में इस मत का परिचय दिया गया है। महेश्वरचित पाशुपतसूत्र (कौण्डिन्यकृत पंचार्थी भाष्य
178 / संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only