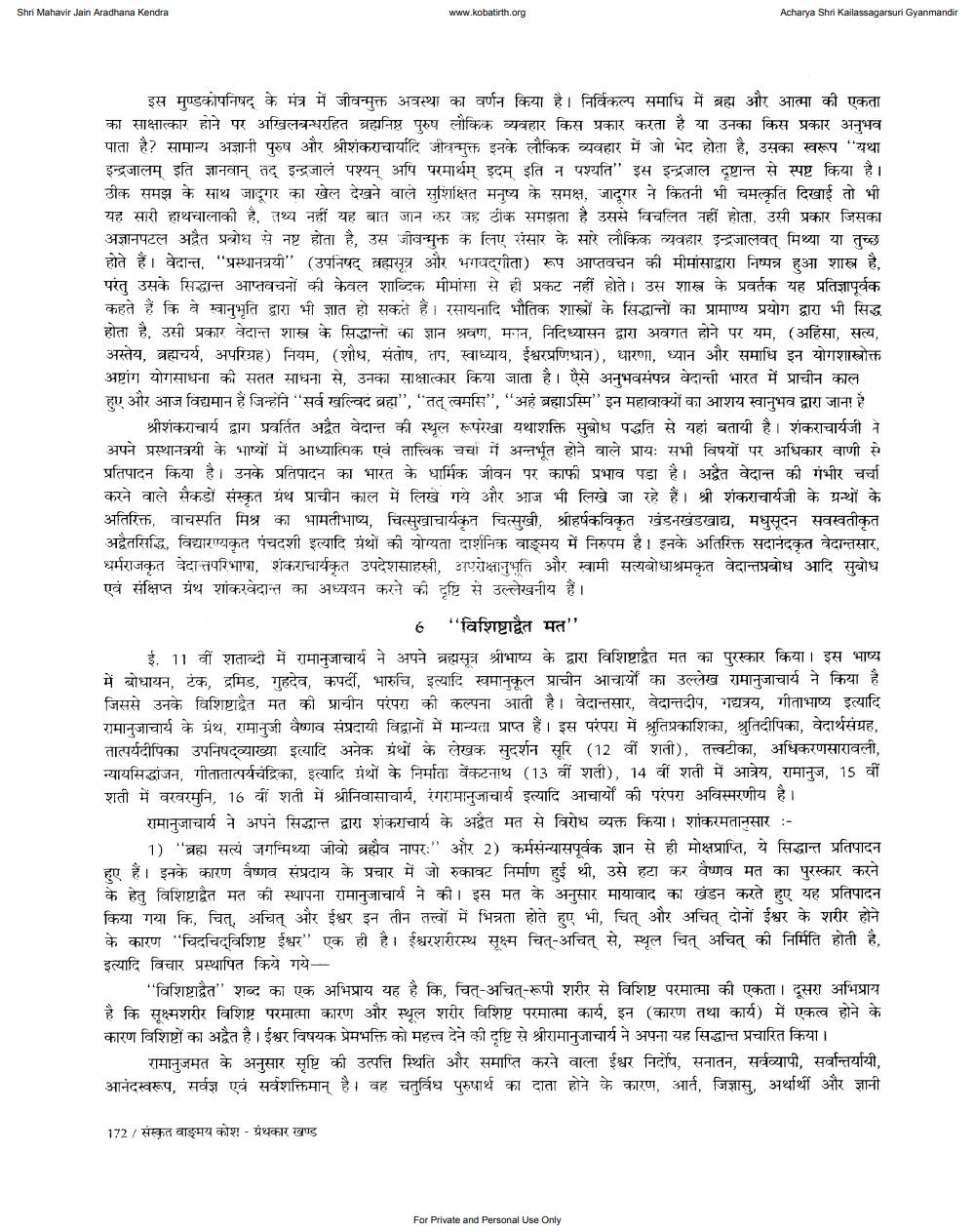________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
इस मुण्डकोपनिषद् के मंत्र में जीवन्मुक्त अवस्था का वर्णन किया है। निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार होने पर अखिलबन्धरहित ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लौकिक व्यवहार किस प्रकार करता है या उनका किस प्रकार अनुभव पाता है? सामान्य अज्ञानी पुरुष और श्रीशंकराचार्यादि जीवन्मुक्त इनके लौकिक व्यवहार में जो भेद होता है, उसका स्वरूप "यथा इन्द्रजालम् इति ज्ञानवान् तद् इन्द्रजालं पश्यन् अपि परमार्थम् इदम् इति न पश्यति" इस इन्द्रजाल दृष्टान्त से स्पष्ट किया है। ठीक समझ के साथ जादूगर का खेल देखने वाले सुशिक्षित मनुष्य के समक्ष, जादूगर ने कितनी भी चमत्कृति दिखाई तो भी यह सारी हाथचालाकी है, तथ्य नहीं यह बात जान कर वह ठीक समझता है उससे विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जिसका अज्ञानपटल अद्वैत प्रबोध से नष्ट होता है, उस जीवन्मुक्त के लिए संसार के सारे लौकिक व्यवहार इन्द्रजालवत् मिथ्या या तुच्छ होते हैं। वेदान्त, "प्रस्थानत्रयो" (उपनिषद् ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता) रूप आप्तवचन की मीमांसाद्वारा निष्पन्न हुआ शास्त्र है, परंतु उसके सिद्धान्त आप्तवचनों की केवल शाब्दिक मीमांसा से ही प्रकट नहीं होते। उस शास्त्र के प्रवर्तक यह प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि वे स्वानुभृति द्वारा भी ज्ञात हो सकते हैं। रसायनादि भौतिक शास्त्रों के सिद्धान्तों का प्रामाण्य प्रयोग द्वारा भी सिद्ध होता है, उसी प्रकार वेदान्त शास्त्र के सिद्धान्तों का ज्ञान श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा अवगत होने पर यम, (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) नियम, (शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान), धारणा, ध्यान और समाधि इन योगशास्त्रोक्त अष्टांग योगसाधना को सतत साधना से, उनका साक्षात्कार किया जाता है। ऐसे अनुभवसंपन्न वेदान्ती भारत में प्राचीन काल हुए और आज विद्यमान हैं जिन्होंने “सर्व खल्विद ब्रह्म", "तत् त्वमसि", "अहं ब्रह्माऽस्मि” इन महावाक्यों का आशय स्वानुभव द्वारा जाना हे
श्रीशंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैत वेदान्त की स्थूल रूपरेखा यथाशक्ति सुबोध पद्धति से यहां बतायी है। शंकराचार्यजी ने अपने प्रस्थानत्रयी के भाष्यों में आध्यात्मिक एवं तात्त्विक चर्चा में अन्तर्भूत होने वाले प्रायः सभी विषयों पर अधिकार वाणी से प्रतिपादन किया है। उनके प्रतिपादन का भारत के धार्मिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। अद्वैत वेदान्त की गंभीर चर्चा करने वाले सैकडों संस्कृत ग्रंथ प्राचीन काल में लिखे गये और आज भी लिखे जा रहे हैं। श्री शंकराचार्यजी के ग्रन्थों के अतिरिक्त, वाचस्पति मिश्र का भामतीभाष्य, चित्सुखाचार्यकृत चित्सुखी, श्रीहर्षकविकृत खंडनखंडखाद्य, मधुसूदन सवस्वतीकृत अद्वैतसिद्धि, विद्यारण्यकृत पंचदशी इत्यादि ग्रंथों की योग्यता दार्शनिक वाङ्मय में निरुपम है। इनके अतिरिक्त सदानंदकृत वेदान्तसार, धर्मराजकृत वेदान्तपरिभाषा, शंकराचार्यकृत उपदेशसाहस्री, अपरोक्षानुभूति और स्वामी सत्यबोधाश्रमकृत वेदान्तप्रबोध आदि सुबोध एवं संक्षिप्त ग्रंथ शांकरवेदान्त का अध्ययन करने की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।
6 "विशिष्टाद्वैत मत" ई. 11 वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्य के द्वारा विशिष्टाद्वैत मत का पुरस्कार किया। इस भाष्य में बोधायन, टंक, द्रमिड, गुहदेव, कपर्दी, भारुचि, इत्यादि स्वमानुकूल प्राचीन आचार्यों का उल्लेख रामानुजाचार्य ने किया है जिससे उनके विशिष्टाद्वैत मत की प्राचीन परंपरा की कल्पना आती है। वेदान्तसार, वेदान्तदीप, गद्यत्रय, गीताभाष्य इत्यादि रामानुजाचार्य के ग्रंथ, रामानुजी वैष्णव संप्रदायी विद्वानों में मान्यता प्राप्त हैं। इस परंपरा में श्रुतिप्रकाशिका, श्रुतिदीपिका, वेदार्थसंग्रह, तात्पर्यदीपिका उपनिषद्व्याख्या इत्यादि अनेक ग्रंथों के लेखक सुदर्शन सूरि (12 वीं शती), तत्त्वटीका, अधिकरणसारावली, न्यायसिद्धांजन, गीतातात्पर्यचंद्रिका, इत्यादि ग्रंथों के निर्माता वेंकटनाथ (13 वीं शती), 14 वीं शती में आत्रेय, रामानुज, 15 वीं शती में वरवरमुनि, 16 वीं शती में श्रीनिवासाचार्य, रंगरामानुजाचार्य इत्यादि आचार्यों की परंपरा अविस्मरणीय है। ___ रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धान्त द्वारा शंकराचार्य के अद्वैत मत से विरोध व्यक्त किया। शांकरमतानुसार :
1) "ब्रह्म सत्यं जगनिमथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः" और 2) कर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञान से ही मोक्षप्राप्ति, ये सिद्धान्त प्रतिपादन हुए हैं। इनके कारण वैष्णव संप्रदाय के प्रचार में जो रुकावट निर्माण हुई थी, उसे हटा कर वैष्णव मत का पुरस्कार करने
के हेतु विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना रामानुजाचार्य ने की। इस मत के अनुसार मायावाद का खंडन करते हुए यह प्रतिपादन किया गया कि, चित्, अचित् और ईश्वर इन तीन तत्त्वों में भिन्नता होते हुए भी, चित् और अचित् दोनों ईश्वर के शरीर होने के कारण "चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर" एक ही है। ईश्वरशरीरस्थ सूक्ष्म चित्-अचित् से, स्थूल चित् अचित् की निर्मिति होती है, इत्यादि विचार प्रस्थापित किये गये
"विशिष्टाद्वैत' शब्द का एक अभिप्राय यह है कि, चित्-अचित्-रूपी शरीर से विशिष्ट परमात्मा की एकता। दूसरा अभिप्राय है कि सूक्ष्मशरीर विशिष्ट परमात्मा कारण और स्थूल शरीर विशिष्ट परमात्मा कार्य, इन (कारण तथा कार्य) में एकत्व होने के कारण विशिष्टों का अद्वैत है। ईश्वर विषयक प्रेमभक्ति को महत्त्व देने की दृष्टि से श्रीरामानुजाचार्य ने अपना यह सिद्धान्त प्रचारित किया।
रामानुजमत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और समाप्ति करने वाला ईश्वर निर्दोष, सनातन, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यायी, आनंदस्वरूप, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् है। वह चतुर्विध पुरुषार्थ का दाता होने के कारण, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी
172 / संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only