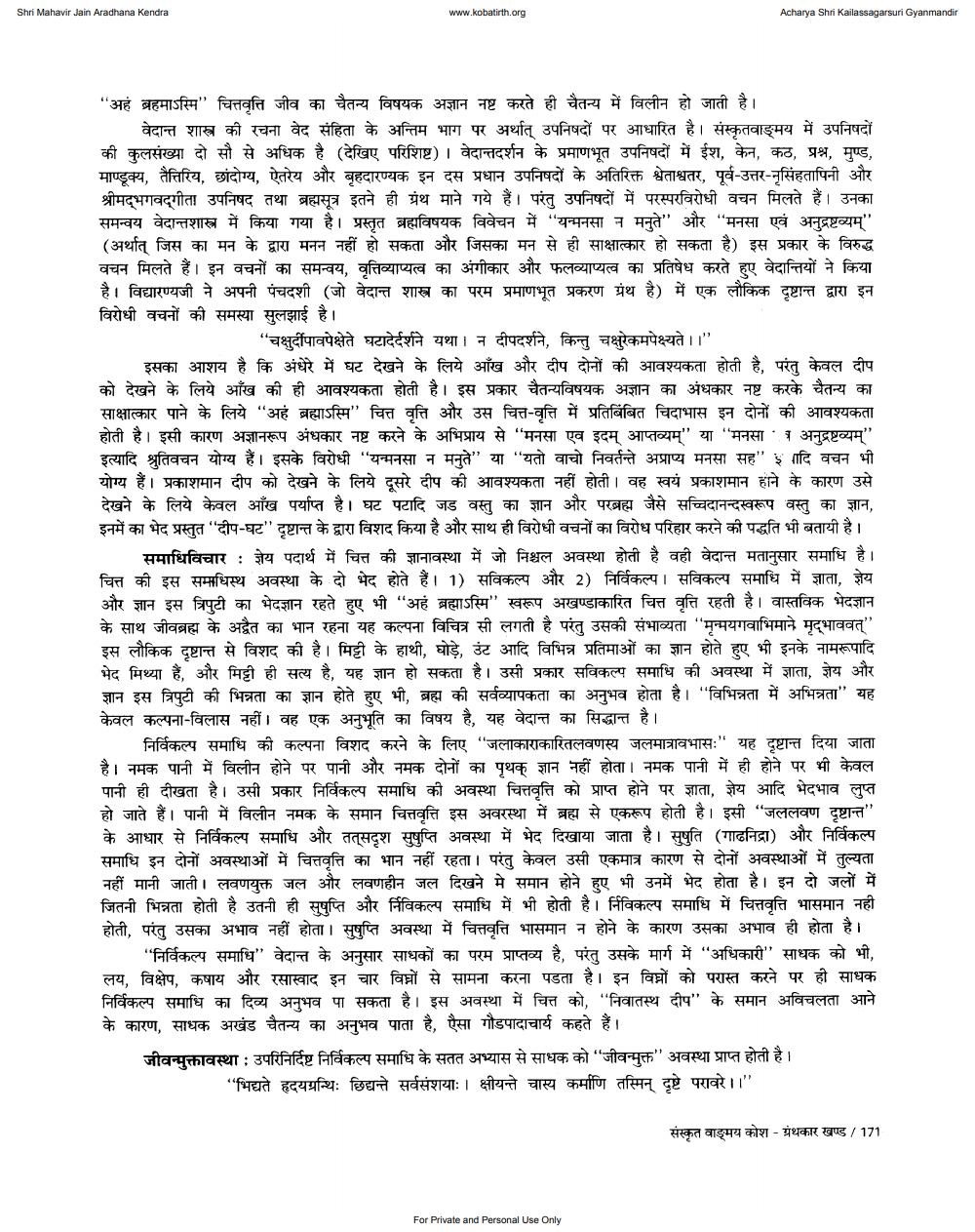________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
"अहं ब्रहमाऽस्मि' चित्तवृत्ति जीव का चैतन्य विषयक अज्ञान नष्ट करते ही चैतन्य में विलीन हो जाती है।
वेदान्त शास्त्र की रचना वेद संहिता के अन्तिम भाग पर अर्थात् उपनिषदों पर आधारित है। संस्कृतवाङ्मय में उपनिषदों की कुलसंख्या दो सौ से अधिक है (देखिए परिशिष्ट)। वेदान्तदर्शन के प्रमाणभूत उपनिषदों में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरिय, छांदोग्य, ऐतरेय और बृहदारण्यक इन दस प्रधान उपनिषदों के अतिरिक्त श्वेताश्वतर, पूर्व-उत्तर-नृसिंहतापिनी और श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद तथा ब्रह्मसूत्र इतने ही ग्रंथ माने गये हैं। परंतु उपनिषदों में परस्परविरोधी वचन मिलते हैं। उनका समन्वय वेदान्तशास्त्र में किया गया है। प्रस्तृत ब्रह्मविषयक विवेचन में "यन्मनसा न मनुते" और "मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम्" (अर्थात् जिस का मन के द्वारा मनन नहीं हो सकता और जिसका मन से ही साक्षात्कार हो सकता है) इस प्रकार के विरुद्ध वचन मिलते हैं। इन वचनों का समन्वय, वृत्तिव्याप्यत्व का अंगीकार और फलव्याप्यत्व का प्रतिषेध करते हुए वेदान्तियों ने किया है। विद्यारण्यजी ने अपनी पंचदशी (जो वेदान्त शास्त्र का परम प्रमाणभूत प्रकरण ग्रंथ है) में एक लौकिक दृष्टान्त द्वारा इन विरोधी वचनों की समस्या सुलझाई है।
"चक्षुर्दीपावपेक्षेते घटादेर्दर्शने यथा। न दीपदर्शने, किन्तु चक्षुरेकमपेक्ष्यते।।" इसका आशय है कि अंधेरे में घट देखने के लिये आँख और दीप दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु केवल दीप को देखने के लिये आँख की ही आवश्यकता होती है। इस प्रकार चैतन्यविषयक अज्ञान का अंधकार नष्ट करके चैतन्य का साक्षात्कार पाने के लिये “अहं ब्रह्माऽस्मि" चित्त वृत्ति और उस चित्त-वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास इन दोनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण अज्ञानरूप अंधकार नष्ट करने के अभिप्राय से “मनसा एव इदम् आप्तव्यम्" या "मनसा · व अनुद्रष्टव्यम्" इत्यादि श्रुतिवचन योग्य हैं। इसके विरोधी “यन्मनसा न मनुते" या "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" ६ गादि वचन भी योग्य हैं। प्रकाशमान दीप को देखने के लिये दूसरे दीप की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं प्रकाशमान हाने के कारण उसे देखने के लिये केवल आँख पर्याप्त है। घट पटादि जड वस्तु का ज्ञान और परब्रह्म जैसे सच्चिदानन्दस्वरूप वस्तु का ज्ञान, इनमें का भेद प्रस्तुत "दीप-घट" दृष्टान्त के द्वारा विशद किया है और साथ ही विरोधी वचनों का विरोध परिहार करने की पद्धति भी बतायी है।
समाधिविचार : ज्ञेय पदार्थ में चित्त की ज्ञानावस्था में जो निश्चल अवस्था होती है वही वेदान्त मतानुसार समाधि है। चित्त की इस समाधिस्थ अवस्था के दो भेद होते हैं। 1) सविकल्प और 2) निर्विकल्प। सविकल्प समाधि में ज्ञाता, ज्ञेय
और ज्ञान इस त्रिपुटी का भेदज्ञान रहते हुए भी "अहं ब्रह्माऽस्मि" स्वरूप अखण्डाकारित चित्त वृत्ति रहती है। वास्तविक भेदज्ञान के साथ जीवब्रह्म के अद्वैत का भान रहना यह कल्पना विचित्र सी लगती है परंतु उसकी संभाव्यता "मृन्मयगवाभिमाने मृद्भाववत्" इस लौकिक दृष्टान्त से विशद की है। मिट्टी के हाथी, घोड़े, उंट आदि विभिन्न प्रतिमाओं का ज्ञान होते हुए भी इनके नामरूपादि भेद मिथ्या हैं, और मिट्टी ही सत्य है, यह ज्ञान हो सकता है। उसी प्रकार सविकल्प समाधि की अवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इस त्रिपुटी की भिन्नता का ज्ञान होते हुए भी, ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है। "विभिन्नता में अभिन्नता" यह केवल कल्पना-विलास नहीं। वह एक अनुभूति का विषय है, यह वेदान्त का सिद्धान्त है।
निर्विकल्प समाधि की कल्पना विशद करने के लिए "जलाकाराकारितलवणस्य जलमात्रावभासः" यह दृष्टान्त दिया जाता है। नमक पानी में विलीन होने पर पानी और नमक दोनों का पृथक् ज्ञान नहीं होता। नमक पानी में ही होने पर भी केवल पानी ही दीखता है। उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि की अवस्था चित्तवृत्ति को प्राप्त होने पर ज्ञाता, ज्ञेय आदि भेदभाव लुप्त हो जाते हैं। पानी में विलीन नमक के समान चित्तवृत्ति इस अवरस्था में ब्रह्म से एकरूप होती है। इसी “जललवण दृष्टान्त" के आधार से निर्विकल्प समाधि और तत्सदृश सुषुप्ति अवस्था में भेद दिखाया जाता है। सुषुति (गाढनिद्रा) और निर्विकल्प समाधि इन दोनों अवस्थाओं में चित्तवृत्ति का भान नहीं रहता। परंतु केवल उसी एकमात्र कारण से दोनों अवस्थाओं में तुल्यता नहीं मानी जाती। लवणयुक्त जल और लवणहीन जल दिखने मे समान होने हुए भी उनमें भेद होता है। इन दो जलों में जितनी भिन्नता होती है उतनी ही सुषुप्ति और निविकल्प समाधि में भी होती है। निविकल्प समाधि में चित्तवृत्ति भासमान नही होती, परंतु उसका अभाव नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में चित्तवृत्ति भासमान न होने के कारण उसका अभाव ही होता है।
"निर्विकल्प समाधि" वेदान्त के अनुसार साधकों का परम प्राप्तव्य है, परंतु उसके मार्ग में "अधिकारी" साधक को भी, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद इन चार विघ्नों से सामना करना पडता है। इन विघ्नों को परास्त करने पर ही साधक निर्विकल्प समाधि का दिव्य अनुभव पा सकता है। इस अवस्था में चित्त को, “निवातस्थ दीप" के समान अविचलता आने के कारण, साधक अखंड चैतन्य का अनुभव पाता है, ऐसा गौडपादाचार्य कहते हैं। जीवन्मुक्तावस्था : उपरिनिर्दिष्ट निर्विकल्प समाधि के सतत अभ्यास से साधक को "जीवन्मुक्त" अवस्था प्राप्त होती है।
"भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।।"
संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड / 171
For Private and Personal Use Only