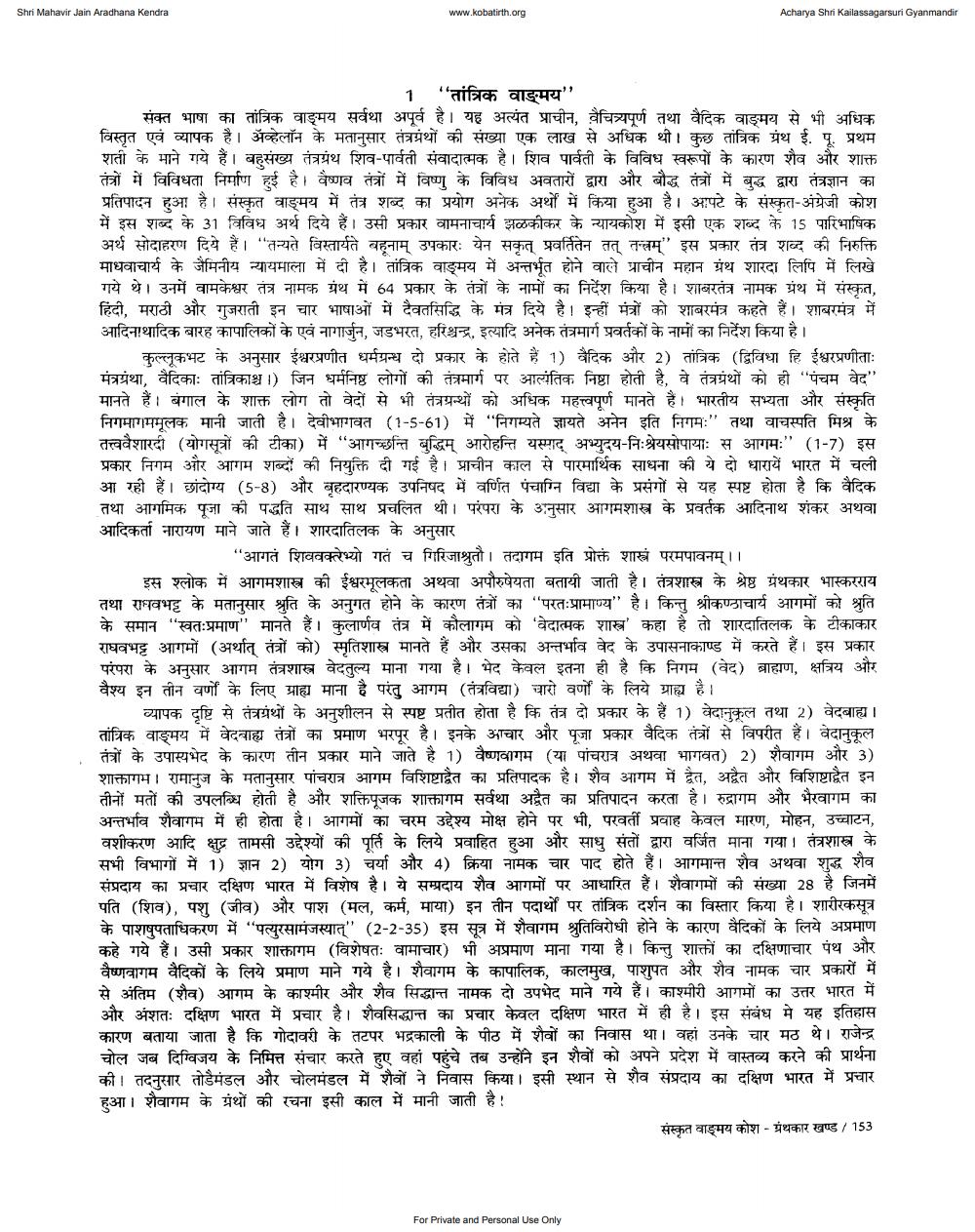________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
ग्रन्था को अधिक महत्त्वपूर्ण
माथी को ही "पंचम वेद"
M
लक मानी जाती है। देवीभागवत
1 "तांत्रिक वाङ्मय" संक्त भाषा का तांत्रिक वाङ्मय सर्वथा अपूर्व है। यह अत्यंत प्राचीन, वैचित्र्यपूर्ण तथा वैदिक वाङ्मय से भी अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। अॅव्हेलॉन के मतानुसार तंत्रग्रंथों की संख्या एक लाख से अधिक थी। कुछ तांत्रिक ग्रंथ ई. पू. प्रथम शती के माने गये हैं। बहुसंख्य तंत्रग्रंथ शिव-पार्वती संवादात्मक है। शिव पार्वती के विविध स्वरूपों के कारण शैव और शाक्त तंत्रों में विविधता निर्माण हुई है। वैष्णव तंत्रों में विष्णु के विविध अवतारों द्वारा और बौद्ध तंत्रों में बुद्ध द्वारा तंत्रज्ञान का प्रतिपादन हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में तंत्र शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया हुआ है। आपटे के संस्कृत-अंग्रेजी कोश में इस शब्द के 31 विविध अर्थ दिये हैं। उसी प्रकार वामनाचार्य झळकीकर के न्यायकोश में इसी एक शब्द के 15 पारिभाषिक अर्थ सोदाहरण दिये हैं। "तन्यते विस्तार्यते बहूनाम् उपकारः येन सकृत् प्रवर्तितेन तत् तन्त्रम्' इस प्रकार तंत्र शब्द की निरुक्ति माधवाचार्य के जैमिनीय न्यायमाला में दी है। तांत्रिक वाङ्मय में अन्तर्भूत होने वाले प्राचीन महान ग्रंथ शारदा लिपि में लिखे गये थे। उनमें वामकेश्वर तंत्र नामक ग्रंथ में 64 प्रकार के तंत्रों के नामों का निर्देश किया है। शाबरतंत्र नामक ग्रंथ में संस्कृत, हिंदी, मराठी और गुजराती इन चार भाषाओं में दैवतसिद्धि के मंत्र दिये है। इन्हीं मंत्रों को शाबरमंत्र कहते हैं। शाबरमंत्र में आदिनाथादिक बारह कापालिकों के एवं नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चन्द्र, इत्यादि अनेक तंत्रमार्ग प्रवर्तकों के नामों का निर्देश किया है।
कुल्लूकभट के अनुसार ईश्वरप्रणीत धर्मग्रन्ध दो प्रकार के होते हैं 1) वैदिक और 2) तांत्रिक (द्विविधा हि ईश्वरप्रणीताः मंत्रग्रंथा, वैदिकाः तांत्रिकाश्च ।) जिन धर्मनिष्ठ लोगों की तंत्रमार्ग पर आत्यंतिक निष्ठा होती है, वे तंत्रग्रंथों को ही "पंचम वेद" मानते हैं। बंगाल के शाक्त लोग तो वेदों से भी तंत्रग्रन्थों को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति निगमागममूलक मानी जाती है। देवीभागवत (1-5-61) में “निगम्यते ज्ञायते अनेन इति निगमः" तथा वाचस्पति मिश्र के तत्त्ववैशारदी (योगसूत्रों की टीका) में “आगच्छन्ति बुद्धिम् आरोहन्ति यस्माद् अभ्युदय-निःश्रेयसोपायाः स आगमः" (1-7) इस प्रकार निगम और आगम शब्दों की नियुक्ति दी गई है। प्राचीन काल से पारमार्थिक साधना की ये दो धारायें भारत में चली आ रही हैं। छांदोग्य (5-8) और बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित पंचाग्नि विद्या के प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक तथा आगमिक पूजा की पद्धति साथ साथ प्रचलित थी। परंपरा के अनुसार आगमशास्त्र के प्रवर्तक आदिनाथ शंकर अथवा आदिकर्ता नारायण माने जाते हैं। शारदातिलक के अनुसार
"आगतं शिववक्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतौ। तदागम इति प्रोक्तं शास्त्रं परमपावनम् ।। इस श्लोक में आगमशास्त्र की ईश्वरमूलकता अथवा अपौरुषेयता बतायी जाती है। तंत्रशास्त्र के श्रेष्ठ ग्रंथकार भास्करराय तथा राघवभट्ट के मतानुसार श्रुति के अनुगत होने के कारण तंत्रों का "परतःप्रामाण्य" है। किन्तु श्रीकण्ठाचार्य आगमों को श्रुति के समान "स्वतःप्रमाण' मानते हैं। कुलार्णव तंत्र में कौलागम को 'वेदात्मक शास्त्र' कहा है तो शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट आगमों (अर्थात् तंत्रों को) स्मृतिशास्त्र मानते हैं और उसका अन्तर्भाव वेद के उपासनाकाण्ड में करते हैं। इस प्रकार परंपरा के अनुसार आगम तंत्रशास्त्र वेदतुल्य माना गया है। भेद केवल इतना ही है कि निगम (वेद) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्गों के लिए ग्राह्य माना है परंतु आगम (तंत्रविद्या) चारो वर्णों के लिये ग्राह्य है।
व्यापक दृष्टि से तंत्रग्रंथों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तंत्र दो प्रकार के हैं 1) वेदानुकूल तथा 2) वेदबाह्य । तांत्रिक वाङ्मय में वेदत्वाह्य तंत्रों का प्रमाण भरपूर है। इनके आचार और पूजा प्रकार वैदिक तंत्रों से विपरीत हैं। वेदानुकूल तंत्रों के उपास्यभेद के कारण तीन प्रकार माने जाते है 1) वैष्णवागम (या पांचरात्र अथवा भागवत) 2) शैवागम और 3) शाक्तागम। रामानुज के मतानुसार पांचरात्र आगम विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादक है। शैव आगम में द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत इन तीनों मतों की उपलब्धि होती है और शक्तिपूजक शाक्तागम सर्वथा अद्वैत का प्रतिपादन करता है। रुद्रागम और भैरवागम का अन्तर्भाव शैवागम में ही होता है। आगमों का चरम उद्देश्य मोक्ष होने पर भी, परवर्ती प्रवाह केवल मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि क्षुद्र तामसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रवाहित हुआ और साधु संतों द्वारा वर्जित माना गया। तंत्रशास्त्र के सभी विभागों में 1) ज्ञान 2) योग 3) चर्या और 4) क्रिया नामक चार पाद होते हैं। आगमान्त शैव अथवा शुद्ध शैव संप्रदाय का प्रचार दक्षिण भारत में विशेष है। ये सम्प्रदाय शैव आगमों पर आधारित हैं। शैवागमों की संख्या 28 है जिनमें पति (शिव), पशु (जीव) और पाश (मल, कर्म, माया) इन तीन पदार्थों पर तांत्रिक दर्शन का विस्तार किया है। शारीरकसूत्र के पाशषुपताधिकरण में “पत्युरसामंजस्यात्' (2-2-35) इस सूत्र में शैवागम श्रुतिविरोधी होने के कारण वैदिकों के लिये अप्रमाण कहे गये हैं। उसी प्रकार शाक्तागम (विशेषतः वामाचार) भी अप्रमाण माना गया है। किन्तु शाक्तों का दक्षिणाचार पंथ और वैष्णवागम वैदिकों के लिये प्रमाण माने गये है। शैवागम के कापालिक, कालमुख, पाशुपत और शैव नामक चार प्रकारों में से अंतिम (शैव) आगम के काश्मीर और शैव सिद्धान्त नामक दो उपभेद माने गये हैं। काश्मीरी आगमों का उत्तर भारत में
और अंशतः दक्षिण भारत में प्रचार है। शैवसिद्धान्त का प्रचार केवल दक्षिण भारत में ही है। इस संबंध मे यह इतिहास कारण बताया जाता है कि गोदावरी के तटपर भद्रकाली के पीठ में शैवों का निवास था। वहां उनके चार मठ थे। राजेन्द्र चोल जब दिग्विजय के निमित्त संचार करते हुए वहां पहुंचे तब उन्होंने इन शैवों को अपने प्रदेश में वास्तव्य करने की प्रार्थना की। तदनुसार तोडैमंडल और चोलमंडल में शैवों ने निवास किया। इसी स्थान से शैव संप्रदाय का दक्षिण भारत में प्रचार हुआ। शैवागम के ग्रंथों की रचना इसी काल में मानी जाती है।
संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड / 153
For Private and Personal Use Only