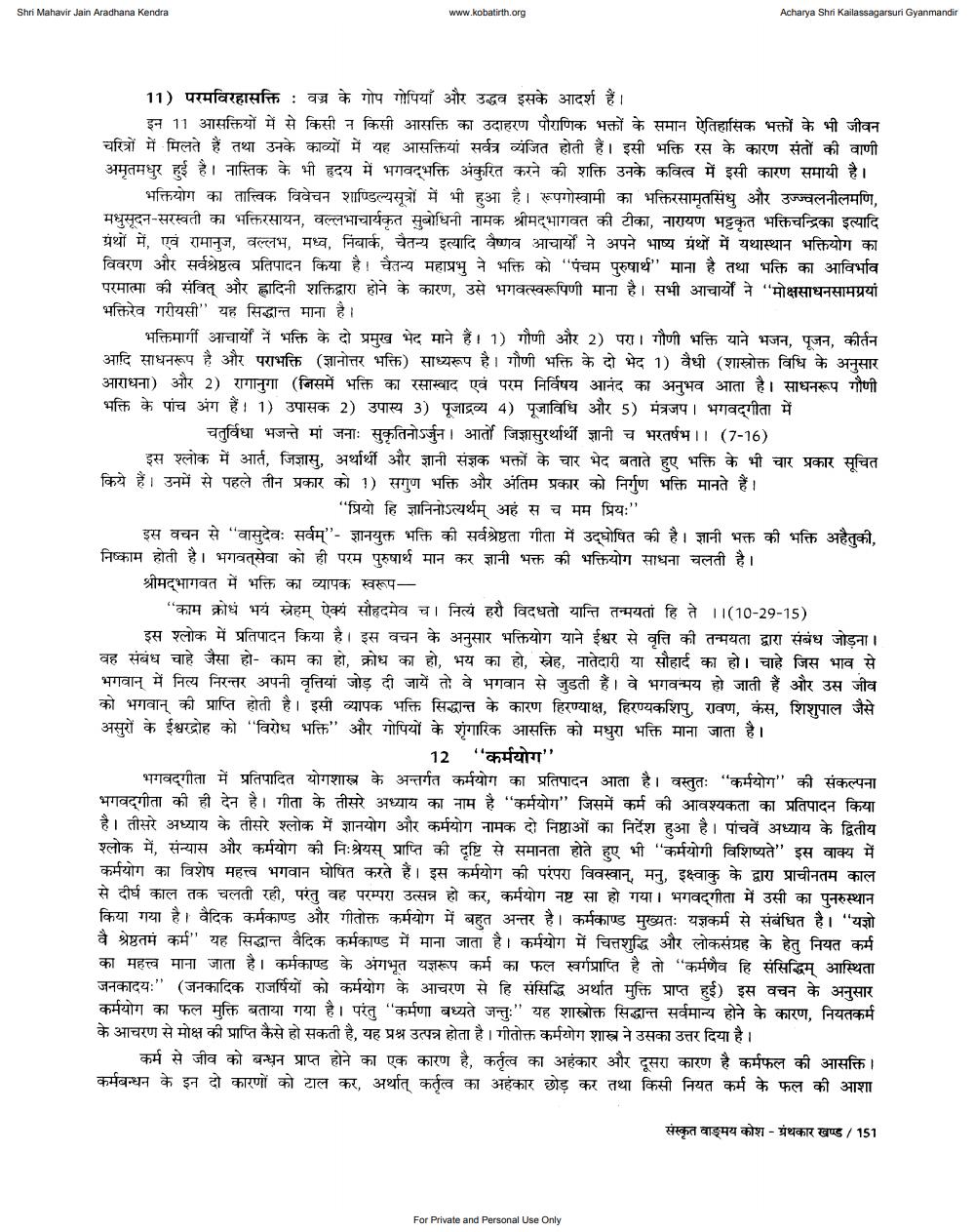________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
11) परमविरहासक्ति : वज्र के गोप गोपियाँ और उद्धव इसके आदर्श हैं।
इन 11 आसक्तियों में से किसी न किसी आसक्ति का उदाहरण पौराणिक भक्तों के समान ऐतिहासिक भक्तों के भी जीवन चरित्रों में मिलते हैं तथा उनके काव्यों में यह आसक्तियां सर्वत्र व्यंजित होती हैं। इसी भक्ति रस के कारण संतों की वाणी अमृतमधुर हुई है। नास्तिक के भी हृदय में भगवद्भक्ति अंकुरित करने की शक्ति उनके कवित्व में इसी कारण समायी है।
भक्तियोग का तात्त्विक विवेचन शाण्डिल्यसूत्रों में भी हुआ है। रूपगोस्वामी का भक्तिरसामृतसिंधु और उज्ज्वलनीलमणि, मधुसूदन-सरस्वती का भक्तिरसायन, वल्लभाचार्यकृत सुबोधिनी नामक श्रीमद्भागवत की टीका, नारायण भट्टकृत भक्तिचन्द्रिका इत्यादि ग्रंथों में, एवं रामानुज, वल्लभ, मध्व, निंबार्क, चैतन्य इत्यादि वैष्णव आचार्यों ने अपने भाष्य ग्रंथों में यथास्थान भक्तियोग का विवरण और सर्वश्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को "पंचम पुरुषार्थ' माना है तथा भक्ति का आविर्भाव परमात्मा की संवित् और ह्लादिनी शक्तिद्वारा होने के कारण, उसे भगवत्स्वरूपिणी माना है। सभी आचार्यों ने "मोक्षसाधनसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी" यह सिद्धान्त माना है।
भक्तिमार्गी आचार्यों में भक्ति के दो प्रमुख भेद माने हैं। 1) गौणी और 2) परा। गौणी भक्ति याने भजन, पूजन, कीर्तन आदि साधनरूप है और पराभक्ति (ज्ञानोत्तर भक्ति) साध्यरूप है। गौणी भक्ति के दो भेद 1) वैधी (शास्रोक्त विधि के अनुसार आराधना) और 2) रागानुगा (जिसमें भक्ति का रसास्वाद एवं परम निर्विषय आनंद का अनुभव आता है। साधनरूप गौणी भक्ति के पांच अंग हैं। 1) उपासक 2) उपास्य 3) पूजाद्रव्य 4) पूजाविधि और 5) मंत्रजप। भगवद्गीता में
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।। (7-16) इस श्लोक में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी संज्ञक भक्तों के चार भेद बताते हुए भक्ति के भी चार प्रकार सूचित किये हैं। उनमें से पहले तीन प्रकार को 1) सगुण भक्ति और अंतिम प्रकार को निर्गुण भक्ति मानते हैं।
"प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः" इस वचन से "वासुदेवः सर्वम्”- ज्ञानयुक्त भक्ति की सर्वश्रेष्ठता गीता में उद्घोषित की है। ज्ञानी भक्त की भक्ति अहैतुकी, निष्काम होती है। भगवत्सेवा को ही परम पुरुषार्थ मान कर ज्ञानी भक्त की भक्तियोग साधना चलती है।
श्रीमद्भागवत में भक्ति का व्यापक स्वरूप___ "काम क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहदमेव च। नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ।।(10-29-15)
इस श्लोक में प्रतिपादन किया है। इस वचन के अनुसार भक्तियोग याने ईश्वर से वृत्ति की तन्मयता द्वारा संबंध जोड़ना। वह संबंध चाहे जैसा हो- काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह, नातेदारी या सौहार्द का हो। चाहे जिस भाव से भगवान् में नित्य निरन्तर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जायें तो वे भगवान से जुडती हैं। वे भगवन्मय हो जाती हैं और उस जीव को भगवान् की प्राप्ति होती है। इसी व्यापक भक्ति सिद्धान्त के कारण हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, शिशुपाल जैसे असुरों के ईश्वरद्रोह को “विरोध भक्ति" और गोपियों के शृंगारिक आसक्ति को मधुरा भक्ति माना जाता है।
12 "कर्मयोग" भगवद्गीता में प्रतिपादित योगशास्त्र के अन्तर्गत कर्मयोग का प्रतिपादन आता है। वस्तुतः "कर्मयोग" की संकल्पना भगवद्गीता की ही देन है। गीता के तीसरे अध्याय का नाम है “कर्मयोग" जिसमें कर्म की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ज्ञानयोग और कर्मयोग नामक दो निष्ठाओं का निर्देश हुआ है। पांचवें अध्याय के द्वितीय श्लोक में, संन्यास और कर्मयोग की निःश्रेयस् प्राप्ति की दृष्टि से समानता होते हुए भी "कर्मयोगी विशिष्यते" इस वाक्य में कर्मयोग का विशेष महत्त्व भगवान घोषित करते हैं। इस कर्मयोग की परंपरा विवस्वान्, मनु, इक्ष्वाकु के द्वारा प्राचीनतम काल से दीर्घ काल तक चलती रही, परंतु वह परम्परा उत्पन्न हो कर, कर्मयोग नष्ट सा हो गया। भगवद्गीता में उसी का पुनरुस्थान किया गया है। वैदिक कर्मकाण्ड और गीतोक्त कर्मयोग में बहुत अन्तर है। कर्मकाण्ड मुख्यतः यज्ञकर्म से संबंधित है। "यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म" यह सिद्धान्त वैदिक कर्मकाण्ड में माना जाता है। कर्मयोग में चित्तशुद्धि और लोकसंग्रह के हेतु नियत कर्म का महत्त्व माना जाता है। कर्मकाण्ड के अंगभूत यज्ञरूप कर्म का फल स्वर्गप्राप्ति है तो "कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः" (जनकादिक राजर्षियों को कर्मयोग के आचरण से हि संसिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त हुई) इस वचन के अनुसार कर्मयोग का फल मुक्ति बताया गया है। परंतु "कर्मणा बध्यते जन्तुः" यह शास्त्रोक्त सिद्धान्त सर्वमान्य होने के कारण, नियतकर्म के आचरण से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह प्रश्न उत्पन्न होता है । गीतोक्त कर्मयोग शास्त्र ने उसका उत्तर दिया है।
__ कर्म से जीव को बन्धन प्राप्त होने का एक कारण है, कर्तृत्व का अहंकार और दूसरा कारण है कर्मफल की आसक्ति। कर्मबन्धन के इन दो कारणों को टाल कर, अर्थात् कर्तत्व का अहंकार छोड़ कर तथा किसी नियत कर्म के फल की आशा
संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड / 151
For Private and Personal Use Only