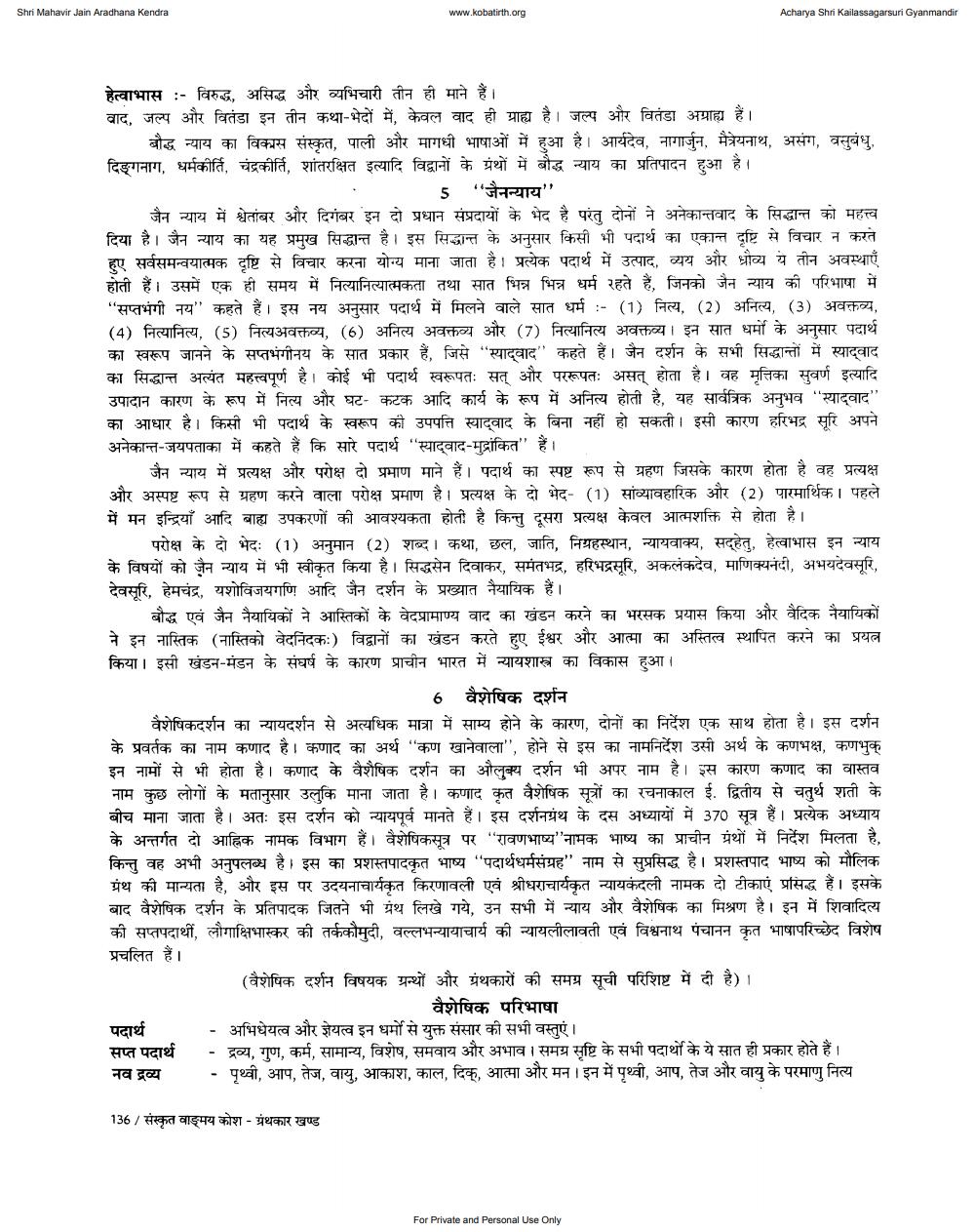________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
हेत्वाभास :- विरुद्ध, असिद्ध और व्यभिचारी तीन ही माने हैं। वाद, जल्प और वितंडा इन तीन कथा-भेदों में, केवल वाद ही ग्राह्य है। जल्प और वितंडा अग्राह्य हैं।
बौद्ध न्याय का विकास संस्कृत, पाली और मागधी भाषाओं में हुआ है। आर्यदेव, नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, असंग, वसुबंधु, दिङ्गनाग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, शांतरक्षित इत्यादि विद्वानों के ग्रंथों में बौद्ध न्याय का प्रतिपादन हुआ है।
5 "जैनन्याय" । जैन न्याय में श्वेतांबर और दिगंबर इन दो प्रधान संप्रदायों के भेद है परंतु दोनों ने अनेकान्तवाद के सिद्धान्त को महत्त्व दिया है। जैन न्याय का यह प्रमुख सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी पदार्थ का एकान्त दृष्टि से विचार न करते हुए सर्वसमन्वयात्मक दृष्टि से विचार करना योग्य माना जाता है। प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। उसमें एक ही समय में नित्यानित्यात्मकता तथा सात भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, जिनको जैन न्याय की परिभाषा में "सप्तभंगी नय" कहते हैं। इस नय अनुसार पदार्थ में मिलने वाले सात धर्म :- (1) नित्य, (2) अनित्य, (3) अवक्तव्य, (4) नित्यानित्य, (5) नित्यअवक्तव्य, (6) अनित्य अवक्तव्य और (7) नित्यानित्य अवक्तव्य। इन सात धर्मों के अनुसार पदार्थ का स्वरूप जानने के सप्तभंगीनय के सात प्रकार हैं, जिसे "स्याद्वाद" कहते हैं। जैन दर्शन के सभी सिद्धान्तों में स्याद्वाद का सिद्धान्त अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कोई भी पदार्थ स्वरूपतः सत् और पररूपतः असत् होता है। वह मृत्तिका सुवर्ण इत्यादि उपादान कारण के रूप में नित्य और घट- कटक आदि कार्य के रूप में अनित्य होती है, यह सार्वत्रिक अनुभव "स्याद्वाद" का आधार है। किसी भी पदार्थ के स्वरूप को उपपत्ति स्याद्वाद के बिना नहीं हो सकती। इसी कारण हरिभद्र सूरि अपने अनेकान्त-जयपताका में कहते हैं कि सारे पदार्थ "स्याद्वाद-मुद्रांकित" हैं।
जैन न्याय में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाण माने हैं। पदार्थ का स्पष्ट रूप से ग्रहण जिसके कारण होता है वह प्रत्यक्ष और अस्पष्ट रूप से ग्रहण करने वाला परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष के दो भेद- (1) सांव्यावहारिक और (2) पारमार्थिक। पहले में मन इन्द्रियाँ आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता होती है किन्तु दूसरा प्रत्यक्ष केवल आत्मशक्ति से होता है।
परोक्ष के दो भेदः (1) अनुमान (2) शब्द। कथा, छल, जाति, निग्रहस्थान, न्यायवाक्य, सद्हेतु, हेत्वाभास इन न्याय के विषयों को जैन न्याय में भी स्वीकृत किया है। सिद्धसेन दिवाकर, समंतभद्र, हरिभद्रसूरि, अकलंकदेव, माणिक्यनंदी, अभयदेवसूरि, देवसूरि, हेमचंद्र, यशोविजयगणि आदि जैन दर्शन के प्रख्यात नैयायिक हैं।
बौद्ध एवं जैन नैयायिकों ने आस्तिकों के वेदप्रामाण्य वाद का खंडन करने का भरसक प्रयास किया और वैदिक नैयायिकों ने इन नास्तिक (नास्तिको वेदनिंदकः) विद्वानों का खंडन करते हुए ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी खंडन-मंडन के संघर्ष के कारण प्राचीन भारत में न्यायशास्त्र का विकास हुआ।
6 वैशेषिक दर्शन वैशेषिकदर्शन का न्यायदर्शन से अत्यधिक मात्रा में साम्य होने के कारण, दोनों का निर्देश एक साथ होता है। इस दर्शन के प्रवर्तक का नाम कणाद है। कणाद का अर्थ "कण खानेवाला", होने से इस का नामनिर्देश उसी अर्थ के कणभक्ष, कणभुक् इन नामों से भी होता है। कणाद के वैशेषिक दर्शन का औलुक्य दर्शन भी अपर नाम है। इस कारण कणाद का वास्तव नाम कुछ लोगों के मतानुसार उलुकि माना जाता है। कणाद कृत वैशेषिक सूत्रों का रचनाकाल ई. द्वितीय से चतुर्थ शती के बीच माना जाता है। अतः इस दर्शन को न्यायपूर्व मानते हैं। इस दर्शनग्रंथ के दस अध्यायों में 370 सूत्र हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्तर्गत दो आह्निक नामक विभाग हैं। वैशेषिकसूत्र पर "रावणभाष्य"नामक भाष्य का प्राचीन ग्रंथों में निर्देश मिलता है, किन्तु वह अभी अनुपलब्ध है। इस का प्रशस्तपादकृत भाष्य “पदार्थधर्मसंग्रह" नाम से सुप्रसिद्ध है। प्रशस्तपाद भाष्य को मौलिक ग्रंथ की मान्यता है, और इस पर उदयनाचार्यकृत किरणावली एवं श्रीधराचार्यकृत न्यायकंदली नामक दो टीकाएं प्रसिद्ध हैं। इसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जितने भी ग्रंथ लिखे गये, उन सभी में न्याय और वैशेषिक का मिश्रण है। इन में शिवादित्य की सप्तपदाथीं, लौगाक्षिभास्कर की तर्ककौमुदी, वल्लभन्यायाचार्य की न्यायलीलावती एवं विश्वनाथ पंचानन कृत भाषापरिच्छेद विशेष प्रचलित हैं। (वैशेषिक दर्शन विषयक ग्रन्थों और ग्रंथकारों की समग्र सूची परिशिष्ट में दी है)।
वैशेषिक परिभाषा - अभिधेयत्व और ज्ञेयत्व इन धर्मों से युक्त संसार की सभी वस्तुएं। सप्त पदार्थ - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव । समग्र सृष्टि के सभी पदार्थो के ये सात ही प्रकार होते हैं। नव द्रव्य - पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन । इन में पृथ्वी, आप, तेज और वायु के परमाणु नित्य
पदार्थ
136/ संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only