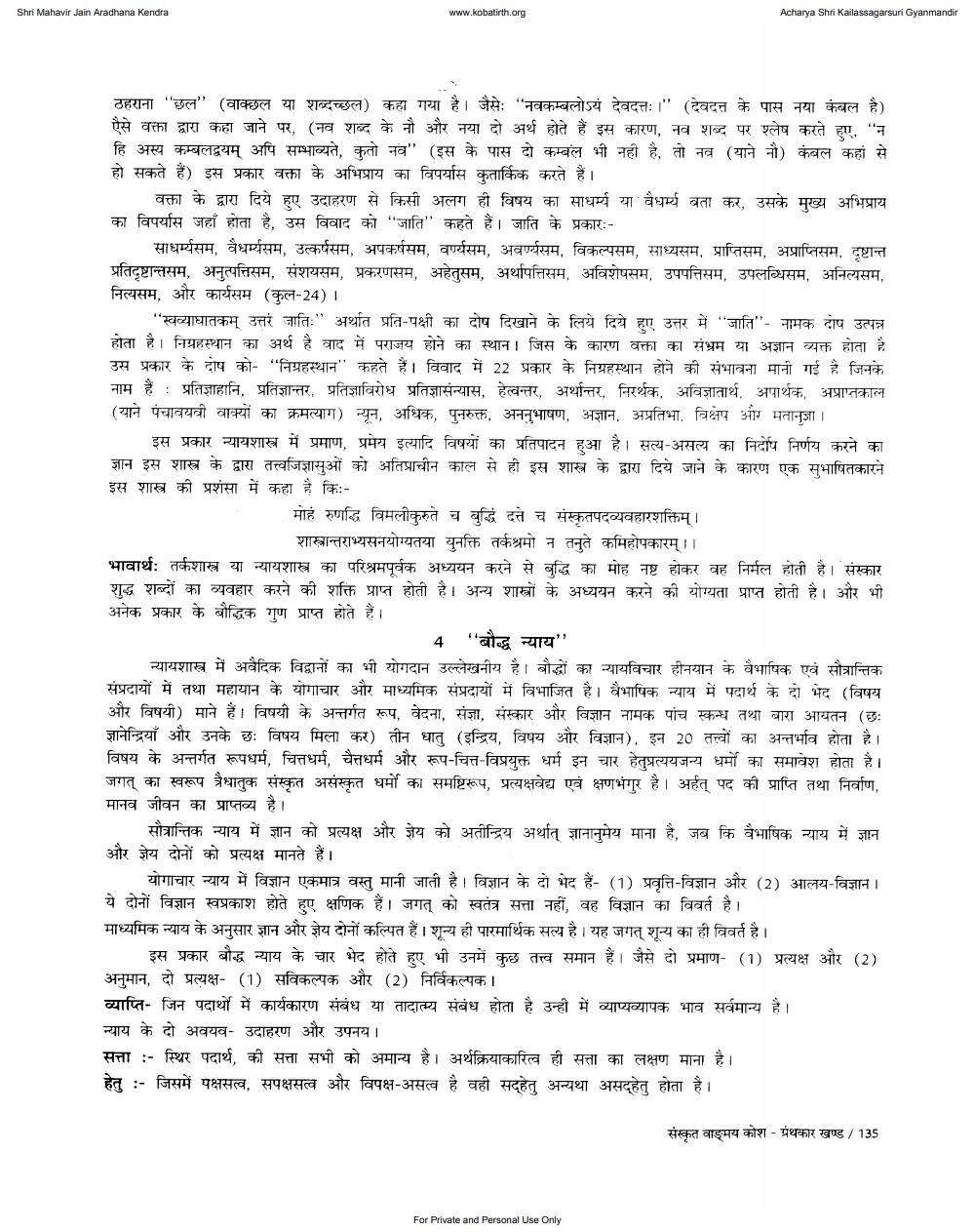________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
ठहराना "छल" (वाक्छल या शब्दच्छल) कहा गया है। जैसे: "नवकम्बलोऽयं देवदत्तः।" (देवदत्त के पास नया कंबल है) ऐसे वक्ता द्वारा कहा जाने पर, (नव शब्द के नौ और नया दो अर्थ होते हैं इस कारण, नव शब्द पर श्लेष करते हुए, "न हि अस्य कम्बलद्वयम् अपि सम्भाव्यते, कुतो नव" (इस के पास दो कम्बल भी नहीं है, तो नव (याने नौ) कंबल कहां से हो सकते हैं। इस प्रकार वक्ता के अभिप्राय का विपर्यास कुतार्किक करते हैं।
वक्ता के द्वारा दिये हुए उदाहरण से किसी अलग ही विषय का साधर्म्य या वैधर्म्य बता कर, उसके मुख्य अभिप्राय का विपर्यास जहाँ होता है, उस विवाद को "जाति' कहते हैं। जाति के प्रकारः
साधर्म्यसम, वैधर्म्यसम, उत्कर्षसम, अपकर्षसम, वर्ण्यसम, अवर्ण्यसम, विकल्पसम, साध्यसम, प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम, दृष्टान्त प्रतिदृष्टान्तसम, अनुत्पत्तिसम, संशयसम, प्रकरणसम, अहेतुसम, अर्थापत्तिसम, अविशेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनिल्यसम, नित्यसम, और कार्यसम (कुल-24)।
"स्वव्याघातकम् उत्तरं जातिः" अर्थात प्रति-पक्षी का दोष दिखाने के लिये दिये हए उत्तर में "जाति"- नामक दोष उत्पन्न होता है। निग्रहस्थान का अर्थ है वाद में पराजय होने का स्थान। जिस के कारण वक्ता का संभ्रम या अज्ञान व्यक्त होता है उस प्रकार के दोष को- "निग्रहस्थान" कहते हैं। विवाद में 22 प्रकार के निग्रहस्थान होने की संभावना मानी गई है जिनके नाम हैं : प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध प्रतिज्ञासंन्यास, हेत्वन्तर, अर्थान्तर, निरर्थक, अविज्ञातार्थ, अपार्थक, अप्राप्तकाल (याने पंचावयवी वाक्यों का क्रमत्याग) न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप और मतानुज्ञा।
इस प्रकार न्यायशास्त्र में प्रमाण, प्रमेय इत्यादि विषयों का प्रतिपादन हुआ है। सत्य-असत्य का निर्दोष निर्णय करने का ज्ञान इस शास्त्र के द्वारा तत्त्वजिज्ञासुओं को अतिप्राचीन काल से ही इस शास्त्र के द्वारा दिये जाने के कारण एक सुभाषितकारने इस शास्त्र की प्रशंसा में कहा है कि:
मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं दत्ते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिम्।
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न तनुते कमिहोपकारम् ।। भावार्थः तर्कशास्त्र या न्यायशास्त्र का परिश्रमपूर्वक अध्ययन करने से बुद्धि का मोह नष्ट होकर वह निर्मल होती है। संस्कार शुद्ध शब्दों का व्यवहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। अन्य शास्त्रों के अध्ययन करने की योग्यता प्राप्त होती है। और भी अनेक प्रकार के बौद्धिक गुण प्राप्त होते हैं।
4 "बौद्ध न्याय" न्यायशास्त्र में अवैदिक विद्वानों का भी योगदान उल्लेखनीय है। बौद्धों का न्यायविचार हीनयान के वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक संप्रदायों में तथा महायान के योगाचार और माध्यमिक संप्रदायों में विभाजित है। वैभाषिक न्याय में पदार्थ के दो भेद (विषय
और विषयी) माने हैं। विषयी के अन्तर्गत रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नामक पांच स्कन्ध तथा बारा आयतन (छः ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके छः विषय मिला कर) तीन धातु (इन्द्रिय, विषय और विज्ञान), इन 20 तत्त्वों का अन्तर्भाव होता है। विषय के अन्तर्गत रूपधर्म, चित्तधर्म, चैत्तधर्म और रूप-चित्त-विप्रयुक्त धर्म इन चार हेतुप्रत्ययजन्य धर्मो का समावेश होता है। जगत् का स्वरूप त्रैधातुक संस्कृत असंस्कृत धर्मो का समष्टिरूप, प्रत्यक्षवेद्य एवं क्षणभंगुर है। अर्हत् पद की प्राप्ति तथा निर्वाण, मानव जीवन का प्राप्तव्य है।
सौत्रान्तिक न्याय में ज्ञान को प्रत्यक्ष और ज्ञेय को अतीन्द्रिय अर्थात् ज्ञानानुमेय माना है, जब कि वैभाषिक न्याय में ज्ञान और ज्ञेय दोनों को प्रत्यक्ष मानते हैं।
योगाचार न्याय में विज्ञान एकमात्र वस्तु मानी जाती है। विज्ञान के दो भेद हैं- (1) प्रवृत्ति-विज्ञान और (2) आलय-विज्ञान । ये दोनों विज्ञान स्वप्रकाश होते हुए क्षणिक हैं। जगत् को स्वतंत्र सत्ता नहीं, वह विज्ञान का विवर्त है। माध्यमिक न्याय के अनुसार ज्ञान और ज्ञेय दोनों कल्पित हैं। शून्य ही पारमार्थिक सत्य है। यह जगत् शून्य का ही विवर्त है।
इस प्रकार बौद्ध न्याय के चार भेद होते हुए भी उनमें कुछ तत्त्व समान हैं। जैसे दो प्रमाण- (1) प्रत्यक्ष और (2) अनुमान, दो प्रत्यक्ष- (1) सविकल्पक और (2) निर्विकल्पक। व्याप्ति- जिन पदार्थों में कार्यकारण संबंध या तादात्म्य संबंध होता है उन्ही में व्याप्यव्यापक भाव सर्वमान्य है। न्याय के दो अवयव- उदाहरण और उपनय। सत्ता :- स्थिर पदार्थ, की सत्ता सभी को अमान्य है। अर्थक्रियाकारित्व ही सत्ता का लक्षण माना है। हेतु :- जिसमें पक्षसत्व, सपक्षसत्व और विपक्ष-असत्व है वही सद्हेतु अन्यथा असद्हेतु होता है।
संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड / 135
For Private and Personal Use Only