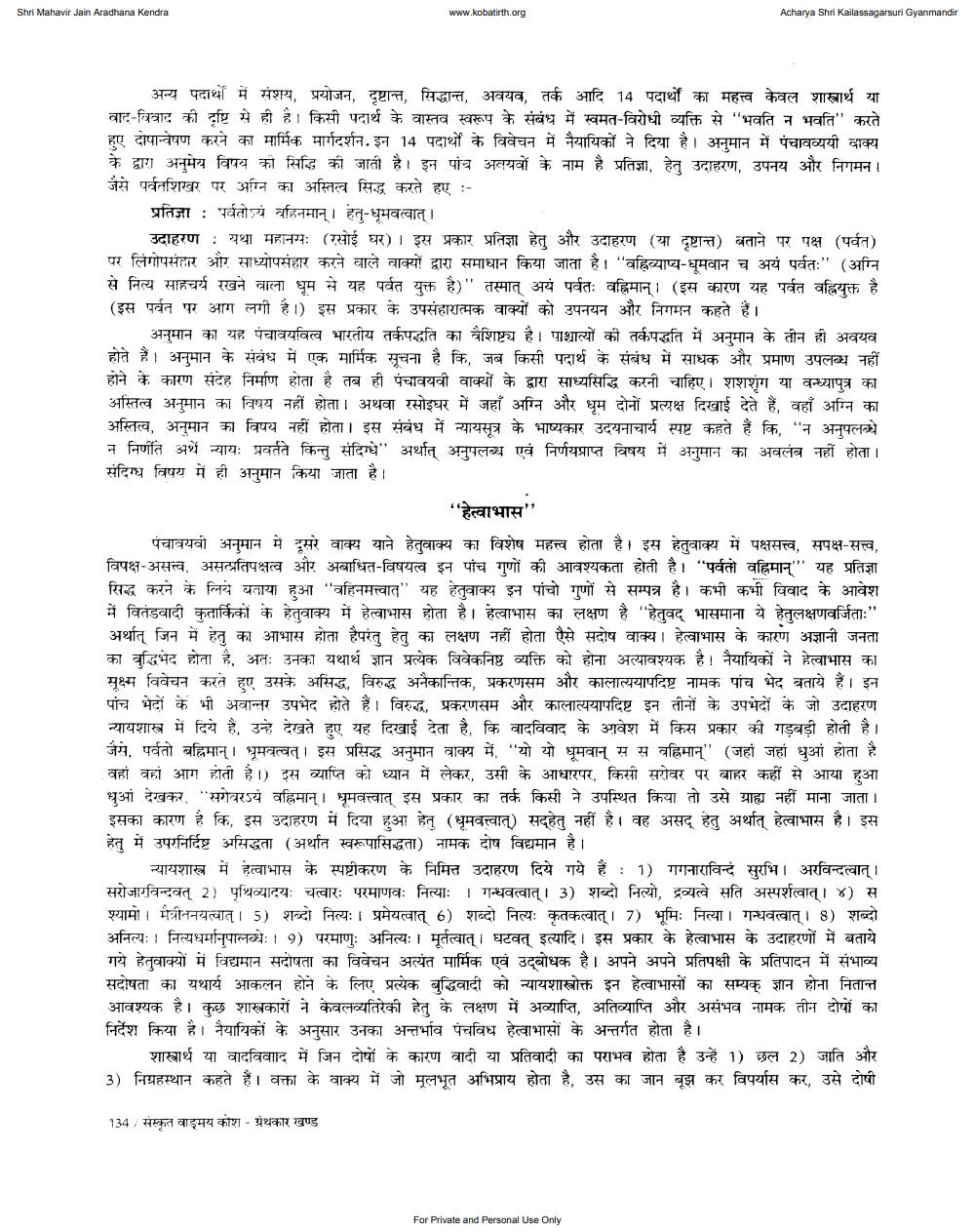________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
अन्य पदार्थों में संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क आदि 14 पदार्थों का महत्त्व केवल शास्त्रार्थ या वाद-विवाद की दृष्टि से ही है। किसी पदार्थ के वास्तव स्वरूप के संबंध में स्वमत-विरोधी व्यक्ति से "भवति न भवति" करते हुए दोषान्वेषण करने का मार्मिक मार्गदर्शन. इन 14 पदार्थों के विवेचन में नैयायिकों ने दिया है। अनुमान में पंचावव्ययी वाक्य के द्वारा अनुमेय विषय को सिद्धि की जाती है। इन पांच अवयवों के नाम है प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन । जैसे पर्वतशिखर पर अग्नि का अस्तित्व सिद्ध करते हए :
प्रतिज्ञा : पर्वतोऽयं वहिनमान्। हेतु-धूमवत्वात् ।
उदाहरण : यथा महानयः (रसोई घर)। इस प्रकार प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण (या दृष्टान्त) बताने पर पक्ष (पर्वत) पर लिंगोपसंहार और साध्योपसंहार करने वाले वाक्यों द्वारा समाधान किया जाता है। "वह्निव्याप्य-धूमवान च अयं पर्वतः" (अग्नि से नित्य साहचर्य रखने वाला धूम से यह पर्वत युक्त है)" तस्मात् अयं पर्वतः वह्निमान्। (इस कारण यह पर्वत वह्नियुक्त है (इस पर्वत पर आग लगी है।) इस प्रकार के उपसंहारात्मक वाक्यों को उपनयन और निगमन कहते हैं।
अनुमान का यह पंचावयवित्व भारतीय तर्कपद्धति का वैशिष्ट्य है। पाश्चात्यों की तर्कपद्धति में अनुमान के तीन ही अवयव होते हैं। अनुमान के संबंध में एक मार्मिक सूचना है कि, जब किसी पदार्थ के संबंध में साधक और प्रमाण उपलब्ध नहीं होने के कारण संदेह निर्माण होता है तब ही पंचावयवी वाक्यों के द्वारा साध्यसिद्धि करनी चाहिए। शशशंग या वन्ध्यापुत्र का अस्तित्व अनुमान का विषय नहीं होता। अथवा रसोइघर में जहाँ अग्नि और धूम दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वहाँ अग्नि का अस्तित्व, अनुमान का विषय नहीं होता। इस संबंध में न्यायसूत्र के भाष्यकार उदयनाचार्य स्पष्ट कहते हैं कि, "न अनुपलब्धे न निर्णीत अर्थे न्यायः प्रवर्तते किन्तु संदिग्धे" अर्थात् अनुपलब्ध एवं निर्णयप्राप्त विषय में अनुमान का अवलंब नहीं होता। संदिग्ध विषय में ही अनुमान किया जाता है।
__"हेत्वाभास" पंचावयवी अनुमान में दूसरे वाक्य याने हेतुवाक्य का विशेष महत्त्व होता है। इस हेतुवाक्य में पक्षसत्त्व, सपक्ष-सत्त्व, विपक्ष-असत्त्व, असत्प्रतिपक्षत्व और अबाधित-विषयत्व इन पांच गुणों की आवश्यकता होती है। “पर्वतो वह्निमान्" यह प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिये बताया हुआ "वहिनमत्त्वात" यह हेतुवाक्य इन पांचो गुणों से सम्पन्न है। कभी कभी विवाद के आवेश में वितंडवादी कुतार्किको के हेतुवाक्य में हेत्वाभास होता है। हेत्वाभास का लक्षण है "हेतुवद् भासमाना ये हेतुलक्षणवर्जिताः" अर्थात् जिन में हेतु का आभास होता हैपरंतु हेतु का लक्षण नहीं होता ऐसे सदोष वाक्य । हेत्वाभास के कारण अज्ञानी जनता का बुद्धिभेद होता है, अतः उनका यथार्थ ज्ञान प्रत्येक विवेकनिष्ठ व्यक्ति को होना अत्यावश्यक है। नैयायिकों ने हेत्वाभास का सूक्ष्म विवेचन करते हुए उसके असिद्ध, विरुद्ध अनैकान्तिक, प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट नामक पांच भेद बताये हैं। इन पांच भेदों के भी अवान्तर उपभेद होते हैं। विरुद्ध, प्रकरणसम और कालात्ययापदिष्ट इन तीनों के उपभेदों के जो उदाहरण न्यायशास्त्र में दिये हैं, उन्हे देखते हुए यह दिखाई देता है, कि वादविवाद के आवेश में किस प्रकार की गड़बड़ी होती है। जैसे, पर्वतो बह्निमान्। धूमवत्वत्। इस प्रसिद्ध अनुमान वाक्य में, "यो यो धूमवान् स स वह्निमान्" (जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है।) इस व्याप्ति को ध्यान में लेकर, उसी के आधारपर, किसी सरोवर पर बाहर कहीं से आया हुआ धुआं देखकर. "सरोवरऽयं वह्निमान्। धूमवत्त्वात् इस प्रकार का तर्क किसी ने उपस्थित किया तो उसे ग्राह्य नहीं माना जाता। इसका कारण है कि, इस उदाहरण में दिया हुआ हेतु (धूमवत्त्वात्) सद्हेतु नहीं है। वह असद् हेतु अर्थात् हेत्वाभास है। इस हेतु में उपरनिर्दिष्ट असिद्धता (अर्थात स्वरूपासिद्धता) नामक दोष विद्यमान है।
न्यायशास्त्र में हत्वाभास के स्पष्टीकरण के निमित्त उदाहरण दिये गये हैं : 1) गगनाराविन्दं सुरभि। अरविन्दत्वात्। सरोजारविन्दवत् 2) पृथिव्यादयः चत्वारः परमाणवः नित्याः । गन्धवत्वात्। 3) शब्दो नित्यो, द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्। ४) स श्यामो। मैत्रीतनयत्वात्। 5) शब्दो नित्यः। प्रमेयत्वात् 6) शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। 7) भूमिः नित्या। गन्धवत्वात्। 8) शब्दो अनित्यः । नित्यधर्मानपालब्धः। 9) परमाणुः अनित्यः। मूर्तत्वात्। घटवत् इत्यादि। इस प्रकार के हेत्वाभास के उदाहरणों में बताये गये हेतुवाक्यों में विद्यमान सदोषता का विवेचन अत्यंत मार्मिक एवं उद्बोधक है। अपने अपने प्रतिपक्षी के प्रतिपादन में संभाव्य सदोषता का यथार्य आकलन होने के लिए प्रत्येक बुद्धिवादी को न्यायशास्त्रोक्त इन हेत्वाभासों का सम्यक् ज्ञान होना नितान्त
आवश्यक है। कुछ शास्त्रकारों ने केवलव्यतिरेकी हेतु के लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नामक तीन दोषों का निर्देश किया है। नैयायिकों के अनुसार उनका अन्तर्भाव पंचविध हेत्वाभासों के अन्तर्गत होता है।
शास्त्रार्थ या वादविवाद में जिन दोषों के कारण वादी या प्रतिवादी का पराभव होता है उन्हें 1) छल 2) जाति और 3) निग्रहस्थान कहते हैं। वक्ता के वाक्य में जो मूलभूत अभिप्राय होता है, उस का जान बूझ कर विपर्यास कर, उसे दोषी
134/ संस्कृत वाड़मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only