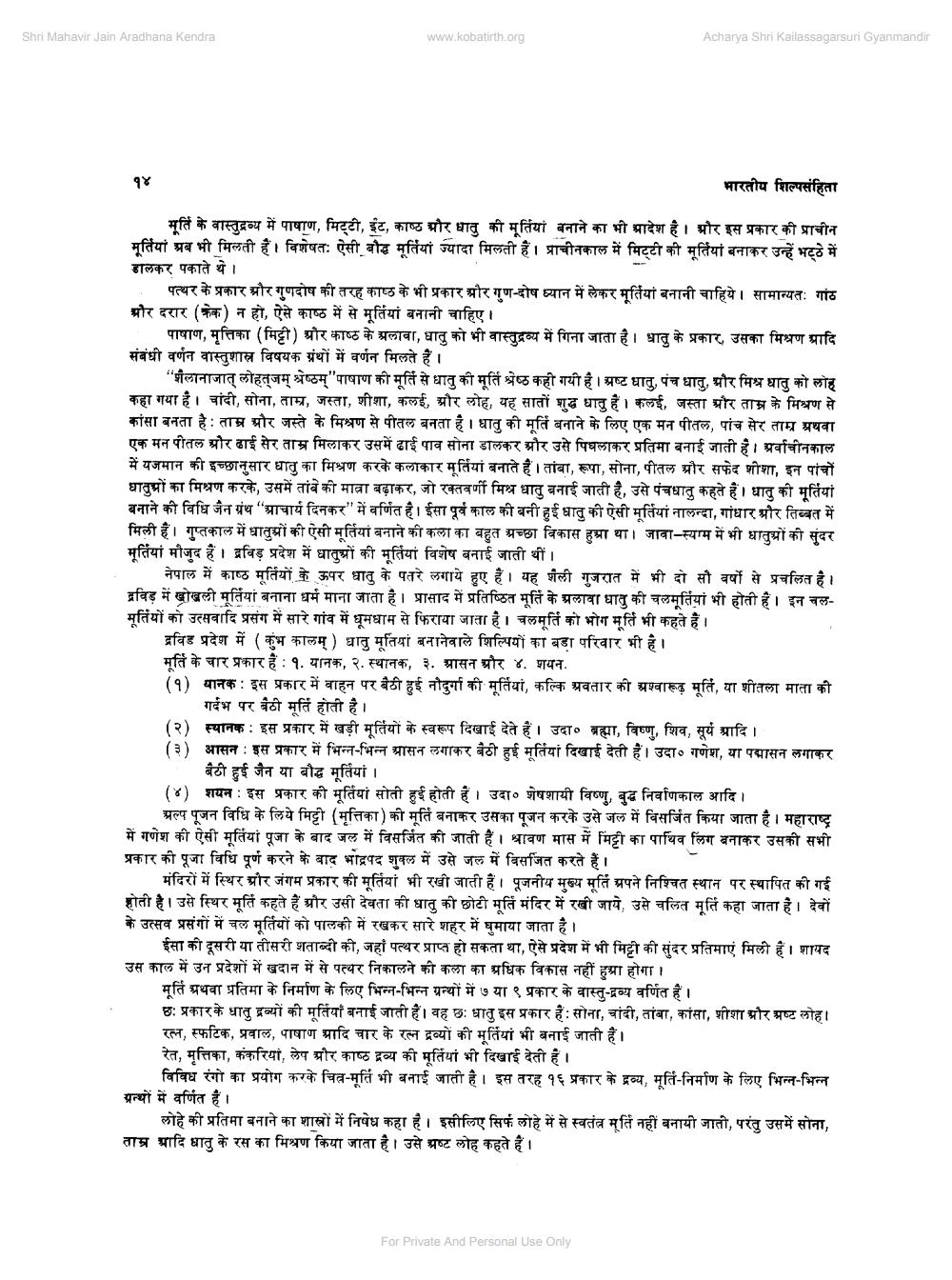________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
१४
भारतीय शिल्पसंहिता
मूर्ति के वास्तुद्रव्य में पाषाण, मिट्टी, इंट, काष्ठ और धातु की मूर्तियां बनाने का भी आदेश है। और इस प्रकार की प्राचीन मूर्तियां अब भी मिलती हैं। विशेषतः ऐसी बौद्ध मूर्तियां ज्यादा मिलती है। प्राचीनकाल में मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें भट्ठे में डालकर पकाते थे।
पत्थर के प्रकार और गुणदोष की तरह काष्ठ के भी प्रकार और गुण-दोष ध्यान में लेकर मूर्तियां बनानी चाहिये । सामान्यतः गांठ और दरार (केक) न हो, ऐसे काष्ठ में से मूर्तियां बनानी चाहिए।
पाषाण, मृत्तिका (मिट्टी) और काष्ठ के अलावा, धातु को भी वास्तुद्रव्य में गिना जाता है। धातु के प्रकार, उसका मिश्रण आदि संबंधी वर्णन वास्तुशास्त्र विषयक ग्रंथों में वर्णन मिलते हैं।
"शैलानाजात् लोहत्जम् श्रेष्ठम्"पाषाण की मूर्ति से धातु की मूर्ति श्रेष्ठ कही गयी है । अष्ट धातु, पंच धातु, और मिश्र धातु को लोह कहा गया है। चांदी, सोना, ताम्र, जस्ता, शीशा, कलई, और लोह, यह सातों शुद्ध धातु है। कलई, जस्ता और ताम्र के मिश्रण से कांसा बनता है : ताम्र और जस्ते के मिश्रण से पीतल बनता है। धातु की मूर्ति बनाने के लिए एक मन पीतल, पांच सेर ताम्र अथवा एक मन पीतल और ढाई सेर ताम्र मिलाकर उसमें ढाई पाव सोना डालकर और उसे पिघलाकर प्रतिमा बनाई जाती है। अर्वाचीनकाल में यजमान की इच्छानुसार धातु का मिश्रण करके कलाकार मूर्तियां बनाते हैं। तांबा, रूपा, सोना, पीतल और सफेद शीशा, इन पांचों धातुओं का मिश्रण करके, उसमें तांबे की मात्रा बढ़ाकर, जो रक्तवर्णी मिश्र धातु बनाई जाती है, उसे पंचधातु कहते है। धातु की मूर्तियां बनाने की विधि जैन ग्रंथ "प्राचार्य दिनकर" में वर्णित है। ईसा पूर्व काल की बनी हुई धातु की ऐसी मूर्तियां नालन्दा, गांधार और तिब्बत में मिली है। गुप्तकाल में धातुओं की ऐसी मूर्तियां बनाने की कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था। जावा-स्याम में भी धातुओं की सुंदर मूर्तियां मौजुद हैं। द्रविड़ प्रदेश में धातुओं की मूर्तियां विशेष बनाई जाती थीं।
नेपाल में काष्ठ मूर्तियों के ऊपर धातु के पतरे लगाये हुए हैं। यह शैली गुजरात में भी दो सौ वर्षों से प्रचलित है। द्रविड़ में खोखली मूर्तियां बनाना धर्म माना जाता है। प्रासाद में प्रतिष्ठित मूर्ति के अलावा धातु की चलमूर्तियां भी होती है। इन चलमूर्तियों को उत्सवादि प्रसंग में सारे गांव में धूमधाम से फिराया जाता है। चलमूर्ति को भोग मूर्ति भी कहते हैं।
द्रविड प्रदेश में ( कुंभ कालम् ) धातु मूर्तियां बनानेवाले शिल्पियों का बड़ा परिवार भी है। मूर्ति के चार प्रकार है : १. यानक, २. स्थानक, ३. आसन और ४. शयन. (१) यानक : इस प्रकार में वाहन पर बैठी हुई नौदुर्गा की मूर्तियां, कल्कि अवतार की अश्वारूढ़ मूर्ति, या शीतला माता की
गर्दभ पर बैठी मूर्ति होती है। (२) स्थानक : इस प्रकार में खड़ी मूर्तियों के स्वरूप दिखाई देते हैं। उदा० ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य आदि । (३) आसन : इस प्रकार में भिन्न-भिन्न आसन लगाकर बैठी हुई मूर्तियां दिखाई देती हैं। उदा० गणेश, या पद्मासन लगाकर
बैठी हुई जैन या बौद्ध मूर्तियां । (४) शयन : इस प्रकार की मूर्तियां सोती हुई होती हैं। उदा० शेषशायी विष्णु, बुद्ध निर्वाणकाल आदि।
अल्प पूजन विधि के लिये मिट्टी (मृत्तिका) की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करके उसे जल में विसर्जित किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश की ऐसी मूर्तियां पूजा के बाद जल में विसर्जित की जाती हैं। श्रावण मास में मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाकर उसकी सभी प्रकार की पूजा विधि पूर्ण करने के बाद भाद्रपद शुक्ल में उसे जल में विसर्जित करते हैं।
__ मंदिरों में स्थिर और जंगम प्रकार की मूर्तियां भी रखी जाती है। पूजनीय मुख्य मूर्ति अपने निश्चित स्थान पर स्थापित की गई होती है। उसे स्थिर मूर्ति कहते हैं और उसी देवता की धातु की छोटी मूर्ति मंदिर में रखी जाये, उसे चलित मूर्ति कहा जाता है। देवों के उत्सव प्रसंगों में चल मूर्तियों को पालकी में रखकर सारे शहर में घमाया जाता है।
ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी की, जहाँ पत्थर प्राप्त हो सकता था, ऐसे प्रदेश में भी मिट्टी की सुंदर प्रतिमाएं मिली है। शायद उस काल में उन प्रदेशों में खदान में से पत्थर निकालने की कला का अधिक विकास नहीं हुआ होगा।
मूर्ति अथवा प्रतिमा के निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में ७ या ९ प्रकार के वास्तु-द्रव्य वर्णित है। छ: प्रकार के धातु द्रव्यों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। वह छः धातु इस प्रकार है : सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा और अष्ट लोह। रल, स्फटिक, प्रवाल, पाषाण आदि चार के रत्न द्रव्यों की मूर्तियां भी बनाई जाती है। रेत, मृत्तिका, कंकरियां, लेप और काष्ठ द्रव्य की मूर्तियां भी दिखाई देती है।
विविध रंगो का प्रयोग करके चित्र-मूर्ति भी बनाई जाती है। इस तरह १६ प्रकार के द्रव्य, मूर्ति-निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में वर्णित है।
लोहे की प्रतिमा बनाने का शास्त्रों में निषेध कहा है। इसीलिए सिर्फ लोहे में से स्वतंत्र मूर्ति नहीं बनायी जातो, परंतु उसमें सोना, ताम्र प्रादि धातु के रस का मिश्रण किया जाता है। उसे प्रष्ट लोह कहते हैं।
For Private And Personal Use Only