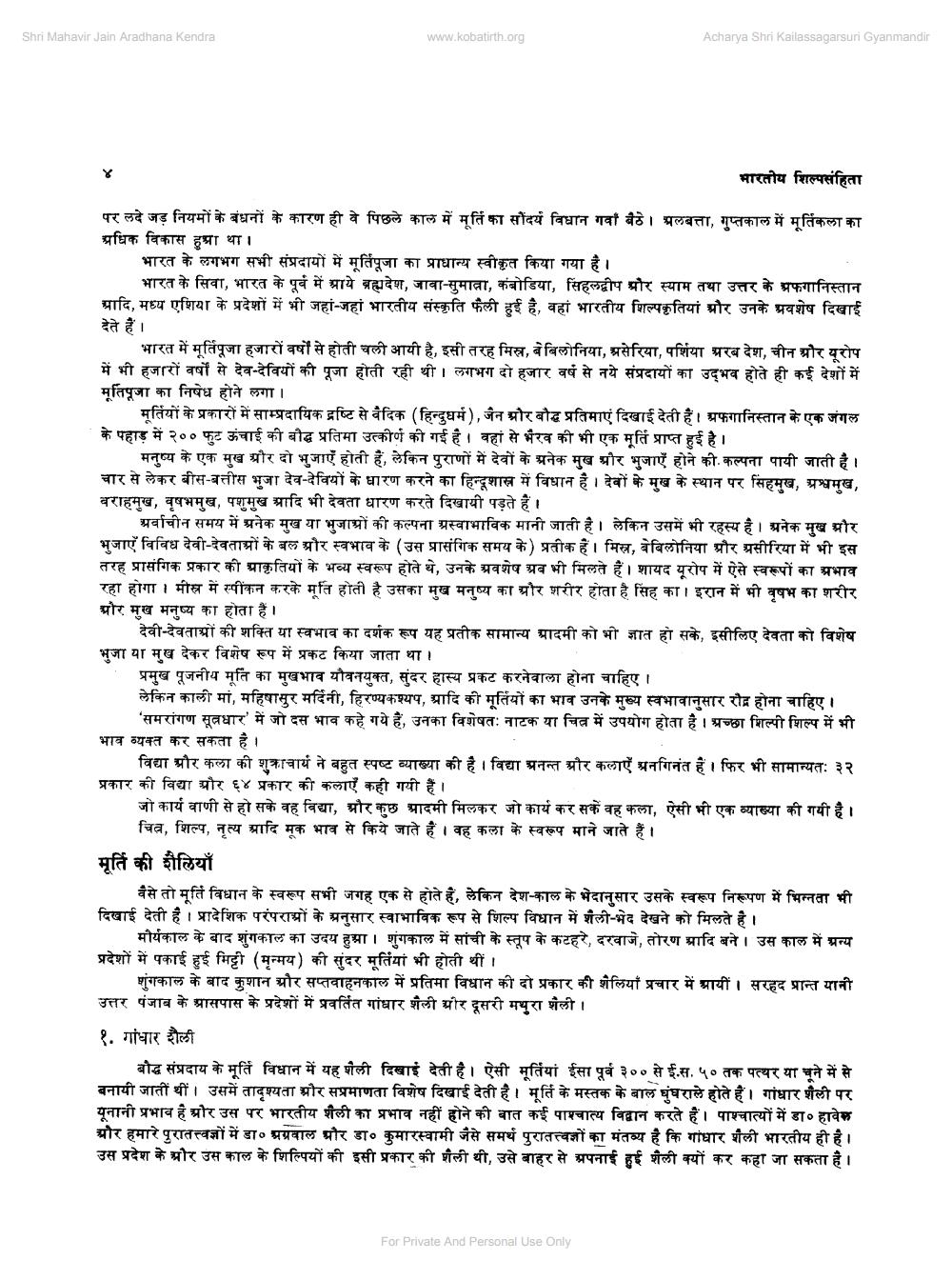________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
भारतीय शिल्पसंहिता
पर लदे जड़ नियमों के बंधनों के कारण ही वे पिछले काल में मूर्ति का सौंदर्य विधान गवाँ बैठे। अलबत्ता, गुप्तकाल में मूर्तिकला का अधिक विकास हुअा था।
भारत के लगभग सभी संप्रदायों में मूर्तिपूजा का प्राधान्य स्वीकृत किया गया है।
भारत के सिवा, भारत के पूर्व में आये ब्रह्मदेश, जावा-सुमात्रा, कंबोडिया, सिंहलद्वीप और स्याम तथा उत्तर के अफगानिस्तान पादि, मध्य एशिया के प्रदेशों में भी जहां-जहां भारतीय संस्कृति फैली हुई है, वहां भारतीय शिल्पकृतियां और उनके अवशेष दिखाई देते हैं।
भारत में मूर्तिपूजा हजारों वर्षों से होती चली आयी है, इसी तरह मिस्र, बेबिलोनिया, असेरिया, पर्शिया अरब देश, चीन और यूरोप में भी हजारों वर्षों से देव-देवियों की पूजा होती रही थी। लगभग दो हजार वर्ष से नये संप्रदायों का उद्भव होते ही कई देशों में मूर्तिपूजा का निषेध होने लगा।
मूर्तियों के प्रकारों में साम्प्रदायिक द्रष्टि से वैदिक (हिन्दुधर्म), जैन और बौद्ध प्रतिमाएं दिखाई देती है। अफगानिस्तान के एक जंगल के पहाड़ में २०० फुट ऊंचाई की बौद्ध प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है। वहां से भैरव की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है।
मनुष्य के एक मुख और दो भुजाएं होती हैं, लेकिन पुराणों में देवों के अनेक मुख और भुजाएँ होने की कल्पना पायी जाती है। चार से लेकर बीस-बत्तीस भुजा देव-देवियों के धारण करने का हिन्दूशास्त्र में विधान है। देवों के मुख के स्थान पर सिंहमुख, अश्वमुख, बराहमुख, वृषभमुख, पशुमुख आदि भी देवता धारण करते दिखायी पड़ते है।
अर्वाचीन समय में अनेक मुख या भुजाओं की कल्पना अस्वाभाविक मानी जाती है। लेकिन उसमें भी रहस्य है। अनेक मुख और भुजाएँ विविध देवी-देवताओं के बल और स्वभाव के (उस प्रासंगिक समय के) प्रतीक है। मिस्र, बेबिलोनिया और असीरिया में भी इस तरह प्रासंगिक प्रकार की प्राकृतियों के भव्य स्वरूप होते थे, उनके अवशेष अब भी मिलते हैं। शायद यूरोप में ऐसे स्वरूपों का प्रभाव रहा होगा। मीन में स्पीकन करके मति होती है उसका मुख मनुष्य का और शरीर होता है सिंह का। इरान में भी वृषभ का शरीर और मुख मनुष्य का होता हैं।
देवी-देवताओं की शक्ति या स्वभाव का दर्शक रूप यह प्रतीक सामान्य आदमी को भी ज्ञात हो सके, इसीलिए देवता को विशेष भुजा या मुख देकर विशेष रूप में प्रकट किया जाता था।
प्रमुख पूजनीय मूर्ति का मुखभाव यौवनयुक्त, सुंदर हास्य प्रकट करनेवाला होना चाहिए। लेकिन काली मां, महिषासुर मर्दिनी, हिरण्यकश्यप, आदि की मूर्तियों का भाव उनके मुख्य स्वभावानुसार रौद्र होना चाहिए।
'समरांगण सूत्रधार' में जो दस भाव कहे गये हैं, उनका विशेषतः नाटक या चित्र में उपयोग होता है । अच्छा शिल्पी शिल्प में भी भाव व्यक्त कर सकता है।
विद्या और कला की शुक्राचार्य ने बहुत स्पष्ट व्याख्या की है । विद्या अनन्त और कलाएँ अनगिनंत हैं। फिर भी सामान्यतः ३२ प्रकार की विद्या और ६४ प्रकार की कलाएँ कही गयी हैं।
जो कार्य वाणी से हो सके वह विद्या, और कुछ आदमी मिलकर जो कार्य कर सकें वह कला, ऐसी भी एक व्याख्या की गयी है।
चित्र, शिल्प, नृत्य आदि मूक भाव से किये जाते हैं । वह कला के स्वरूप माने जाते हैं। मूर्ति की शैलियाँ
वैसे तो मूर्ति विधान के स्वरूप सभी जगह एक से होते हैं, लेकिन देश-काल के भेदानुसार उसके स्वरूप निरूपण में भिन्नता भी दिखाई देती है । प्रादेशिक परंपराओं के अनुसार स्वाभाविक रूप से शिल्प विधान में शैली-भेद देखने को मिलते है।
मौर्यकाल के बाद शुंगकाल का उदय हुआ। शुंगकाल में सांची के स्तूप के कटहरे, दरवाजे, तोरण प्रादि बने । उस काल में अन्य प्रदेशों में पकाई हुई मिट्टी (मृन्मय) की सुंदर मूर्तियां भी होती थीं।
शुंगकाल के बाद कुशान और सप्तवाहनकाल में प्रतिमा विधान की दो प्रकार की शैलियाँ प्रचार में आयीं। सरहद प्रान्त यानी उत्तर पंजाब के आसपास के प्रदेशों में प्रवर्तित गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली। १. गांधार शैली
___ बौद्ध संप्रदाय के मूर्ति विधान में यह शैली दिखाई देती है। ऐसी मूर्तियां ईसा पूर्व ३०० से ई.स. ५० तक पत्थर या चूने में से बनायी जाती थीं। उसमें तादृश्यता और सप्रमाणता विशेष दिखाई देती है। मूर्ति के मस्तक के बाल धुंघराले होते हैं। गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव है और उस पर भारतीय शैली का प्रभाव नहीं होने की बात कई पाश्चात्य विद्वान करते हैं। पाश्चात्यों में डा० हावेक और हमारे पुरातत्त्वज्ञों में डा० अग्रवाल और डा० कुमारस्वामी जैसे समर्थ पुरातत्त्वज्ञों का मंतव्य है कि गांधार शैली भारतीय ही है। उस प्रदेश के और उस काल के शिल्पियों की इसी प्रकार की शैली थी, उसे बाहर से अपनाई हुई शैली क्यों कर कहा जा सकता है।
For Private And Personal Use Only