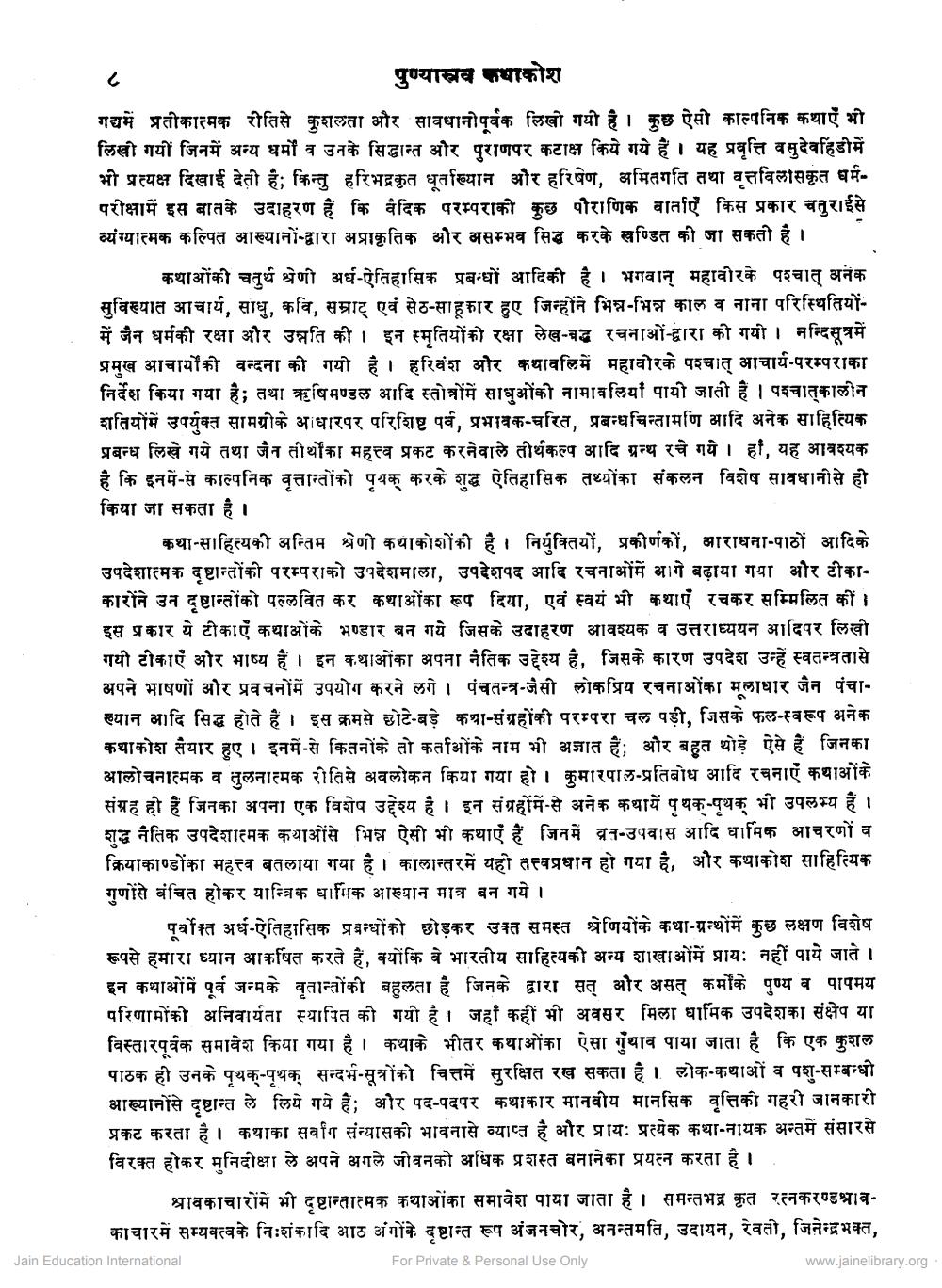________________
८
पुण्यास्रव कथाकोश
गद्य में प्रतीकात्मक रीति से कुशलता और सावधानीपूर्वक लिखो गयी है। कुछ ऐसी काल्पनिक कथाएँ भी लिखी गयीं जिनमें अन्य धर्मों व उनके सिद्धान्त और पुराणपर कटाक्ष किये गये हैं । यह प्रवृत्ति वसुदेवहिडी में भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है; किन्तु हरिभद्रकृत धूर्ताख्यान और हरिषेण अमितगति तथा वृत्तविलासकृत धर्मपरीक्षा में इस बात के उदाहरण हैं कि वैदिक परम्पराको कुछ पौराणिक वार्ताएँ किस प्रकार चतुराईसे व्यंग्यात्मक कल्पित आख्यानों द्वारा अप्राकृतिक और असम्भव सिद्ध करके खण्डित की जा सकती I
कथाओंकी चतुर्थ श्रेणी अर्ध- ऐतिहासिक प्रबन्धों आदिकी है । भगवान् महावीरके पश्चात् अनेक सुविख्यात आचार्य, साधु, कवि, सम्राट् एवं सेठ साहूकार हुए जिन्होंने भिन्न-भिन्न काल व नाना परिस्थितियोंमें जैन धर्मकी रक्षा और उन्नति की। इन स्मृतियोंको रक्षा लेख-बद्ध रचनाओं द्वारा की गयी । नन्दिसूत्र में प्रमुख आचार्योंकी वन्दना की गयी है । हरिवंश और कथावलिमें महावोरके पश्चात् आचार्य परम्पराका निर्देश किया गया है; तथा ऋषिमण्डल आदि स्तोत्रोंमें साधुओंकी नामावलियाँ पायी जाती हैं । पश्चात्कालीन शतियों में उपर्युक्त सामग्री के आधारपर परिशिष्ट पर्व, प्रभावक-चरित, प्रबन्धचिन्तामणि आदि अनेक साहित्यिक प्रबन्ध लिखे गये तथा जैन तीर्थोंका महत्त्व प्रकट करनेवाले तीर्थकल्प आदि ग्रन्थ रचे गये । हाँ, यह आवश्यक है कि इनमें से काल्पनिक वृत्तान्तोंको पृथक् करके शुद्ध ऐतिहासिक तथ्योंका संकलन विशेष सावधानी से हो किया जा सकता है ।
कथा-साहित्यकी अन्तिम श्रेणी कथाकोशोंकी है। नियुक्तियों, प्रकीर्णकों, आराधना पाठों आदिके उपदेशात्मक दृष्टान्तों की परम्पराको उपदेशमाला, उपदेशवद आदि रचनाओंमें आगे बढ़ाया गया और टीकाकारोंने उन दृष्टान्तोंको पल्लवित कर कथाओंका रूप दिया, एवं स्वयं भी कथाएँ रचकर सम्मिलित कीं । इस प्रकार ये टीकाएँ कथाओंके भण्डार बन गये जिसके उदाहरण आवश्यक व उत्तराध्ययन आदिपर लिखी गयी टीकाएँ और भाष्य हैं । इन कथाओंका अपना नैतिक उद्देश्य है, जिसके कारण उपदेश उन्हें स्वतन्त्रता से अपने भाषणों और प्रवचनोंमें उपयोग करने लगे । पंचतन्त्र-जैसी लोकप्रिय रचनाओंका मूलाधार जैन पंचाख्यान आदि सिद्ध होते हैं । इस क्रमसे छोटे-बड़े कथा-संग्रहोंकी परम्परा चल पड़ी, जिसके फल स्वरूप अनेक कथाकोश तैयार हुए । इनमें से कितनोंके तो कर्ताओंके नाम भी अज्ञात हैं; और बहुत थोड़े ऐसे हैं जिनका आलोचनात्मक व तुलनात्मक रीति से अवलोकन किया गया हो । कुमारपाल प्रतिबोध आदि रचनाएँ कथाओं के संग्रह हो हैं जिनका अपना एक विशेष उद्देश्य है । इन संग्रहों में से अनेक कथायें पृथक्-पृथक् भी उपलभ्य हैं । शुद्ध नैतिक उपदेशात्मक कथाओंसे भिन्न ऐसी भी कथाएँ हैं जिनमें व्रत-उपवास आदि धार्मिक आचरणों व क्रियाकाण्डों का महत्त्व बतलाया गया है । कालान्तर में यही तत्त्वप्रधान हो गया है, और कथाकोश साहित्यिक गुणोंसे वंचित होकर यान्त्रिक धार्मिक आख्यान मात्र बन गये ।
पूर्वोक्त अर्ध ऐतिहासिक प्रबन्धोंको छोड़कर उक्त समस्त श्रेणियोंके कथा-ग्रन्थोंमें कुछ लक्षण विशेष रूपसे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे भारतीय साहित्यकी अन्य शाखाओंमें प्रायः नहीं पाये जाते । इन कथाओं में पूर्व जन्म के वृतान्तोंकी बहुलता है जिनके द्वारा सत् और असत् कर्मोंके पुण्य व पापमय परिणामोंकी अनिवार्यता स्थापित की गयी है । जहाँ कहीं भी अवसर मिला धार्मिक उपदेशका संक्षेप या विस्तारपूर्वक समावेश किया गया है । कथाके भीतर कथाओंका ऐसा गुंथाव पाया जाता है कि एक कुशल पाठक ही उनके पृथक्-पृथक् सन्दर्भ सूत्रोंको चित्तमें सुरक्षित रख सकता है। लोक-कथाओं व पशु-सम्बन्धी आख्यानोंसे दृष्टान्त ले लिये गये हैं; और पद-पदपर कथाकार मानवीय मानसिक वृत्तिकी गहरी जानकारी प्रकट करता है । कथाका सर्वांग संन्यासको भावनासे व्याप्त है और प्रायः प्रत्येक कथा- नायक अन्त में संसार से विरक्त होकर मुनिदीक्षा ले अपने अगले जीवनको अधिक प्रशस्त बनाने का प्रयत्न करता है ।
श्रावकाचारोंमें भी दृष्टान्तात्मक कथाओंका समावेश पाया जाता है । समन्तभद्र कृत रत्नकरण्डश्रावकाचारमें सम्यक्त्वके निःशंकादि आठ अंगों के दृष्टान्त रूप अंजनचोर, अनन्तमति, उदायन, रेवती, जिनेन्द्रभक्त, For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International