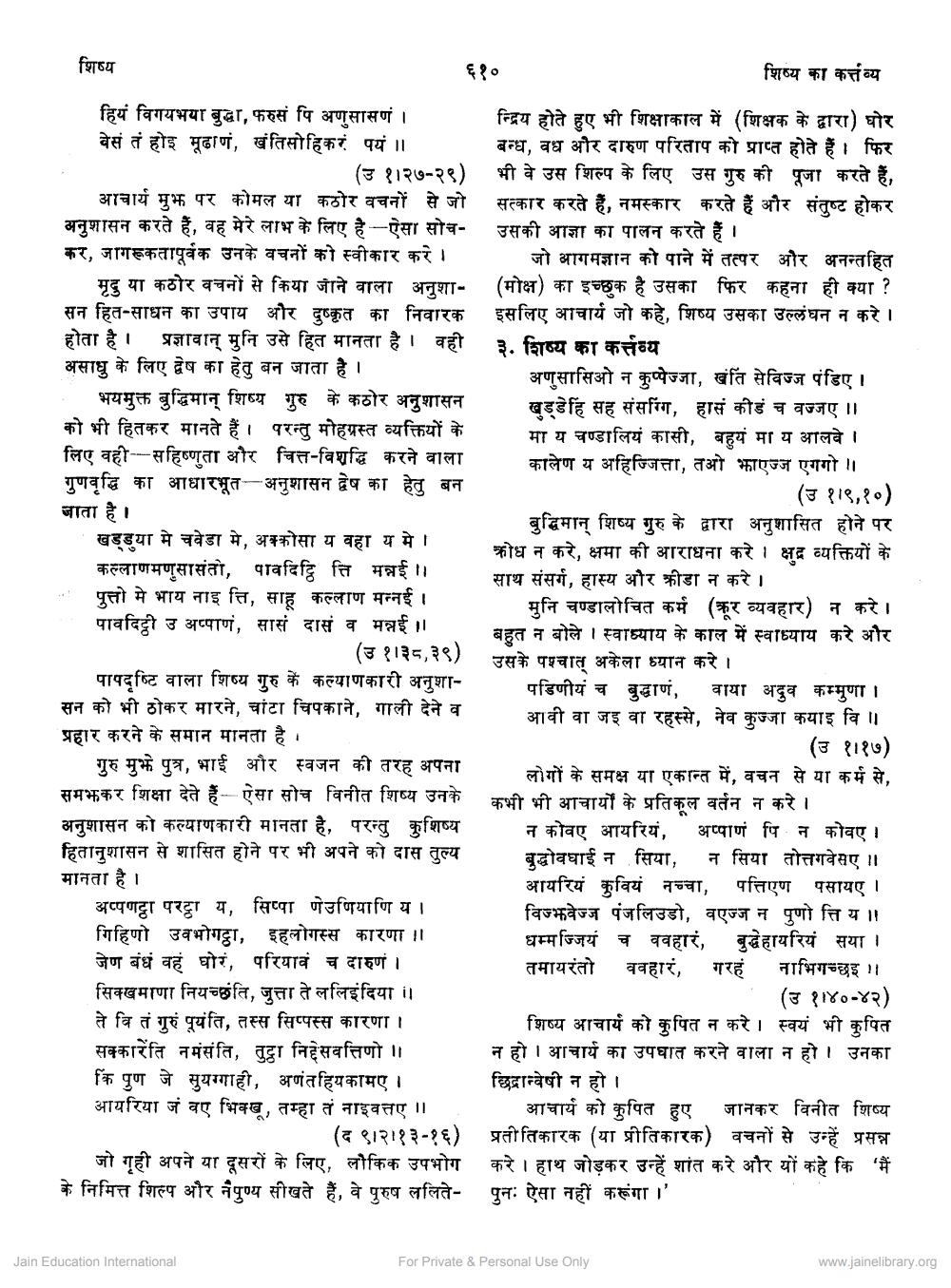________________
शिष्य
६१०
शिष्य का कर्तव्य
हियं विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं । न्द्रिय होते हुए भी शिक्षाकाल में (शिक्षक के द्वारा) घोर वेसं तं होइ मूढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ।।
बन्ध, वध और दारुण परिताप को प्राप्त होते हैं। फिर
(उ १२७-२९) भी वे उस शिल्प के लिए उस गुरु की पूजा करते हैं, आचार्य मुझ पर कोमल या कठोर वचनों से जो सत्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं और संतुष्ट होकर अनुशासन करते हैं, वह मेरे लाभ के लिए है -ऐसा सोच- उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कर, जागरूकतापूर्वक उनके वचनों को स्वीकार करे । जो आगमज्ञान को पाने में तत्पर और अनन्तहित
मृदु या कठोर वचनों से किया जाने वाला अनुशा- (मोक्ष) का इच्छुक है उसका फिर कहना ही क्या ? सन हित-साधन का उपाय और दुष्कृत का निवारक इसलिए आचार्य जो कहे, शिष्य उसका उल्लंघन न करे । होता है। प्रज्ञावान् मुनि उसे हित मानता है। वही ३. शिष्य का कर्तव्य असाधु के लिए द्वेष का हेतु बन जाता है।
अणुसासिओ न कुप्पेज्जा, खंति सेविज्ज पंडिए । ___ भयमुक्त बुद्धिमान् शिष्य गुरु के कठोर अनुशासन
खड्डे हिं सह संसरिंग, हासं कीडं च वज्जए ।। को भी हितकर मानते हैं। परन्तु मोहग्रस्त व्यक्तियों के
मा य चण्डालियं कासी, बहुयं मा य आलवे । लिए वही-सहिष्णुता और चित्त-विशद्धि करने वाला
कालेण य अहिज्जित्ता, तओ झाएज्ज एगगो ।। गुणवृद्धि का आधारभूत-अनुशासन द्वेष का हेतु बन
(उ १।९,१०) जाता है।
बुद्धिमान् शिष्य गुरु के द्वारा अनुशासित होने पर खड्डया मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे।
क्रोध न करे, क्षमा की आराधना करे । क्षद्र व्यक्तियों के कल्लाणमणुसासंतो, पावदिट्ठि त्ति मन्नई।।
साथ संसर्ग, हास्य और क्रीडा न करे। पुत्तो मे भाय नाइ त्ति, साहू कल्लाण मन्नई।
मुनि चण्डालोचित कर्म (कर व्यवहार) न करे । पावदिट्टी उ अप्पाणं, सासं दासं व मन्नई।।
बहत न बोले । स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करे और (उ ११३८,३९)
उसके पश्चात् अकेला ध्यान करे । पापदृष्टि वाला शिष्य गुरु के कल्याणकारी अनुशा- पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अदुव कम्मुणा । सन को भी ठोकर मारने, चांटा चिपकाने, गाली देने व
आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइ वि ।। प्रहार करने के समान मानता है।
(उ १११७) गुरु मुझे पुत्र, भाई और स्वजन की तरह अपना
लोगों के समक्ष या एकान्त में, वचन से या कर्म से, समझकर शिक्षा देते हैं. ऐसा सोच विनीत शिष्य उनके कभी भी आचार्यों के प्रतिकूल वर्तन न करे । अनुशासन को कल्याणकारी मानता है, परन्तु कुशिष्य न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए। हितानुशासन से शासित होने पर भी अपने को दास तुल्य बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए । मानता है।
आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए । अप्पणट्टा परट्ठा य, सिप्पा उणियाणि य । विज्झवेज्ज पंजलिउडो, वएज्ज न पुणो त्ति य ॥ गिहिणो उवभोगट्ठा, इहलोगस्स कारणा ।।
धम्मज्जियं च ववहारं, बुद्धेहायरियं सया । जेण बंधं वहं घोरं, परियावं च दारुणं ।
तमायरंतो ववहारं, गरहं नाभिगच्छइ ।। सिक्खमाणा नियच्छति, जूत्ता ते ललिइंदिया ।।
(उ १६४०-४२) ते वि तं गुरुं पूयंति, तस्स सिप्पस्स कारणा।
शिष्य आचार्य को कुपित न करे। स्वयं भी कुपित सक्कारेंति नमसंति, तुट्टा निद्देसवत्तिणो ।। न हो । आचार्य का उपघात करने वाला न हो। उनका किं पुण जे सुयग्गाही, अणंतहियकामए । छिद्रान्वेषी न हो। आयरिया जं वए भिक्खू, तम्हा तं नाइवत्तए ।।
आचार्य को कुपित हुए जानकर विनीत शिष्य
(द ९।२।१३-१६) प्रतीतिकारक (या प्रीतिकारक) वचनों से उन्हें प्रसन्न जो गही अपने या दूसरों के लिए, लौकिक उपभोग करे । हाथ जोड़कर उन्हें शांत करे और यों कहे कि 'मैं के निमित्त शिल्प और नैपुण्य सीखते हैं, वे पुरुष ललिते- पुनः ऐसा नहीं करूंगा।'
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org