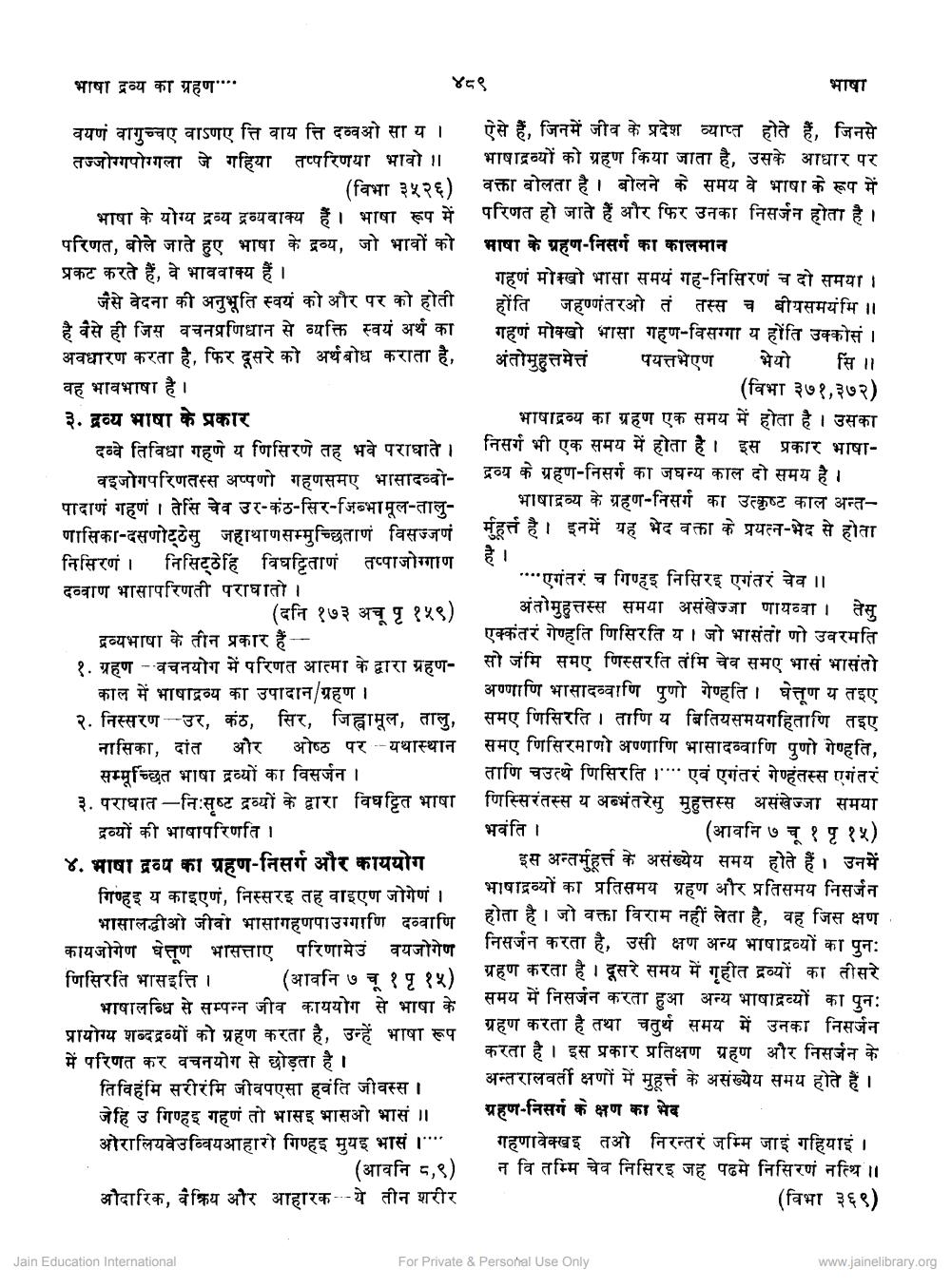________________
भाषा द्रव्य का ग्रहण"
ari वागुच्च वाण त्ति वायत्ति दव्वओ साय । तज्जोग्गपोग्गला जे गहिया तप्परिणया भावो ||
४८९
( विभा ३५२६) भाषा रूप में जो भावों को
भाषा के योग्य द्रव्य द्रव्यवाक्य हैं। परिणत, बोले जाते हुए भाषा के द्रव्य, प्रकट करते हैं, वे भाववाक्य हैं।
जैसे वेदना की अनुभूति स्वयं को और पर को होती है वैसे ही जिस वचनप्रणिधान से व्यक्ति स्वयं अर्थ का अवधारण करता है, फिर दूसरे को अर्थबोध कराता है, वह भावभाषा है ।
३. द्रव्य भाषा के प्रकार
God तिविधा गहणे य णिसिरणे तह भवे पराघाते । वइजोगपरिणतस्स अप्पणो गहणसमए भासादव्वोपादाणं गहणं । तेसिं चेव उर-कंठ-सिर- जिब्भा मूल-तालुणासिका-दसणोट्ठेसु जहाथाणसम्मुच्छिताणं विसज्जणं निसिरणं । निट्ठेिहि विघट्टिताणं तप्पाजोग्गाण दव्वाण भासापरिणती पराघातो ।
(दनि ९७३ अचू पृ १५९) द्रव्यभाषा के तीन प्रकार हैं१. ग्रहण - वचनयोग में परिणत आत्मा के द्वारा ग्रहणकाल में भाषाद्रव्य का उपादान / ग्रहण |
२. निस्सरण -उर, कंठ, सिर, जिह्वामूल, तालु, नासिका, दांत और ओष्ठ पर यथास्थान सम्मूच्छित भाषा द्रव्यों का विसर्जन ।
३. पराघात - निःसृष्ट द्रव्यों के द्वारा विघट्टित भाषा द्रव्यों की भाषापरिणति ।
Jain Education International
४. भाषा द्रव्य का ग्रहण- निसर्ग और काययोग
frogs य काइए, निस्सरइ तह वाइएण जोगेणं । भासालद्धीओ जीवो भासा गहणपा उग्गाणि दव्वाणि कायजोगेण घेत्तूण भासत्ताए परिणामेउं वयजोगेण णिसिरति भासइति । ( आवनि ७ चू १ पृ १५ ) भाषालब्धि से सम्पन्न जीव काययोग से भाषा के प्रायोग्य शब्दद्रव्यों को ग्रहण करता है, उन्हें भाषा रूप में परिणत कर वचनयोग से छोड़ता है ।
तिविहमि सरीरंमि जीवपएसा हवंति जीवस्स । जेहि उ गिण्हइ गहणं तो भासइ भासओ भासं ॥ ओरालियवेउब्वियआहारो गिण्हइ मुयइ भासं ।''''' ( आवनि ८, ९ ) औदारिक, वैक्रिय और आहारक- ये तीन शरीर
भाषा
ऐसे हैं, जिनमें जीव के प्रदेश व्याप्त होते हैं, जिनसे भाषाद्रव्यों को ग्रहण किया जाता है, उसके आधार पर वक्ता बोलता है। बोलने के समय वे भाषा के रूप में परिणत हो जाते हैं और फिर उनका निसर्जन होता है । भाषा के ग्रहण निसर्ग का कालमान
गहणं मोक्खो भासा समयं गह-निसिरणं च दो समया । होंति जहणंतरओ तं तस्स च बीयसमयंमि ॥ गहणं मोक्खो भासा गहण - विसग्गा य होंति उक्कोसं । अंतमुत्तमेत्तं पयत्तभेएण भेयो सिं ॥ ( विभा ३७१, ३७२ )
भाषाद्रव्य का ग्रहण एक समय में होता है । उसका निसर्ग भी एक समय में होता है । इस प्रकार भाषाद्रव्य के ग्रहण - निसर्ग का जघन्य काल दो समय है ।
भाषाद्रव्य के ग्रहण निसर्ग का उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। इनमें यह भेद वक्ता के प्रयत्न-भेद से होता है ।
..... एगंतरं च गिण्हइ निसिरइ एगंतरं चेव ||
अंतोमुहुत्तस्स समया असंखेज्जा णायव्वा । तेसु एक्कंतरं गेहति णिसिरति य । जो भासतो णो उवरमति सो जंमि समए णिस्सरति तंमि चेव समए भासं भासतो अण्णाणि भासाव्वाणि पुणो गेण्हति । घेत्तूण य तइए समए णिसिरति । ताणि य बितियसमयगहिताणि तइए समए णिसिरमाणो अण्णाणि भासादव्वाणि पुणो गेहति, ताणि उत्थे णिसिरति । एवं एगंतरं गेव्हंतस्स एगंतरं णिस्सिरतस्स य अब्भं तरेसु मुहुत्तस्स असंखेज्जा समया भवंति ।
( आवनि ७ चू १ पृ १५ ) अन्तर्मुहूर्त के असंख्येय समय होते हैं । उनमें भाषाद्रव्यों का प्रतिसमय ग्रहण और प्रतिसमय निसर्जन होता है । जो वक्ता विराम नहीं लेता है, वह जिस क्षण निसर्जन करता है, उसी क्षण अन्य भाषाद्रव्यों का पुनः ग्रहण करता है । दूसरे समय में गृहीत द्रव्यों का तीसरे समय में निसर्जन करता हुआ अन्य भाषाद्रव्यों का पुनः ग्रहण करता है तथा चतुर्थ समय में उनका निसर्जन करता है । इस प्रकार प्रतिक्षण ग्रहण और निसर्जन के अन्तरालवर्ती क्षणों में मुहूर्त्त के असंख्येय समय होते हैं । ग्रहण- निसर्ग के क्षण का भेद
गहणावेक्खइ तओ निरन्तरं जम्मि जाई गहियाई । न वितम्मि चेव निसिरइ जह पढमे निसिरणं नत्थि ॥ ( विभा ३६९ )
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org