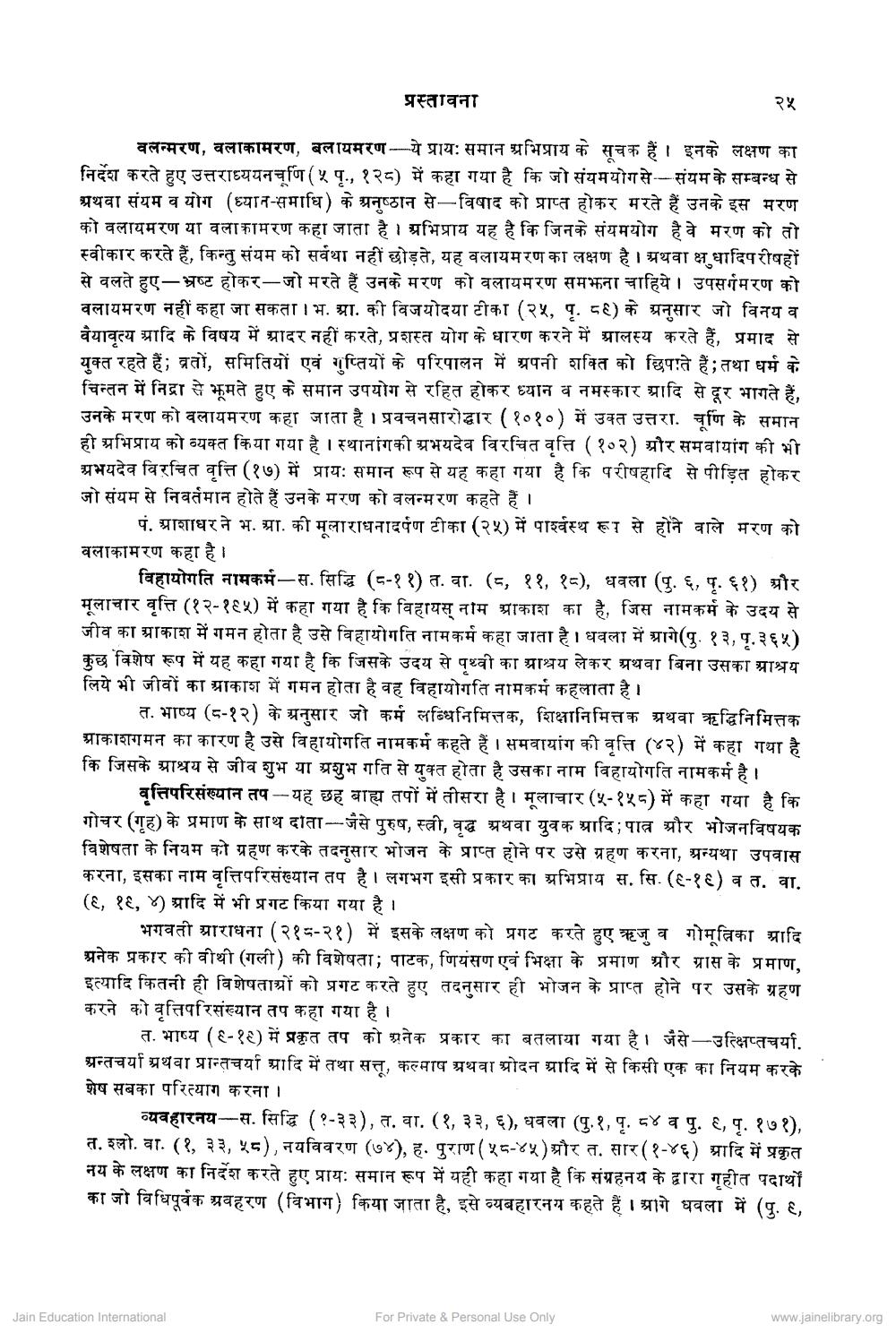________________
प्रस्तावना
वलन्मरण, वलाकामरण, बलायमरण - ये प्राय: समान अभिप्राय के सूचक हैं। इनके लक्षण का निर्देश करते हुए उत्तराध्ययनचूर्णि ( ५ पृ. १२८) में कहा गया है कि जो संयमयोग से - संयम के सम्बन्ध अथवा संयम व योग (ध्यान-समाधि) के अनुष्ठान से - विषाद को प्राप्त होकर मरते हैं उनके इस मरण को वलायमरण या वलाकामरण कहा जाता है । अभिप्राय यह है कि जिनके संयमयोग है वे मरण को तो स्वीकार करते हैं, किन्तु संयम को सर्वथा नहीं छोड़ते, यह वलायमरण का लक्षण है । अथवा क्षुधादिपरीषहों से वलते हुए - भ्रष्ट होकर – जो मरते हैं उनके मरण को वलायमरण समझना चाहिये । उपसर्गमरण को वलायमरण नहीं कहा जा सकता । भ. आ. की विजयोदया टीका (२५, पृ. ८६ ) के अनुसार जो विनय व वैयावृत्य आदि के विषय में आदर नहीं करते, प्रशस्त योग के धारण करने में आलस्य करते हैं, प्रमाद से युक्त रहते हैं; व्रतों समितियों एवं गुप्तियों के परिपालन में अपनी शक्ति को छिपाते हैं; तथा धर्म के चिन्तन में निद्रा से झूमते हुए के समान उपयोग से रहित होकर ध्यान व नमस्कार आदि से दूर भागते हैं, उनके मरण को वलायमरण कहा जाता है । प्रवचनसारोद्धार (१०१०) में उक्त उत्तरा चूर्णि के समान
२५
भिप्राय को व्यक्त किया गया है । स्थानांग की अभयदेव विरचित वृत्ति (१०२) और समवायांग की भी अभयदेव विरचित वृत्ति (१७) में प्राय: समान रूप से यह कहा गया है कि परीषहादि से पीड़ित होकर जो संयम से निवर्तमान होते हैं उनके मरण को वलन्मरण कहते हैं ।
पं. आशाधर ने भ. प्रा. की मूलाराधनादर्पण टीका (२५) में पार्श्वस्थ रूप से होने वाले मरण को वलाकामरण कहा है।
विहायोगति नामकर्म - स. सिद्धि ( ८-११) त. वा. (८, ११, १८ ), धवला (पु. ६, पृ. ६१) और मूलाचार वृत्ति (१२-१६५) में कहा गया है कि विहायस् नाम श्राकाश का है, जिस नामकर्म के उदय से जीव का आकाश में गमन होता है उसे विहायोगति नामकर्म कहा जाता है । धवला में प्रागे (पु. १३, पृ. ३६५ ) कुछ विशेष रूप में यह कहा गया है कि जिसके उदय से पृथ्वी का आश्रय लेकर अथवा बिना उसका प्राश्रय लिये भी जीवों का आकाश में गमन होता है वह विहायोगति नामकर्म कहलाता है ।
त. भाष्य (८-१२ ) के अनुसार जो कर्म लब्धिनिमित्तक, शिक्षानिमित्तक अथवा ऋद्धिनिमित्तक आकाशगमन का कारण है उसे विहायोगति नामकर्म कहते हैं । समवायांग की वृत्ति (४२) में कहा गया है कि जिसके आश्रय से जीव शुभ या अशुभ गति से युक्त होता है उसका नाम विहायोगति नामकर्म है ।
वृत्तिपरिसंख्यान तप – यह छह बाह्य तपों में तीसरा है । मूलाचार ( ५- १५८) में कहा गया है कि गोचर (गृह) के प्रमाण के साथ दाता - जैसे पुरुष, स्त्री, वृद्ध अथवा युवक आदि; पात्र और भोजनविषयक विशेषता के नियम को ग्रहण करके तदनुसार भोजन के प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करना, अन्यथा उपवास करना, इसका नाम वृत्तिपरिसंख्यान तप है । लगभग इसी प्रकार का अभिप्राय स. सि. (६-१६) व त. वा. (६, १६, ४) आदि में भी प्रगट किया गया है ।
भगवती आराधना ( २१ - २१ ) में इसके लक्षण को प्रगट करते हुए ऋजु व गोमूत्रिका आदि अनेक प्रकार की वीथी (गली) की विशेषता; पाटक, णियंसण एवं भिक्षा के प्रमाण और ग्रास के प्रमाण, इत्यादि कितनी ही विशेषताओं को प्रगट करते हुए तदनुसार ही भोजन के प्राप्त होने पर उसके ग्रहण करने को वृत्तिपरिसंख्यान तप कहा गया है ।
त. भाष्य ( ६-१६) में प्रकृत तप को अनेक प्रकार का बतलाया गया । जैसे—उत्क्षिप्तचर्या. श्रन्तचर्या अथवा प्रान्तचर्या आदि में तथा सत्तू, कल्माष अथवा श्रोदन यादि में से किसी एक का नियम करके शेष सबका परित्याग करना ।
Jain Education International
व्यवहारनय - स. सिद्धि (१३३), त. वा. (१, ३३, ६), धवला (पु. १, पृ. ८४ व पु. ६, पृ. १७१), त. इलो. वा. (१, ३३, ५८), नयविवरण (७४), ह. पुराण ( ५८-४५ ) और त. सार (१-४६ ) आदि में प्रकृत नय के लक्षण का निर्देश करते हुए प्रायः समान रूप में यही कहा गया है कि संग्रहनय के द्वारा गृहीत पदार्थों का जो विधिपूर्वक प्रवहरण ( विभाग ) किया जाता है, इसे व्यबहारनय कहते हैं। आगे धवला में (पु. ६,
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org