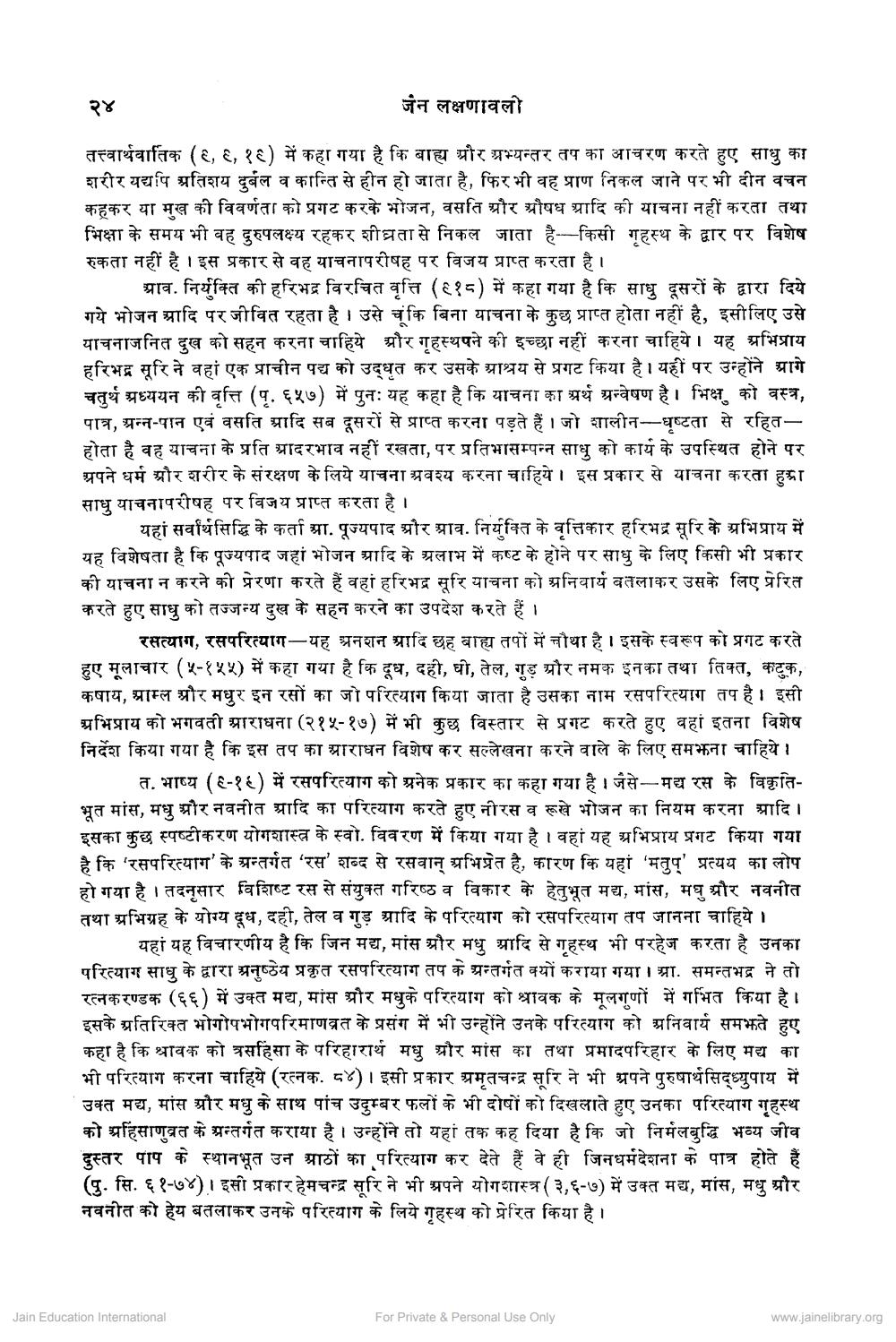________________
२४
जन लक्षणावली
तत्त्वार्थवार्तिक (8, ६, १६) में कहा गया है कि बाह्य और अभ्यन्तर तप का आचरण करते हुए साधु का शरीर यद्यपि अतिशय दुर्बल व कान्ति से हीन हो जाता है, फिर भी वह प्राण निकल जाने पर भी दीन वचन
मा मख की विवर्णता को प्रगट करके भोजन, वसति और औषध ग्रादि की याचना नहीं करता तथा भिक्षा के समय भी वह दुरुपलक्ष्य रहकर शीघ्रता से निकल जाता है--किसी गृहस्थ के द्वार पर विशेष रुकता नहीं है । इस प्रकार से वह याचनापरीषह पर विजय प्राप्त करता है।
आव. नियुक्ति की हरिभद्र विरचित वृत्ति (६१८) में कहा गया है कि साधु दूसरों के द्वारा दिये गये भोजन आदि पर जीवित रहता है । उसे चूंकि बिना याचना के कुछ प्राप्त होता नहीं है, इसीलिए उसे याचनाजनित दुख को सहन करना चाहिये और गृहस्थपने की इच्छा नहीं करना चाहिये। यह अभिप्राय हरिभद्र सूरि ने वहां एक प्राचीन पद्य को उद्धत कर उसके आश्रय से प्रगट किया है। यहीं पर उन्होंने आगे चतुर्थ अध्ययन की वृत्ति (प. ६५७) में पुनः यह कहा है कि याचना का अर्थ अन्वेषण है। भिक्ष को वस्त्र, पात्र, अन्न-पान एवं वसति आदि सब दूसरों से प्राप्त करना पड़ते हैं । जो शालीन-धृष्टता से रहितहोता है वह याचना के प्रति आदरभाव नहीं रखता, पर प्रतिभासम्पन्न साधु को कार्य के उपस्थित होने पर अपने धर्म और शरीर के संरक्षण के लिये याचना अवश्य करना चाहिये। इस प्रकार से याचना करता हुआ साधु याचनापरीषह पर विजय प्राप्त करता है।
___ यहां सर्वार्थसिद्धि के कर्ता आ. पूज्यपाद और प्राव. नियुक्ति के वृत्तिकार हरिभद्र सूरि के अभिप्राय में यह विशेषता है कि पूज्यपाद जहां भोजन आदि के अलाभ में कष्ट के होने पर साधु के लिए किसी भी प्रकार की याचना न करने की प्रेरणा करते हैं वहां हरिभद्र सुरि याचना को अनिवार्य बतलाकर उसके लिए प्रेरित करते हुए साधु को तज्जन्य दुख के सहन करने का उपदेश करते हैं।
रसत्याग, रसपरित्याग-यह अनशन आदि छह बाह्य तपों में नौथा है । इसके स्वरूप को प्रगट करते हुए मूलाचार (५-१५५) में कहा गया है कि दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और नमक इनका तथा तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर इन रसों का जो परित्याग किया जाता है उसका नाम रसपरित्याग तप है। इसी अभिप्राय को भगवती आराधना (२१५-१७) में भी कुछ विस्तार से प्रगट करते हुए वहां इतना विशेष निर्देश किया गया है कि इस तप का पाराधन विशेष कर सल्लेखना करने वाले के लिए समझना चाहिये।
त. भाष्य (8-१६) में रसपरित्याग को अनेक प्रकार का कहा गया है। जैसे-मद्य रस के विकृतिभूत मांस, मधु और नवनीत आदि का परित्याग करते हुए नीरस व रूखे भोजन का नियम करना आदि । इसका कुछ स्पष्टीकरण योगशास्त्र के स्वो. विवरण में किया गया है। वहां यह अभिप्राय प्रगट किया गया है कि 'रसपरित्याग' के अन्तर्गत 'रस' शब्द से रसवान् अभिप्रेत है, कारण कि यहां 'मतुप' प्रत्यय का लोप हो गया है। तदनुसार विशिष्ट रस से संयुक्त गरिष्ठ व विकार के हेतुभूत मद्य, मांस, मघु और नवनीत तथा अभिग्रह के योग्य दूध, दही, तेल व गुड़ आदि के परित्याग को रसपरित्याग तप जानना चाहिये।
यहां यह विचारणीय है कि जिन मद्य, मांस और मधु आदि से गहस्थ भी परहेज करता है उनका परित्याग साधु के द्वारा अनुष्ठेय प्रकृत रसपरित्याग तप के अन्तर्गत क्यों कराया गया। प्रा. समन्तभद्र ने तो रत्नकरण्डक (६६) में उक्त मद्य, मांस और मधुके परित्याग को श्रावक के मूलगणों में गभित किया है। इसके अतिरिक्त भोगोपभोगपरिमाणवत के प्रसंग में भी उन्होंने उनके परित्याग को अनिवार्य समझते हुए कहा है कि श्रावक को त्रसहिंसा के परिहारार्थ मधु और मांस का तथा प्रमादपरिहार के लिए मद्य का भी परित्याग करना चाहिये (रत्नक. ८४)। इसी प्रकार अमृतचन्द्र सूरि ने भी अपने पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में उक्त मद्य, मांस और मधु के साथ पांच उदुम्बर फलों के भी दोषों को दिखलाते हुए उनका परित्याग गृहस्थ को अहिंसाणुव्रत के अन्तर्गत कराया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जो निर्मलबुद्धि भव्य जीव दुस्तर पाप के स्थानभूत उन आठों का परित्याग कर देते हैं वे ही जिनधर्मदेशना के पात्र होते हैं (पु. सि. ६१-७४)। इसी प्रकार हेमचन्द्र सूरि ने भी अपने योगशास्त्र (३,६-७) में उक्त मद्य, मांस, मधु और नवनीत को हेय बतलाकर उनके परित्याग के लिये गृहस्थ को प्रेरित किया है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org