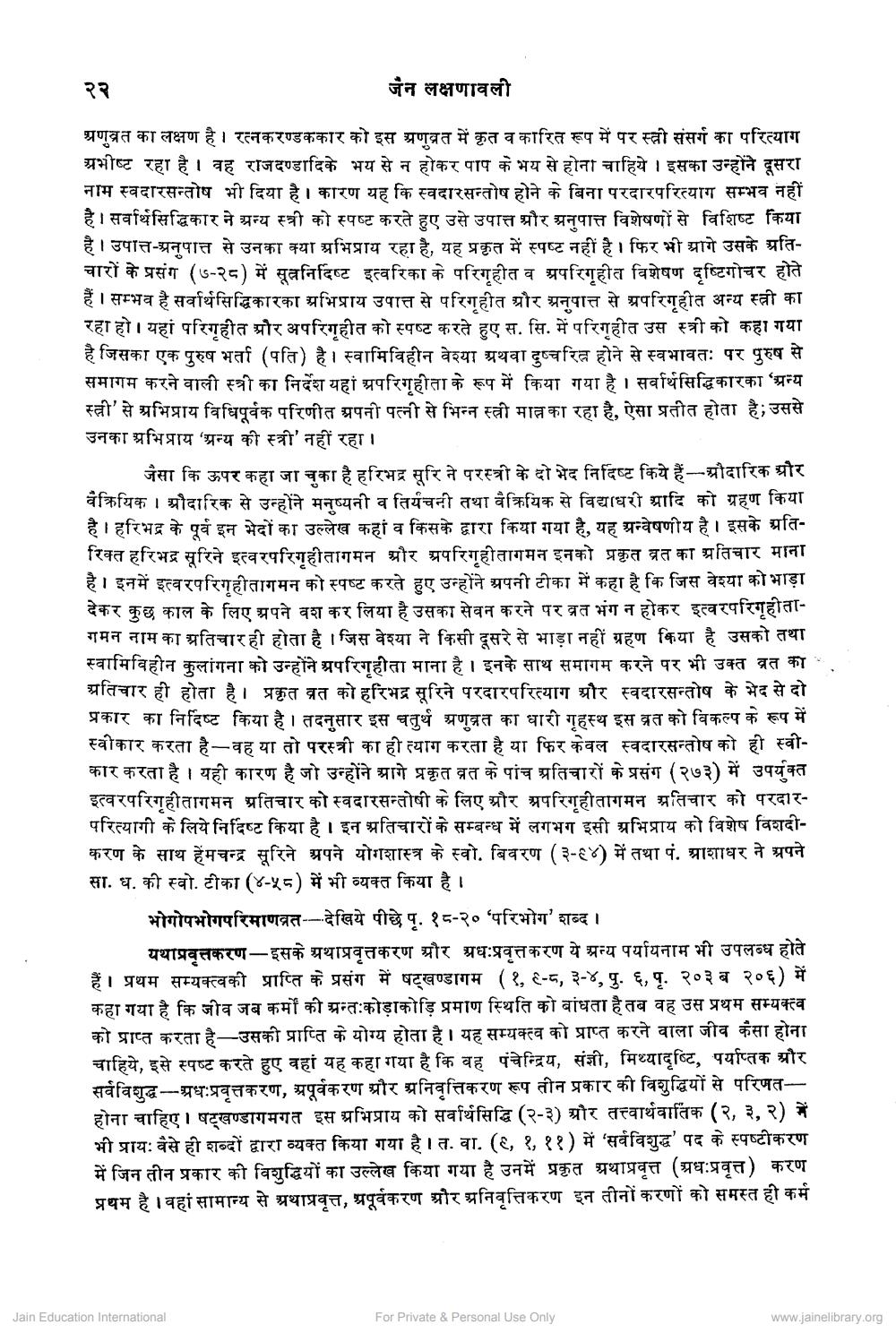________________
२२
जैन लक्षणावली
अणुव्रत का लक्षण है। रत्नकरण्डककार को इस अणुव्रत में कृत व कारित रूप में पर स्त्री संसर्ग का परित्याग अभीष्ट रहा है। वह राजदण्डादिके भय से न होकर पाप के भय से होना चाहिये । इसका उन्होंने दूसरा नाम स्वदारसन्तोष भी दिया है। कारण यह कि स्वदारसन्तोष होने के बिना परदारपरित्याग सम्भव नहीं है। सर्वार्थसिद्धिकार ने अन्य स्त्री को स्पष्ट करते हुए उसे उपात्त और अनुपात्त विशेषणों से विशिष्ट किया है। उपात्त-अनुपात्त से उनका क्या अभिप्राय रहा है, यह प्रकृत में स्पष्ट नहीं है। फिर भी पागे उसके अतिचारों के प्रसंग (७-२८) में सूत्रनिर्दिष्ट इत्वरिका के परिगहीत व अपरिगहीत विशेषण दष्टिगोचर होते हैं । सम्भव है सर्वार्थसिद्धिकारका अभिप्राय उपात्त से परिगृहीत और अनुपात्त से अपरिगृहीत अन्य स्त्री का रहा हो । यहां परिगृहीत और अपरिगृहीत को स्पष्ट करते हुए स. सि. में परिगृहीत उस स्त्री को कहा गया है जिसका एक पुरुष भर्ता (पति) है। स्वामिविहीन वेश्या अथवा दुष्चरित्न होने से स्वभावतः पर पुरुष से समागम करने वाली स्त्री का निर्देश यहां अपरिगृहीता के रूप में किया गया है। सर्वार्थसिद्धिकारका 'अन्य स्त्री' से अभिप्राय विधिपूर्वक परिणीत अपनी पत्नी से भिन्न स्त्री मान का रहा है, ऐसा प्रतीत होता है; उससे उनका अभिप्राय 'अन्य की स्त्री' नहीं रहा।
जैसा कि ऊपर कहा जा चका है हरिभद्र सूरि ने परस्त्री के दो भेद निदिष्ट किये हैं--प्रौदारिक और वक्रियिक । औदारिक से उन्होंने मनष्यनी व तियंचनी तथा वैक्रियिक से विद्याधरी आदि को ग्रहण किया है। हरिभद्र के पूर्व इन भेदों का उल्लेख कहां व किसके द्वारा किया गया है, यह अन्वेषणीय है। इसके अतिरिक्त हरिभद्र सूरिने इत्वरपरिगृहीतागमन और अपरिगृहीतागमन इनको प्रकृत व्रत का अतिचार माना है। इनमें इत्वरपरिगृहीतागमन को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपनी टीका में कहा है कि जिस वेश्या को भाड़ा देकर कुछ काल के लिए अपने वश कर लिया है उसका सेवन करने पर व्रत भंग न होकर इत्वरपरिगृहीतागमन नाम का अतिचारही होता है । जिस वेश्या ने किसी दूसरे से भाड़ा नहीं ग्रहण किया है उसको तथा स्वामिविहीन कुलांगना को उन्होंने अपरिगृहीता माना है । इनके अतिचार ही होता है। प्रकृत व्रत को हरिभद्र सूरिने परदारपरित्याग और स्वदारसन्तोष के भेद से दो प्रकार का निर्दिष्ट किया है। तदनुसार इस चतुर्थ अणुव्रत का धारी गृहस्थ इस व्रत को विकल्प के रूप में स्वीकार करता है-वह या तो परस्त्री का ही त्याग करता है या फिर केवल स्वदारसन्तोष को ही स्वीकार करता है। यही कारण है जो उन्होंने आगे प्रकृत व्रत के पांच अतिचारों के प्रसंग (२७३) में उपर्युक्त इत्वरपरिगृहीतागमन अतिचार को स्वदारसन्तोषी के लिए और अपरिगहीतागमन अतिचार को परदारपरित्यागी के लिये निर्दिष्ट किया है । इन अतिचारों के सम्बन्ध में लगभग इसी अभिप्राय को विशेष विशदीकरण के साथ हेमचन्द्र सूरिने अपने योगशास्त्र के स्वो. बिवरण (३-६४) में तथा पं. प्राशाधर ने अपने सा. ध. की स्वो. टीका (४-५८) में भी व्यक्त किया है।
भोगोपभोगपरिमाणव्रत-देखिये पीछे पृ. १८-२० 'परिभोग' शब्द।
यथाप्रवृत्तकरण-इसके अथाप्रवृत्तकरण और अधःप्रवृत्त करण ये अन्य पर्यायनाम भी उपलब्ध होते हैं। प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति के प्रसंग में षट्खण्डागम (१, ६-८, ३-४, पु. ६, पृ. २०३ ब २०६) में कहा गया है कि जीव जब कर्मों की अन्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थिति को बांधता है तब वह उस प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उसकी प्राप्ति के योग्य होता है। यह सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव कैसा होना चाहिये, इसे स्पष्ट करते हुए वहां यह कहा गया है कि वह पंचेन्द्रिय, संजी, मिथ्यादृष्टि, पर्याप्तक और सर्वविशुद्ध-अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप तीन प्रकार की विशुद्धियों से परिणतहोना चाहिए। षट्खण्डागमगत इस अभिप्राय को सर्वार्थसिद्धि (२-३) और तत्त्वार्थवार्तिक (२, ३,२) में भी प्रायः वैसे ही शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। त. वा. (९, १, ११) में 'सर्वविशुद्ध' पद के स्पष्टीकरण में जिन तीन प्रकार की विशुद्धियों का उल्लेख किया गया है उनमें प्रकृत प्रथाप्रवृत्त (अधःप्रवृत्त) करण प्रथम है । वहां सामान्य से अथाप्रवृत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणों को समस्त ही कर्म
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org