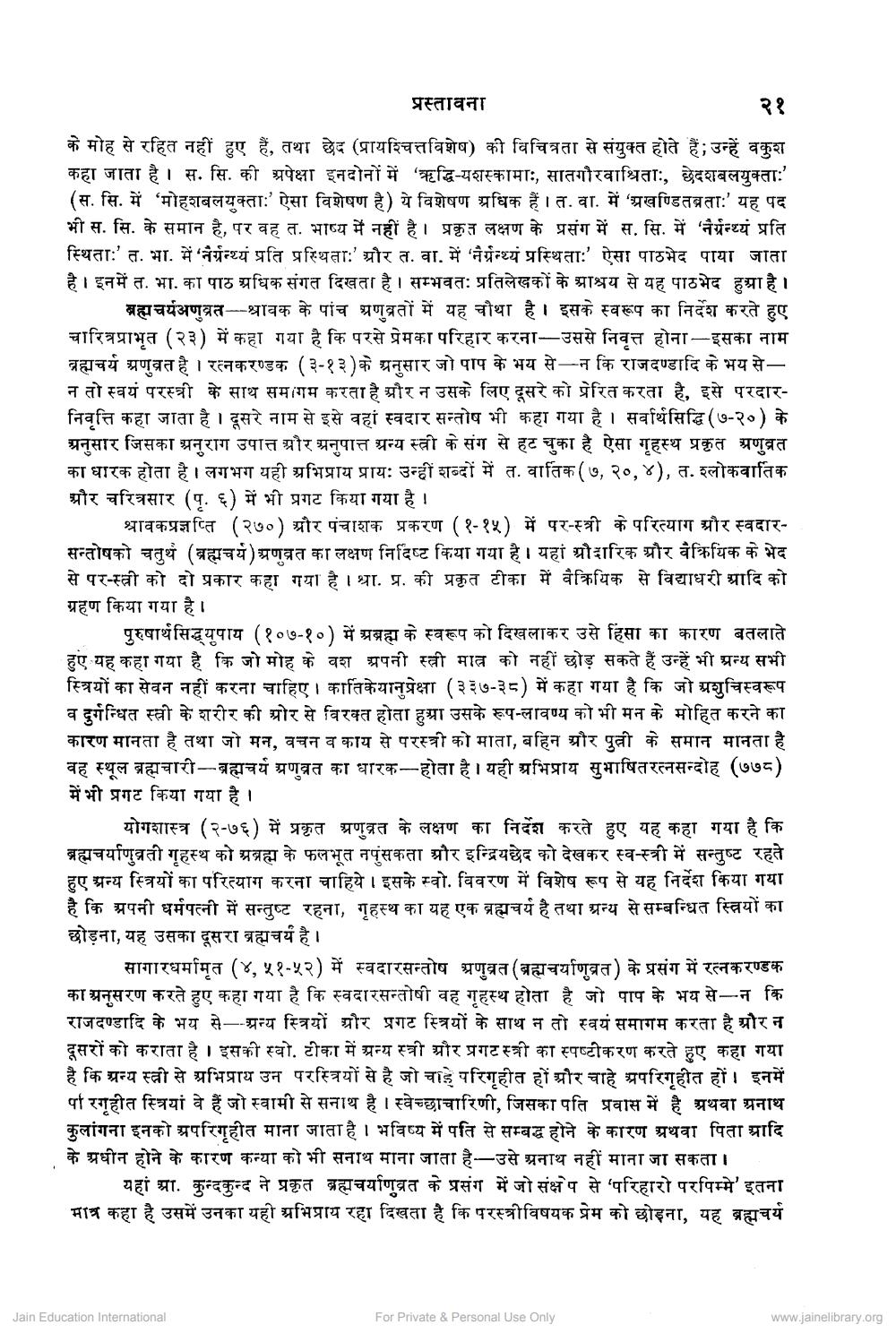________________
प्रस्तावना
२१
के मोह से रहित नहीं हुए हैं, तथा छेद (प्रायश्चित्तविशेष) की विचित्रता से संयुक्त होते हैं। उन्हें वकुश कहा जाता है। स. सि. की अपेक्षा इनदोनों में 'ऋद्धि-यशस्कामाः, सातगौरवाश्रिताः, छेदशबलयुक्ताः' (स. सि. में 'मोहशबलयुक्ताः ' ऐसा विशेषण है) ये विशेषण अधिक हैं। त. वा. में 'अखण्डितब्रताः' यह पद भी स. सि. के समान है, पर वह त. भाष्य में नहीं है। प्रकृत लक्षण के प्रसंग में स. सि. में 'नैर्ग्रन्थ्यं प्रति स्थिताः' त. भा. में 'नर्ग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिता:' और त. वा. में 'नैन्थ्यं प्रस्थिता:' ऐसा पाठभेद पाया जाता है। इनमें त. भा. का पाठ अधिक संगत दिखता है । सम्भवतः प्रतिलेखकों के आश्रय से यह पाठभेद हुआ है।
ब्रह्मचर्यअणुव्रत-श्रावक के पांच अणुव्रतों में यह चौथा है। इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए चारित्रप्राभृत (२३) में कहा गया है कि परसे प्रेमका परिहार करना-उससे निवृत्त होना-इसका नाम ब्रह्मचर्य अणुवत है । रत्नकरण्डक (३-१३) के अनुसार जो पाप के भय से-न कि राजदण्डादि के भय सेन तो स्वयं परस्त्री के साथ समागम करता है और न उसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, इसे परदारनिवृत्ति कहा जाता है। दूसरे नाम से इसे वहां स्वदार सन्तोष भी कहा गया है। सर्वार्थसिद्धि (७-२०) के अनुसार जिसका अनुराग उपात्त और अनुपात्त अन्य स्त्री के संग से हट चुका है ऐसा गृहस्थ प्रकृत अणुव्रत का धारक होता है। लगभग यही अभिप्राय प्रायः उन्हीं शब्दों में त. वार्तिक (७, २०,४), त. श्लोकवार्तिक और चरित्रसार (प. ६) में भी प्रगट किया गया है ।
श्रावकप्रज्ञप्ति (२७०) और पंचाशक प्रकरण (१-१५) में पर-स्त्री के परित्याग और स्वदारसन्तोषको चतुर्थ (ब्रह्मचर्य)अणवत का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है। यहां औदारिक और वैक्रियिक के भेद से पर-स्त्री को दो प्रकार कहा गया है। श्रा. प्र. की प्रकृत टीका में वैक्रियिक से विद्याधरी आदि को ग्रहण किया गया है।
पुरुषार्थसिद्ध्यपाय (१०७-१०) में अब्रह्म के स्वरूप को दिखलाकर उसे हिंसा का कारण बतलाते हुए यह कहा गया है कि जो मोह के वश अपनी स्त्री मात्र को नहीं छोड़ सकते हैं उन्हें भी अन्य सभी स्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिकेयानुप्रेक्षा (३३७-३८) में कहा गया है कि जो अशुचिस्वरूप व दुर्गन्धित स्त्री के शरीर की ओर से विरक्त होता हया उसके रूप-लावण्य को भी मन के मोहित करने का कारण मानता है तथा जो मन, वचन व काय से परस्त्री को माता, बहिन और पुत्री के समान मानता है वह स्थूल ब्रह्मचारी-ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारक होता है। यही अभिप्राय सुभाषितरत्नसन्दोह (७७८) में भी प्रगट किया गया है।
योगशास्त्र (२-७६) में प्रकृत अणुव्रत के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि ब्रह्मचर्याणुव्रती गृहस्थ को अब्रह्म के फलभूत नपुंसकता और इन्द्रियछेद को देखकर स्व-स्त्री में सन्तुष्ट रहते
अन्य स्त्रियों का परित्याग करना चाहिये । इसके स्वो. विवरण में विशेष रूप से यह निर्देश किया गया है कि अपनी धर्मपत्नी में सन्तुष्ट रहना, गृहस्थ का यह एक ब्रह्मचर्य है तथा अन्य से सम्बन्धित स्त्रियों का छोड़ना, यह उसका दूसरा ब्रह्मचर्य है।
सागारधर्मामृत (४, ५१-५२) में स्वदारसन्तोष अणुव्रत (ब्रह्मचर्याणुव्रत) के प्रसंग में रत्नकरण्डक का अनुसरण करते हुए कहा गया है कि स्वदारसन्तोषी वह गृहस्थ होता है जो पाप के भय से-न कि राजदण्डादि के भय से--अन्य स्त्रियों और प्रगट स्त्रियों के साथ न तो स्वयं समागम करता है और न दूसरों को कराता है । इसकी स्वो. टीका में अन्य स्त्री और प्रगट स्त्री का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि अन्य स्त्री से अभिप्राय उन परस्त्रियों से है जो चाई परिगृहीत हों और चाहे अपरिगृहीत हों। इनमें पा रगृहीत स्त्रियां वे हैं जो स्वामी से सनाथ है । स्वेच्छाचारिणी, जिसका पति प्रवास में है अथवा अनाथ कुलांगना इनको अपरिगहीत माना जाता है । भविष्य में पति से सम्बद्ध होने के कारण अथवा पिता आदि के अधीन होने के कारण कन्या को भी सनाथ माना जाता है-उसे अनाथ नहीं माना जा सकता।
यहां प्रा. कुन्दकुन्द ने प्रकृत ब्रह्मचर्याणुव्रत के प्रसंग में जो संक्षेप से 'परिहारो परपिम्मे' इतना मात्र कहा है उसमें उनका यही अभिप्राय रहा दिखता है कि परस्त्रीविषयक प्रेम को छोड़ना, यह ब्रह्मचर्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org