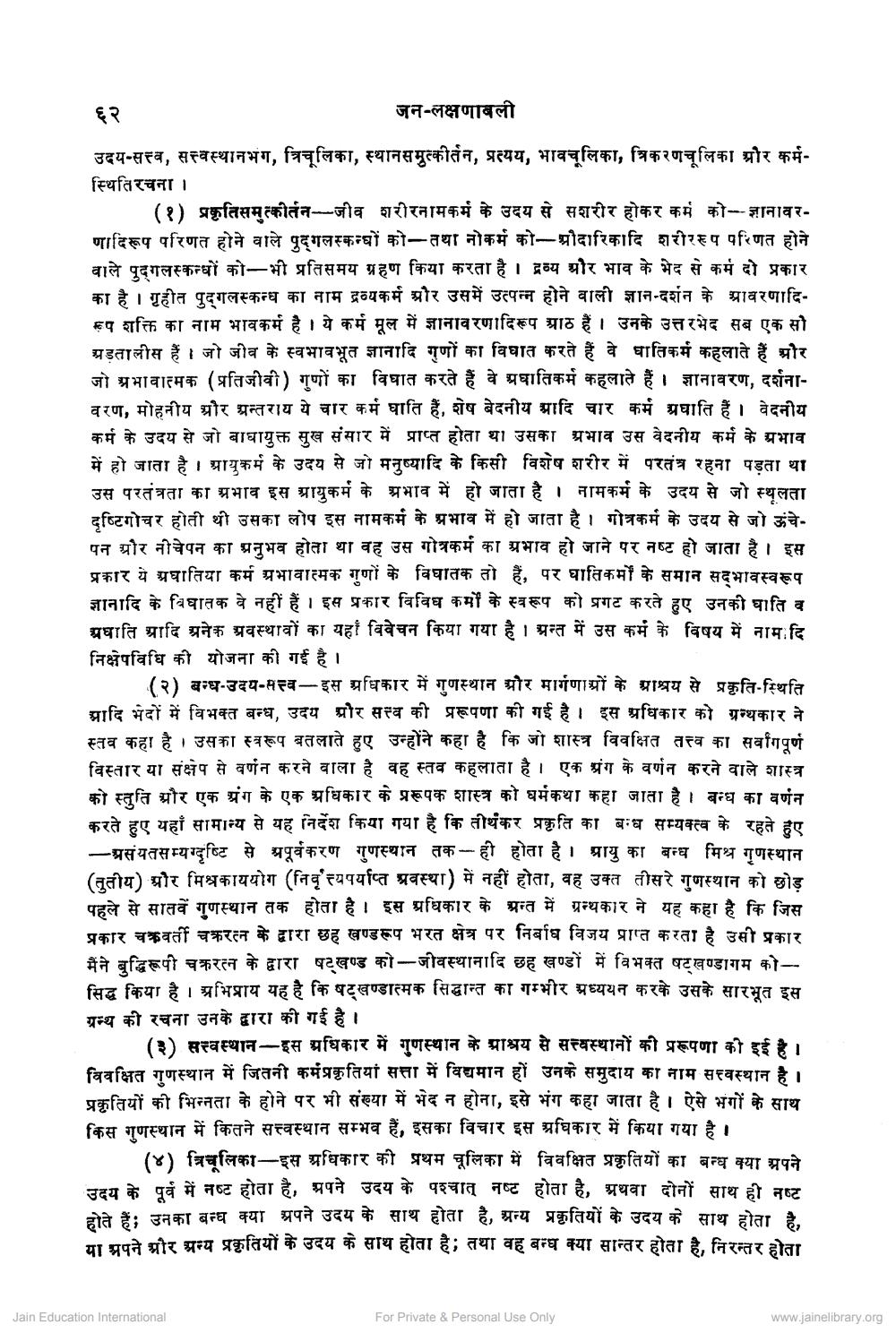________________
६२
जन-लक्षणाबली उदय-सत्त्व, सत्त्वस्थानभंग, त्रिचूलिका, स्थानसमुत्कीर्तन, प्रत्यय, भावचूलिका, त्रिकरणचूलिका और कर्मस्थिति रचना।
(१) प्रकृतिसमुत्कीर्तन-जीव शरीरनामकर्म के उदय से सशरीर होकर कर्म को-ज्ञानावरणादिरूप परिणत होने वाले पूदगलस्कन्धों को-तथा नोकर्म को-प्रौदारिकादि शरीररूप परिणत होने वाले पूदगलस्कन्धों को भी प्रतिसमय ग्रहण किया करता है । द्रव्य और भाव के भेद से कर्म दो प्रकार का है । गृहीत पुद्गलस्कन्ध का नाम द्रव्यकर्म और उसमें उत्पन्न होने वाली ज्ञान-दर्शन के प्रावरणादि
प शक्ति का नाम भावकर्म है। ये कर्म मूल में ज्ञानावरणादिरूप पाठ हैं। उनके उत्तरभेद सब एक सौ अडतालीस हैं। जो जीव के स्वभावभूत ज्ञानादि गणों का विधात करते हैं वे घातिकर्म कहलाते हैं । जो अभावात्मक (प्रतिजीवी) गुणों का विघात करते हैं वे अघातिकर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण. मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घाति हैं. शेष बेदनीय आदि चार कर्म अघाति हैं। वेटनी कर्म के उदय से जो बाघायुक्त सुख संसार में प्राप्त होता था उसका प्रभाव उस वेदनीय कर्म के प्रभाव में हो जाता है। प्रायुकर्म के उदय से जो मनुष्यादि के किसी विशेष शरीर में परतंत्र रहना पड़ता था उस परतंत्रता का प्रभाव इस प्रायुकर्म के अभाव में हो जाता है । नामकर्म के उदय से जो स्थलता दष्टिगोचर होती थी उसका लोप इस नामकर्म के प्रभाव में हो जाता है। गोत्रकर्म के उदय से जो ऊंचेपन और नीचेपन का अनुभव होता था वह उस गोत्रकर्म का प्रभाव हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये अघातिया कर्म अभावात्मक गुणों के विघातक तो हैं, पर घातिकर्मों के समान सदभावस्वरूप ज्ञानादि के विघातक वे नहीं हैं । इस प्रकार विविध कर्मों के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनकी घाति व प्रघाति आदि अनेक अवस्थावों का यहाँ विवेचन किया गया है। अन्त में उस कर्म के विषय में नाम दि निक्षेपविधि की योजना की गई है।
(२) बन्ध-उदय-सत्त्व- इस अधिकार में गुणस्थान और मार्गणाओं के प्राश्रय से प्रकृति-स्थिति आदि भेदों में विभक्त बन्ध, उदय और सत्त्व की प्ररूपणा की गई है। इस अधिकार को ग्रन्थकार ने स्तव कहा है। उसका स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि जो शास्त्र विवक्षित तत्त्व का सर्वांगपर्ण विस्तार या संक्षेप से वर्णन करने वाला है वह स्तव कहलाता है। एक अंग के वर्णन करने वाले शास्त्र को स्तुति और एक अंग के एक अधिकार के प्ररूपक शास्त्र को धर्मकथा कहा जाता है। बन्ध का वर्णन करते हए यहाँ सामान्य से यह निर्देश किया गया है कि तीर्थकर प्रकृति का बन्ध सम्यक्त्व के रहते हैए
-असंयतसम्यग्दृष्टि से अपूर्वकरण गुणस्थान तक- ही होता है। प्रायु का बन्ध मिथ गणस्थान (तृतीय) और मिश्रकाययोग (
नित्यपर्याप्त अवस्था) में नहीं होता, वह उक्त तीसरे गुणस्थान को छोड पहले से सातवें गुणस्थान तक होता है। इस अधिकार के अन्त में ग्रन्थकार ने यह कहा है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती चक्ररत्न के द्वारा छह खण्डरूप भरत क्षेत्र पर निर्बाध विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार मैंने बद्धिरूपी चक्ररत्न के द्वारा षट्खण्ड को-जीवस्थानादि छह खण्डों में विभक्त षटखण्डागम कोसिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि षट्खण्डात्मक सिद्धान्त का गम्भीर अध्ययन करके उसके सारभूत इस ग्रन्थ की रचना उनके द्वारा की गई है।
(३) सस्वस्थान-इस अधिकार में गुणस्थान के प्राश्रय से सत्वस्थानों की प्ररूपणा की इई है। विवक्षित गणस्थान में जितनी कर्मप्रकृतियां सत्ता में विद्यमान हों उनके समुदाय का नाम सत्त्वस्थान है। प्रकृतियों की भिन्नता के होने पर भी संख्या में भेद न होना, इसे भंग कहा जाता है। ऐसे भगों के साथ किस गुणस्थान में कितने सत्त्वस्थान सम्भव हैं, इसका विचार इस अधिकार में किया गया है।
त्रिचलिका-इस अधिकार की प्रथम चूलिका में विवक्षित प्रकृतियों का बन्ध क्या अपने उदय के पूर्व में नष्ट होता है, अपने उदय के पश्चात् नष्ट होता है, अथवा दोनों साथ ही नष्ट होते हैं। उनका बन्ध क्या अपने उदय के साथ होता है, अन्य प्रकृतियों के उदय के साथ होता है
प्रय प्रतियों के उदय के साथ होता है तथा वह बन्ध क्या सान्तर होता है, निरन्तर होता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org