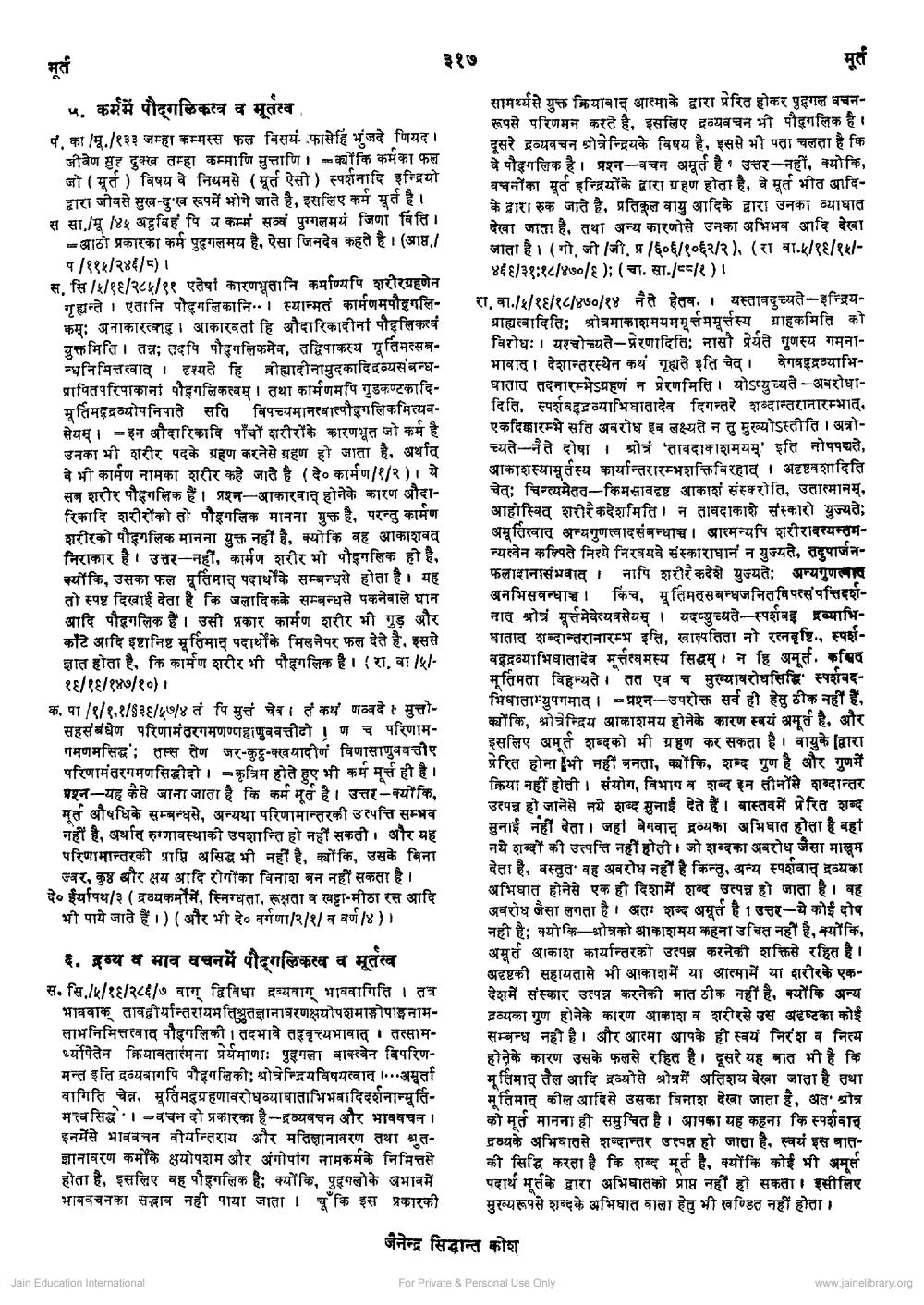________________
मूर्त
५. कर्ममें पौद्गलिकत्व व मूर्तस्व
.का./१११ हा कम्मरस फल विसयं फार्महिं भंजदे जियर जीवेण ह दुक्ख तम्हा कम्माणि मुत्ताणि । - क्योंकि कर्मका फल जो मूर्त) विषय के नियमसे (पूर्त ऐसी) स्पर्शनादि इन्द्रियो द्वारा जीवसे सुख-दुख रूपमें भोगे जाते है, इसलिए कर्म मूर्त है ।
४५ अहिं पिय कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिया मिति । - आठो प्रकारका कर्म पुद्गलमय है, ऐसा जिनदेव कहते है। (आप्त / 9/884/284/=) 1
BE
स. सि / ५ /११/२८५/११ एतेषां कारणभूतानि कर्माण्यपि शरीरग्रहणेन गृह्यन्ते एतानि पोहुगतिकानि स्याम्म कार्मणमपौगलि कम्ः अनाकारत्वाद् | आकारवतां हि औदारिकादीनां पौलिकत्वं युक्तमिति राज्ञः तदपि पौगलिकमेन टद्विपाकस्य मूर्तिमसम निमित्तत्वात्स्यते हि श्रोह्यारीनामुदकादिव्यमन्धप्राचितपरिणाम पौगलिकम तथा कार्मणमपि गुडकण्टकादि मूर्तिमयोपनिपाते सति विपतपमानत्वात्पौलिकमित्यवसेयर इन औदारिकादि पाँचों शरीरोंके कारणभूत जो कर्म है उनका भी शरीर पदके ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है, अर्थात् ये भी कार्मण नामका शरीर कहे जाते है (दे० कार्मण /१/२)। ये सम शरीर पौगलिक हैं। मकारा होनेके कारण औदारिकादि शरीरोंको सो पौगलिक मानना मुक्त है, परन्तु कार्मण शरीरको पौगलिक मानना युक्त नहीं है, क्योंकि यह आकाशव निराकार है। उत्तर-नहीं, कार्मण शरीर भी पौगलिक ही है. क्योंकि, उसका फल मूर्तिमान पदार्थोंके सम्बन्धसे होता है। यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि दिने सम्बन्धसे पढनेवाले धान आदि पौगलिक हैं । उसी प्रकार कार्मण शरीर भी गुड़ और काँटे आदि हशनिष्ठ मूर्तिमात् परायोंके मिलनेयर फस देते है. इससे ज्ञात होता है, कि कार्मण शरीर भी पौगलिक है। रा. वा /५/२६/११/१४०/९०) ।
,
क. पा /१/११/६३६/५७/४ तं पि मुत्तं चेत्र । तं कथं णव्वदे। मुत्तोसहसंबंधेण परिणामंतरणमणावसीटोणच परिणामगमगमसिद्ध' तुम्स ते जर कुटुयादी विमासाती परिणामंतरगमगसिद्धोदो। कृत्रिम होते हुए भी कर्म मूर्त ही है। प्रश्न- यह कैसे जाना जाता है कि कर्म मूर्त है। उत्तर क्यों
औषधि सम्बन्ध, अन्यथा परिणामान्तरकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, अर्थात रुग्णावस्थाकी उपशान्ति हो नहीं सकती और यह परिणामान्तरकी प्रति असिद्ध भी नहीं है, खोकि, उसके बिना ज्वर, कुष्ठ और क्षय आदि रोगोंका विनाश बन नहीं सकता है । ०२ (मौने, स्निग्धता, रूक्षता व खट्टा-मीठा रस आदि भी पाये जाते हैं।) (और भी दे० वर्गणा/२/२/ व वर्ण /४) ।
६. द्रव्य व माव वचनमें पौद्गलिकत्व व मूर्तस्व स.सि./५/११/२८६/७ बाग द्विविधा द्रष्णवान् भवागिति । तत्र भाववाकू तावद्वीर्यान्तरायमतिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामसामनिमित्तनाद पौगतिको तदभावे तत्वभावात् तत्सामयोपेतेन कियावतारमा प्रेर्यमाणाः नापत्येन विपरिण मन्त इति द्रव्यापि पौगलिको धोत्रेन्द्रियविषयत्वात्... अमृ वागिति चेन्न मूर्तिमग्रहणावरोधव्याघाताभिभवादिदर्शनान्मूर्तिमत्त्व सिद्ध । - वचन दो प्रकारका है-द्रव्यवचन और भाववचन । इनमेंसे भाववचन वीर्यान्तराय और मतिज्ञानावरण तथा श्रुतज्ञानावरण कर्मोके क्षयोपशम और अंगोपांग नामकर्मके निमित्तसे होता है, इसलिए वह पौगलिक है क्योंकि गलोके अभाव भाववचनका सद्भाव नहीं पाया जाता। चूँकि इस प्रकारकी
Jain Education International
३१७
मूर्त
सामर्थ्य युक्त क्रियामात् आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनरूपसे परिणमन करते है, इसलिए इव्ययचन भी पौगलिक है। दूसरे द्रव्यवचन श्रोत्रेन्द्रियके विषय है, इससे भी पता चलता है कि वे पौगलिक है। प्रश्न-वचन अमूर्त है उत्तर नहीं, क्यो वचनों का सूर्त इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होता है, वे मूर्त भीत आि के द्वारा रुक जाते है, प्रतिकूल वायु आदिके द्वारा उनका व्याघात देखा जाता है, तथा अन्य कारणोसे उनका अभिभव आदि देखा जाता है। (गो. जी / जी. प्र / ६०६/१०६२/२), ( रा बा.५/११/१५/४६६/२१:२८/४००/२); (चा. खा./९/२)।
-
रा. वा./२/११/१८/४००/९४ मेरी हेलन यस्तावदुच्यते इद्रियब्राह्मत्यादिति श्रोत्रमाकाशमयम सममूर्तस्य ग्राहकमिति को निशेषः । यश्चोच्यते प्रेरणादिति नासौ प्रेर्य गुणस्य गमनाभावात् । देशान्तरस्थेन कथं गृह्यते इति चेत् । बेगवद्रव्याभि घाताय तदनारम्भेऽग्रहणं न प्रेरणमिति योऽप्युच्यते-अवरोधा दिति स्पर्शव्याभिघातादेव दिगन्तरे शब्दान्तरानारम्भाव. एकविचारम्भे सति अबरोध एव लक्ष्यते न तु मुख्योऽस्तीति । खत्रो स्वतेनेसे दोषा । श्रोत्रं 'तावदानाशमयम् इति नोपपद्यते आकाशस्यार्तस्य कार्यान्तरारम्भशक्तिविरहात अस्वशादिति चेदः पिन्व्यमेतद- किमसावदष्ट आकायां संस्करोति उतारनामस् आहोस्वित् शरीरैकदेशमिति । न तावदाकाशे संस्कारो युज्यते; अमूर्तिलाद अन्यगुणादन्याच आत्मन्यपि शरीरावयन्तमन्यत्वेन कल्पिते निरये निरवयवे संस्काराधानं न युज्यते, उडुपार्जन फलानाम्वाद । नापि शरीरं कदेवी युज्यते अन्यगुणाव अनभिसन्धाञ्च । किंच, मूर्तिमत्सबन्धजनित विपरसंपत्तिदर्शनाव सूर्तमेवमय । यदप्युच्यते स्पर्श हव्या धाताद शम्दान्तरानारम्भ इति खपतिता नो रत्नवृष्टि, स्पर्शमद्रव्याभिवादादेव मूर्खत्यमस्य सिद्धम्। न हि अमूर्त कविय मूर्तिमता विहन्यते । तत एव च मुख्यावरोधसिद्धि' स्पर्शबदभिघाताम्युपगमात् प्रश्न-उपरोक्त सर्व ही हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि, श्रोद्रय आकाशमय होनेके कारण स्वयं अमूर्त है, और इसलिए अमूर्त शब्दको भी ग्रहण कर सकता है। वायुके द्वारा प्रेरित होना भी नहीं बनता, क्योंकि, शब्द गुण है और गुण में क्रिया नहीं होती। संयोग, विभाग व शब्द इन तीनोंसे शब्दान्तर उत्पन्न हो जानेसे नये सम्य सुनाई देते हैं। वास्तव में प्रेरित शब्द सुनाई नहीं देता। जहां वेगवाद प्रव्यका अभिघात होता है वहाँ नये शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती। जो शब्दका अबरोध जैसा मालूम देता है, वस्तुत' यह अवरोध नहीं है किन्तु अन्य स्पर्शवाद द्रव्यका अभिघात होनेसे एक ही दिशामें शब्द उत्पन्न हो जाता है । वह अवरोध जैसा लगता है । अतः शब्द अमूर्त है 1 उत्तर- ये कोई दोष नही है; क्योकि - भोत्रको आकाशमय कहना उचित नहीं है, क्योंकि, अमूर्त आकाश कार्यान्तरको उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित है। अटकी सहायतासे भी आकाश में या आत्मामें या वारीरके एकदेश में संस्कार उत्पन्न करनेकी बात ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्यका गुण होनेके कारण आकाश व शरीरसे उस अदृष्टका कोई सम्बन्ध नही है । और आत्मा आपके ही स्वयं निरंश व नित्य होनेके कारण उसके फासे रहित है। दूसरे यह बात भी है कि मूर्तिमा तेल आदि द्रव्योसे श्रोत्रमें अतिशय देखा जाता है तथा मूर्तिमान कील आदि उसका विनाश देखा जाता है, अतोत्र को मूर्त मानना ही समुचित है। आपका यह कहना कि स्पर्शमाच द्रव्यके अभिघात से शब्दान्तर उत्पन्न हो जाता है, स्वयं इस बातकी सिद्धि करता है कि शब्द मूर्त है, क्योंकि कोई भी अमूर्त पदार्थ मूर्तके द्वारा अभियानको प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्यरूप से शब्द के अभिघात वाला हेतु भी खण्डित नहीं होता ।
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
-
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org