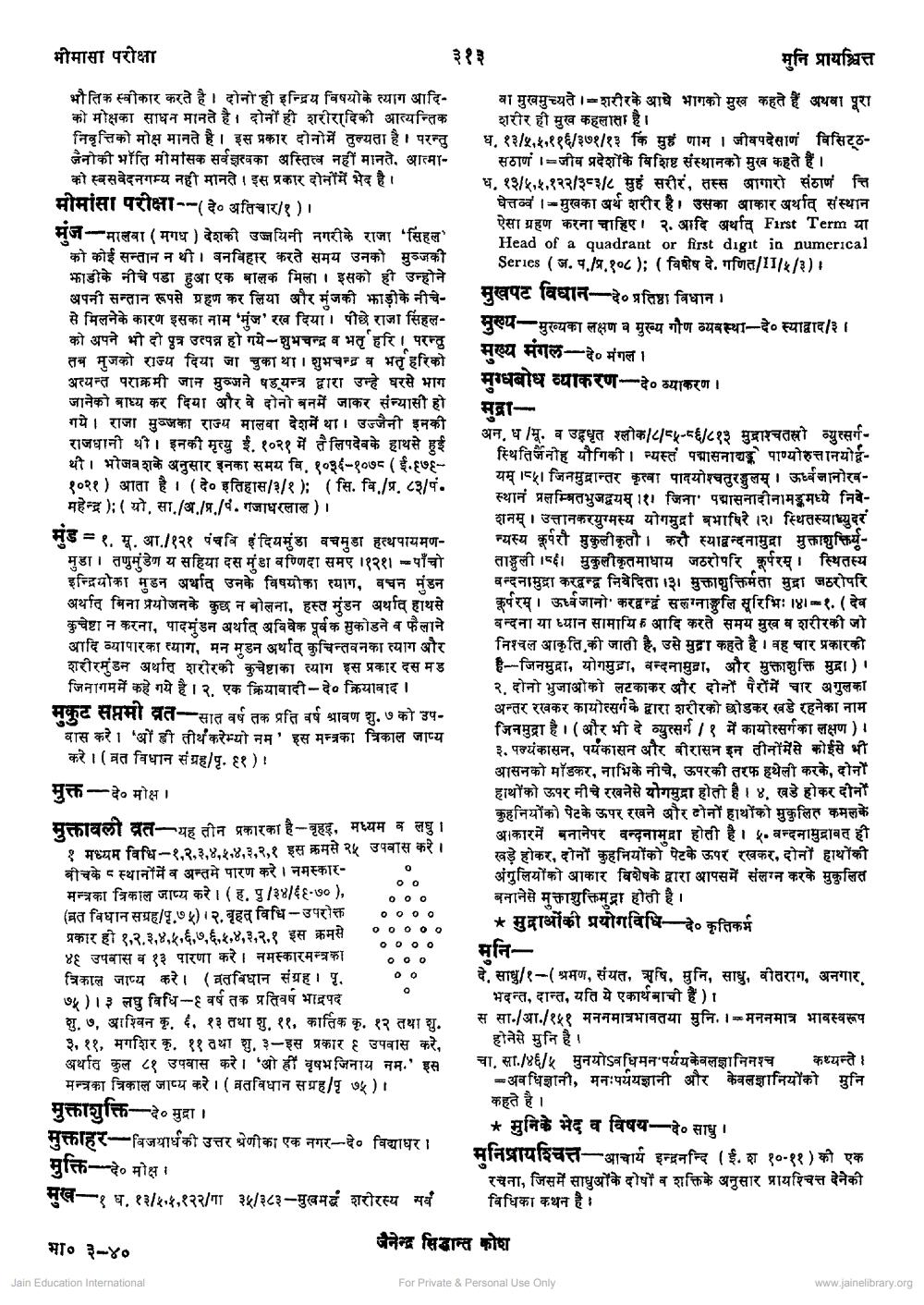________________
भीमासा परीक्षा
३१३
मुनि प्रायश्चित्त
वा मुखमुच्यते। शरीरके आधे भागको मुख कहते हैं अथवा पूरा
शरीर ही मुख कहलाता है। ध. १३/५,६,११६/३७१/१३ किं मुहं णाम । जीवपदेसाणं विसिट्ठ
सठाणं ।जीव प्रदेशोंके विशिष्ट संस्थानको मुख कहते हैं। ध. १३/५,५,१२२/३८३/८ मुहं सरीरं, तस्स आगारो संठाणं त्ति
घेत्तव्यं ।-मुखका अर्थ शरीर है। उसका आकार अर्थात् संस्थान ऐसा ग्रहण करना चाहिए। २. आदि अर्थात First Term या Head of a quadrant or first digit in numerical Series (ज. प./प्र.१०८); (विशेष दे. गणित/II/५/३)।
मुखपट विधान-दे० प्रतिष्ठा विधान । मुख्य-मुख्यका लक्षण व मुख्य गौण व्यवस्था-दे० स्याद्वाद/३ । मुख्य मंगल-दे० मंगल । मुग्धबोध व्याकरण-दे० व्याकरण ।
भौतिक स्वीकार करते है। दोनो ही इन्द्रिय विषयोके त्याग आदिको मोक्षका साधन मानते है। दोनों ही शरीरादिकी आत्यन्तिक निवृत्तिको मोक्ष मानते है। इस प्रकार दोनोमें तुल्यता है। परन्तु जैनोकी भॉति मीमांसक सर्वज्ञत्वका अस्तित्व नहीं मानते, आत्मा
को स्वसवेदनगम्य नही मानते । इस प्रकार दोनोंमें भेद है। मीमांसा परीक्षा--(दे० अतिचार/१)। मुज-मालवा (मगध ) देशको उज्जयिनी नगरीके राजा "सिंहल'
को कोई सन्तान न थी। बनविहार करते समय उनको मुजकी झाडीके नीचे पड़ा हुआ एक बालक मिला। इसको ही उन्होने अपनी सन्तान रूपसे ग्रहण कर लिया और मुंजकी झाड़ीके नीचेसे मिलनेके कारण इसका नाम 'मुंज' रख दिया। पीछे राजा सिंहलको अपने भी दो पुत्र उत्पन्न हो गये- शुभचन्द्र व भतृ हरि । परन्तु तब मुजको राज्य दिया जा चुका था। शुभचन्द्र व भतृहरिको अत्यन्त पराक्रमी जान मुञ्जने षडयन्त्र द्वारा उन्हे घरसे भाग जानेको बाध्य कर दिया और वे दोनो बनमें जाकर संन्यासी हो गये। राजा मुब्जका राज्य मालवा देशमें था। उज्जैनी इनकी राजधानी थी। इनकी मृत्यु ई. १०२१ में तैलिपदेवके हाथसे हुई थी। भोजव शके अनुसार इनका समय वि. १०३६-१०७८ ( ई.६७६१०२१) आता है। (दे० इतिहास/३/१); (सि. वि./प्र.८३/पं. महेन्द्र ); ( यो, सा./अ./प्र./व. गजाधरलाल )। मुड%१. मू. आ./१२१ पंचवि इंदियमुंडा वचमुडा हत्थपायमणमुडा। तणुमुंडेण य सहिया दस मुंडा वण्णिदा समए ।१२११ - पाँचो इन्द्रियोका मुडन अर्थात उनके विषयोका त्याग, वचन मुंडन अर्थात् बिना प्रयोजनके कुछ न बोलना, हस्त मुंडन अर्थात हाथसे कुचेष्टा न करना, पादमुंडन अर्थात् अविवेक पूर्वक सुकोडने व फैलाने
आदि व्यापार का त्याग, मन मुडन अर्थात् कुचिन्तवनका त्याग और शरीरमुंडन अर्थात शरीरको कुचेष्टाका त्याग इस प्रकार दस मड जिनागममें कहे गये है। २. एक क्रियावादी-दे० क्रियावाद । मकुट सप्तमी व्रत-सात वर्ष तक प्रति वर्ष श्रावण शु.७ को उपवास करे। "ओं ही तीर्थकरेभ्यो नम' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य
करे । (व्रत विधान संग्रह/पृ.११)। मुक्त-दे० मोक्ष। मुक्तावली व्रत-यह तीन प्रकारका है-बृहद्, मध्यम व लघु ।
१ मध्यम विधि-१,२,३,४,५४,३,२,१ इस क्रमसे २५ उपवास करे। बीचके ८ स्थानों में व अन्तमे पारण करे। नमस्कार- . मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (ह.पु/३४/६६-७०),
००० (व्रत विधान सग्रह/पृ.७५) १२.बृहत विधि- उपरोक्त ००००
००००० प्रकार ही १,२,३,४,५,६,७,६,१,४,३,२.१ इस क्रमसे
०००० ४६ उपवास व १३ पारणा करे। नमस्कारमन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (व्रतविधान संग्रह । पृ. ७५) । ३ लघु विधि-६ वर्ष तक प्रतिवष भाद्रपद शु.७, आश्विन कृ. ६, १३ तथा शु. ११, कार्तिक कृ. १२ तथा शु. ३, ११, मगशिर कृ. ११ तथा शु.३-इस प्रकार, उपवास करे, अर्थात कुल ८१ उपवास करे। 'ओ ह्रीं वृषभजिनाय नमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । ( बतविधान सग्रह/पृ ७५) । मुक्ताशुक्ति-दे० मुद्रा। मुक्ताहर-विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । मुक्ति-दे० मोक्ष मुख-१ घ. १३/११,१२२/गा ३५/३८३-मुखमद्धं शरीरस्य सर्व
अन. ध /म. व उद्धृत श्लोका-८६/८१३ मुद्राश्चतस्रो व्युत्सर्गस्थितिजैनोह यौगिकी। न्यस्तं पद्मासनाद्यडू पाण्योरुत्तानयोर्द्वयम् ।८। जिनमुद्रान्तर कृत्वा पादयोश्चतुरङ्गलम् । ऊध्र्वनानोरवस्थानं प्रलम्बितभुजद्वयम् ॥ जिना' पद्मासनादीनामङ्कमध्ये निवेशनम् । उत्तानकरयुग्मस्य योगमुद्रा बभाषिरे २१ स्थितस्याध्युदरं न्यस्य कूर्परौ मुकुलीकृतौ। करौ स्याद्वन्दनामुद्रा मुक्ताशुक्तिर्युताङ्गुली।६। मुकुलीकृतमाधाय जठरोपरि कूर्परम् । स्थितस्य वन्दनामुद्रा करद्वन्द्व निवेदिता ३. मुक्ताशुक्तिर्मता मुद्रा जठरोपरि कूर्परम् । ऊर्ध्वजानो' करद्वन्द्वं सलग्नाङ्गुलि सूरिभिः ।४।- १. ( देव वन्दना या ध्यान सामायिक आदि करते समय मुख व शरीरकी जो निश्चल आकृति की जाती है, उसे मुद्रा कहते है । वह चार प्रकारकी है-जिनमुद्रा, योगमुद्रा, वन्दनामुद्रा, और मुक्ताशुक्ति मुद्रा)। २. दोनो भुजाओको लटकाकर और दोनों पैरोंमें चार अगुलका अन्तर रखकर कायोत्सर्ग के द्वारा शरीरको छोड़कर खडे रहनेका नाम जिनमुद्रा है । (और भी दे व्युत्सर्ग/१ में कायोत्सर्गका लक्षण )। ३. पन्यंकासन, पर्यकासन और वीरासन इन तीनोंमें से कोईसे भी आसनको मॉडकर, नाभिके नीचे, ऊपरकी तरफ हथेली करके, दोनों हाथोंको ऊपर नीचे रखनेसे योगमुद्रा होती है । ४. खडे होकर दोनों कुहनियोंको पेट के ऊपर रखने और दोनों हाथोंको मुकुलित कमलके
कारमें बनानेपर वन्दनामुद्रा होती है। ५. वन्दनामुद्रावत ही खड़े होकर, दोनों कुहनियोंको पेटके ऊपर रखकर, दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको आकार विशेषके द्वारा आपसमें संलग्न करके मुकुलित बनानेसे मुक्ताशुक्तिमुद्रा होती है।
* मुद्राओंकी प्रयोगविधि-दे० कतिकर्म मनिदे. साधु/१-(श्रमण, संयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार.
भदन्त, दान्त, यति ये एकार्थबाची हैं)। स सा./आ./१५१ मननमात्रभावतया मुनि. -मननमात्र भावस्वरूप
होनेसे मुनि है। चा, सा./४६/५ मुनयोऽवधिमन'पर्ययकेवलज्ञानिनश्च कथ्यन्ते।
- अवधिज्ञानी, मनापर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंको मुनि कहते है। * मुनिके भेद व विषय-दे० साधु । मनिप्रायश्चित्त-आचार्य इन्द्रनन्दि (ई. श १०-११) की एक रचना, जिसमें साधुओंके दोषों व शक्ति के अनुसार प्रायश्चित्त देनेकी विधिका कथन है।
०००
भा०३-४०
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org