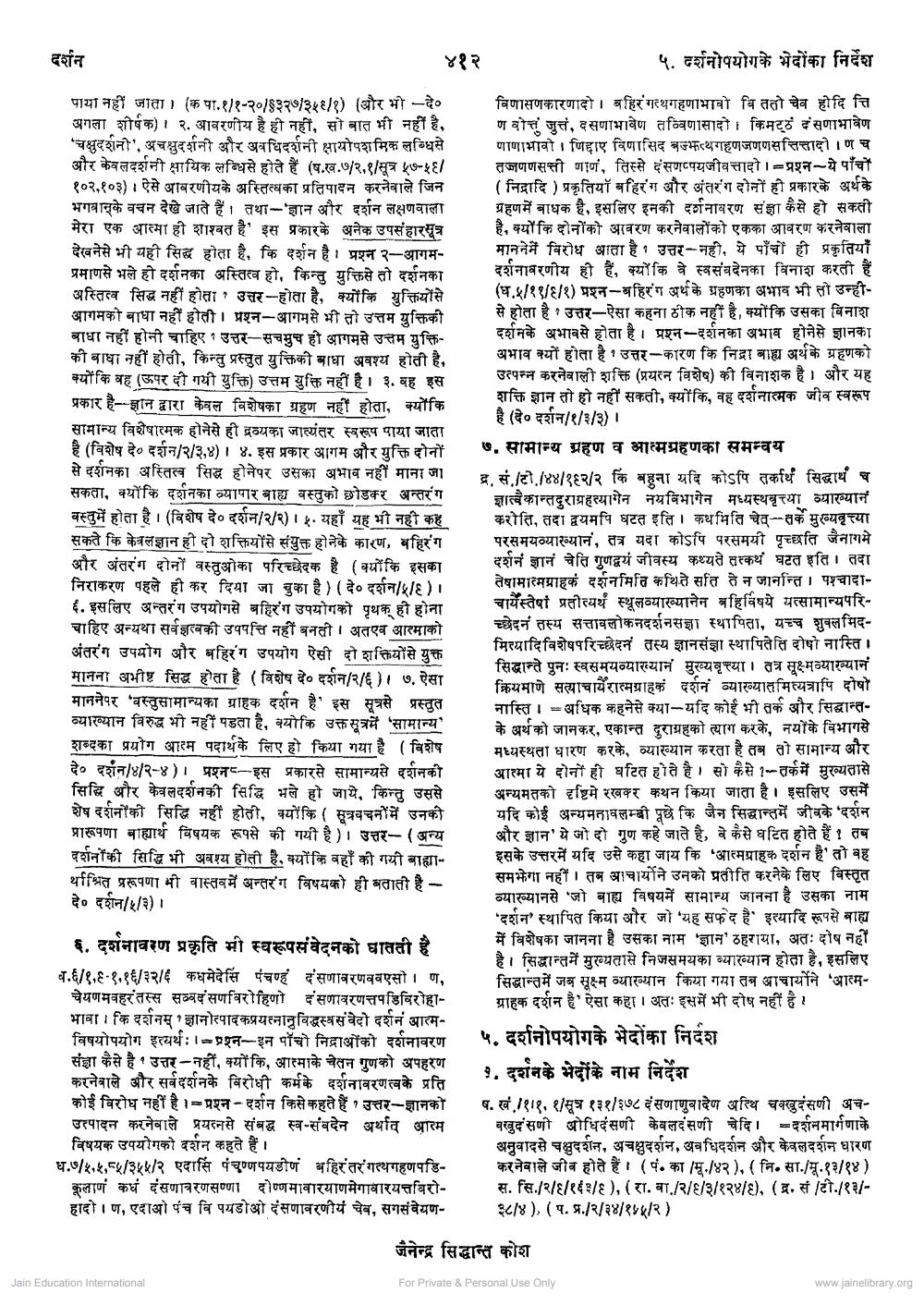________________
दर्शन
४१२
५. दर्शनोपयोगके भेदोंका निर्देश
पाया नहीं जाता। (क पा.१/१-२०/६३२७/३५६/१) (और भी-दे० अगला शीर्षक)। २. आवरणीय है ही नहीं, सो बात भी नहीं है, 'चक्षुदर्शनी', अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्शनी क्षायोपशमिक लब्धिसे और केवलदर्शनी क्षायिक लब्धिसे होते हैं (प.व.७/२,१/सूत्र ५७-५६/ १०२,१०३)। ऐसे आवरणीयके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाले जिन भगवान्के वचन देखे जाते हैं। तथा-'ज्ञान और दर्शन लक्षणवाला मेरा एक आत्मा ही शाश्वत है' इस प्रकारके अनेक उपसंहारसूत्र देखनेसे भी यही सिद्ध होता है, कि दर्शन है। प्रश्न २-आगमप्रमाणसे भले ही दर्शनका अस्तित्व हो, किन्तु युक्तिसे तो दर्शनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ? उत्तर-होता है, क्योंकि युक्तियोंसे आगमको बाधा नहीं होती। प्रश्न-आगमसे भी तो उत्तम युक्तिकी बाधा नहीं होनी चाहिए। उत्तर-सचमुच ही आगमसे उत्तम युक्तिकी बाधा नहीं होती, किन्तु प्रस्तुत युक्तिकी बाधा अवश्य होती है, क्योंकि वह (ऊपर दी गयी युक्ति) उत्तम युक्ति नहीं है। ३. वह इस प्रकार है--ज्ञान द्वारा केवल विशेषका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक होनेसे ही द्रव्यका जात्यंतर स्वरूप पाया जाता है (विशेष दे० दर्शन/२/३,४)। ४. इस प्रकार आगम और युक्ति दोनों से दर्शनका अस्तित्व सिद्ध होनेपर उसका अभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि दर्शनका व्यापार बाह्य वस्तुको छोडकर अन्तरंग वस्तुमें होता है । (विशेष दे० दर्शन/२/२) । ३. यहाँ यह भी नही कह सकते कि केवलज्ञान ही दो शक्तियोंसे संयुक्त होनेके कारण, बहिरंग
और अंतरंग दोनों वस्तुओका परिच्छेदक है (क्योंकि इसका निराकरण पहले ही कर दिया जा चुका है। (दे० दर्शन//९) । ६. इसलिए अन्तरंग उपयोगसे बहिरंग उपयोगको पृथक् ही होना चाहिए अन्यथा सर्वज्ञत्वकी उपपत्ति नहीं बनती। अतएव आत्माको अंतरंग उपयोग और बहिरंग उपयोग ऐसी दो शक्तियों से युक्त मानना अभीष्ट सिद्ध होता है (विशेष दे० दर्शन/२/६ )। ७. ऐसा माननेपर 'वस्तुसामान्यका ग्राहक दर्शन है' इस सूत्रसे प्रस्तुत व्याख्यान विरुद्ध भी नहीं पड़ता है, क्योकि उक्त सूत्रमै 'सामान्य' शब्दका प्रयोग आत्म पदार्थ के लिए हो किया गया है (विशेष दे० दर्शन/४/२-४)। प्रश्न-इस प्रकारसे सामान्यसे दर्शनकी सिद्धि और केवलदर्शनकी सिद्धि भले हो जाये, 'किन्तु उससे शेष दर्शनोकी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि ( सूत्रवचनों में उनकी प्रारूपणा बाह्यार्थ विषयक रूपसे की गयी है)। उत्तर-(अन्य दर्शनोंकी सिद्धि भी अवश्य होती है, क्योंकि वहाँ की गयी बाह्या
र्थाश्रित प्ररूपणा भी वास्तव में अन्तरंग विषयको ही बताती है - दे० दर्शन/१/३)।
विणासणकारणादो। बहिरं गत्थगहणाभावो वि ततो चेव होदि त्ति ण वोत्तुं जुत्तं, दसणाभावेण तविणासादो। किमट्ठ दसणाभावेण णाणाभावो । णिहाए विणासिद बज्झत्थगहणजणणसत्तित्तादो । ण च तज्जणणसत्ती णाणं, तिस्से दसणप्पयजीवत्तादो। प्रश्न-ये पाँचों (निद्रादि ) प्रकृतियाँ बहिरंग और अंतरंग दोनों ही प्रकारके अर्थके ग्रहण में बाधक है, इसलिए इनकी दर्शनावरण संज्ञा कैसे हो सकती है, क्योंकि दोनोंको आवरण करनेवालोंको एकका आवरण करनेवाला मानने में विरोध आता है। उत्तर-नही, ये पाँचों ही प्रकृतियाँ दर्शनावरणीय ही हैं, क्योंकि वे स्वसंवदेनका विनाश करती हैं (ध.२/११/६/१) प्रश्न-बहिरंग अर्थ के ग्रहणका अभाव भी तो उन्हीसे होता है ? उत्तर-ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका विनाश दर्शनके अभावसे होता है। प्रश्न-दर्शनका अभाव होनेसे ज्ञानका अभाव क्यों होता है । उत्तर-कारण कि निद्रा बाह्य अर्थके ग्रहणको उत्पन्न करनेवाली शक्ति (प्रयत्न विशेष) की विनाशक है। और यह शक्ति ज्ञान तो हो नहीं सकती, क्योंकि, वह दर्शनात्मक जीव स्वरूप है (दे० दर्शन/१/३/३)। ७. सामान्य ग्रहण व आत्मग्रहणका समन्वय द्र, सं./टी./४४/१९२/२ किं बहुना यदि कोऽपि तार्थ सिद्धार्थ च
ज्ञात्वैकान्तदुराग्रहत्यागेन नय विभागेन मध्यस्थवृत्त्या व्याख्यान करोति, तदा द्वयमपि घटत इति । कथमिति चेत्-तर्के मुख्यवृत्त्या परसमयव्याख्यान, तत्र यदा कोऽपि परसमयी पृच्छति जैनागमे दर्शनं ज्ञानं चेति गुणद्वयं जीवस्य कथ्यते तत्कथं घटत इति। तदा तेषामात्मग्राहकं दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । पश्चादाचार्यैस्तेषां प्रतीत्यर्थं स्थूलव्याख्यानेन बहिर्विषये यत्सामान्यपरिच्छेदनं तस्य सत्तावलोकनदर्शनसज्ञा स्थापिता, यच्च शुक्ल मिदमित्यादिविशेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति। सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यानं मुख्यवृत्त्या। तत्र सूक्ष्मव्याख्यानं क्रियमाणे सत्याचारात्मग्राहकं दर्शनं व्याख्यातमित्यत्रापि दोषो नास्ति । = अधिक कहनेसे क्या-यदि कोई भी तर्क और सिद्धान्तके अर्थ को जानकर, एकान्त दुराग्रहको त्याग करके, नयोंके विभागसे मध्यस्थता धारण करके, व्याख्यान करता है तब तो सामान्य और आत्मा ये दोनों ही घटित होते है। सो कैसे ?-तर्कमें मुख्यतासे अन्यमतको दृष्टिमे रखकर कथन किया जाता है। इसलिए उसमें यदि कोई अन्यमतावलम्बी पूछे कि जैन सिद्धान्तमें जीवके 'दर्शन और ज्ञान' ये जो दो गुण कहे जाते है, वे कैसे घटित होते हैं ! तब इसके उत्तरमें यदि उसे कहा जाय कि 'आत्मग्राहक दर्शन है' तो वह समझेगा नहीं। तन आचार्योंने उनको प्रतीति करनेके लिए विस्तृत व्याख्यानसे 'जो बाह्य विषयमें सामान्य जानना है उसका नाम 'दर्शन' स्थापित किया और जो 'यह सफेद है' इत्यादि रूपसे बाह्य में विशेषका जानना है उसका नाम 'ज्ञान' ठहराया, अतः दोष नहीं है। सिद्धान्तमें मुख्यतासे निजसमयका व्याख्यान होता है, इसलिए सिद्धान्तमें जब सूक्ष्म व्याख्यान किया गया तब आचार्योने 'आत्मग्राहक दर्शन है' ऐसा कहा । अतः इसमें भी दोष नहीं है। ५. दर्शनोपयोगके भेदोंका निर्दश १. दर्शनके भेदों के नाम निर्देश ष. वं. १३१, १/सूत्र १३१/३७८ दंसणाणुवादेण अस्थि चवखुदंसणी अचबखुदंसणी अोधिदसणी केवलदंसणी चेदि। -दर्शनमार्गणाके अनुवादसे चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन धारण करनेवाले जीव होते हैं। (पं. का /मू./४२), (नि. सा./मू.१३/१४ ) स. सि./२/६/१६३/६ ), (रा. वा./२/६/३/१२४/१), (द्र. सं /टी./१३/३८/४), (प.प्र./२/३४/१५५४२)
६. दर्शनावरण प्रकृति भी स्वरूपसंवेदनको घातती है व.६/१,६-१,१६/३२/६ कधमेदेसि पंचण्हं दसणावरणववएसो। ण,
चेयणमवहरंतस्स सव्वदं सणविरोहिणो दसणावरणत्तपडिविरोहाभावा । कि दर्शनम् ' ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदो दर्शनं आत्मविषयोपयोग इत्यर्थः।- प्रश्न-इन पाँचो निद्राओंको दर्शनावरण संज्ञा कैसे है । उत्तर-नहीं, क्योंकि, आत्माके चेतन गुणको अपहरण करनेवाले और सर्वदर्शनके विरोधी कर्म के दर्शनावरणत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है। - प्रश्न-दर्शन किसे कहते हैं । उत्तर-ज्ञानको उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे संबद्ध स्व-संवदेन अर्थात् आत्म विषयक उपयोगको दर्शन कहते हैं। ध.७/५१,८५/३५५/२ एदासिं पंचण्णपयडीणं अहिरंतरंगत्थगहणपडिकूलाणं कधं दंसणावरणसण्णा दोण्णमावारयाणमेगावारयतविरोहादो। ण, एदाओ पंच वि पयडोओ दंसणावरणीयं चेव, सगसंवेयण
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org