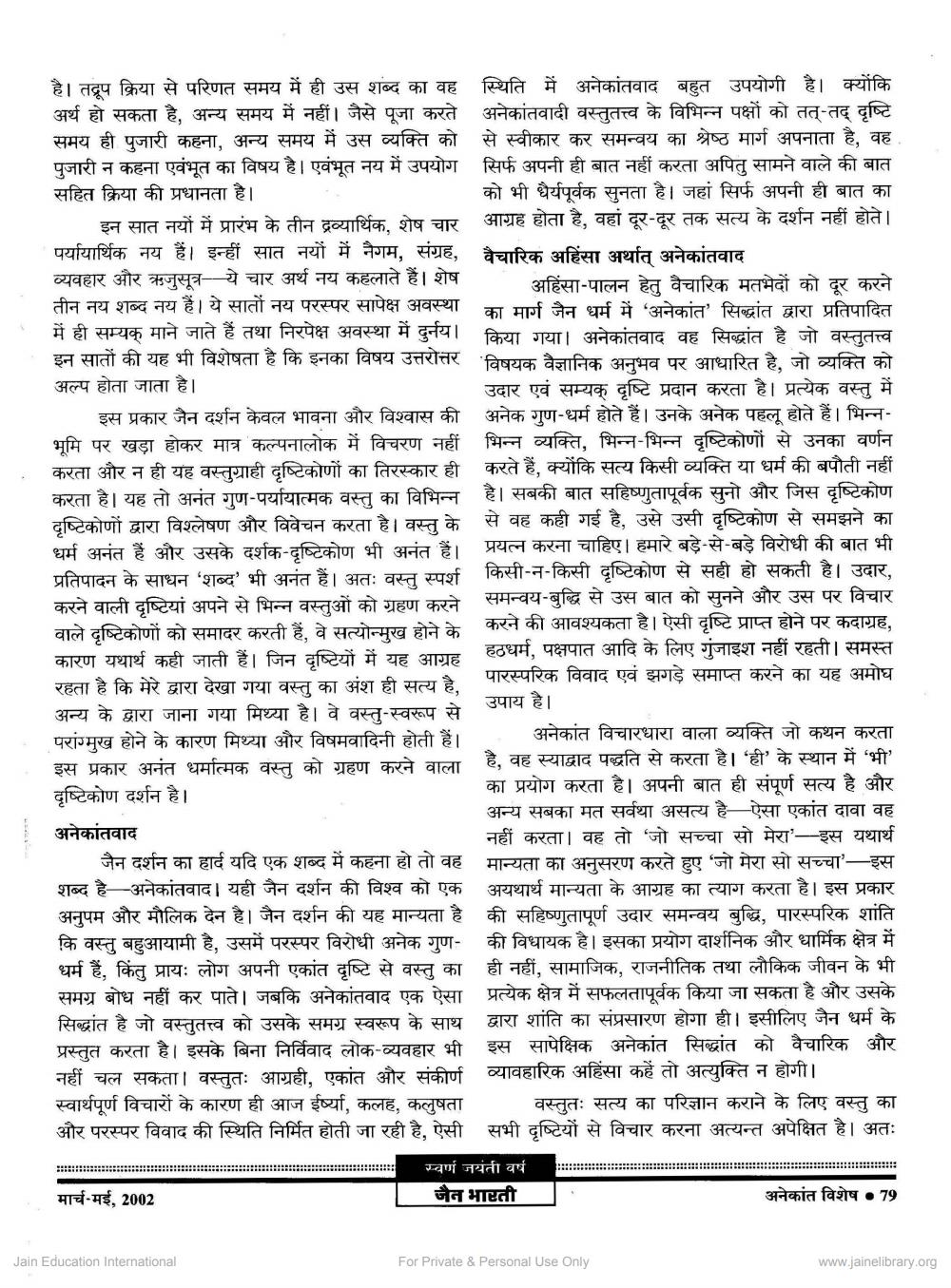________________
है तद्रूप क्रिया से परिणत समय में ही उस शब्द का वह अर्थ हो सकता है, अन्य समय में नहीं। जैसे पूजा करते समय ही पुजारी कहना, अन्य समय में उस व्यक्ति को पुजारी न कहना एवंभूत का विषय है। एवंभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की प्रधानता है।
इन सात नयों में प्रारंभ के तीन द्रव्यार्थिक, शेष चार पर्यायार्थिक नय हैं। इन्हीं सात नयों में नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार अर्थ नय कहलाते हैं। शेष तीन नय शब्द नय हैं। ये सातों नय परस्पर सापेक्ष अवस्था में ही सम्यक् माने जाते हैं तथा निरपेक्ष अवस्था में दुर्नय । इन सातों की यह भी विशेषता है कि इनका विषय उत्तरोत्तर अल्प होता जाता है।
इस प्रकार जैन दर्शन केवल भावना और विश्वास की भूमि पर खड़ा होकर मात्र कल्पनालोक में विचरण नहीं करता और न ही यह वस्तुग्राही दृष्टिकोणों का तिरस्कार ही करता है। यह तो अनंत गुण पर्यायात्मक वस्तु का विभिन्न दृष्टिकोणों द्वारा विश्लेषण और विवेचन करता है । वस्तु के धर्म अनंत हैं और उसके दर्शक दृष्टिकोण भी अनंत है। प्रतिपादन के साधन 'शब्द' भी अनंत हैं। अतः वस्तु स्पर्श करने वाली दृष्टियां अपने से भिन्न वस्तुओं को ग्रहण करने वाले दृष्टिकोणों को समादर करती हैं, वे सत्योन्मुख होने के कारण यथार्थ कही जाती हैं। जिन दृष्टियों में यह आग्रह रहता है कि मेरे द्वारा देखा गया वस्तु का अंश ही सत्य है, अन्य के द्वारा जाना गया मिथ्या है। वे वस्तु स्वरूप से परांग्मुख होने के कारण मिथ्या और विषमवादिनी होती हैं। इस प्रकार अनंत धर्मात्मक वस्तु को ग्रहण करने वाला दृष्टिकोण दर्शन है।
मार्च मई, 2002
-
अनेकांतवाद
जैन दर्शन का हार्द यदि एक शब्द में कहना हो तो वह शब्द है—अनेकांतवाद । यही जैन दर्शन की विश्व को एक अनुपम और मौलिक देन है। जैन दर्शन की यह मान्यता है कि वस्तु बहुआयामी है, उसमें परस्पर विरोधी अनेक गुणधर्म हैं, किंतु प्रायः लोग अपनी एकांत दृष्टि से वस्तु का समय बोध नहीं कर पाते। जबकि अनेकांतवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो वस्तुतत्त्व को उसके समग्र स्वरूप के साथ प्रस्तुत करता है। इसके बिना निर्विवाद लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता। वस्तुतः आग्रही, एकांत और संकीर्ण स्वार्थपूर्ण विचारों के कारण ही आज ईर्ष्या, कलह, कलुषता और परस्पर विवाद की स्थिति निर्मित होती जा रही है, ऐसी
Jain Education International
स्थिति में अनेकांतवाद बहुत उपयोगी है। क्योंकि अनेकांतवादी वस्तुतत्त्व के विभिन्न पक्षों को तत्-तद् दृष्टि से स्वीकार कर समन्वय का श्रेष्ठ मार्ग अपनाता है, वह सिर्फ अपनी ही बात नहीं करता अपितु सामने वाले की बात को भी धैर्यपूर्वक सुनता है। जहां सिर्फ अपनी ही बात का आग्रह होता है, वहां दूर-दूर तक सत्य के दर्शन नहीं होते। वैचारिक अहिंसा अर्थात् अनेकांतवाद
अहिंसा - पालन हेतु वैचारिक मतभेदों को दूर करने का मार्ग जैन धर्म में 'अनेकांत' सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद वह सिद्धांत है जो वस्तुतत्त्व विषयक वैज्ञानिक अनुभव पर आधारित है, जो व्यक्ति को उदार एवं सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। उनके अनेक पहलू होते हैं। भिन्नभिन्न व्यक्ति, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि सत्य किसी व्यक्ति या धर्म की बपौती नहीं है। सबकी बात सहिष्णुतापूर्वक सुनो और जिस दृष्टिकोण से वह कही गई है, उसे उसी दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे बड़े से बड़े विरोधी की बात भी किसी-न-किसी दृष्टिकोण से सही हो सकती है । उदार, समन्वय बुद्धि से उस बात को सुनने और उस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी दृष्टि प्राप्त होने पर कदाग्रह, हठधर्म, पक्षपात आदि के लिए गुंजाइश नहीं रहती। समस्त पारस्परिक विवाद एवं झगड़े समाप्त करने का यह अमोघ उपाय है।
अनेकांत विचारधारा वाला व्यक्ति जो कथन करता है, वह स्याद्वाद पद्धति से करता है । 'ही' के स्थान में 'भी' का प्रयोग करता है। अपनी बात ही संपूर्ण सत्य है और अन्य सबका मत सर्वथा असत्य है—ऐसा एकांत दावा वह नहीं करता। वह तो 'जो सच्चा सो मेरा' – इस यथार्थ मान्यता का अनुसरण करते हुए 'जो मेरा सो सच्चा' - इस अयथार्थ मान्यता के आग्रह का त्याग करता है। इस प्रकार की सहिष्णुतापूर्ण उदार समन्वय बुद्धि, पारस्परिक शांति की विधायक है । इसका प्रयोग दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, राजनीतिक तथा लौकिक जीवन के भी प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है और उसके द्वारा शांति का संप्रसारण होगा ही । इसीलिए जैन धर्म के इस सापेक्षिक अनेकांत सिद्धांत को वैचारिक और । व्यावहारिक अहिंसा कहें तो अत्युक्ति न होगी।
वस्तुतः सत्य का परिज्ञान कराने के लिए वस्तु का सभी दृष्टियों से विचार करना अत्यन्त अपेक्षित है। अतः स्वर्ण जयंती वर्ष
जैन भारती
For Private & Personal Use Only
अनेकांत विशेष • 79
www.jainelibrary.org