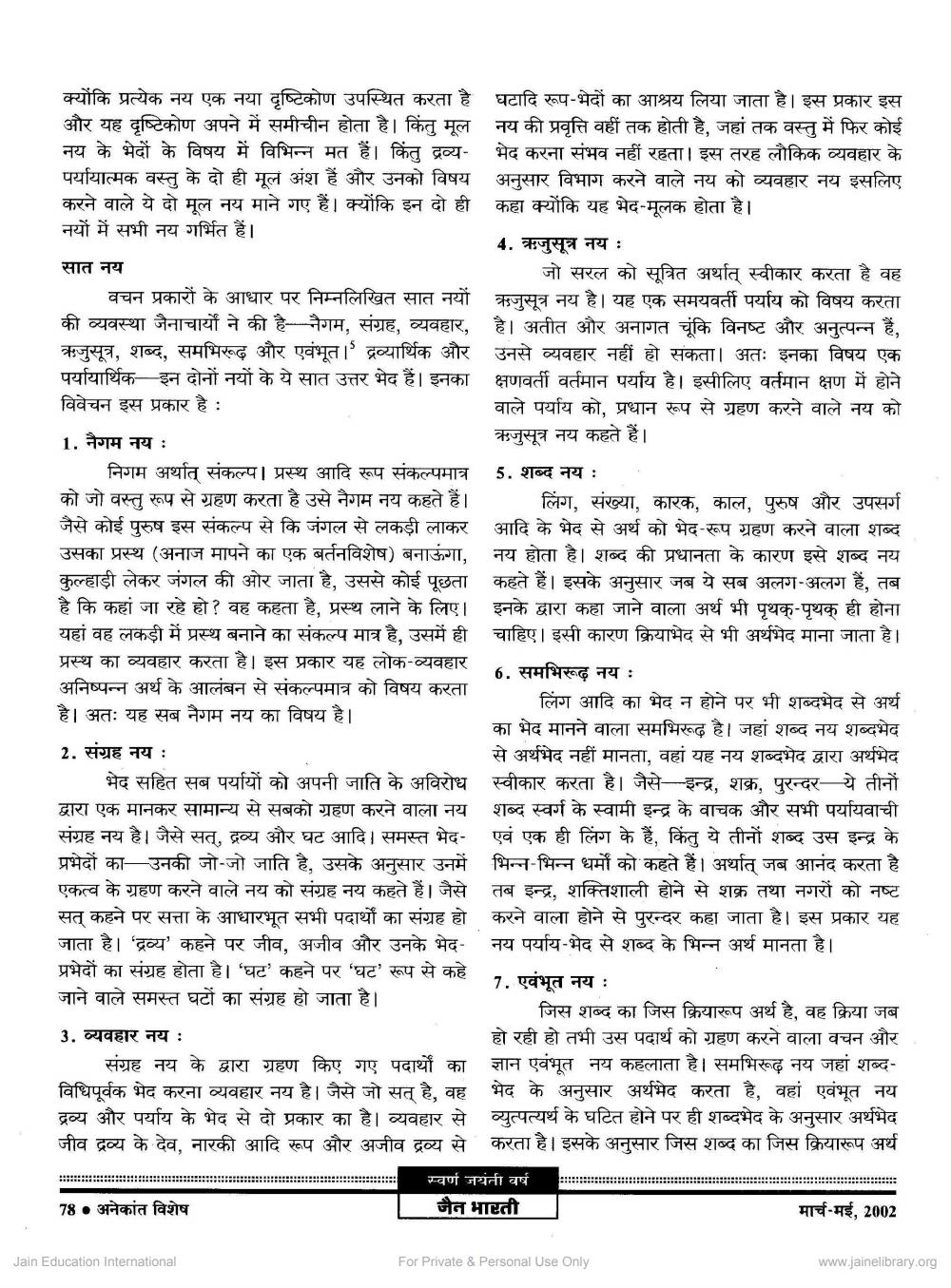________________
क्योंकि प्रत्येक नय एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता है और यह दृष्टिकोण अपने में समीचीन होता है। किंतु मूल नय के भेदों के विषय में विभिन्न मत हैं। किंतु द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु के दो ही मूल अंश हैं और उनको विषय करने वाले ये दो मूल नय माने गए हैं। क्योंकि इन दो ही नयों में सभी नय गर्भित हैं।
सात नय
वचन प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित सात नयों की व्यवस्था जैनाचार्यों ने की है—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूद और एवंभूत' द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के ये सात उत्तर भेद हैं। इनका विवेचन इस प्रकार है:
1. नैगम नय :
निगम अर्थात् संकल्प | प्रस्थ आदि रूप संकल्पमात्र को जो वस्तु रूप से ग्रहण करता है उसे नैगम नय कहते हैं। जैसे कोई पुरुष इस संकल्प से कि जंगल से लकड़ी लाकर उसका प्रस्थ (अनाज मापने का एक बर्तनविशेष) बनाऊंगा, कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है, उससे कोई पूछता है कि कहां जा रहे हो ? वह कहता है, प्रस्थ लाने के लिए। यहां वह लकड़ी में प्रस्थ बनाने का संकल्प मात्र है, उसमें ही प्रस्थ का व्यवहार करता है। इस प्रकार यह लोक व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के आलंबन से संकल्पमात्र को विषय करता है । अतः यह सब नैगम नय का विषय है।
2. संग्रह नय :
भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है। जैसे सत्, द्रव्य और घट आदि । समस्त भेद प्रभेदों का उनकी जो-जो जाति है, उसके अनुसार उनमें एकत्व के ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं । जैसे सत् कहने पर सत्ता के आधारभूत सभी पदार्थों का संग्रह हो जाता है। 'द्रव्य' कहने पर जीव, अजीव और उनके भेदप्रभेदों का संग्रह होता है 'घट' कहने पर 'घट' रूप से कड़े जाने वाले समस्त घटों का संग्रह हो जाता है।
-
3. व्यवहार नय :
संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधिपूर्वक भेद करना व्यवहार नय है जैसे जो सत् है, वह द्रव्य और पर्याय के भेद से दो प्रकार का है। व्यवहार से जीव द्रव्य के देव, नारकी आदि रूप और अजीव द्रव्य से
78 • अनेकांत विशेष
Jain Education International
घटादि रूप भेदों का आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार इस नय की प्रवृत्ति वहीं तक होती है, जहां तक वस्तु में फिर कोई भेद करना संभव नहीं रहता। इस तरह लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाले नय को व्यवहार नय इसलिए कहा क्योंकि यह भेद-मूलक होता है।
4. ऋजुसूत्र नय :
जो सरल को सूत्रित अर्थात् स्वीकार करता है वह ऋजुसूत्र नय है। यह एक समयवर्ती पर्याय को विषय करता है अतीत और अनागत चूंकि विनष्ट और अनुत्पन्न हैं, उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। अतः इनका विषय एक क्षणवर्ती वर्तमान पर्याय है इसीलिए वर्तमान क्षण में होने वाले पर्याय को, प्रधान रूप से ग्रहण करने वाले नय को ऋजुसूत्र नय कहते हैं।
5. शब्द नय :
लिंग, संख्या, कारक, काल, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से अर्थ को भेद-रूप ग्रहण करने वाला शब्द नय होता है। शब्द की प्रधानता के कारण इसे शब्द नय कहते हैं। इसके अनुसार जब ये सब अलग-अलग हैं, तब इनके द्वारा कहा जाने वाला अर्थ भी पृथक्-पृथक् ही होना चाहिए। इसी कारण क्रियाभेद से भी अर्थभेद माना जाता है।
6. समभिरू नय
लिंग आदि का भेद न होने पर भी शब्दभेद से अर्थ का भेद मानने वाला समभिरुद्ध है। जहां शब्द नय शब्दभेद से अर्थभेद नहीं मानता, वहां यह नय शब्दभेद द्वारा अर्थभेद स्वीकार करता है जैसे इन्द्र, शक्र, पुरन्दर – ये तीनों शब्द स्वर्ग के स्वामी इन्द्र के वाचक और सभी पर्यायवाची एवं एक ही लिंग के हैं, किंतु ये तीनों शब्द उस इन्द्र के भिन्न-भिन्न धर्मों को कहते हैं अर्थात् जब आनंद करता है तब इन्द्र, शक्तिशाली होने से शक्र तथा नगरों को नष्ट करने वाला होने से पुरन्दर कहा जाता है। इस प्रकार यह नय पर्याय भेद से शब्द के भिन्न अर्थ मानता है।
7. एवंभूत नय :
जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ है, वह क्रिया जब हो रही हो तभी उस पदार्थ को ग्रहण करने वाला वचन और ज्ञान एवंभूत नय कहलाता है । समभिरूढ़ नय जहां शब्द - भेद के अनुसार अर्थभेद करता है, वहां एवंभूत नय व्युत्पत्यर्थ के घटित होने पर ही शब्दभेद के अनुसार अर्थभेद करता है। इसके अनुसार जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ
स्वर्ण जयंती वर्ष
जैन भारती
For Private & Personal Use Only
मार्च - मई, 2002
www.jainelibrary.org