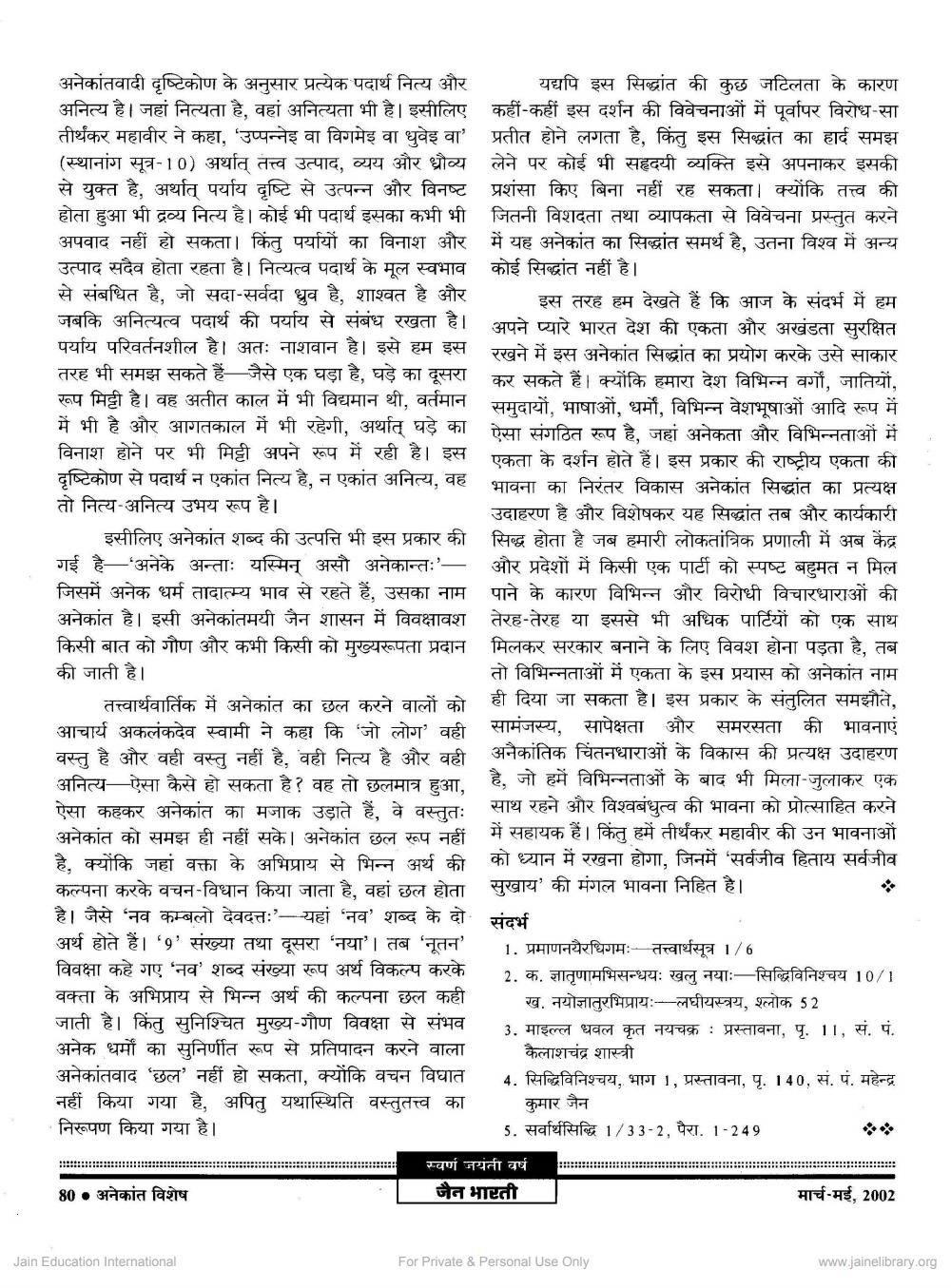________________
अनेकांतवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक पदार्थ नित्य और यद्यपि इस सिद्धांत की कुछ जटिलता के कारण अनित्य है। जहां नित्यता है, वहां अनित्यता भी है। इसीलिए कहीं-कहीं इस दर्शन की विवेचनाओं में पूर्वापर विरोध-सा तीर्थंकर महावीर ने कहा, 'उप्पन्नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा' प्रतीत होने लगता है, किंतु इस सिद्धांत का हार्द समझ (स्थानांग सूत्र-10) अर्थात् तत्त्व उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लेने पर कोई भी सहृदयी व्यक्ति इसे अपनाकर इसकी से युक्त है, अर्थात् पर्याय दृष्टि से उत्पन्न और विनष्ट प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि तत्त्व की होता हुआ भी द्रव्य नित्य है। कोई भी पदार्थ इसका कभी भी जितनी विशदता तथा व्यापकता से विवेचना प्रस्तुत करने अपवाद नहीं हो सकता। किंतु पर्यायों का विनाश और में यह अनेकांत का सिद्धांत समर्थ है, उतना विश्व में अन्य उत्पाद सदैव होता रहता है। नित्यत्व पदार्थ के मूल स्वभाव कोई सिद्धांत नहीं है। से संबधित है, जो सदा-सर्वदा ध्रुव है, शाश्वत है और
इस तरह हम देखते हैं कि आज के संदर्भ में हम जबकि अनित्यत्व पदार्थ की पर्याय से संबंध रखता है। अपने प्यारे भारत देश की एकता और अखंडता सुरक्षित पर्याय परिवर्तनशील है। अतः नाशवान है। इसे हम इस रखने में इस अनेकांत सिद्धांत का प्रयोग करके उसे साकार तरह भी समझ सकते हैं जैसे एक घड़ा है, घड़े का दूसरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश विभिन्न वर्गों, जातियों, रूप मिट्टी है। वह अतीत काल में भी विद्यमान थी, वर्तमान समदायों भाषाओंभों विभिन्न भाषाओं आदि कप में में भी है और आगतकाल में भी रहेगी, अर्थात् घड़े का
ऐसा संगठित रूप है, जहां अनेकता और विभिन्नताओं में विनाश होने पर भी मिट्टी अपने रूप में रही है। इस
एकता के दर्शन होते हैं। इस प्रकार की राष्ट्रीय एकता की दृष्टिकोण से पदार्थ न एकांत नित्य है, न एकांत अनित्य, वह
भावना का निरंतर विकास अनेकांत सिद्धांत का प्रत्यक्ष तो नित्य-अनित्य उभय रूप है।
उदाहरण है और विशेषकर यह सिद्धांत तब और कार्यकारी इसीलिए अनेकांत शब्द की उत्पत्ति भी इस प्रकार की सिद्ध होता है जब हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में अब केंद्र गई है—'अनेके अन्ताः यस्मिन् असौ अनेकान्तः'- और प्रदेशों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल जिसमें अनेक धर्म तादात्म्य भाव से रहते हैं, उसका नाम पाने के कारण विभिन्न और विरोधी विचारधाराओं की
अनेकांत है। इसी अनेकांतमयी जैन शासन में विवक्षावश तेरह-तेरह या इससे भी अधिक पार्टियों को एक साथ किसी बात को गौण और कभी किसी को मुख्यरूपता प्रदान मिलकर सरकार बनाने के लिए विवश होना पड़ता है, तब की जाती है।
तो विभिन्नताओं में एकता के इस प्रयास को अनेकांत नाम तत्त्वार्थवार्तिक में अनेकांत का छल करने वालों को ही दिया जा सकता है। इस प्रकार के संतुलित समझौते. आचार्य अकलंकदेव स्वामी ने कहा कि जो लोग' वही सामंजस्य, सापेक्षता और समरसता की भावनाएं वस्तु है और वही वस्तु नहीं है, वही नित्य है और वही अनेकांतिक चिंतनधाराओं के विकास की प्रत्यक्ष उदाहरण अनित्य—ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो छलमात्र हुआ, ह, जा हम वा
हा है, जो हमें विभिन्नताओं के बाद भी मिला-जुलाकर एक ऐसा कहकर अनेकांत का मजाक उड़ाते हैं, वे वस्तुतः
साथ रहने और विश्वबंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने अनेकांत को समझ ही नहीं सके। अनेकांत छल रूप नहीं में सहायक हैं। किंतु हमें तीर्थंकर महावीर की उन भावनाओं है, क्योंकि जहां वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की को ध्यान में रखना होगा, जिनमें 'सर्वजीव हिताय सर्वजीव कल्पना करके वचन-विधान किया जाता है. वहां छल होता सुखाय' की मंगल भावना निहित है। है। जैसे 'नव कम्बलो देवदत्तः'- यहां 'नव' शब्द के दो संदर्भ अर्थ होते हैं। '9' संख्या तथा दूसरा 'नया'| तब 'नूतन' 1. प्रमाणनयैरधिगमः तत्त्वार्थसूत्र 1/6 विवक्षा कहे गए 'नव' शब्द संख्या रूप अर्थ विकल्प करके
2. क. ज्ञातृणामभिसन्धयः खलु नयाः-सिद्धिविनिश्चय 10/1 वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना छल कही
ख. नयोज्ञातुरभिप्राय:-लघीयस्त्रय, श्लोक 52 जाती है। किंतु सुनिश्चित मुख्य-गौण विवक्षा से संभव
3. माइल्ल धवल कृत नयचक्र : प्रस्तावना, पृ. 11, सं. पं. अनेक धर्मों का सुनिर्णीत रूप से प्रतिपादन करने वाला
कैलाशचंद्र शास्त्री अनेकांतवाद 'छल' नहीं हो सकता, क्योंकि वचन विघात
4. सिद्धिविनिश्चय, भाग 1, प्रस्तावना, पृ. 140, सं. पं. महेन्द्र नहीं किया गया है, अपितु यथास्थिति वस्तुतत्त्व का कुमार जैन निरूपण किया गया है।
5. सर्वार्थसिद्धि 1/33-2, पैरा. 1-249
स्वर्ण जयंती वर्ष 80. अनेकांत विशेष
जैन भारती
मार्च-मई, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org