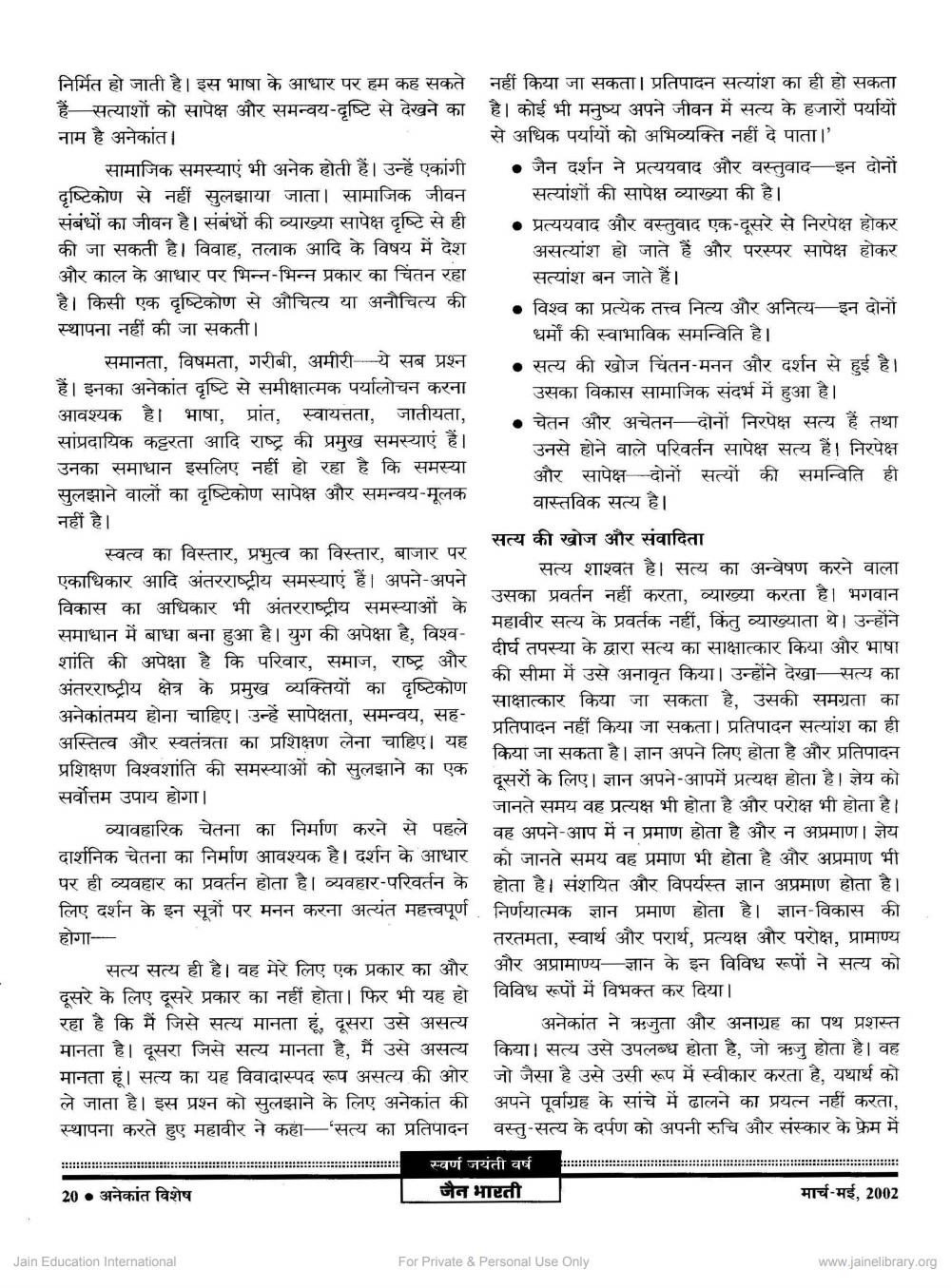________________
निर्मित हो जाती है। इस भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं— सत्याशों को सापेक्ष और समन्वय-दृष्टि से देखने का नाम है अनेकांत ।
सामाजिक समस्याएं भी अनेक होती हैं। उन्हें एकांगी दृष्टिकोण से नहीं सुलझाया जाता। सामाजिक जीवन संबंधों का जीवन है। संबंधों की व्याख्या सापेक्ष दृष्टि से ही की जा सकती है विवाह, तलाक आदि के विषय में देश और काल के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार का चिंतन रहा है किसी एक दृष्टिकोण से औचित्य या अनौचित्य की स्थापना नहीं की जा सकती।
समानता, विषमता, गरीबी, अमीरी ये सब प्रश्न हैं। इनका अनेकांत दृष्टि से समीक्षात्मक पर्यालोचन करना आवश्यक है। भाषा, प्रांत, स्वायत्तता, जातीयता, सांप्रदायिक कहरता आदि राष्ट्र की प्रमुख समस्याएं हैं। उनका समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि समस्या सुलझाने वालों का दृष्टिकोण सापेक्ष और समन्वय-मूलक नहीं है।
स्वत्व का विस्तार, प्रभुत्व का विस्तार, बाजार पर एकाधिकार आदि अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं। अपने-अपने विकास का अधिकार भी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में बाधा बना हुआ है। युग की अपेक्षा है, विश्वशांति की अपेक्षा है कि परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों का दृष्टिकोण अनेकांतमय होना चाहिए। उन्हें सापेक्षता, समन्वय, सहअस्तित्व और स्वतंत्रता का प्रशिक्षण लेना चाहिए। यह प्रशिक्षण विश्वशांति की समस्याओं को सुलझाने का एक सर्वोत्तम उपाय होगा।
व्यावहारिक चेतना का निर्माण करने से पहले दार्शनिक चेतना का निर्माण आवश्यक है। दर्शन के आधार पर ही व्यवहार का प्रवर्तन होता है। व्यवहार परिवर्तन के लिए दर्शन के इन सूत्रों पर मनन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा
सत्य सत्य ही है। वह मेरे लिए एक प्रकार का और दूसरे के लिए दूसरे प्रकार का नहीं होता। फिर भी यह हो रहा है कि मैं जिसे सत्य मानता हूं, दूसरा उसे असत्य मानता है। दूसरा जिसे सत्य मानता है, मैं उसे असत्य मानता हूं। सत्य का यह विवादास्पद रूप असत्य की ओर ले जाता है। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए अनेकांत की स्थापना करते हुए महावीर ने कहा- 'सत्य का प्रतिपादन
20 • अनेकांत विशेष
Jain Education International
नहीं किया जा सकता । प्रतिपादन सत्यांश का ही हो सकता है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सत्य के हजारों पर्यायों से अधिक पर्यायों को अभिव्यक्ति नहीं दे पाता ।'
जैन दर्शन ने प्रत्ययवाद और वस्तुवाद— इन दोनों सत्यांशों की सापेक्ष व्याख्या की है।
• प्रत्ययवाद और वस्तुवाद एक-दूसरे से निरपेक्ष होकर असत्यांश हो जाते हैं और परस्पर सापेक्ष होकर सत्यांश बन जाते हैं।
● विश्व का प्रत्येक तत्त्व नित्य और अनित्य इन दोनों धर्मों की स्वाभाविक समन्विति है।
• सत्य की खोज चिंतन-मनन और दर्शन से हुई है। उसका विकास सामाजिक संदर्भ में हुआ है।
• चेतन और अचेतन— दोनों निरपेक्ष सत्य हैं तथा उनसे होने वाले परिवर्तन सापेक्ष सत्य हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों सत्यों की समन्विति ही वास्तविक सत्य है ।
सत्य की खोज और संवादिता
सत्य शाश्वत है। सत्य का अन्वेषण करने वाला उसका प्रवर्तन नहीं करता, व्याख्या करता है। भगवान महावीर सत्य के प्रवर्तक नहीं, किंतु व्याख्याता थे। उन्होंने दीर्घ तपस्या के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया और भाषा की सीमा में उसे अनावृत किया। उन्होंने देखा – सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है, उसकी समग्रता का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। प्रतिपादन सत्यांश का ही किया जा सकता है। ज्ञान अपने लिए होता है और प्रतिपादन दूसरों के लिए। ज्ञान अपने-आपमें प्रत्यक्ष होता है । ज्ञेय को जानते समय वह प्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। वह अपने आप में न प्रमाण होता है और न अप्रमाण ज्ञेय को जानते समय वह प्रमाण भी होता है और अप्रमाण भी होता है। संशयित और विपर्यस्त ज्ञान अप्रमाण होता है। निर्णयात्मक ज्ञान प्रमाण होता है। ज्ञान विकास की तरतमता, स्वार्थ और परार्थ, प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रामाण्य और अप्रामाण्य- -ज्ञान के इन विविध रूपों ने सत्य को विविध रूपों में विभक्त कर दिया।
अनेकांत ने ऋजुता और अनाग्रह का पथ प्रशस्त किया। सत्य उसे उपलब्ध होता है, जो ऋजु होता है। वह जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करता है, यथार्थ को अपने पूर्वाग्रह के सांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करता, वस्तु सत्य के दर्पण को अपनी रुचि और संस्कार के फ्रेम में स्वर्ण जयंती वर्ष जैन भारती
For Private & Personal Use Only
मार्च - मई, 2002
www.jainelibrary.org