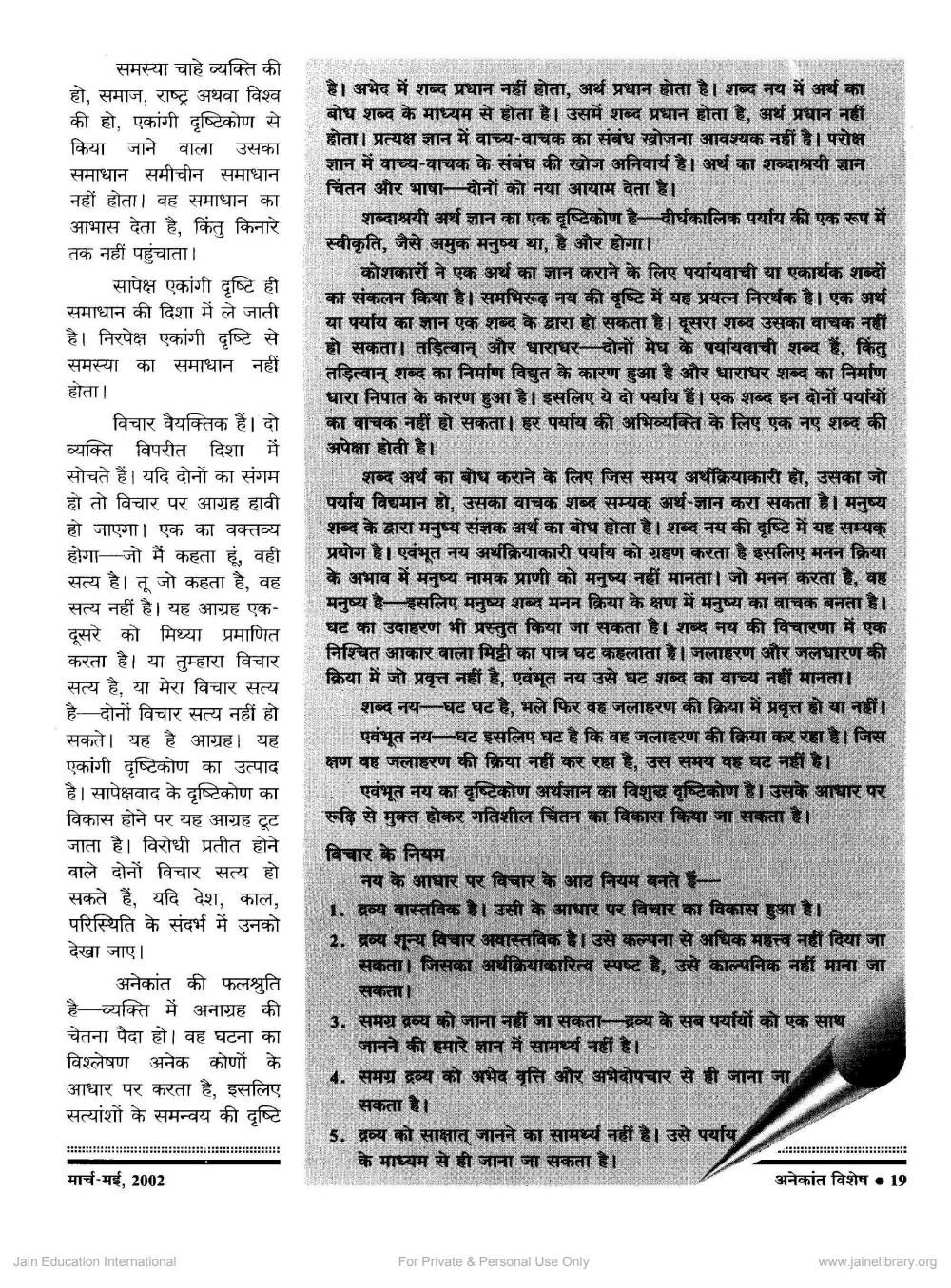________________
समस्या चाहे व्यक्ति की हो, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व की हो, एकांगी दृष्टिकोण से किया जाने वाला उसका समाधान समीचीन समाधान नहीं होता। वह समाधान का आभास देता है, किंतु किनारे तक नहीं पहुंचाता।
सापेक्ष एकांगी दृष्टि ही समाधान की दिशा में ले जाती है। निरपेक्ष एकांगी दृष्टि से समस्या का समाधान नहीं होता।
विचार वैयक्तिक हैं। दो व्यक्ति विपरीत दिशा में सोचते हैं। यदि दोनों का संगम हो तो विचार पर आग्रह हावी हो जाएगा। एक का वक्तव्य होगा—जो मैं कहता हूं, वही सत्य है। तू जो कहता है, वह सत्य नहीं है। यह आग्रह एकदूसरे को मिथ्या प्रमाणित करता है। या तुम्हारा विचार सत्य है, या मेरा विचार सत्य है—दोनों विचार सत्य नहीं हो सकते। यह है आग्रह। यह एकांगी दृष्टिकोण का उत्पाद है। सापेक्षवाद के दृष्टिकोण का विकास होने पर यह आग्रह टूट जाता है। विरोधी प्रतीत होने वाले दोनों विचार सत्य हो सकते हैं, यदि देश, काल, परिस्थिति के संदर्भ में उनको देखा जाए।
अनेकांत की फलश्रुति है—व्यक्ति में अनाग्रह की चेतना पैदा हो। वह घटना का विश्लेषण अनेक कोणों के आधार पर करता है, इसलिए सत्यांशों के समन्वय की दृष्टि
है। अभेद में शब्द प्रधान नहीं होता, अर्थ प्रधान होता है। शब्द नय में अर्थ का बोध शब्द के माध्यम से होता है। उसमें शब्द प्रधान होता है, अर्थ प्रधान नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान में वाच्य-वाचक का संबंध खोजना आवश्यक नहीं है। परोक्ष ज्ञान में वाच्य-वाचक के संबंध की खोज अनिवार्य है। अर्थ का शब्दाश्रयी ज्ञान चिंतन और भाषा-दोनों को नया आयाम देता है।
- शब्दाश्रयी अर्थ ज्ञान का एक दृष्टिकोण है-दीर्घकालिक पर्याय की एक रूप में - स्वीकृति, जैसे अमुक मनुष्य था, है और होगा।
कोशकारों ने एक अर्थ का ज्ञान कराने के लिए पर्यायवाची या एकार्थक शब्दों का संकलन किया है। समभिरूढ नय की दृष्टि में यह प्रयत्न निरर्थक है। एक अर्थ या पर्याय का ज्ञान एक शब्द के द्वारा हो सकता है। दूसरा शब्द उसका वाचक नहीं हो सकता। तडित्वान् और धाराधर-दोनों मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु तड़ित्वान् शब्द का निर्माण विद्युत के कारण हुआ है और धाराधर शब्द का निर्माण धारा निपात के कारण हुआ है। इसलिए ये दो पर्याय हैं। एक शब्द इन दोनों पर्यायों । का वाचक नहीं हो सकता। हर पर्याय की अभिव्यक्ति के लिए एक नए शब्द की अपेक्षा होती है।।
शब्द अर्थ का बोध कराने के लिए जिस समय अर्थक्रियाकारी हो, उसका जो पर्याय विद्यमान हो, उसका वाचक शब्द सम्यक् अर्थ-ज्ञान करा सकता है। मनुष्य शब्द के द्वारा मनुष्य संज्ञक अर्थ का बोध होता है। शब्द नय की दृष्टि में यह सम्यक प्रयोग है। एवंभूत नय अर्थक्रियाकारी पर्याय को ग्रहण करता है इसलिए मनन क्रिया
के अभाव में मनुष्य नामक प्राणी को मनुष्य नहीं मानता। जो मनन करता है, वह 1 मनुष्य है इसलिए मनुष्य शब्द मनन क्रिया के क्षण में मनुष्य का वाचक बनता है। । घट का उदाहरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शब्द नय की विचारणा में एक
निश्चित आकार वाला मिट्टी का पात्र घट कहलाता है। जलाहरण और जलधारण की क्रिया में जो प्रवृत्त नहीं है, एवंभूत नय उसे घट शब्द का वाच्य नहीं मानता।
शब्द नय-घट घट है, भले फिर वह जलाहरण की क्रिया में प्रवृत्त हो या नहीं।
एवंभूत नय-घट इसलिए घट है कि वह जलाहरण की क्रिया कर रहा है। जिस । क्षण वह जलाहरण की क्रिया नहीं कर रहा है, उस समय वह घट नहीं है।
एवंभूत नय का दृष्टिकोण अर्थज्ञान का विशुद्ध दृष्टिकोण है। उसके आधार पर । रूढ़ि से मुक्त होकर गतिशील चिंतन का विकास किया जा सकता है। विचार के नियम
नय के आधार पर विचार के आठ नियम बनते हैं। द्रव्य वास्तविक है। उसी के आधार पर विचार का विकास हुआ है। . द्रव्य शून्य विचार अवास्तविक है। उसे कल्पना से अधिक महत्त्व नहीं दिया जा
सकता। जिसका अर्थक्रियाकारित्व स्पष्ट है, उसे काल्पनिक नहीं माना जा । सकता। 13. समग्र द्रव्य को जाना नहीं जा सकता-द्रव्य के सब पर्यायों को एक साथ
जानने की हमारे ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है। 14. समग्र द्रव्य को अभेद वृत्ति और अभेदोपचार से ही जाना जा
सकता है। 5. द्रव्य को साक्षात् जानने का सामर्थ्य नहीं है। उसे पर्याय के माध्यम से ही जाना जा सकता है।
अनेकांत विशेष.19
TrumDE
मार्च-मई, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org