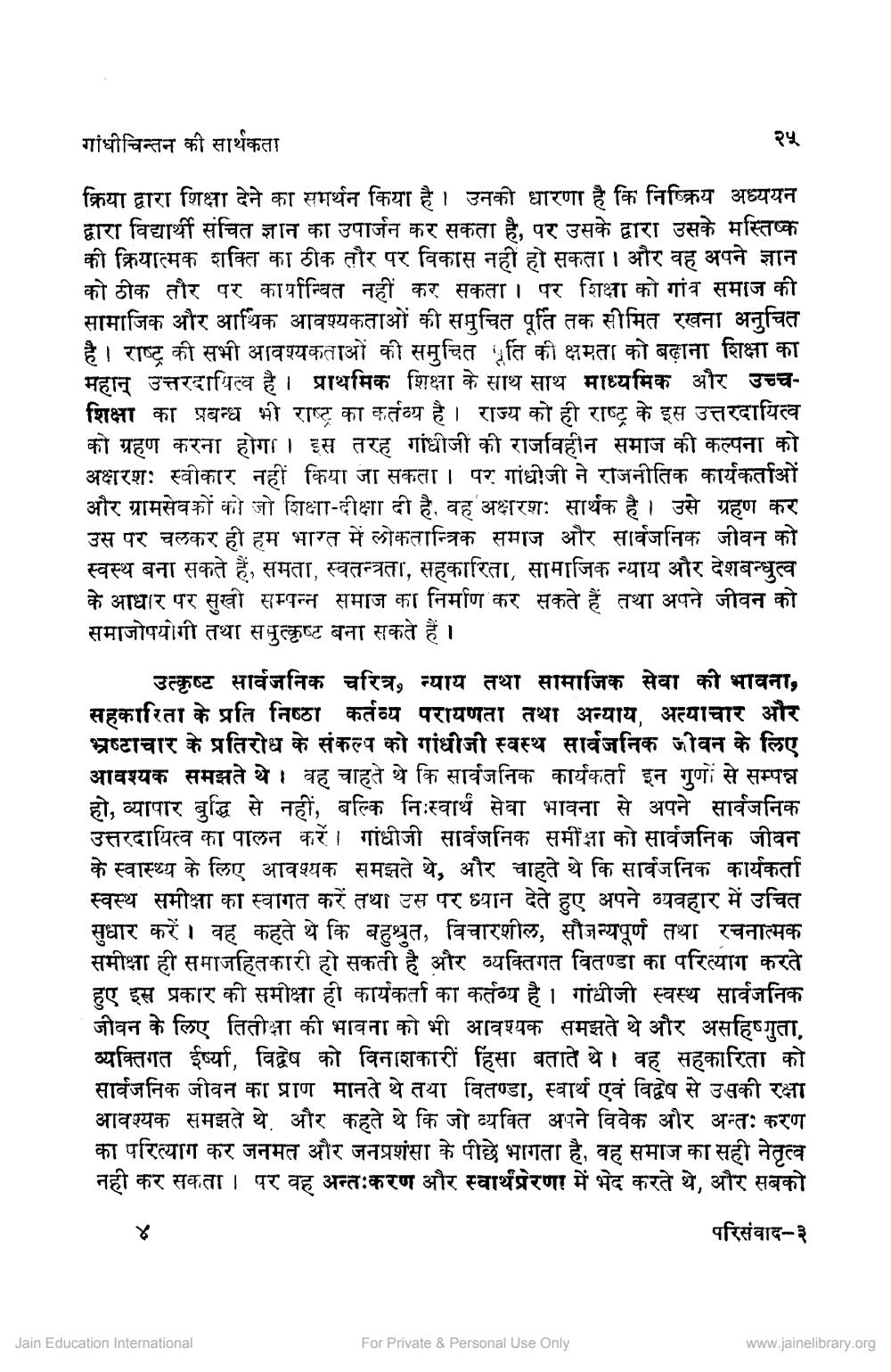________________
गांधीचिन्तन की सार्थकता
ર૫ क्रिया द्वारा शिक्षा देने का समर्थन किया है। उनको धारणा है कि निष्क्रिय अध्ययन द्वारा विद्यार्थी संचित ज्ञान का उपार्जन कर सकता है, पर उसके द्वारा उसके मस्तिष्क की क्रियात्मक शक्ति का ठीक तौर पर विकास नहीं हो सकता। और वह अपने ज्ञान को ठीक तौर पर कार्यान्वित नहीं कर सकता। पर शिक्षा को गांव समाज की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति तक सीमित रखना अनुचित है। राष्ट्र की सभी आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति की क्षमता को बढ़ाना शिक्षा का महान् उत्तरदायित्व है। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक और उच्चशिक्षा का प्रबन्ध भी राष्ट्र का कर्तव्य है। राज्य को ही राष्ट्र के इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करना होगा। इस तरह गांधीजी की राजविहीन समाज की कल्पना को अक्षरशः स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर गांधीजी ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ग्रामसेवकों को जो शिक्षा-दीक्षा दी है, वह अक्षरशः सार्थक है। उसे ग्रहण कर उस पर चलकर ही हम भारत में लोकतान्त्रिक समाज और सार्वजनिक जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, समता, स्वतन्त्रता, सहकारिता, सामाजिक न्याय और देशबन्धुत्व के आधार पर सुखी सम्पन्न समाज का निर्माण कर सकते हैं तथा अपने जीवन को समाजोपयोगी तथा समुत्कृष्ट बना सकते हैं।
उत्कृष्ट सार्वजनिक चरित्र, न्याय तथा सामाजिक सेवा की भावना, सहकारिता के प्रति निष्ठा कर्तव्य परायणता तथा अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के प्रतिरोध के संकल्प को गांधीजी स्वस्थ सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक समझते थे। वह चाहते थे कि सार्वजनिक कार्यकर्ता इन गुणों से सम्पन्न हो, व्यापार बुद्धि से नहीं, बल्कि निःस्वार्थ सेवा भावना से अपने सार्वजनिक उत्तरदायित्व का पालन करें। गांधीजी सार्वजनिक समीक्षा को सार्वजनिक जीवन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक समझते थे, और चाहते थे कि सार्वजनिक कार्यकर्ता स्वस्थ समीक्षा का स्वागत करें तथा उस पर ध्यान देते हुए अपने व्यवहार में उचित सुधार करें। वह कहते थे कि बहुश्रुत, विचारशील, सौजन्यपूर्ण तथा रचनात्मक समीक्षा ही समाजहितकारी हो सकती है और व्यक्तिगत वितण्डा का परित्याग करते हुए इस प्रकार की समीक्षा ही कार्यकर्ता का कर्तव्य है। गांधीजी स्वस्थ सार्वजनिक जीवन के लिए तितीक्षा की भावना को भी आवश्यक समझते थे और असहिष्णुता, व्यक्तिगत ईर्ष्या, विद्वेष को विनाशकारी हिंसा बताते थे। वह सहकारिता को सार्वजनिक जीवन का प्राण मानते थे तथा वितण्डा, स्वार्थ एवं विद्वेष से उसकी रक्षा आवश्यक समझते थे. और कहते थे कि जो व्यक्ति अपने विवेक और अन्तः करण का परित्याग कर जनमत और जनप्रशंसा के पीछे भागता है, वह समाज का सही नेतृत्व नही कर सकता । पर वह अन्तःकरण और स्वार्थप्रेरणा में भेद करते थे, और सबको
परिसंवाद-३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org