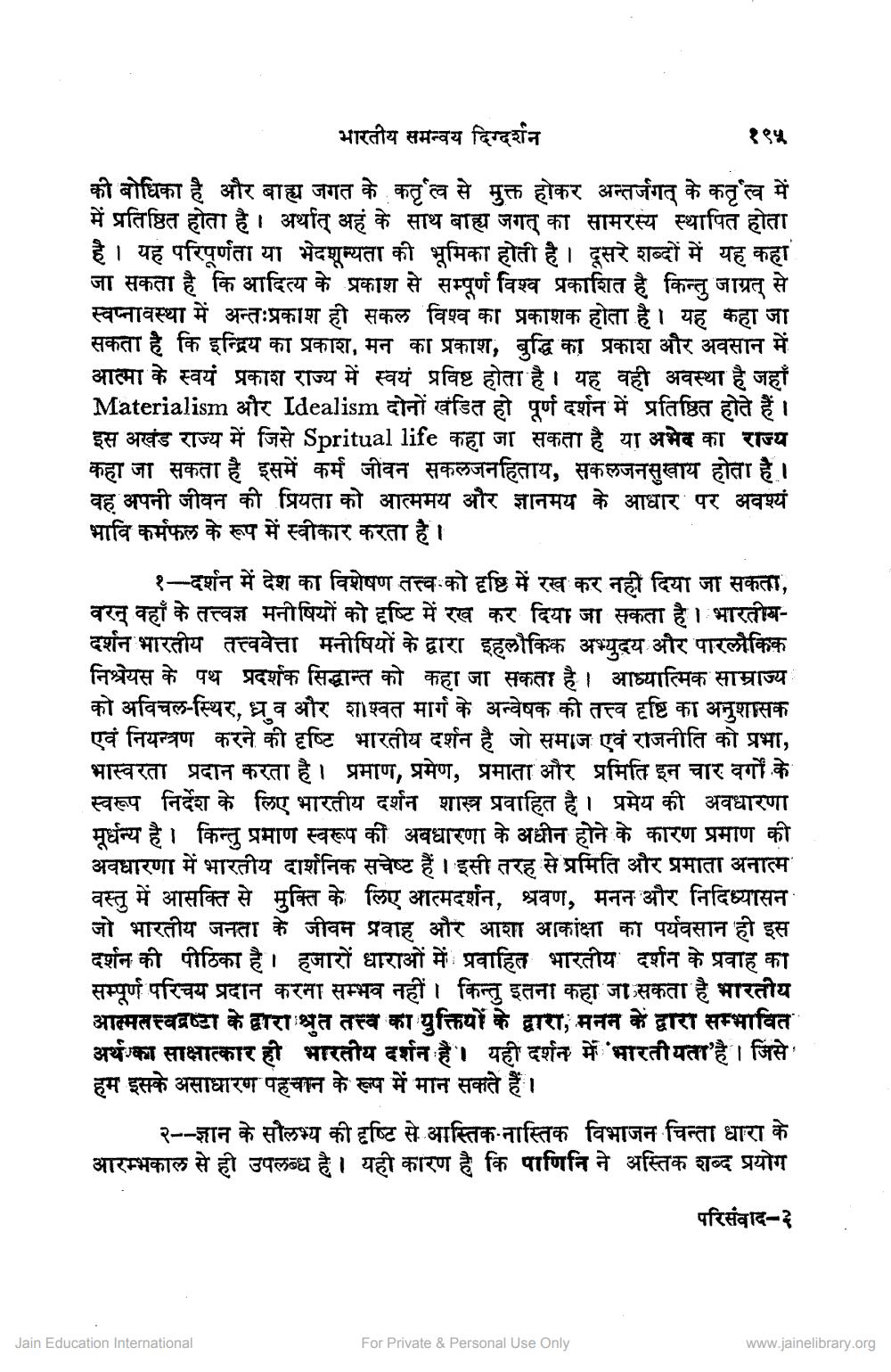________________
भारतीय समन्वय दिग्दर्शन
की बोधिका है और बाह्य जगत के कर्तृत्व से मुक्त होकर अन्तर्जगत् के कर्तृत्व में में प्रतिष्ठित होता है। अर्थात् अहं के साथ बाह्य जगत् का सामरस्य स्थापित होता है। यह परिपूर्णता या भेदशून्यता की भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आदित्य के प्रकाश से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित है किन्तु जाग्रत् से स्वप्नावस्था में अन्तःप्रकाश ही सकल विश्व का प्रकाशक होता है। यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिय का प्रकाश, मन का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश और अवसान में आत्मा के स्वयं प्रकाश राज्य में स्वयं प्रविष्ट होता है। यह वही अवस्था है जहाँ Materialism और Idealism दोनों खंडित हो पूर्ण दर्शन में प्रतिष्ठित होते हैं। इस अखंड राज्य में जिसे Spritual life कहा जा सकता है या अभेद का राज्य कहा जा सकता है इसमें कर्म जीवन सकलजनहिताय, सकलजनसुखाय होता है। वह अपनी जीवन की प्रियता को आत्ममय और ज्ञानमय के आधार पर अवश्यं भावि कर्मफल के रूप में स्वीकार करता है।
१-दर्शन में देश का विशेषण तत्त्व को दृष्टि में रख कर नहीं दिया जा सकता, वरन् वहाँ के तत्त्वज्ञ मनीषियों को दृष्टि में रख कर दिया जा सकता है। भारतीयदर्शन भारतीय तत्त्ववेत्ता मनीषियों के द्वारा इहलौकिक अभ्युदय और पारलौकिक निश्रेयस के पथ प्रदर्शक सिद्धान्त को कहा जा सकता है। आध्यात्मिक साम्राज्य को अविचल-स्थिर, ध्रुव और शाश्वत मार्ग के अन्वेषक की तत्त्व दृष्टि का अनुशासक एवं नियन्त्रण करने की दृष्टि भारतीय दर्शन है जो समाज एवं राजनीति को प्रभा, भास्वरता प्रदान करता है। प्रमाण, प्रमेण, प्रमाता और प्रमिति इन चार वर्गों के स्वरूप निर्देश के लिए भारतीय दर्शन शास्त्र प्रवाहित है। प्रमेय की अवधारणा मूर्धन्य है। किन्तु प्रमाण स्वरूप की अवधारणा के अधीन होने के कारण प्रमाण की अवधारणा में भारतीय दार्शनिक सचेष्ट हैं । इसी तरह से प्रमिति और प्रमाता अनात्म वस्तु में आसक्ति से मुक्ति के लिए आत्मदर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन जो भारतीय जनता के जीवन प्रवाह और आशा आकांक्षा का पर्यवसान ही इस दर्शन की पीठिका है। हजारों धाराओं में प्रवाहित भारतीय दर्शन के प्रवाह का सम्पूर्ण परिचय प्रदान करना सम्भव नहीं। किन्तु इतना कहा जा सकता है भारतीय आत्मतत्त्वद्रष्टा के द्वारा श्रुत तत्त्व का युक्तियों के द्वारा, मनन के द्वारा सम्भावित अर्थका साक्षात्कार ही भारतीय दर्शन है। यही दर्शन में भारतीयता है। जिसे हम इसके असाधारण पहचान के रूप में मान सकते हैं।
२--ज्ञान के सौलभ्य की दृष्टि से आस्तिक-नास्तिक विभाजन चिन्ता धारा के आरम्भकाल से ही उपलब्ध है। यही कारण है कि पाणिनि ने अस्तिक शब्द प्रयोग
परिसंवाद-३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org