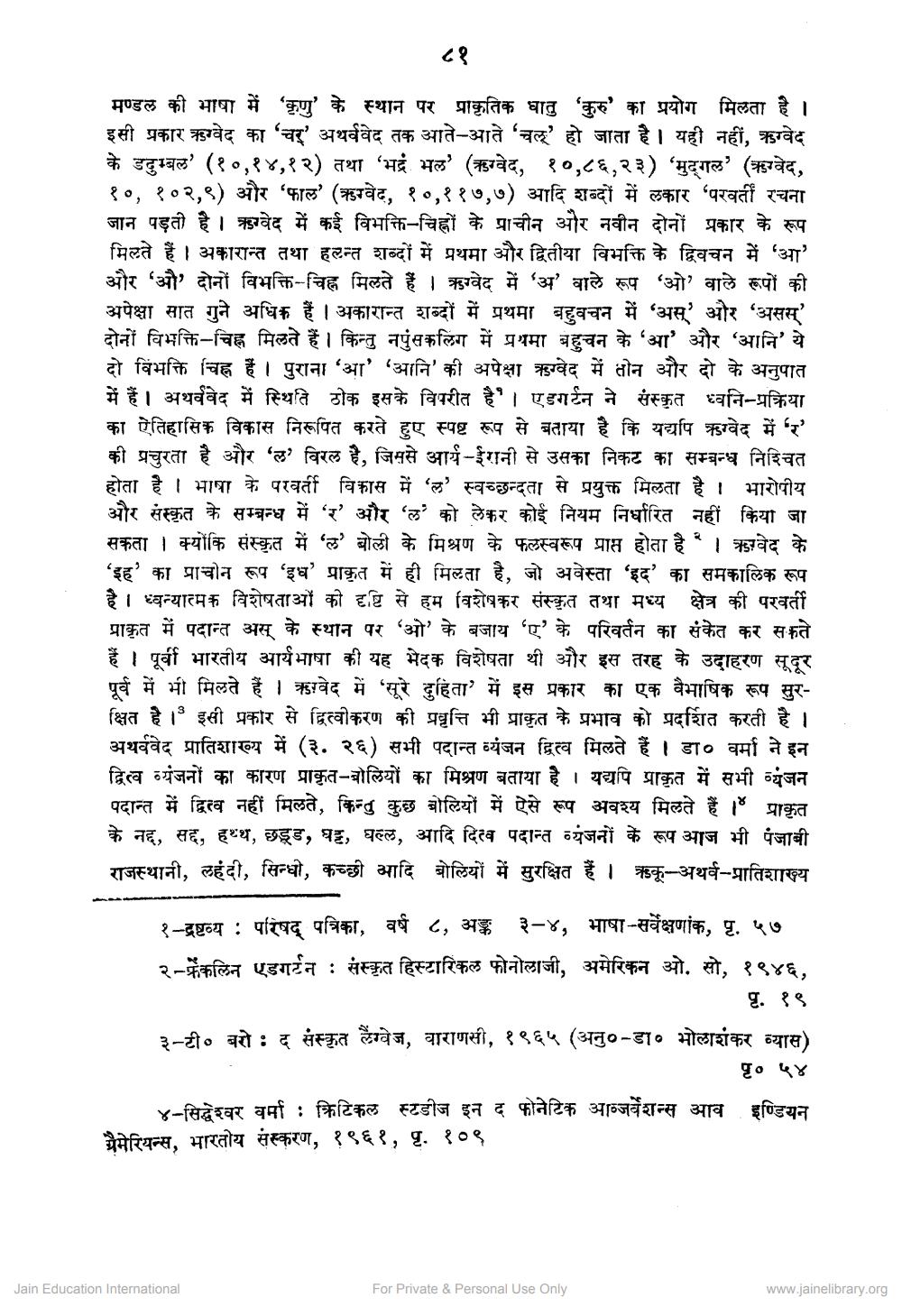________________
मण्डल की भाषा में 'कृणु' के स्थान पर प्राकृतिक धातु 'कुरु' का प्रयोग मिलता है । इसी प्रकार ऋग्वेद का 'चर्' अथर्ववेद तक आते-आते 'चल्' हो जाता है। यही नहीं, ऋग्वेद के उदुम्बल' (१०,१४,१२) तथा 'भद्रं भल' (ऋग्वेद, १०,८६,२३) 'मुद्गल' (ऋग्वेद, १०, १०२,९) और 'फाल' (ऋग्वेद, १०,११७,७) आदि शब्दों में लकार 'परवर्ती रचना जान पड़ती है । ऋग्वेद में कई विभक्ति-चिह्नों के प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं । अकारान्त तथा हलन्त शब्दों में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में 'आ' और 'औ' दोनों विभक्ति-चिह्न मिलते हैं । ऋग्वेद में 'अ' वाले रूप 'ओ' वाले रूपों की अपेक्षा सात गुने अधिक हैं । अकारान्त शब्दों में प्रथमा बहुवचन में 'अस्' और 'असस्' दोनों विभक्ति-चिह्न मिलते हैं । किन्तु नपुंसकलिंग में प्रथमा बहुचन के 'आ' और 'आनि' ये
भक्ति चिह्न है । पुराना 'आ' 'आनि' की अपेक्षा ऋग्वेद में तोन और दो के अनुपात में हैं । अथर्ववेद में स्थिति ठोक इसके विपरीत है। एडगर्टन ने संस्कृत ध्वनि-प्रक्रिया का ऐतिहासिक विकास निरूपित करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि यद्यपि ऋग्वेद में 'र' की प्रचुरता है और 'ल' विरल है, जिससे आर्य-ईरानी से उसका निकट का सम्बन्ध निश्चित होता है । भाषा के परवर्ती विकास में 'ल' स्वच्छन्दता से प्रयुक्त मिलता है। भारोपीय
और संस्कृत के सम्बन्ध में 'र' और 'ल' को लेकर कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता । क्योंकि संस्कृत में 'ल' बोली के मिश्रण के फलस्वरूप प्राप्त होता है २ । ऋग्वेद के 'इह' का प्राचीन रूप 'इध' प्राकृत में ही मिलता है, जो अवेस्ता 'इद' का समकालिक रूप है। ध्वन्यात्मक विशेषताओं को दृष्टि से हम विशेषकर संस्कृत तथा मध्य क्षेत्र की परवर्ती प्राकृत में पदान्त अस् के स्थान पर 'ओ' के बजाय 'ए' के परिवर्तन का संकेत कर सकते हैं । पूर्वी भारतीय आर्यभाषा की यह भेदक विशेषता थी और इस तरह के उदाहरण सूदूर पूर्व में भी मिलते हैं । ऋग्वेद में 'सूरे दुहिता' में इस प्रकार का एक वैभाषिक रूप सुरक्षित है। इसी प्रकार से द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति भी प्राकृत के प्रभाव को प्रदर्शित करती है ।
अथर्ववेद प्रातिशाख्य में (३. २६) सभी पदान्त व्यंजन द्वित्व मिलते हैं । डा० वर्मा ने इन द्वित्व व्यंजनों का कारण प्राकृत-बोलियों का मिश्रण बताया है । यद्यपि प्राकृत में सभी व्यंजन पदान्त में द्वित्व नहीं मिलते, किन्तु कुछ बोलियों में ऐसे रूप अवश्य मिलते हैं। प्राकृत के नद, सद्द, हथ्थ, छडूड, घट्ट, घल्ल, आदि दित्व पदान्त व्यंजनों के रूप आज भी पंजाबी राजस्थानी, लहंदी, सिन्धो, कच्छी आदि बोलियों में सुरक्षित हैं । ऋकू-अथर्व-प्रातिशाख्य
१-द्रष्टव्य : परिषद् पत्रिका, वर्ष ८, अङ्क ३-४, भाषा-सर्वेक्षणांक, पृ. ५७ २-फ्रेंकलिन एडगर्टन : संस्कृत हिस्टारिकल फोनोलाजी, अमेरिकन ओ. सो, १९४६,
३-टी० बरो : द संस्कृत लैंग्वेज, वाराणसी, १९६५ (अनु०-डा. भोलाशंकर व्यास)
पृ० ५४ ४-सिद्धेश्वर वर्मा : क्रिटिकल स्टडीज इन द फोनेटिक आब्जर्वेशन्स आव इण्डियन ग्रैमेरियन्स, भारतीय संस्करण, १९६१, पृ. १०९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org