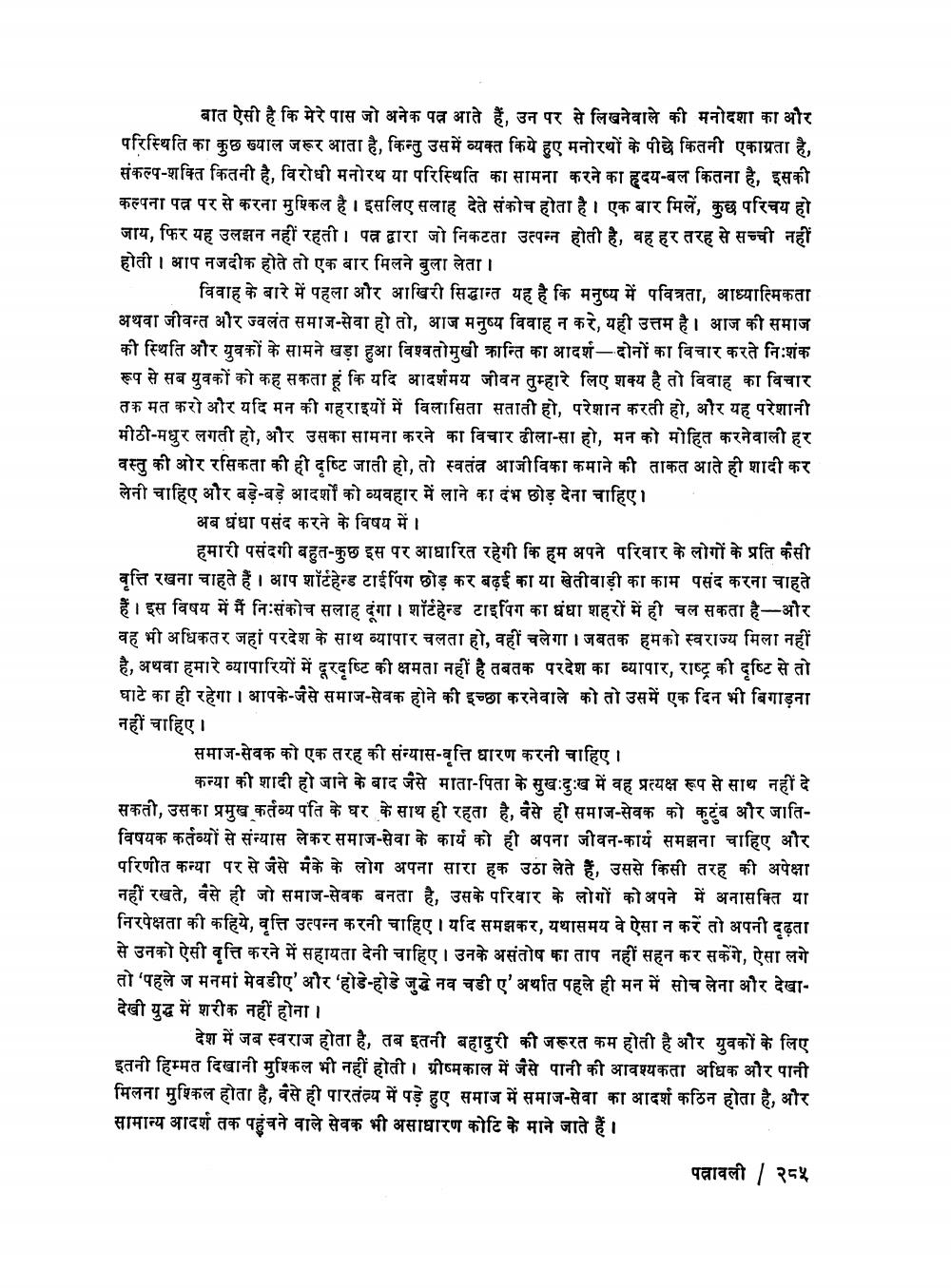________________
बात ऐसी है कि मेरे पास जो अनेक पत्र आते हैं, उन पर से लिखनेवाले की मनोदशा का और परिस्थिति का कुछ ख्याल जरूर आता है, किन्तु उसमें व्यक्त किये हुए मनोरथों के पीछे कितनी एकाग्रता है, संकल्प-शक्ति कितनी है, विरोधी मनोरथ या परिस्थिति का सामना करने का हृदय-बल कितना है, इसकी कल्पना पत्र पर से करना मुश्किल है। इसलिए सलाह देते संकोच होता है। एक बार मिलें, कुछ परिचय हो जाय, फिर यह उलझन नहीं रहती। पत्र द्वारा जो निकटता उत्पन्न होती है, वह हर तरह से सच्ची नहीं होती। आप नजदीक होते तो एक बार मिलने बुला लेता।
विवाह के बारे में पहला और आखिरी सिद्धान्त यह है कि मनुष्य में पवित्रता, आध्यात्मिकता अथवा जीवन्त और ज्वलंत समाज-सेवा हो तो, आज मनुष्य विवाह न करे, यही उत्तम है। आज की समाज की स्थिति और युवकों के सामने खड़ा हुआ विश्वतोमुखी क्रान्ति का आदर्श-दोनों का विचार करते निःशंक रूप से सब युवकों को कह सकता हूं कि यदि आदर्शमय जीवन तुम्हारे लिए शक्य है तो विवाह का विचार तक मत करो और यदि मन की गहराइयों में विलासिता सताती हो, परेशान करती हो, और यह परेशानी मीठी-मधुर लगती हो, और उसका सामना करने का विचार ढीला-सा हो, मन को मोहित करनेवाली हर वस्तु की ओर रसिकता की ही दृष्टि जाती हो, तो स्वतंत्र आजीविका कमाने की ताकत आते ही शादी कर लेनी चाहिए और बडे-बडे आदर्शों को व्यवहार में लाने का दंभ छोड देना चाहिए।
अब धंधा पसंद करने के विषय में।
हमारी पसंदगी बहुत-कुछ इस पर आधारित रहेगी कि हम अपने परिवार के लोगों के प्रति कैसी वृत्ति रखना चाहते हैं । आप शॉर्टहेन्ड टाईपिंग छोड़ कर बढ़ई का या खेतीवाड़ी का काम पसंद करना चाहते हैं । इस विषय में मैं निःसंकोच सलाह दूंगा। शॉर्टहेन्ड टाइपिंग का धंधा शहरों में ही चल सकता है और वह भी अधिकतर जहां परदेश के साथ व्यापार चलता हो, वहीं चलेगा। जबतक हमको स्वराज्य मिला नहीं है, अथवा हमारे व्यापारियों में दूरदृष्टि की क्षमता नहीं है तबतक परदेश का व्यापार, राष्ट्र की दृष्टि से तो घाटे का ही रहेगा। आपके-जैसे समाज-सेवक होने की इच्छा करनेवाले को तो उसमें एक दिन भी बिगाड़ना नहीं चाहिए।
समाज-सेवक को एक तरह की संन्यास-वृत्ति धारण करनी चाहिए।
कन्या की शादी हो जाने के बाद जैसे माता-पिता के सुखःदुःख में वह प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं दे सकती, उसका प्रमुख कर्तव्य पति के घर के साथ ही रहता है, वैसे ही समाज-सेवक को कुटुंब और जातिविषयक कर्तव्यों से संन्यास लेकर समाज-सेवा के कार्य को ही अपना जीवन-कार्य समझना चाहिए और परिणीत कन्या पर से जैसे मैके के लोग अपना सारा हक उठा लेते हैं, उससे किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखते, वैसे ही जो समाज-सेवक बनता है, उसके परिवार के लोगों को अपने में अनासक्ति या निरपेक्षता की कहिये, वृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। यदि समझकर, यथासमय वे ऐसा न करें तो अपनी दृढ़ता से उनको ऐसी वृत्ति करने में सहायता देनी चाहिए। उनके असंतोष का ताप नहीं सहन कर सकेंगे, ऐसा लगे तो 'पहले ज मनमां मेवडीए' और 'होडे-होडे जुद्धे नव चडी ए' अर्थात पहले ही मन में सोच लेना और देखादेखी युद्ध में शरीक नहीं होना।
देश में जब स्वराज होता है, तब इतनी बहादुरी की जरूरत कम होती है और युवकों के लिए इतनी हिम्मत दिखानी मुश्किल भी नहीं होती। ग्रीष्मकाल में जैसे पानी की आवश्यकता अधिक और पानी मिलना मुश्किल होता है, वैसे ही पारतंत्र्य में पड़े हुए समाज में समाज-सेवा का आदर्श कठिन होता है, और सामान्य आदर्श तक पहुंचने वाले सेवक भी असाधारण कोटि के माने जाते हैं।
पत्नावली | २८५