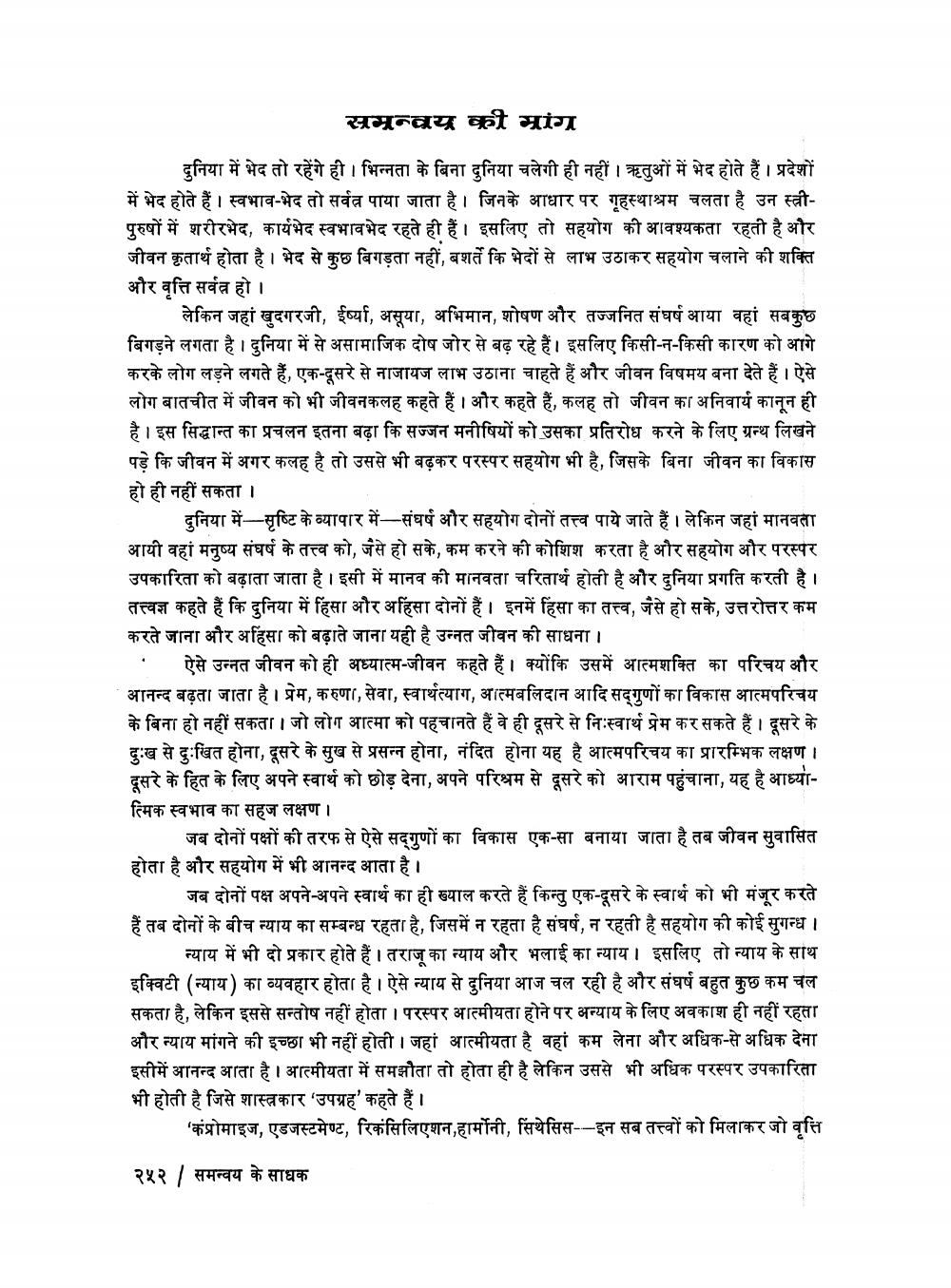________________
समन्वय की मांग
दुनिया में भेद तो रहेंगे ही। भिन्नता के बिना दुनिया चलेगी ही नहीं। ऋतुओं में भेद होते हैं। प्रदेशों में भेद होते हैं। स्वभाव-भेद तो सर्वत्र पाया जाता है। जिनके आधार पर गृहस्थाश्रम चलता है उन स्त्रीपुरुषों में शरीरभेद, कार्यभेद स्वभावभेद रहते ही हैं। इसलिए तो सहयोग की आवश्यकता रहती है और जीवन कृतार्थ होता है। भेद से कुछ बिगड़ता नहीं, बशर्ते कि भेदों से लाभ उठाकर सहयोग चलाने की शक्ति और वृत्ति सर्वत्र हो।
लेकिन जहां खुदगरजी, ईर्ष्या, असूया, अभिमान, शोषण और तज्जनित संघर्ष आया वहां सबकुछ बिगड़ने लगता है। दुनिया में से असामाजिक दोष जोर से बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी-न-किसी कारण को आगे करके लोग लड़ने लगते हैं, एक-दूसरे से नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं और जीवन विषमय बना देते हैं । ऐसे लोग बातचीत में जीवन को भी जीवनकलह कहते हैं। और कहते हैं, कलह तो जीवन का अनिवार्य कानून ही है। इस सिद्धान्त का प्रचलन इतना बढ़ा कि सज्जन मनीषियों को उसका प्रतिरोध करने के लिए ग्रन्थ लिखने पडे कि जीवन में अगर कलह है तो उससे भी बढ़कर परस्पर सहयोग भी है, जिसके बिना जीवन का विकास हो ही नहीं सकता।
दुनिया में-सृष्टि के व्यापार में संघर्ष और सहयोग दोनों तत्त्व पाये जाते हैं। लेकिन जहां मानवता आयी वहां मनुष्य संघर्ष के तत्त्व को, जैसे हो सके, कम करने की कोशिश करता है और सहयोग और परस्पर उपकारिता को बढ़ाता जाता है। इसी में मानव की मानवता चरितार्थ होती है और दुनिया प्रगति करती है। तत्त्वज्ञ कहते हैं कि दुनिया में हिंसा और अहिंसा दोनों हैं। इनमें हिंसा का तत्त्व, जैसे हो सके, उत्तरोत्तर कम करते जाना और अहिंसा को बढ़ाते जाना यही है उन्नत जीवन की साधना।
- ऐसे उन्नत जीवन को ही अध्यात्म-जीवन कहते हैं। क्योंकि उसमें आत्मशक्ति का परिचय और आनन्द बढ़ता जाता है। प्रेम, करुणा, सेवा, स्वार्थत्याग, आत्मबलिदान आदि सद्गुणों का विकास आत्मपरिचय के बिना हो नहीं सकता। जो लोग आत्मा को पहचानते हैं वे ही दूसरे से निःस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। दूसरे के दुःख से दुःखित होना, दूसरे के सुख से प्रसन्न होना, नंदित होना यह है आत्मपरिचय का प्रारम्भिक लक्षण । दूसरे के हित के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देना, अपने परिश्रम से दूसरे को आराम पहुंचाना, यह है आध्यात्मिक स्वभाव का सहज लक्षण।
जब दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे सदगुणों का विकास एक-सा बनाया जाता है तब जीवन सुवासित होता है और सहयोग में भी आनन्द आता है।
जब दोनों पक्ष अपने-अपने स्वार्थ का ही ख्याल करते हैं किन्तु एक-दूसरे के स्वार्थ को भी मंजूर करते हैं तब दोनों के बीच न्याय का सम्बन्ध रहता है, जिसमें न रहता है संघर्ष, न रहती है सहयोग की कोई सुगन्ध ।
न्याय में भी दो प्रकार होते हैं । तराज का न्याय और भलाई का न्याय। इसलिए तो न्याय के साथ इक्विटी (न्याय) का व्यवहार होता है। ऐसे न्याय से दुनिया आज चल रही है और संघर्ष बहुत कुछ कम चल सकता है, लेकिन इससे सन्तोष नहीं होता। परस्पर आत्मीयता होने पर अन्याय के लिए अवकाश ही नहीं रहता और न्याय मांगने की इच्छा भी नहीं होती। जहां आत्मीयता है वहां कम लेना और अधिक से अधिक देना इसीमें आनन्द आता है । आत्मीयता में समझौता तो होता ही है लेकिन उससे भी अधिक परस्पर उपकारिता भी होती है जिसे शास्त्रकार 'उपग्रह' कहते हैं।
'कंप्रोमाइज, एडजस्टमेण्ट, रिकंसिलिएशन,हार्मोनी, सिंथेसिस--इन सब तत्त्वों को मिलाकर जो वृत्ति
२५२ / समन्वय के साधक