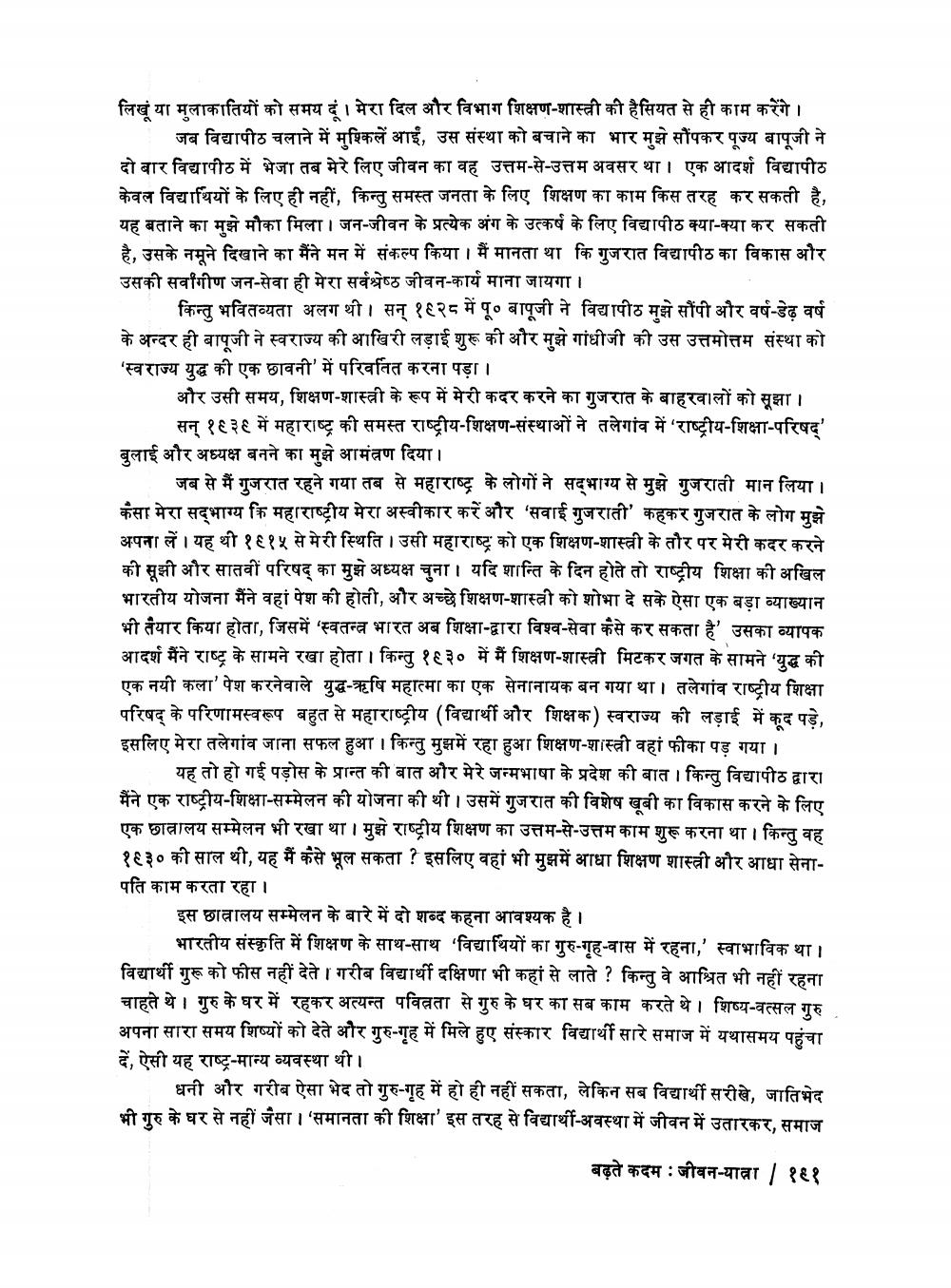________________
लिखू या मुलाकातियों को समय दूं। मेरा दिल और विभाग शिक्षण-शास्त्री की हैसियत से ही काम करेंगे।
जब विद्यापीठ चलाने में मुश्किलें आईं, उस संस्था को बचाने का भार मुझे सौंपकर पूज्य बापूजी ने दो बार विद्यापीठ में भेजा तब मेरे लिए जीवन का वह उत्तम-से-उत्तम अवसर था। एक आदर्श विद्यापीठ केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, किन्तु समस्त जनता के लिए शिक्षण का काम किस तरह कर सकती है, यह बताने का मुझे मौका मिला। जन-जीवन के प्रत्येक अंग के उत्कर्ष के लिए विद्यापीठ क्या-क्या कर सकती है, उसके नमूने दिखाने का मैंने मन में संकल्प किया। मैं मानता था कि गुजरात विद्यापीठ का विकास और उसकी सर्वांगीण जन-सेवा ही मेरा सर्वश्रेष्ठ जीवन-कार्य माना जायगा।
किन्तु भवितव्यता अलग थी। सन् १६२८ में पू० बापूजी ने विद्यापीठ मुझे सौंपी और वर्ष-डेढ़ वर्ष के अन्दर ही बापूजी ने स्वराज्य की आखिरी लड़ाई शुरू की और मुझे गांधीजी की उस उत्तमोत्तम संस्था को 'स्वराज्य युद्ध की एक छावनी' में परिवर्तित करना पड़ा।
और उसी समय, शिक्षण-शास्त्री के रूप में मेरी कदर करने का गुजरात के बाहरवालों को सुझा।
सन् १९३६ में महाराष्ट्र की समस्त राष्ट्रीय-शिक्षण-संस्थाओं ने तलेगांव में 'राष्ट्रीय-शिक्षा-परिषद' बुलाई और अध्यक्ष बनने का मुझे आमंत्रण दिया।
जब से मैं गुजरात रहने गया तब से महाराष्ट्र के लोगों ने सद्भाग्य से मुझे गुजराती मान लिया। कैसा मेरा सदभाग्य कि महाराष्ट्रीय मेरा अस्वीकार करें और 'सवाई गुजराती' कहकर गुजरात के लोग मझे अपना लें। यह थी १९१५ से मेरी स्थिति । उसी महाराष्ट्र को एक शिक्षण-शास्त्री के तौर पर मेरी कदर करने की सूझी और सातवीं परिषद् का मुझे अध्यक्ष चुना। यदि शान्ति के दिन होते तो राष्ट्रीय शिक्षा की अखिल भारतीय योजना मैंने वहां पेश की होती, और अच्छे शिक्षण-शास्त्री को शोभा दे सके ऐसा एक बड़ा व्याख्यान भी तैयार किया होता, जिसमें 'स्वतन्त्र भारत अब शिक्षा-द्वारा विश्व-सेवा कैसे कर सकता है उसका व्यापक आदर्श मैंने राष्ट्र के सामने रखा होता। किन्तु १९३० में मैं शिक्षण-शास्त्री मिटकर जगत के सामने 'युद्ध की एक नयी कला' पेश करनेवाले युद्ध-ऋषि महात्मा का एक सेनानायक बन गया था। तलेगांव राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् के परिणामस्वरूप बहुत से महाराष्ट्रीय (विद्यार्थी और शिक्षक) स्वराज्य की लड़ाई में कूद पड़े, इसलिए मेरा तलेगांव जाना सफल हुआ। किन्तु मुझमें रहा हुआ शिक्षण-शास्त्री वहां फीका पड़ गया।
यह तो हो गई पड़ोस के प्रान्त की बात और मेरे जन्मभाषा के प्रदेश की बात । किन्तु विद्यापीठ द्वारा मैंने एक राष्ट्रीय-शिक्षा-सम्मेलन की योजना की थी। उसमें गुजरात की विशेष खूबी का विकास करने के लिए एक छात्रालय सम्मेलन भी रखा था। मुझे राष्ट्रीय शिक्षण का उत्तम-से-उत्तम काम शुरू करना था। किन्तु वह १९३० की साल थी, यह मैं कैसे भूल सकता? इसलिए वहां भी मुझमें आधा शिक्षण शास्त्री और आधा सेनापति काम करता रहा।
इस छात्रालय सम्मेलन के बारे में दो शब्द कहना आवश्यक है।
भारतीय संस्कृति में शिक्षण के साथ-साथ 'विद्यार्थियों का गुरु-गृह-वास में रहना,' स्वाभाविक था। विद्यार्थी गुरू को फीस नहीं देते। गरीब विद्यार्थी दक्षिणा भी कहां से लाते ? किन्तु वे आश्रित भी नहीं रहना चाहते थे। गुरु के घर में रहकर अत्यन्त पवित्रता से गुरु के घर का सब काम करते थे। शिष्य-वत्सल गुरु अपना सारा समय शिष्यों को देते और गुरु-गृह में मिले हुए संस्कार विद्यार्थी सारे समाज में यथासमय पहंचा दें, ऐसी यह राष्ट्र-मान्य व्यवस्था थी।
धनी और गरीब ऐसा भेद तो गुरु-गृह में हो ही नहीं सकता, लेकिन सब विद्यार्थी सरीखे, जातिभेद भी गुरु के घर से नहीं जैसा। 'समानता की शिक्षा' इस तरह से विद्यार्थी-अवस्था में जीवन में उतारकर, समाज
बढ़ते कदम : जीवन-यात्रा | १६१