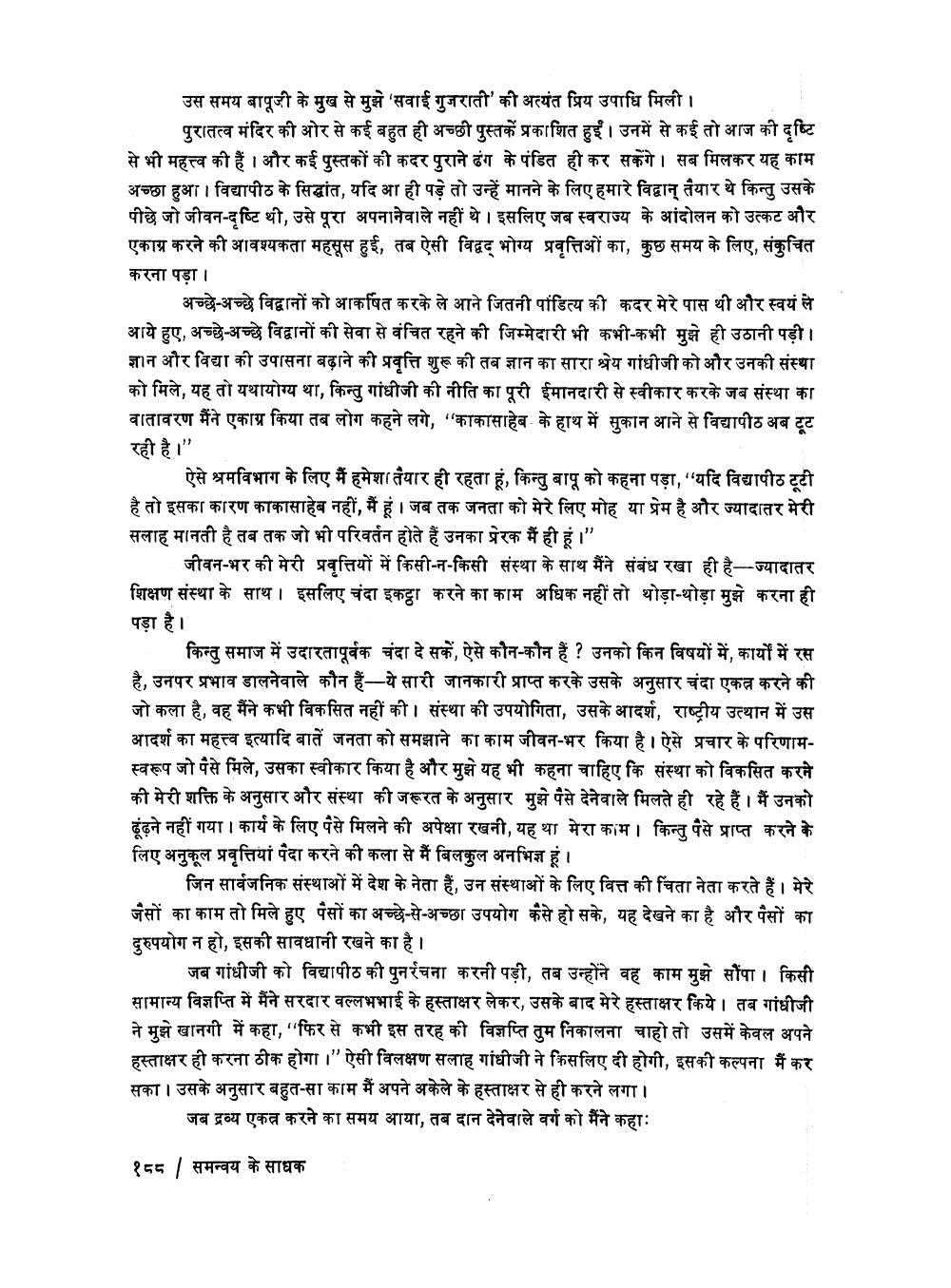________________
उस समय बापूजी के मुख से मुझे 'सवाई गुजराती' की अत्यंत प्रिय उपाधि मिली।
पुरातत्व मंदिर की ओर से कई बहुत ही अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनमें से कई तो आज की दृष्टि से भी महत्त्व की हैं । और कई पुस्तकों की कदर पुराने ढंग के पंडित ही कर सकेंगे। सब मिलकर यह काम अच्छा हुआ। विद्यापीठ के सिद्धांत, यदि आ ही पड़े तो उन्हें मानने के लिए हमारे विद्वान् तैयार थे किन्तु उसके पीछे जो जीवन-दृष्टि थी, उसे पूरा अपनानेवाले नहीं थे। इसलिए जब स्वराज्य के आंदोलन को उत्कट और एकाग्र करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब ऐसी विद्वद् भोग्य प्रवृत्तिओं का, कुछ समय के लिए, संकुचित करना पड़ा।
अच्छे-अच्छे विद्वानों को आकर्षित करके ले आने जितनी पांडित्य की कदर मेरे पास थी और स्वयं ले आये हुए, अच्छे-अच्छे विद्वानों की सेवा से वंचित रहने की जिम्मेदारी भी कभी-कभी मुझे ही उठानी पड़ी। ज्ञान और विद्या की उपासना बढ़ाने की प्रवृत्ति शुरू की तब ज्ञान का सारा श्रेय गांधीजी को और उनकी संस्था को मिले, यह तो यथायोग्य था, किन्तु गांधीजी की नीति का पूरी ईमानदारी से स्वीकार करके जब संस्था का वातावरण मैंने एकाग्र किया तब लोग कहने लगे, 'काकासाहेब के हाथ में सुकान आने से विद्यापीठ अब टूट रही है।"
ऐसे श्रमविभाग के लिए मैं हमेशा तैयार ही रहता हूं, किन्तु बापू को कहना पड़ा, “यदि विद्यापीठ टूटी है तो इसका कारण काकासाहेब नहीं, मैं हूं। जब तक जनता को मेरे लिए मोह या प्रेम है और ज्यादातर मेरी सलाह मानती है तब तक जो भी परिवर्तन होते हैं उनका प्रेरक मैं ही हूं।"
जीवन-भर की मेरी प्रवृत्तियों में किसी-न-किसी संस्था के साथ मैंने संबंध रखा ही है--ज्यादातर शिक्षण संस्था के साथ। इसलिए चंदा इकट्ठा करने का काम अधिक नहीं तो थोड़ा-थोड़ा मुझे करना ही पड़ा है।
किन्तु समाज में उदारतापूर्वक चंदा दे सकें, ऐसे कौन-कौन हैं ? उनको किन विषयों में, कार्यों में रस है, उनपर प्रभाव डालनेवाले कौन हैं—ये सारी जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार चंदा एकत्र करने की जो कला है, वह मैंने कभी विकसित नहीं की। संस्था की उपयोगिता, उसके आदर्श, राष्ट्रीय उत्थान में उस आदर्श का महत्त्व इत्यादि बातें जनता को समझाने का काम जीवन-भर किया है। ऐसे प्रचार के परिणामस्वरूप जो पैसे मिले, उसका स्वीकार किया है और मुझे यह भी कहना चाहिए कि संस्था को विकसित करने की मेरी शक्ति के अनुसार और संस्था की जरूरत के अनुसार मुझे पैसे देनेवाले मिलते ही रहे हैं। मैं उनको ढंढने नहीं गया। कार्य के लिए पैसे मिलने की अपेक्षा रखनी, यह था मेरा काम। किन्तु पैसे प्राप्त करने के लिए अनुकूल प्रवृत्तियां पैदा करने की कला से मैं बिलकुल अनभिज्ञ हैं।
जिन सार्वजनिक संस्थाओं में देश के नेता हैं, उन संस्थाओं के लिए वित्त की चिंता नेता करते हैं। मेरे जैसों का काम तो मिले हुए पैसों का अच्छे-से-अच्छा उपयोग कैसे हो सके, यह देखने का है और पैसों का दुरुपयोग न हो, इसकी सावधानी रखने का है।
जब गांधीजी को विद्यापीठ की पुनर्रचना करनी पड़ी, तब उन्होंने वह काम मुझे सौंपा। किसी सामान्य विज्ञप्ति में मैंने सरदार वल्लभभाई के हस्ताक्षर लेकर, उसके बाद मेरे हस्ताक्षर किये। तब गांधीजी ने मुझे खानगी में कहा, "फिर से कभी इस तरह की विज्ञप्ति तुम निकालना चाहो तो उसमें केवल अपने हस्ताक्षर ही करना ठीक होगा।" ऐसी विलक्षण सलाह गांधीजी ने किसलिए दी होगी, इसकी कल्पना मैं कर सका। उसके अनुसार बहुत-सा काम मैं अपने अकेले के हस्ताक्षर से ही करने लगा।
जब द्रव्य एकत्र करने का समय आया, तब दान देनेवाले वर्ग को मैंने कहाः
१८८ / समन्वय के साधक