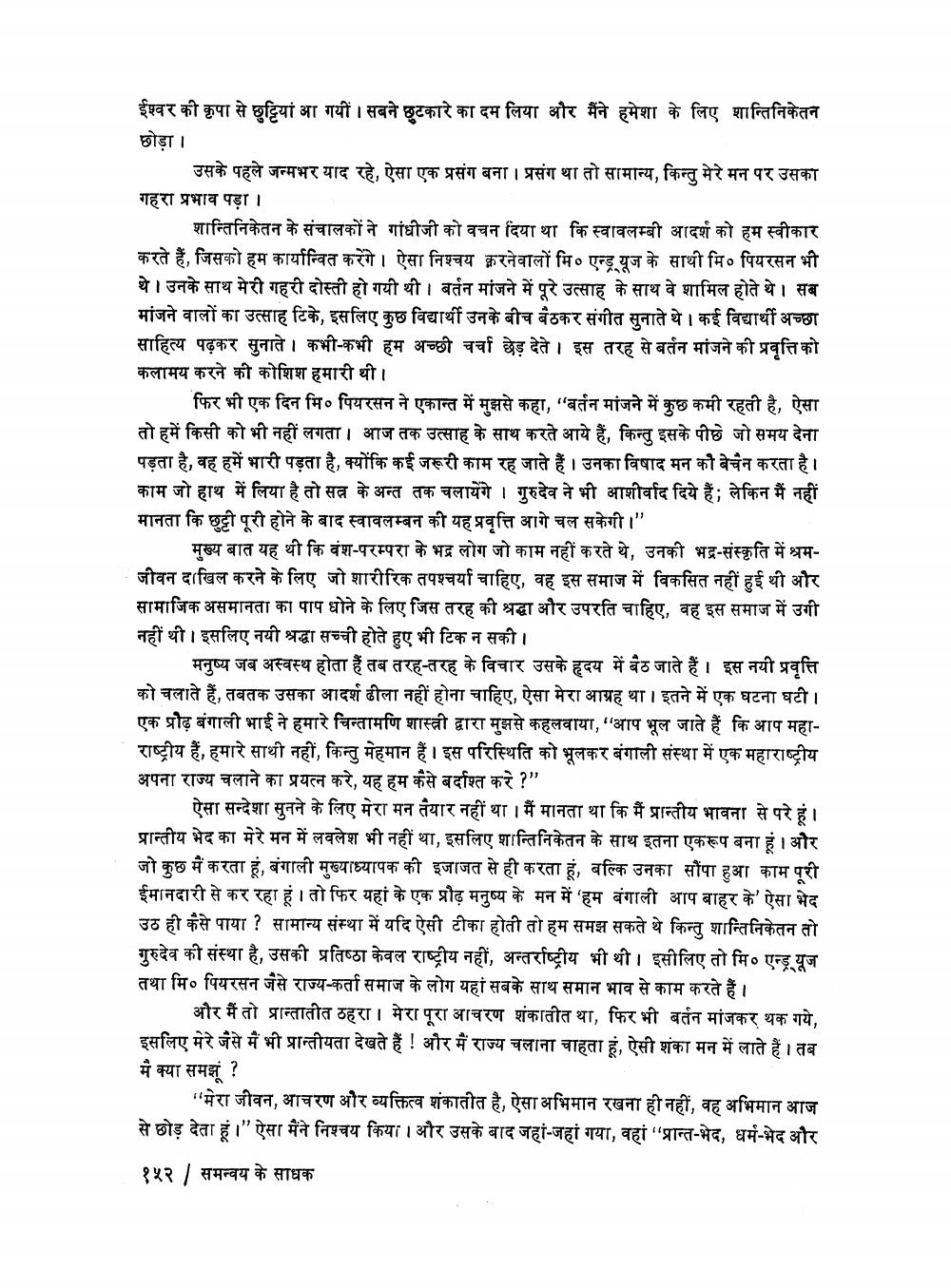________________
ईश्वर की कृपा से छुट्टियां आ गयीं। सबने छुटकारे का दम लिया और मैंने हमेशा के लिए शान्तिनिकेतन छोड़ा।
उसके पहले जन्मभर याद रहे, ऐसा एक प्रसंग बना। प्रसंग था तो सामान्य, किन्तु मेरे मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा।
शान्तिनिकेतन के संचालकों ने गांधीजी को वचन दिया था कि स्वावलम्बी आदर्श को हम स्वीकार करते हैं, जिसको हम कार्यान्वित करेंगे। ऐसा निश्चय करनेवालों मि० एन्ड यूज के साथी मि० पियरसन भी थे। उनके साथ मेरी गहरी दोस्ती हो गयी थी। बर्तन मांजने में पूरे उत्साह के साथ वे शामिल होते थे। सब मांजने वालों का उत्साह टिके, इसलिए कुछ विद्यार्थी उनके बीच बैठकर संगीत सुनाते थे। कई विद्यार्थी अच्छा साहित्य पढ़कर सुनाते। कभी-कभी हम अच्छी चर्चा छेड़ देते। इस तरह से बर्तन मांजने की प्रवृत्तिको कलामय करने की कोशिश हमारी थी।
फिर भी एक दिन मि० पियरसन ने एकान्त में मुझसे कहा, "बर्तन मांजने में कुछ कमी रहती है, ऐसा तो हमें किसी को भी नहीं लगता। आज तक उत्साह के साथ करते आये हैं, किन्तु इसके पीछे जो समय देना पडता है, वह हमें भारी पड़ता है, क्योंकि कई जरूरी काम रह जाते हैं। उनका विषाद मन को बेचैन करता है। काम जो हाथ में लिया है तो सत्र के अन्त तक चलायेंगे । गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिये हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि छुट्टी पूरी होने के बाद स्वावलम्बन की यह प्रवृत्ति आगे चल सकेगी।"
मुख्य बात यह थी कि वंश-परम्परा के भद्र लोग जो काम नहीं करते थे, उनकी भद्र-संस्कृति में श्रमजीवन दाखिल करने के लिए जो शारीरिक तपश्चर्या चाहिए, वह इस समाज में विकसित नहीं हुई थी और सामाजिक असमानता का पाप धोने के लिए जिस तरह की श्रद्धा और उपरति चाहिए, वह इस समाज में उगी नहीं थी। इसलिए नयी श्रद्धा सच्ची होते हुए भी टिक न सकी।
मनुष्य जब अस्वस्थ होता हैं तब तरह-तरह के विचार उसके हृदय में बैठ जाते हैं। इस नयी प्रवृत्ति को चलाते हैं, तबतक उसका आदर्श ढीला नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह था। इतने में एक घटना घटी। एक प्रौढ़ बंगाली भाई ने हमारे चिन्तामणि शास्त्री द्वारा मुझसे कहलवाया, "आप भूल जाते हैं कि आप महाराष्ट्रीय हैं, हमारे साथी नहीं, किन्तु मेहमान हैं। इस परिस्थिति को भूलकर बंगाली संस्था में एक महाराष्ट्रीय अपना राज्य चलाने का प्रयत्न करे, यह हम कैसे बर्दाश्त करे?"
ऐसा सन्देशा सुनने के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। मैं मानता था कि मैं प्रान्तीय भावना से परे हैं। प्रान्तीय भेद का मेरे मन में लवलेश भी नहीं था, इसलिए शान्तिनिकेतन के साथ इतना एकरूप बना हूं। और जो कुछ मैं करता हूं, बंगाली मुख्याध्यापक की इजाजत से ही करता हूं, बल्कि उनका सौंपा हुआ काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। तो फिर यहां के एक प्रौढ़ मनुष्य के मन में 'हम बंगाली आप बाहर के' ऐसा भेद उठ ही कैसे पाया ? सामान्य संस्था में यदि ऐसी टीका होती तो हम समझ सकते थे किन्तु शान्तिनिकेतन तो गुरुदेव की संस्था है, उसकी प्रतिष्ठा केवल राष्ट्रीय नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय भी थी। इसीलिए तो मि० एन्ड यूज तथा मि० पियरसन जैसे राज्य-कर्ता समाज के लोग यहां सबके साथ समान भाव से काम करते हैं।
और मैं तो प्रान्तातीत ठहरा। मेरा पूरा आचरण शंकातीत था, फिर भी बर्तन मांजकर थक गये, इसलिए मेरे जैसे मैं भी प्रान्तीयता देखते हैं ! और मैं राज्य चलाना चाहता है, ऐसी शंका मन में लाते हैं। तब मै क्या समझं?
"मेरा जीवन, आचरण और व्यक्तित्व शंकातीत है, ऐसा अभिमान रखना ही नहीं, वह अभिमान आज से छोड़ देता हूं।" ऐसा मैंने निश्चय किया । और उसके बाद जहां-जहां गया, वहां "प्रान्त-भेद, धर्म-भेद और
१५२ / समन्वय के साधक