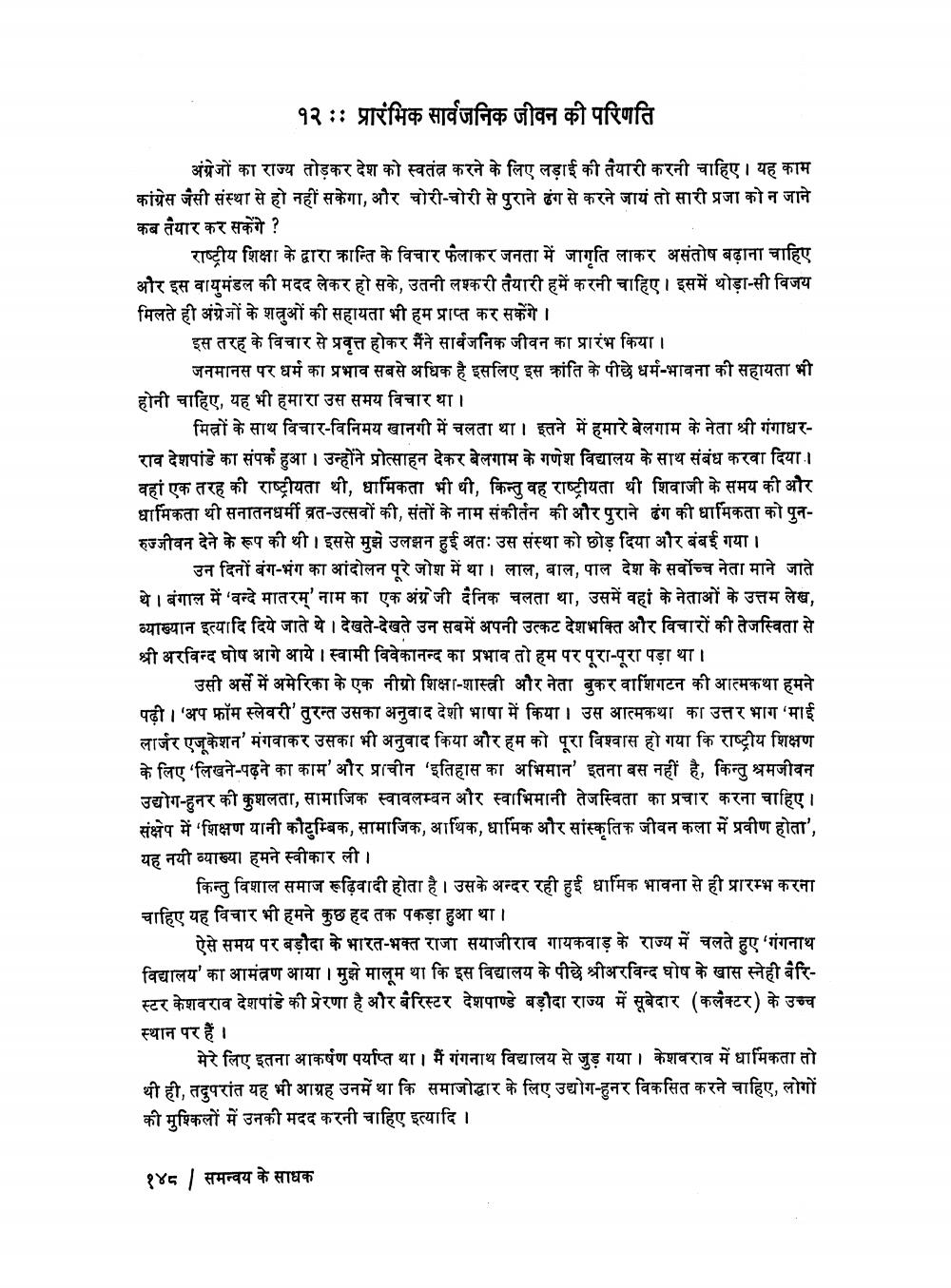________________
१२:: प्रारंभिक सार्वजनिक जीवन की परिणति
अंग्रेजों का राज्य तोड़कर देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। यह काम कांग्रेस जैसी संस्था से हो नहीं सकेगा, और चोरी-चोरी से पुराने ढंग से करने जायं तो सारी प्रजा को न जाने कब तैयार कर सकेंगे?
राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा क्रान्ति के विचार फैलाकर जनता में जागति लाकर असंतोष बढ़ाना चाहिए और इस वायुमंडल की मदद लेकर हो सके, उतनी लश्करी तैयारी हमें करनी चाहिए। इसमें थोड़ा-सी विजय मिलते ही अंग्रेजों के शत्रुओं की सहायता भी हम प्राप्त कर सकेंगे।
इस तरह के विचार से प्रवृत्त होकर मैंने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया।
जनमानस पर धर्म का प्रभाव सबसे अधिक है इसलिए इस क्रांति के पीछे धर्म-भावना की सहायता भी होनी चाहिए, यह भी हमारा उस समय विचार था।
मित्रों के साथ विचार-विनिमय खानगी में चलता था। इतने में हमारे बेलगाम के नेता श्री गंगाधरराव देशपांडे का संपर्क हुआ। उन्होंने प्रोत्साहन देकर बेलगाम के गणेश विद्यालय के साथ संबंध करवा दिया। वहां एक तरह की राष्ट्रीयता थी, धार्मिकता भी थी, किन्तु वह राष्ट्रीयता थी शिवाजी के समय की और धार्मिकता थी सनातनधर्मी व्रत-उत्सवों की, संतों के नाम संकीर्तन की और पुराने ढंग की धार्मिकता को पुनरुज्जीवन देने के रूप की थी। इससे मुझे उलझन हुई अतः उस संस्था को छोड़ दिया और बंबई गया।
उन दिनों बंग-भंग का आंदोलन पूरे जोश में था। लाल, बाल, पाल देश के सर्वोच्च नेता माने जाते थे। बंगाल में 'वन्दे मातरम्' नाम का एक अंग्रेजी दैनिक चलता था, उसमें वहां के नेताओं के उत्तम लेख, व्याख्यान इत्यादि दिये जाते थे। देखते-देखते उन सबमें अपनी उत्कट देशभक्ति और विचारों की तेजस्विता से श्री अरविन्द घोष आगे आये । स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव तो हम पर पूरा-पूरा पड़ा था।
उसी अर्से में अमेरिका के एक नीग्रो शिक्षा-शास्त्री और नेता बुकर वाशिंगटन की आत्मकथा हमने पढ़ी। 'अप फ्रॉम स्लेवरी' तुरन्त उसका अनुवाद देशी भाषा में किया। उस आत्मकथा का उत्तर भाग 'माई लार्जर एजकेशन' मंगवाकर उसका भी अनुवाद किया और हम को पूरा विश्वास हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षण के लिए लिखने-पढ़ने का काम' और प्राचीन इतिहास का अभिमान' इतना बस नहीं है, किन्तु श्रमजीवन उद्योग-हनर की कुशलता, सामाजिक स्वावलम्बन और स्वाभिमानी तेजस्विता का प्रचार करना चाहिए। संक्षेप में शिक्षण यानी कौटुम्बिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कतिक जीवन कला में प्रवीण होता', यह नयी व्याख्या हमने स्वीकार ली।
किन्तु विशाल समाज रूढ़िवादी होता है। उसके अन्दर रही हुई धार्मिक भावना से ही प्रारम्भ करना चाहिए यह विचार भी हमने कुछ हद तक पकड़ा हुआ था।
ऐसे समय पर बड़ौदा के भारत-भक्त राजा सयाजीराव गायकवाड़ के राज्य में चलते हए 'गंगनाथ विद्यालय' का आमंत्रण आया। मुझे मालूम था कि इस विद्यालय के पीछे श्रीअरविन्द घोष के खास स्नेही बैरिस्टर केशवराव देशपांडे की प्रेरणा है और बैरिस्टर देशपाण्डे बड़ौदा राज्य में सूबेदार (कलैक्टर) के उच्च स्थान पर हैं।
मेरे लिए इतना आकर्षण पर्याप्त था। मैं गंगनाथ विद्यालय से जुड़ गया। केशवराव में धार्मिकता तो थी ही, तदुपरांत यह भी आग्रह उनमें था कि समाजोद्धार के लिए उद्योग-हुनर विकसित करने चाहिए, लोगों की मुश्किलों में उनकी मदद करनी चाहिए इत्यादि ।
१४८ / समन्वय के साधक