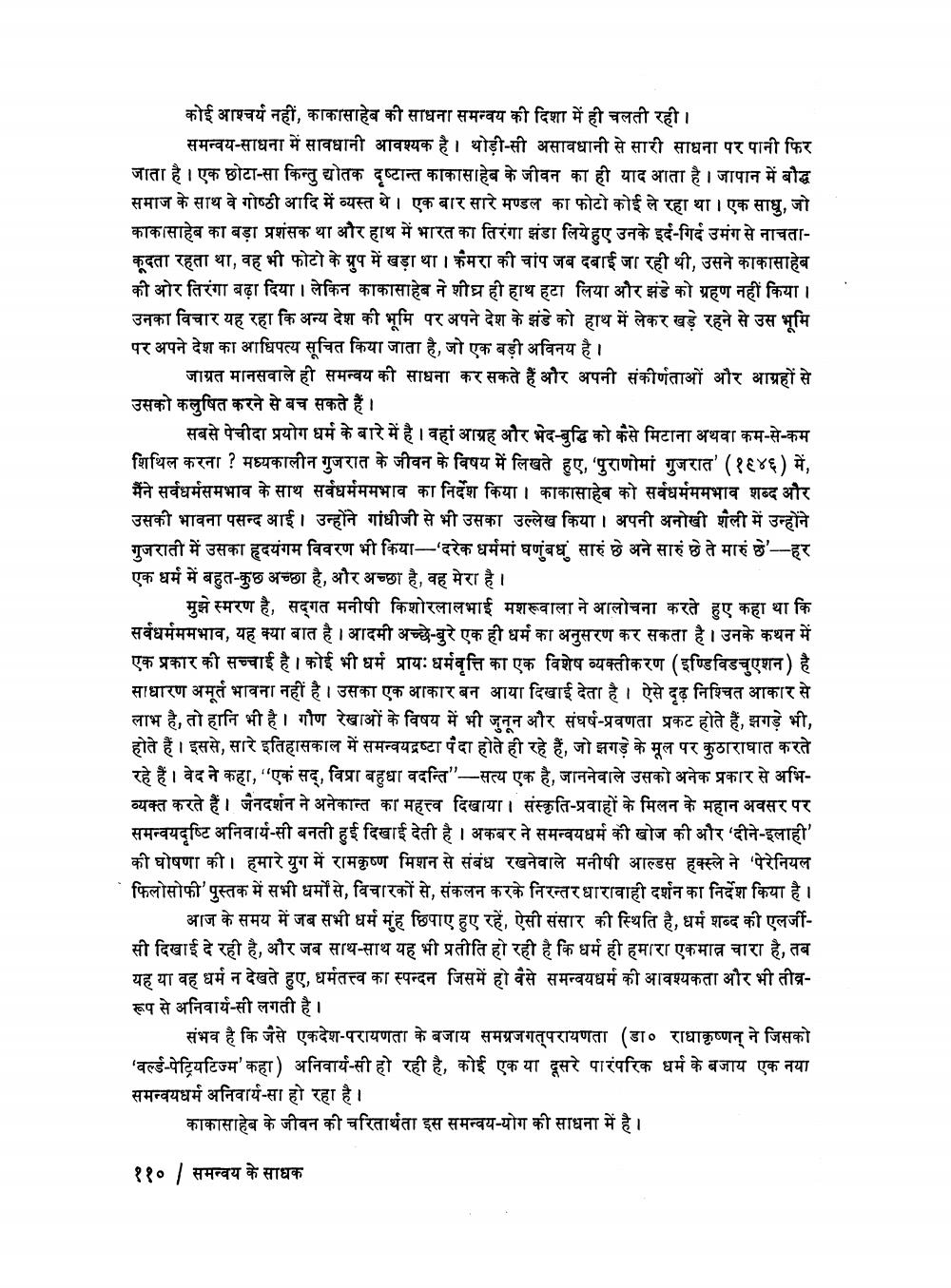________________
कोई आश्चर्य नहीं, काकासाहेब की साधना समन्वय की दिशा में ही चलती रही।
समन्वय साधना में सावधानी आवश्यक है। थोड़ी-सी असावधानी से सारी साधना पर पानी फिर जाता है। एक छोटा-सा किन्तु द्योतक दृष्टान्त काकासाहेब के जीवन का ही याद आता है । जापान में बौद्ध समाज के साथ वे गोष्ठी आदि में व्यस्त थे । एक बार सारे मण्डल का फोटो कोई ले रहा था। एक साधु, जो काकासाहेब का बड़ा प्रशंसक था और हाथ में भारत का तिरंगा झंडा लिये हुए उनके इर्द-गिर्द उमंग से नाचताकूदता रहता था, वह भी फोटो के ग्रुप में बड़ा था कैमरा की चांप जब दबाई जा रही थी, उसने काकासाहेब की ओर तिरंगा बढ़ा दिया। लेकिन काकासाहेब ने शीघ्र ही हाथ हटा लिया और झंडे को ग्रहण नहीं किया । उनका विचार यह रहा कि अन्य देश की भूमि पर अपने देश के झंडे को हाथ में लेकर खड़े रहने से उस भूमि पर अपने देश का आधिपत्य सूचित किया जाता है, जो एक बड़ी अविनय है ।
।
जाग्रत मानसवाले ही समन्वय की साधना कर सकते हैं और अपनी संकीर्णताओं और आग्रहों से उसको कलुषित करने से बच सकते हैं।
सबसे पेचीदा प्रयोग धर्म के बारे में है। वहां आग्रह और भेद-बुद्धि को कैसे मिटाना अथवा कम-से-कम शिथिल करना ? मध्यकालीन गुजरात के जीवन के विषय में लिखते हुए, 'पुराणोमां गुजरात' (१९४६) में, मैंने सर्वधर्मसमभाव के साथ सर्वधर्मसमभाव का निर्देश किया। काकासाहेब को सर्वधर्मसमभाव शब्द और उसकी भावना पसन्द आई। उन्होंने गांधीजी से भी उसका उल्लेख किया। अपनी अनोखी शैली में उन्होंने गुजराती में उसका हृदयंगम विवरण भी किया- 'दरेक धर्ममां घणुंबधुं सारं छे अने सारुं छे ते मारुं छे' - हर एक धर्म में बहुत-कुछ अच्छा है, और अच्छा है, वह मेरा है ।
1
मुझे स्मरण है, सद्गत मनीषी किशोरलालभाई मशरूवाला ने आलोचना करते हुए कहा था कि सर्वधर्मसमभाव, यह क्या बात है। आदमी अच्छे-बुरे एक ही धर्म का अनुसरण कर सकता है। उनके कथन में एक प्रकार की सच्चाई है। कोई भी धर्म प्रायः धर्मवृत्ति का एक विशेष व्यक्तीकरण ( इण्डिविडचुएशन) है साधारण अमूर्त भावना नहीं है। उसका एक आकार बन आया दिखाई देता है । ऐसे दृढ़ निश्चित आकार से लाभ है, तो हानि भी है। गौण रेखाओं के विषय में भी जुनून और संघर्ष-प्रवणता प्रकट होते हैं, झगड़े भी, होते हैं । इससे सारे इतिहासकाल में समन्वयद्रष्टा पैदा होते ही रहे हैं, जो झगड़े के मूल पर कुठाराघात करते रहे हैं । वेद ने कहा, “एकं सद्, विप्रा बहुधा वदन्ति” – सत्य एक है, जाननेवाले उसको अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। जनदर्शन ने अनेकान्त का महत्त्व दिखाया। संस्कृति प्रवाहों के मिलन के महान अवसर पर समन्वयदृष्टि अनिवार्य -सी बनती हुई दिखाई देती है । अकबर ने समन्वयधर्म की खोज की और 'दीने-इलाही' की घोषणा की। हमारे युग में रामकृष्ण मिशन से संबंध रखनेवाले मनीषी आल्डस हक्स्ले ने 'पेरेनियल फिलोसोफी' पुस्तक में सभी धर्मों से, विचारकों से, संकलन करके निरन्तर धारावाही दर्शन का निर्देश किया है । आज के समय में जब सभी धर्म मुंह छिपाए हुए रहें, ऐसी संसार की स्थिति है, धर्म शब्द की एलर्जीसी दिखाई दे रही है, और जब साथ-साथ यह भी प्रतीति हो रही है कि धर्म ही हमारा एकमात्र चारा है, तब यह या वह धर्म न देखते हुए, धर्मतत्त्व का स्पन्दन जिसमें हो वैसे समन्वयधर्म की आवश्यकता और भी तीव्ररूप से अनिवार्य -सी लगती है।
संभव है कि जैसे एकदेश-परायणता के बजाय समग्रजगत्परायणता (डा० राधाकृष्णन् ने जिसको 'वर्ल्ड-पेट्रियटिज्म' कहा) अनिवार्य सी हो रही है, कोई एक या दूसरे पारंपरिक धर्म के बजाय एक नया समन्वयधर्म अनिवार्य सा हो रहा है।
काकासाहेब के जीवन की चरितार्थता इस समन्वय-योग की साधना में है।
११० / समन्वय के साधक